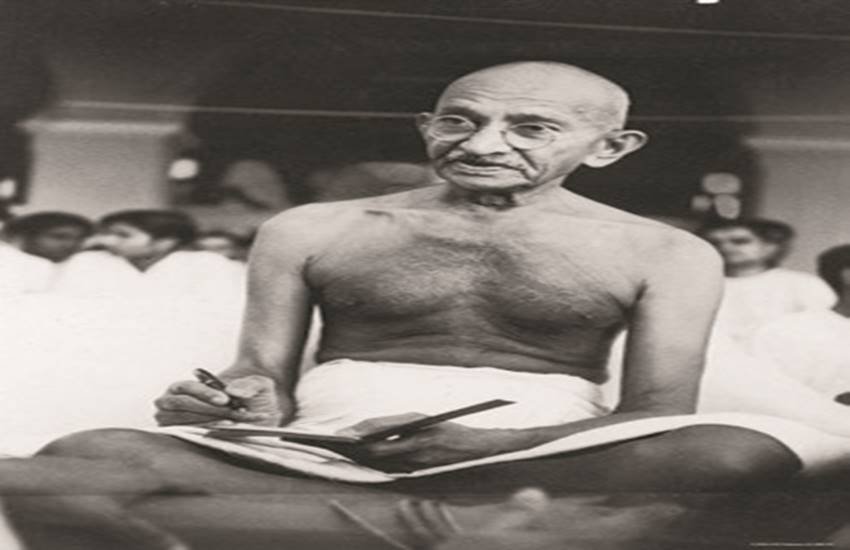साहित्य के संबंध में गांधी की ‘रस-दृष्टि’ भी पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रीय मान्यताओं से पृथक स्वरूप की रही है। सर्वविदित है कि हमारे काव्यशास्त्र ने साहित्य में शृंगार रस को सर्वोपरि महत्त्व देते हुए उसे ‘रसराज’ तक की संज्ञा दे डाली और इस ‘रसराज’ ने ऐसी असीम छूट दी कि कई साहित्यकारों ने शृंगार के नाम पर स्त्री के विभिन्न अंगों, कोमोत्तेजक चेष्टाओं के साथ-साथ संभोग, शृंगार तक का खुल कर चित्रण कर डाला। गांधीजी इसे साहित्य की गरिमा के अनुकूल नहीं मानते। 2 मई, 1936 को नागपुर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की बैठक में अध्यक्षीय भाषण करते हुए गांधीजी ने कहा- ‘आजकल शृंगार युक्त अश्लील साहित्य की बाढ़ सब प्रांतों में आ रही है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि एक शृंगार को छोड़ कर और कोई रस है ही नहीं। शृंगार रस को बढ़ाने के कारण ऐसे सज्जन दूसरों को त्यागी कह कर उनकी उपेक्षा और उपहास करते हैं। जो सब चीजों का त्याग कर बैठते हैं वे भी रस का त्याग तो नहीं कर पाते। किसी न किसी प्रकार के रस से हम सब भरे हैं। दादाभाई ने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी वे बड़े रसिक थे। देश-सेवा को ही उन्होंने अपना रस बना रखा था। चैतन्य को रसहीन कहना रस को ही न जानना है। अगर आपको मेरी बात न अखरे तो मैं यहां तक कहूंगा कि मैं शृंगार रस को तुच्छ रस समझता हूं और जब उसमें अश्लीलता आती है, तब उसे सर्वथा त्याज्य मानता हूं। अगर मेरी चले तो मैं इस संस्था में ऐसे रस को त्याज्य मनवा दूं। इसी तरह जो साहित्य कौमी भेदों को, धर्मांधता को तथा प्रजा में या व्यक्तियों में वैमनस्य को बढ़ाता है, उसका भी त्याग होना आवश्यक है।’
जाहिर है, गांधी की अपनी ‘रस-दृष्टि’ है, जो सिर्फ शृंगार रस को साहित्य का ‘रस’ नहीं मानती। दादाभाई नौरोजी, चैतन्य आदि के उदाहरणों से सिद्ध है कि वे साहित्य-रस को कितने व्यापक दायरे में देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में कह सकते हैं कि गांधी की ‘रस-दृष्टि’ नायिका के तीन फुट के नख-शिख संसार तक सीमित नहीं है। नख-शिख सौंदर्य के वर्णन से आत्ममुग्ध होने वाली स्त्रियों को सजग करते हुए उन्होंने 21 नवंबर, 1936 के ‘हरिजन सेवक’ में लिखा ‘आश्चर्य तो यह है कि पुरुषों के सौंदर्य की प्रशंसा में पुस्तकें बिलकुल नहीं लिखी गर्इं। तो फिर पुरुष की विषय-वासना को उत्तेजित करने के लिए ही साहित्य क्यों हमेशा तैयार होता रहे? यह बात तो नहीं कि पुरुष ने स्त्री को जिन विशेषणों से भूषित किया है उन विशेषताओं को सार्थक करना उसे पसंद है। स्त्री को क्या यह अच्छा लगता होगा कि उसके शरीर के सौंदर्य का पुरुष अपनी भोग-लालसा के लिए दुरुपयोग करे? पुरुष के आगे अपनी देह की सुंदरता दिखाना क्या उसे पसंद होगा? अगर हां, तो किसलिए! मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न सुशिक्षित बहनें स्वयं अपने दिल से पूछें। अगर ऐसे अश्लील विज्ञापनों और साहित्य से उनका दिल दुखता हो तो उन्हें इसके विरुद्ध अविराम युद्ध चलाना चाहिए।’ इस प्रकार गांधी वैसे साहित्य के सख्त खिलाफ हैं, जो शृंगार रस के नाम पर युवा-युवतियों में विषय-वासना का उद्रेक करे। उनकी दृष्टि में साहित्य का प्रयोजन होना चाहिए कि वह युवा मन में स्वस्थ भावनाओं को पुरुषार्थ को जागृत करे, न कि वासना को भड़कावे। यही कारण था कि जयदेव की शृंगार-रस की उत्कृष्ट काव्यकृति को गांधी ने तनिक महत्त्व नहीं दिया। 18 जुलाई, 1926 के
‘नवजीवन’ (गुजराती) में उनके छपे लेख का यह अंश द्रष्टव्य है- ‘मैंने कई लोगों से कई बार जयदेव कृत ‘गीत गोविंद’ की तारीफ सुनी थी और मेरी इच्छा थी कि मैं उसे कभी न कभी पढ़ूंगा। पढ़ तो गया, किन्तु उसके वर्णन पढ़ कर मुझे दुख हुआ। मुझे यह मानते हुए कोई संकोच नहीं है कि संभव है इसमें दोष मेरा ही हो। मैं तो यहां केवल पाठकों के सामने अपनी स्थिति रख रहा हूं। ‘गीत गोविंद’ का मेरे ऊपर अच्छा असर नहीं हुआ, इसलिए मेरे लेखे तो वह त्याज्य भी रहा, इसका कारण यह है कि मेरे पास अपना एक मानदंड है। जो वस्तु मुझे निर्विकार कर सकती है, मेरे राग-द्वेष आदि को नरम बना सकती है, जिस वस्तु का मनन मुझे सूली पर चढ़ते हुए भी सत्य पर दृढ़ रखने में सहायक हो सकता है, वही वस्तु मेरे लिए धार्मिक शिक्षण हो सकती है। ‘गीत गोविंद’ इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा और इसलिए मेरे लेखे वह पुस्तक त्याज्य ही है।’ किसी भी साहित्यिक या कलाकृति को पसंद करने, स्वीकार करने का गांधीजी का अपना मानदंड या प्रतिमान था और वह था सत्य अहिंसा, दया, करुणा, सेवा आदि को पुष्ट करने में वह कृति किस हद तक सहायक होती है। इसी उपयोगितावादी प्रतिमान पर उन्होंने साहित्य को देखा-परखा और जो साहित्यिक कृति इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी, उसे उन्होंने महत्त्व नहीं दिया।