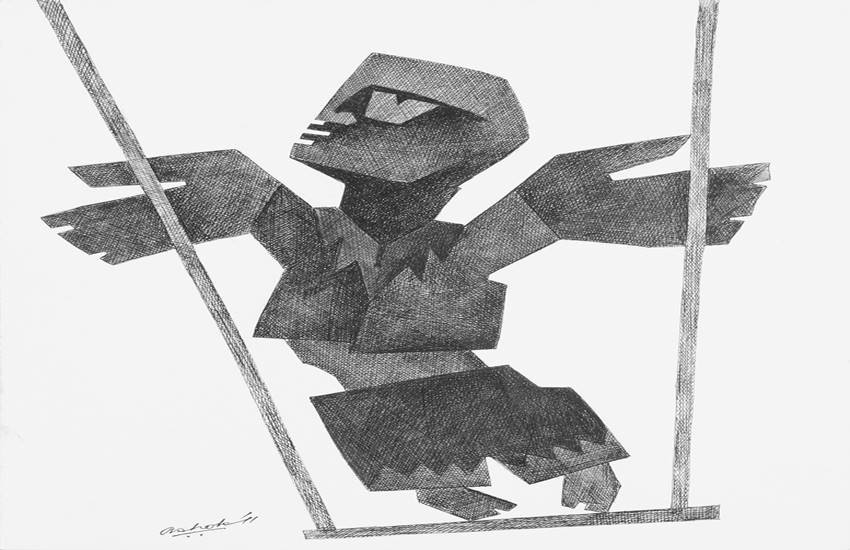ज्योतिष जोशी
समकालीन हिंदी कहानी का फलक बढ़ा है। वह अब हर तरह के पाठकों के पास पहुंच रही है। पहले भी वह अपनी व्यापकता को लेकर कवि समाज में ईर्ष्या का विषय रही है, क्योंकि अपने आरंभ से ही वह उन विषयों पर टिकती रही है, जो बेहद असुविधाजनक रहे हैं और कविता उनसे भागती रही है। भारत विभाजन हो या देश की कोई बड़ी समस्या, हिंदी कहानी हमेशा एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में सामने आई है। लगभग सवा सौ वर्षों की यह यात्रा किसी सुखद स्वप्न के पूरे होने से कम नहीं है। पर पिछले कुछ वर्षों से उसमें कई ऐसी फांकें दिखने लगी हैं, जो चिंता जगाती हैं। कहानी दरअसल, जीवन को एक बिंदु पर ग्रहण करने वाली उस विधा के रूप में सामने आई थी, जिसे देखने पर समस्त जीवन रेखा प्रकाशित हो उठती थी। यह बड़ी चुनौती का काम रहा है और इसमें लेखक के अनुभव, सामर्थ्य और दृष्टि की परख भी होती रही है। पर इधर कुछ वर्षों में वह जिन परिवर्तनों का शिकार हुई है, उससे चिंता होना स्वाभाविक है। असल चिंता की बात यह है कि उसमें अब विवरण को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है। कहानी के रचाव की आवश्यक तैयारी और उसमें स्वयं को विन्यस्त करने का लेखकीय दायित्व कम हो गया है। भाषा की स्फीति में घटनाओं का विवरण, स्थितियों के परीक्षण के बजाय उनका वर्णन और अनावश्यक लेखकीय हस्तक्षेप से उपजे बड़े-बड़े वक्तव्य कहानी की स्वाभाविकता को क्षति पहुंचा रहे हैं। बहुधा हमें ऐसी कहानियों को पढ़ते हुए किसी खबर या सपाट वृत्तांत को पढ़ने का बोध होता है, जो मन पर उतरने के बजाय एक विचित्र वितृष्णा जगा जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण अपेक्षित साहित्य संस्कार का न होना है। कहानीकार, गल्पकार और पत्रकार भी हो सकता है, तो व्यंग्यकार भी। पर पहले उसे कहानीकार तो होना होगा। एक गहन अनुभव, उस अनुभव को अनुभूति बना लेने की हिकमत और उसमें अपने को समो लेने की धुन अगर न हो तो कहानी कितनी बन पाएगी यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है।
एक अजीब किस्म की हड़बड़ी से भरे समय में सब कुछ को समेट लेने की आतुरता ने कहानी में अब इसीलिए न तो अविस्मरणीय चरित्र बन पा रहे हैं और न ऐसे मर्मस्थल उभर कर आ रहे हैं, जो हमें सोचने पर विवश करें या जिन्हें हम कभी विस्मृत न कर सकें। यह औचक नहीं हुआ है। इसके स्पष्ट कारण हैं।अब न कहानी में कोई आंदोलन है न कहानी पर विचार और विश्लेषण का कोई मान्य मंच ही है। जो जहां है वहीं उसका अपना दर्शन है और इस तरह अन्य विधाओं की तरह ही कहानी को भी अपनी ही तरह बरत लेने की हड़बड़ी है। इस हड़बड़ी के कारण कहानी की परंपरा और उसके बोध से अनजान और तथाकथित बड़बोले लेखक उस दृष्टि को ही विकसित कर पाने में नाकाम हो जाते हैं, जिससे कहानी बनती या जन्म लेती है और वह एक बड़े मानवीय प्रश्न को उठा पाती है। असल सवाल उस दृष्टि के न होने की है, जाहिर है, ऐसी दृष्टि के न होने से हम यह समझ ही नहीं पाते कि भाषा की स्फीति से कहानी नहीं बनती, न हमारी निजी प्रतिक्रियाओं से उसका कोई विशेष वास्ता होता है। हम यह भी नहीं समझ पाते कि मनोनुकूल चरित्रों का जखीरा खड़ा कर देने, हमारे अनावश्यक लेखकीय हस्तक्षेप करने से या कोई सवाल उठा कर उसे जिरह बना देने से भी कहानी नहीं बनती। वर्णन और विश्लेषण के अतिरिक्त कहानी में कहानीपन के साथ वह आत्म ही नहीं आ पाता, जो उसे प्राण देता है। इसमें कहीं-कहीं लेखक की वाचालता इतनी अधिक हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि हम कहानी पढ़ रहे हैं या किसी राजनीतिक बहस से गुजर रहे हैं। यह प्रवृत्ति समकालीन कहानी को अराजकता की तरफ ले जा रही है।
कहानी बहत चुनौतीपूर्ण विधा है। उसमें मारक क्षमता बेहद तीक्ष्ण होती है। वह बयान नहीं, न बहस है, न भाषाई स्फीति का प्रदर्शन, न कोई रपट, न कोई घटनात्मक विवरण या न कोई राजनीतिक-सामाजिक बहस खड़ा करने का कोई मंच। वह तो मानवीय प्रश्नों को हमारी चेतना में झंकृत करने वाली ऐसी विधा है, जो चुपके से हमें आंदोलित कर देती है और हमें अपनी जगह की याद दिला देती है। वह बुनी नहीं जाती, जी जाती है। उसमें आए चरित्र हमारे अपने ही प्रतिरूप होते हैं, जिनमें प्रवेश कर हम उन क्षणों को जीते हैं, जिनसे होकर एक कथा गुजरती है और उस कथा में आए घटनात्मक मोड़ जिन सवालों में हमें ले जाते हैं, वे हमारे अस्तित्व से जुड़े होते हैं। लेखक चूंकि सबमें होता है, इसलिए उससे अपेक्षा नहीं होती कि वह आगे बढ़ कर कोई स्पष्ट बयान दे और पूरी कहानी को अपने किसी ध्येय की बलि चढ़ा दे। लेकिन हो यही रहा है और चाहे जिस भी व्यवसाय का कोई व्यक्ति हो, भले उसमें साहित्य का स्वाभाविक संस्कार न हो या न ही सृजन की अदम्य छटपटाहट से गुजर पाने का कोई अनुभव हो, वह कहानी लिखने बैठ जाता है।
अन्य अनेक विधाओं की तरह कहानी भी तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक बहसों का शिकार है। सबको जल्दबाजी है कि सारे प्रश्न इन्हीं के माध्यम से उठा कर इनका समाधान पा लेना है। समाधान तो नहीं मिल पाता, पर कहानी को हम कहानी ही नहीं रहने देते। वे कौन-सी बहसें हैं, जो हम पर तारी हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि उन्हें उठाने की नहीं, यहां बरतने की आवश्यकता है। कहानी न तो कथा है और न किसी घटना का वृत्तांत, वह तो अपने देखे, भोगे और जिए गए अनुभव को एक बार फिर जीकर अपने को व्यक्त करने की विधा है, जिसमें पाठक को संवेदित करने की अपार क्षमता होती है। उसे जैसा मान या जान लिया गया है, उसे देख कर सचमुच हैरानी होती है।
हैरानी इसलिए भी होती है कि यह उस कहानी का हाल है, जिसकी एक समृद्ध परंपरा रही है। जिसमें कहानी को लेकर अनेक आंदोलन हुए हैं और उसे अपने देशकाल के साथ-साथ वैश्विक विमर्शों और मानकों के अनुकूल परिभाषित करने की सतत चेष्टा हुई है। यह भी अचरज भरी बात है कि आज भी दृश्य में ऐसे कुछ बड़े कहानीकार हैं, जिनकी कहानियों ने नए मानक बनाए हैं, पर आज के कहानीकारों के प्रेरक नहीं रहे। उत्तेजना, प्रतिक्रिया, घटनात्मक चमत्कार और भाषाई अराजकता के इस दौर में श्लीलता-अश्लीलता का फर्क भी मिट गया है। अब त्वरित आस्वाद को वरीयता देने का चलन बढ़ा है। अब हर तरह के फैसले कहानी में ही सुना देने का ताव है, गोया कहानी अखबार ही समझ ली गई हो। यह खतरनाक संकेत है। जीवन के अनुभव, मानवीय प्रश्नों के अंतस्तल तक जाकर विश्लेषण करने की क्षमता और चरित्रों को जी पाने का अभाव भी इस संकट का एक बड़ा कारण है। इन दिक्कतों से उबरे बिना हिंदी की समकालीन कहानी के लिए स्थायी पहचान मिलना तो दूर, तात्कालिकता की सीमा पार करना भी मुश्किल है। फिर यह भी प्रश्न है कि अगर कहानी में कहानी ही नहीं रहेगी तो किसकी आलोचना होगी और क्यों होगी? कहानी चाहे जिस प्रयोग से गुजरे, अगर वह कहानी ही न रह जाए तो चिंता होती है। आवश्यक है कि इसकी चिंता करने वाले लोग आगे आएं और कहानी के सृजन की इन समस्याओं पर विचार करें।