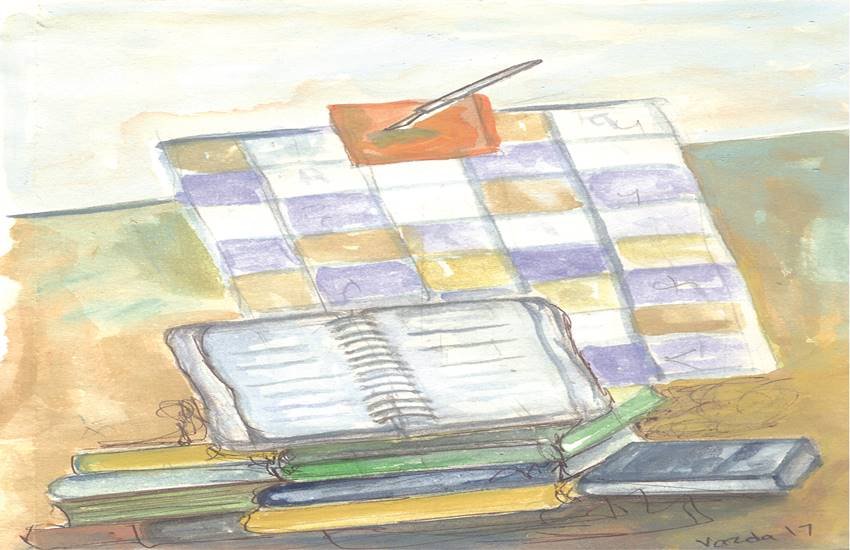पंकज पराशर
कल्पना और विचारों की उड़ान तभी परवान चढ़ती है, जब मन मुक्त और माहौल उन्मुक्त हो। अगर कला का इतिहास देखें, तो प्रतिरोध में ही कोई कला अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाती है। ऐसी कला समय के घेरे से बाहर निकल कर हमेशा अपनी प्रासंगिकता और सार्थकता बनाए रखती है, जिसमें जीवन-विवेक तथा समाज-विवेक को नष्ट करने वाली अमानवीय और अलोकतांत्रिक सत्ता के प्रतिरोध का साहस और सौंदर्य सन्निहित हो। इतिहास में सत्ता के अवसान के साथ ही विरुदावलियां अप्रासंगिक और अर्थहीन हो जाती हैं, जबकि प्रतिरोधी कला समय और काल से परे सार्थक और प्रासंगिक बनी रहती है। चूंकि सत्ता राजनीतिक दांव-पेंच और प्रचार माध्यमों के दम पर आमजन की चिंतन-प्रक्रिया को प्रभावित करती है, इसलिए आमजन उसके असली चरित्र को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। एक चिंतक, कलाकार, चित्रकार और लेखक सत्ता की इन कारगुजारियों को न केवल भली-भांति समझता और अपने कला-माध्यमों से अनावृत्त करता है, बल्कि रचनात्मक तरीके से निरंतर प्रतिरोध भी रचता है। इसके चलते सत्ता के निर्बाध दुरुपयोग में सत्ताधीशों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जनता के बीच अपनी पोल खुलने और कथित जन-हितैषी छवि के खंडित होने का भय बना रहता है।
चालाक और शातिर सत्ता सार्वजनिक छवि बचाए रखने, लोकतांत्रिक और मानवीय दिखते रहने के लिए प्राय: विरोधी विचारों को मंच प्रदान करती है। पद, पुरस्कार और अन्य प्रलोभनों के सहारे विरोधियों को अपने पक्ष में अनुकूलित करने का प्रयत्न करती है। कई बार वह विरोधी आवाजों को दबाने के लिए हथकंडे भी इस्तेमाल करती है। लेकिन साफ माथे का समाज अपनी समझ पर भरोसा करता है और चंडीदास जैसा संत कवि खुलेआम कहता है- ‘शुनह मानुष भाई/ सबाई ऊपरे मानुष सत्य/ ताहार ऊपरे केऊ नाई।’ मानुष सत्य को सब चीजों से ऊपर मानने वाला हमारा समाज गांधी की बातों को तो ध्यान से सुनता है, गांधी के ‘रघुपति राघव राजा राम’ को बखुशी गाता है, उसे मोहनदास करमचंद गांधी से ‘महात्मा गांधी’ बना देता है, लेकिन इस देश की मिट्टी को सिर्फ एक धर्म की जागीर मानने वालों को किनारे कर देता है! लेखक अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों से मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों का पोषक और संरक्षक होता है। इसलिए जिन ताकतों को लेखक, कलाकार, फिल्मकार इसके विरोध में देखता है, स्वाभाविक तौर पर वह उसका विरोध करता है। बिना इस बात की परवाह किए कि इससे उनको क्या-क्या नुकसान होगा और किन-किन मोर्चों पर उसे इस चीज की कीमत चुकानी होगी। सच्चा और प्रतिबद्ध कलाकार जब व्यक्तिगत नफा-नुकसान को ही लोकतंत्र और मनुष्यता का स्थानापन्न समझ लेता है, तो वह अपनी कला की बोली लगा कर आसानी से सत्ता का प्रवक्ता बन जाता है। पर जब वह सत्ता बदल जाती है और आमजन की हितैषी ताकतें सत्ता पर काबिज होती हैं, तो तमाम शानो-शौकत और चमक इतिहास के कृष्ण-विवर में खो जाती है। किसी सच्चे और ईमानदार लेखक-कलाकार के लिए पुरस्कार उसके सृजन का काम्य नहीं होता। पुरस्कार और सम्मान उसकी सृजन-यात्रा में एक पड़ाव भर होता है। लेकिन वैचारिक मतवैभिन्य के कारण किसी लेखक को पुरस्काराकांक्षी बता कर उसके लेखन और लेखकीय छवि का अवमूल्यन करना आजकल सत्ता का व्यवहार बनता जा रहा है। किसी सरकार या सत्ता द्वारा प्रदत्त पुरस्कार तब किसी लेखक को दिए जाते हैं, जब उस लेखक की स्वीकार्यता समाज में बढ़ जाती है और उसकी लोकप्रियता स्थापित हो चुकी होती है। मगर जब सत्ता यह कहती है कि लेखक को समाज ने तभी जाना, जब उसने लेखक को पुरस्कृत किया, तो इससे अधिक किसी लेखक का अपमान और क्या हो सकता है?
सत्ता अपनी बौखलाहट और चिड़चिड़ेपन में हर उस चीज को खारिज करने लगती है, जो उसके अनुकूल नहीं होती, जो व्यक्ति उसके अनुकूलन प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते। ऐसे में अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए सत्ता साम-दाम-दंड और भेद सभी का बेहिचक इस्तेमाल करती है। उसकी कार्यप्रणाली में ताकत का इतना दंभ आ जाता है कि वह खुलेआम यह कहने से गुरेज नहीं करती कि जो मेरे साथ नहीं है, वह मेरा दुश्मन है। और जब एक बार वे किसी को दुश्मन मान लेती हैं, तो फिर हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि या तो आप उनकी गुलामी स्वीकार कर लें, या उनका चारण बन जाएं या अपने को इस तरह अनूकूलित कर लें कि ‘जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे’। पर सत्ता यहां इस बात को भूल जाती है कि कलाकार विदूषक नहीं होता, न अपने को चारण के रूप में देखा जाना पसंद करता है। वह अपने राज्य और समाज ही नहीं, देश के स्तर पर भी अगर कुछ अमानवीय और अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति को महूसस करता है, तो उसके विरोध में अपने नाम और नामा दोनों को दांव पर लगा कर विरोध में उतरने में तनिक भी संकोच नहीं करता। फिर कोई हिटलर जैसा शासक गैस चैंबर का डर दिखाए या सुकरात की तरह जहर का प्याला पीने को विवश करे, लेखक तो वही कहता है, जो संपूर्ण मानवता के हित में होता है। कलाकार इस बात से बेपरवाह होता है कि कोई उसके सत्य का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। कलाकार अपने सत्य के लिए, मानवीयता और बहुजन हिताय के लिए बखुशी अपनी जान की बाजी लगा देता है, लेकिन अपने सत्य से समझौता करने को तैयार नहीं होता। जो इसके लिए तैयार होता है, वह दरअसल कला का व्यापारी होता है। कला के व्यापारी हर समय और हर समाज में होते रहे हैं। ऐसे पैसा बटोरू कलाकार सत्ता को सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं, जिन्हें पुरस्कृत और समादृत करके असहिष्णु और आतताई सत्ता अपने कृत्य को वैध और सच्चे कलाकारों के ईमानदार प्रतिरोध को अवैध ठहराने का प्रयास करती है। चूंकि सच्चा सृजन अपने स्वभाव और ताप से ही प्रतिरोधी होता है, इसलिए उसकी ताप से उतप्त सत्ता तमाम तरह की व्यूह रचना करके कला की धार को भोथरा करने का प्रयास करती है और जब इसमें उसको सफलता नहीं मिलती, तो दमनकारी कदम उठा लेती है। इतिहास गवाह है कि दमन और उत्पीड़न का सहारा लेने वाली सत्ता मिट कर नष्ट हो जाती है, जबकि कला दबाए जाने पर और अधिक दिनों तक परिदृश्य पर छाई रहती है, जिसकी आवाज से सदियों तक लोग अपनी आवाज मिलाते हैं। उसके मूल्यों और उसके सत्य से अपने जीवन-विवेक को सुपुष्ट करते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि कला का विरोध कला को और अधिक प्रासंगिक बनाता है।
पिछले पांच हजार वर्षों में अनेक सल्तनतें बनीं, वे नष्ट हो गर्इं। आज कौन उन सत्ताधीशों को याद करता है? जबकि कालिदास, भारवि, भवभूति, भरतमुनि, पंडितराज जगन्नाथ, विद्यापति, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, भारतेंदु आदि को दुनिया जानती है। उन्हें स्मृतियों से नष्ट होने में सदियां गुजर जाएंगी। सत्ता के सामने झुकने से इनकार करने वाले आज लेखक इन महान लेखकों के वंशज हैं, जिन्हें सत्ता के डंडे से डराया नहीं जा सकता। कलाकार ऐसी परंपरा के संवाहक हैं, जिसमें इसके लिए कीमत चुकाने से पीछे हटने की परंपरा नहीं है। शायर, सूफी, संत किसी बादशाह का इंतजार नहीं करता, न किसी बादशाह से कुछ पाने की उम्मीद करता है। मलिक मुहम्मद जायसी जैसा कवि जब अकबराबाद में बादशाह को अल्लाह से दुआ मांगते हुए देखता है, तो वह यह कहते हुए कि यह जिससे मांग रहा है, मैं भी सीधे उसी से मांग लूंगा- और यह कहते हुए बिना कुछ लिए वहां से चल देता है। सूफियों, संतों, दरवेशों, कलाकारों, लेखकों आदि के पास कोई बादशाही मसरुफियत नहीं होती है। मगर वे ठसक से कहते हैं- ‘बादशाह का इंतजार करें, इतनी फुर्सत कहां हम फकीरों को।’