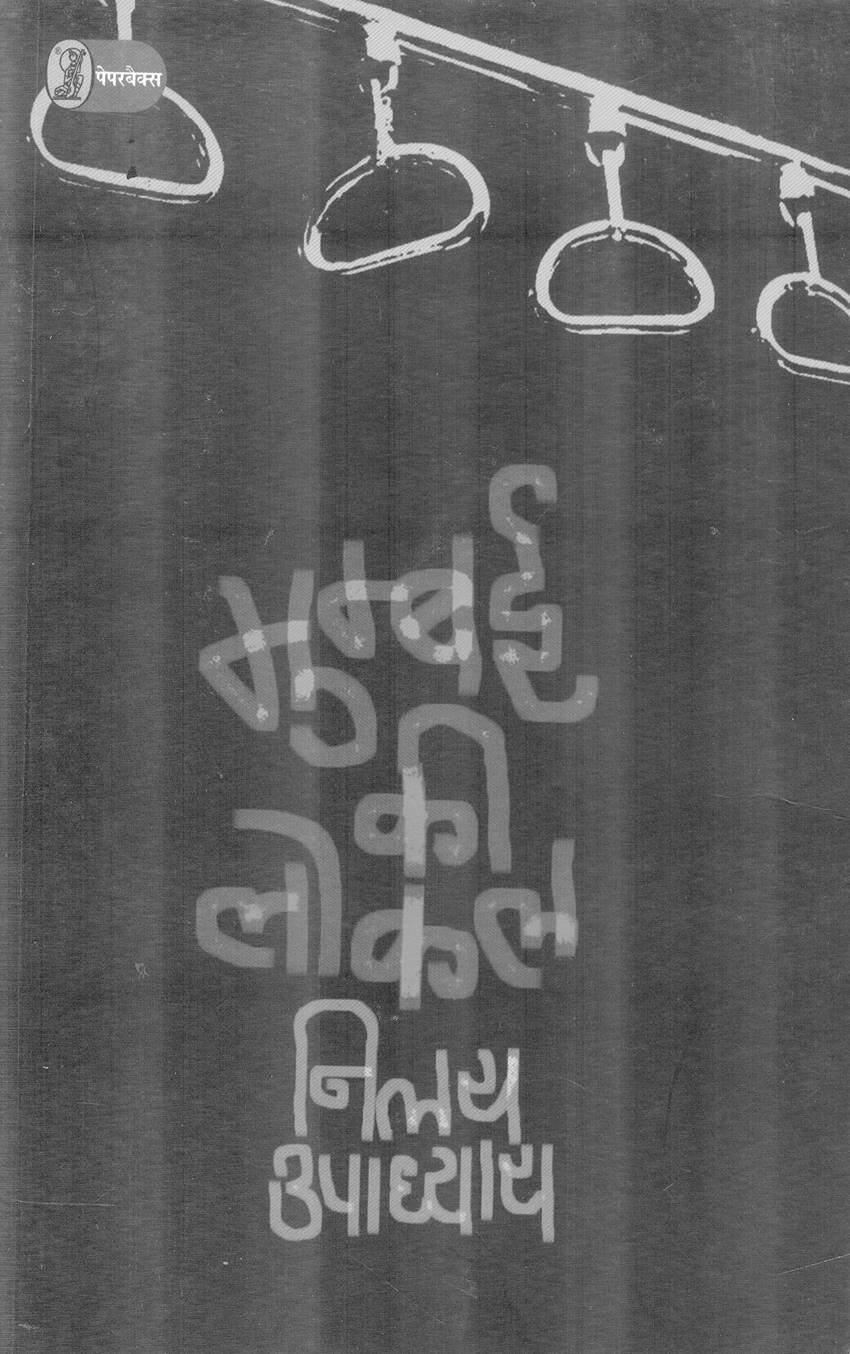परस्पर
किसी समाज का बहुमुखी होना उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का परिचायक है। इस समृद्धि के साथ कुछ समस्याएं भी पल्लवित-पुष्पित होती हैं। चाहे समृद्धि हो या समस्या, दोनों भू-राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना से गहरे प्रभावित होती हैं। न तो भाषा की समृद्धि निर्दोष एवं निरापद होती है और न ही समस्या। समृद्धि और समस्या की अन्योन्य क्रिया इसे जटिलता प्रदान करती है। ये दोनों विशिष्टताएं एक-दूसरे से गोया भिन्न दिख रही हों, एक-दूसरे को अपना ‘गैर’ मान रही हों, पर दोनों के भीतर भी दीगर मुख्तसर प्रवृत्तियां विराजमान रहती हैं। बहुभाषी समाज में भाषायी समस्या अपनी अस्मिता के रेखांकन का परिणाम भी होती है। अपनी भाषायी अस्मिता पर बल लोकतांत्रिक आकांक्षा से भी पनपती है। आधुनिकता, शहरीकरण, बढ़ते मध्यवर्ग और मीडिया के प्रसार इसके लिए जमीन तैयार करते हैं।
इस पुस्तक में संकलित शोध निबंध इसी बात की स्थापना करते हैं। इसमें तीन शोध निबंध हैं- ‘उन्नीसवीं सदी में ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली विवाद’, ‘राष्ट्र निर्माण, संविधानसभा और भाषा विमर्श’ तथा ‘बीच बहस में लघुपत्रिकाएं : आंदोलन, संरचना और प्रासंगिकता’। ये तीनों शोध निबंध बड़े फलक पर भाषा संबंधी बहसों को उठते और उनका विश्लेषण करते हैं। राजीवरंजन गिरि ने भाषा संबंधी विमर्श और संघर्ष के कई पहलू उजागर किए हैं और कई विवादों का विवरण भी सटीक ढंग से दिया है। इस तरह यह पुस्तक बहुत प्रासंगिक बन गई है।
परस्पर- भाषा-साहित्य-आंदोलन : राजीव रंजन गिरि; राजकमल प्रकाशन, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 595 रुपए।
मार्जिन में पिटता आदमी
इस किताब में शामिल व्यंग्य रचनाओं में हम हमारे देश के इस कठिन समय में सुलगते संकटों और सवालों से रू-ब-रू होते हैं। इनका रचनाकार अपने ताजगी, नैसर्गिकता और गहराई लिए हुए मेधावी हास्यबोध के साथ, समकालीन समय की विद्रूपताओं, विडंबनाओं और विकृतियों से संवादरत बना हुआ नजर आता है। इन रचनाओं की जड़ें अपने समय, समाज और संस्कृति में धंसी हुई जान पड़ती हैं और इनका समकालीनता बोध, साहित्य और जीवन के संगम और संयोजन के लेखकीय दायित्व का एहसास प्रदान करता है।
कुछ पंक्तियों में इन रचनाओं के कुछ ही आशयों, आयामों और भावों को रेखांकित किया जाना संभव है लेकिन पाठक इन रचनाओं पर ठहरते-ठिठकते हुए यह जरूर जान पाएंगे कि बुरी तरह मुनाफे और मुफ्तखोरी पर खड़ी होती हुई हमारा आधुनिक सभ्यता ने साधारण लोगों पर जीवन का कितना ज्यादा असहनीय बोझ डाल दिया है, मामूली आदमी को कितनी अमानवीयता के साथ हाशिए पर फेंका जा रहा है, मानवीय मूल्यों के कैसे पतन के दौर से हमारा समय गुजर रहा है।
ये रचनाएं हमारे समकालीन जीवन की क्रूर सच्चाइयों और हकीकतों को व्यक्त करते हुए, हमें अपने समय का विश्लेषण और आकलन करने के लिए, हमारा अपना आत्म-मंथन करने के लिए, आत्म-मंथन की घड़ियों से गुजरने के लिए प्रेरित करती हैं। इन रचनाओं की भ्रमजनित सादगी सिर्फ पढ़ने और मनोरंजन की सामग्री भर नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक तरह का आत्मीय अनिवार्य-सा पाठकीय अनुभव बनता है।
मार्जिन में पिटता आदमी : शांतिलाल जैन; क प्रकाशन, 43, गणेश नगर-॥, गली नं. 2, शकरपुर, दिल्ली; 200 रुपए।
रंगमंच : नया परिदृश्य
रीतारानी पालीवाल की यह पुस्तक रंगमंच की अवधारणा का समग्र बिंब प्रस्तुत करने का प्रयास है। जहां नाटक और रंगमंच की पारस्परिकता को विभिन्न कोणों और पहलुओं से देखते हुए नवीन परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है। इसमें नाट्यधर्मी और लोकधर्मी परंपराओं के सांस्कृतिक मिथकों, आख्यानों, प्रतीकों, बिंबों से साक्षात्कार करते हुए प्राच्य और पाश्चात्य रंग-दृष्टियों की स्वतंत्र निजी पहचान को उद्घाटित किया गया है। भारतीय, एशियाई और पश्चिमी रंग-परंपराओं के स्वरूप और विशिष्टताओं को सामने लाने के साथ ही यह उनके बीच आदान-प्रदान की उपलब्धियों और सीमाओं को भी रेखांकित करती है।
औपनिवेशिक विरासत के चलते हम भारतीयों की मनोभूमिका में पश्चिम के प्रभाव-दबाव इतने प्रबल रहे कि पूर्व एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया की रंग-परंपराओं की ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया। पूर्व एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के साहित्य, नाट्य-परंपरा और संस्कृति से हम लंबे समय तक लगभग अनभिज्ञ बने रहे। हिंदी में तो यह जानकारी लगभग उपलब्ध ही नहीं है। लंबे समय तक भारतीय रंग-परंपरा से भी हम वैसा रिश्ता कायम न कर सके जैसा चीन, जापान, थाईलैंड आदि ने कायम रखा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुस्तक में एशियाई रंग-परंपरा पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है जिसमें जापान के नोह और काबुकी, चीन के शीक्यू, थाईलैंड के लाकोन खोन, रामकिएन, इंडोनेशिया के सेंद्रातारी, कंबोडिया के रेयेउंग के विषय में जानकारी शामिल करके रंग-परिदृश्य का अपेक्षित विस्तार किया गया है।
रंगमंच- नया परिदृश्य : रीतारानी पालीवाल; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 595 रुपए।
लोक, आस्था और पर्यावरण
जिस तरह से ‘विकास’ एक नई अवधारणा है, ठीक उसी तरह पर्यावरण संरक्षण भी एक नए जमाने की समस्या है। विकास, प्रगति का उत्प्रेरक तत्व है, लेकिन इसका मूल महज आर्थिक तत्व नहीं है, बल्कि गुणात्मक उन्नति है। मुल्क के हर बाशिंदे, चाहे वो इंसान हो या फिर जीव-जंतु, साफ हवा मिलें सांस लेने के लिए, नदी-तालाब, समुद्र स्वच्छ हो, लाखों-लाख किस्म के पेड़-पौधे, कीट-पतंगे, जानवर-पक्षी उन्मुक्त होकर अपने नैसर्गिक स्वरूप में जीवन यापन कर रहे हों- एसा विकास ही जनभावनाओं की संकल्पना होता है। विडंबना है कि भौतिक सुख की बढ़ती लालसा और कथित विकास की अवधारणा ने एक भयानक समस्या को उपजाया और फिर उसके निराकरण के नाम पर अपनी सारी ऊर्जा और संचय शक्ति तथा धन व्यय कर दिया।
हमारे प्राचीनतम ग्रंथ और सदियों से आदिवासी व लोक में प्रचलित धारणाओं को गंभीरता से देखें तो पाएंगे कि हमारे पुरखों की सीख, पर्व, उत्सव और जीवन शैली उसी तरह की थी कि सारा विश्व और उसके प्राणी सहजता से जीवन जी सकें, न तो कोई बीमार हो, न ही कोई भूखा। इसके लिए अनिवार्य था कि जल, वायु और भोजन निरापद हो।
यह पुस्तक हमारे पर्व-त्योहारों की मूल भावना और उसमें आए परिवर्तनों से उपजते सामाजिक व पर्यावरणीय विग्रह की बात तो करती ही है, हमारे गांव-जंगलों में रहने वाले पुरखों की ऐसी परंपरा पर भी विमर्श करती है, जिसे आज का कथित साक्षर समाज भले ही पिछड़ापन कहे, असल में उसके पीछे गूढ़ वैज्ञानिक चेतना और तार्किक अनुभव थे।
लोक, आस्था और पर्यावरण : पंकज चतुर्वेदी; परिकल्पना, बी-7, सरस्वती कांप्लेक्स, तृतीय तल, सुभाष चौक, लक्ष्मीनगर, दिल्ली; 325 रुपए।