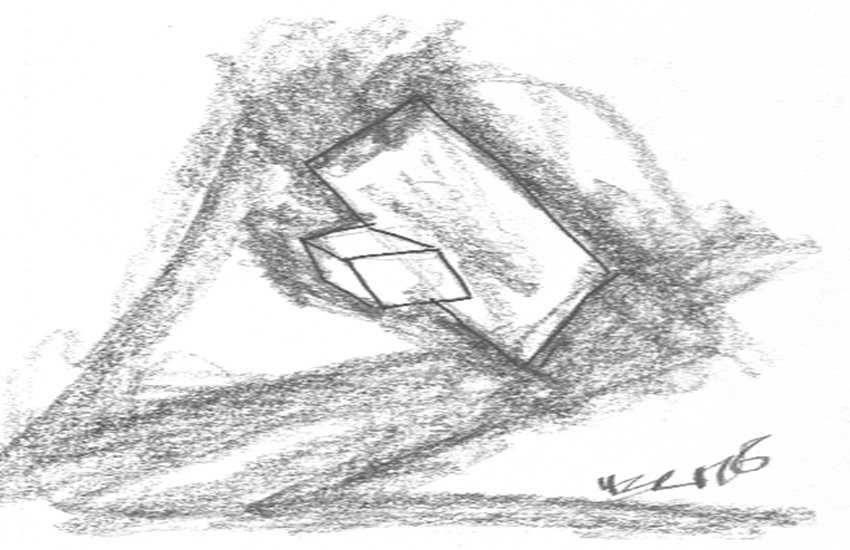अजयेंद्र नाथ त्रिवेदी
एक हमारा एक सुपरिचित शब्द है। विभिन्न संदर्भों में इसका प्रयोग पता नहीं कब से होता आ रहा है। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, पुराणों से लेकर भक्ति और संत साहित्य तक में यह शब्द मिलता है। हमारे संविधान में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इन सभी संदर्भों में लोक एक व्यापक, महनीय और उदात्त अर्थ का व्यंजक शब्द है। इसके बावजूद, फोक का हिंदी प्रतिशब्द बन कर लोक ने अपना स्वत्व खो दिया है। इसी के साथ भारतीय संदर्भ में इसका अर्थगौरव घटता गया और लोक की भारतीय उदात्तता फोक की पाश्चात्य धूसरता में पर्यवसित होती गई। यूरोपीय संदर्भ में फोकलोर का अर्थ है- पुराने समय की जातियों के पारंपरिक ज्ञान का शास्त्र। एक पश्चिमी विचारक के अनुसार फोक का तात्पर्य उस समाज से है, जिसने आधुनिक सभ्यता का प्रकाश नहीं देखा है और परंपरा-प्राप्त ज्ञान से अपना निर्वाह कर रहा है। फोक के अध्ययन के शास्त्र को फोकलोर कहा गया। फोकलोर में जोर पुरातनता पर है। इसमें अतीत की खोज है। फोकलोर नृतत्व शास्त्र का करीबी शास्त्र है। भारत में ऐसे किसी अकादमिक अध्ययन की परंपरा नहीं थी। यहां यह ज्ञान पौराणिक विषयों के अंतर्गत आता था। भारतीय परंपरा में लोक, फोक की तरह विगत की स्मृति नहीं है। यह निरंतर विद्यमान एक अस्तित्व का अनुभवात्मक प्रत्यक्षीकरण है। इसमें निरंतरता है, समष्टि परायणता है और मानव-प्रकृति की अन्योन्याश्रितता है। फोक शब्द की अर्थ व्याप्ति से लोक शब्द की अर्थ व्याप्ति गुरुतर है। तथापि, बेहतर विकल्प के अभाव में फोक के लिए भारतीय संदर्भ में लोक शब्द को धीरे-धीरे सबने स्वीकार कर लिया।
लोक का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है- जो देखा/ प्रकाशित किया जा सके। यह संस्कृत की रुच् और लुच् धातु से निष्पन्न है। जिसमें प्रकाशित होने या प्रकाशित करने का अर्थ है। इस प्रकार सारी सृष्टि ही लोक की परिभाषा में आ जाती है। लोक में समस्त परिदृश्य समाहित हैं। इसमें भूमि और वन, नदियां और समुद्र, पर्वत और मैदान तो आते ही हैं, पशु-पक्षी, ग्रह-नक्षत्र सभी इसमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए भारत में लोक एक विद्यमान सत्ता है। जन इसके केंद्र में है। चूंकि लोक, फोक की अपेक्षा अधिक जीवंत, प्रासंगिक और समावेशी है, अत: लोक को फोक के बरक्स रखने से लोक की उदात्त पहचान धूमिल होती चली गई।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्थापित किया है कि लोक का अर्थ ग्राम या जनपद नहीं है। उनके अनुसार लोक का विस्तार ग्रामों से लेकर नगरों तक है। हालांकि उन्होंने कहा है कि लोक अपने व्यावहारिक ज्ञान के लिए पोथियों पर आश्रित नहीं रहता। अज्ञेय ने लोक को नित नूतन होती जा रही अभिव्यक्ति कहा है। इस प्रकार लोक एक गहन और व्यापक अनुभव है। यह मानव और प्रकृति की अन्योन्याश्रितता है। इसमें व्यतीत की नहीं, आज और अभी की बात है। वांछनीय इतिहास यहां अपनी प्रांगिकता के साथ विद्यमान रहता है और वर्तमान भी अगर अवांछित हो, तो तिरस्कृत हो जाता है। जैसा फोक के साथ हुआ करता है, लोक महज एक स्मृति बन कर रह जाए या प्रदर्शन की वस्तु बन जाए, भारतीय संदर्भ में यह काम्य नहीं है।
भारतीय परंपरा में लोक की महनीय प्रतिष्ठा रही है। यहां इसे मात्र बुद्धि का कुतूहल नहीं समझा गया है। लोक को देखना ही सबको देखना समझा गया है। यहां शास्त्र लोक के साथ जुड़ कर ही सार्थक हुआ है और लोक शास्त्र का पूरक रहा है। जैमिनीय उपनिषद में कहा गया है- ‘बहु व्याहतो वा अयं बहुशो लोक:/ क एत अस्य पुनरीहितो अयात्।’ यानी यह लोक बहुविध फैला हुआ है। प्रत्येक वस्तु में यह प्रभूत रूप में विद्यमान है। यही वजह है कि लोक के परिचय के बिना कलाओं, शास्त्रों का ज्ञान पर्याप्त नहीं समझा जाता। कहा भी गया है- शुद्धं लोक विरुद्धं न हि करणीयं न हि करणीयम्। पाश्चात्य परंपरा से आगत इस विद्या-सरणी में भारतीय परंपरा के प्रति कोई खास समादर नहीं था। नतीजतन भारतीय लोक की उदात्त छवि ठीक से उजागर न हो सकी। विद्यानिवास मिश्र के लिए यह अस्वीकार्य था। उन्होंने अपनी विशिष्ट निबंध शैली में भारतीय लोक के उदात्त पक्षों का मुखर उपस्थापन किया और इस संबंध में विचार-विमर्श का परिवेश तैयार किया। यही नहीं, इस विषय को केंद्र में रख कर उन्होंने पुस्तकें भी लिखीं और विद्वानों का ध्यान खींचा। उनके अधिकांश निबंध लोक की पहचान की उत्कंठा में रचे गए हैं।
विद्यानिवास मिश्र की मान्यता है कि संस्कृति की दृष्टि से श्रेष्ठता की पहचान शील से होती है और शील की कसौटी है लोक। उपनिषद में अनवद्य (अनिंद्य) कार्य करने का उपदेश दिया गया है, इतर कार्य का नहीं। लोक में ही महान और अनुकरणीय आदर्श के ज्वलंत उदाहरण मिलते हैं, उनकी प्रेरक गाथाएं मिलती हैं। मानव जीवन हमारी सामूहिक धरोहर है और सभी संबंध इस धरोहर की श्रीवृद्धि के लिए बने हैं। पूर्णता को प्राप्त करना हमारी महत आकांक्षा है। जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और भौगोलिक परिवेश से जुड़ कर ही मानव जीवन को पूर्णता मिलती है। ऐसे जुड़ाव के लिए लोक-परंपराओं का पालन किया जाता है। हमारे जीवन के आधार हैं हमारी पृथ्वी, उसके वन और नदियां, पहाड़ और मैदान। ये सभी संरक्षणीय हैं- यह संदेश हमें लोक कथाओं में मिलता है। विद्यानिवास मिश्र ने अपने व्यक्तिव्यंजक निबंधों में इन विषयों को बार-बार उठाया है।
वे लोक संस्कृति को अध्ययन और शोध का नहीं, जीवन का विषय मानते हैं। वे कहते हैं- मैंने अपनी मां से जो सीखा है उसे मैं संग्रह की वस्तु या अलमारी में सजाने की वस्तु नहीं मानता। मैं उसे जीवन का प्रेरणास्रोत मानता हूं। ये प्रेरणाएं उन्हें अपने लोक के परिवेश से मिलीं, उसकी परंपराओं से मिलीं, उसके गीतों से मिलीं, लोक के शिल्प और लोक की कलाओं से मिलीं और उनके शत-शत निबंधों का स्थायी भाव बन गर्इं। उन्होंने साहस के साथ कहा कि लोक को हमने फोक मान कर बड़ी भूल की है। हम निर्मम संग्रही और तर्कशुष्क विश्लेषक हो गए हैं। लोक को जीवन-रस के निर्झर के रूप में देखने में हम चूक गए हैं। उनकी मान्यता है कि लोक के उदात्त रूप को नृतत्व वैज्ञानिक अथवा समाज वैज्ञानिक रीति से समझा-समझाया नहीं जा सकता।
विद्यानिवास मिश्र के अनुसार भारतीय परंपरा के दो अक्षय स्रोत हैं। एक है- शास्त्र तो दूसरा है लोक। वे कहते हैं, लोक दूब है। इसको उजाड़ने वाले उजड़ सकते हैं, पर ये कभी नहीं उजड़ते। एक जगह से उजड़ते हैं तो फिर दूसरी जगह बस जाते हैं। लोक के फल-फूल, व्रत-त्योहार, नृत्य-गीत, रिश्ते-नाते, ऋतु-मास आदि उन्हें लिखने के लिए उकसाते रहे हैं। ये प्रसंग लोक जीवन की रसधार बनते हैं। व्रत-त्योहार भारतीय लोक का उल्लास हैं। इसमें मिलने-मिलाने, जुड़ने-जोड़ने की, खाने-खिलाने, पहनने-पहनाने के कई बहाने मिलते हैं। भारतीय परिवेश में जो व्याप्त है, जो दृश्य है वह सब लोक ही है। लोक में अंतत: सब आनंद ही आनंद है, क्योंकि वह स्वभाव से विस्तरणशील है। वह घटाकाश की अपनी आरोपित सीमा में नहीं, मठाकाश की अपनी व्याप्ति में विश्वास रखता है। यह एक अनुभूत तथ्य है कि लघु में नहीं, विराट में ही सबकी गुंजाइश हो सकती है। लोक विराट की छाया है और भूमा की संभावना। लोक के सारे प्रतीक, सारी कलाएं, सारे अनुष्ठान और सारे समारंभ विराट की छाया में भूमा की संभावना से प्रेरित हैं। डॉ. मिश्र के व्यक्तिव्यंजक निबंधों का लगभग सारा प्रस्तार लोक के प्रत्यभिज्ञान का प्रयास है। ०