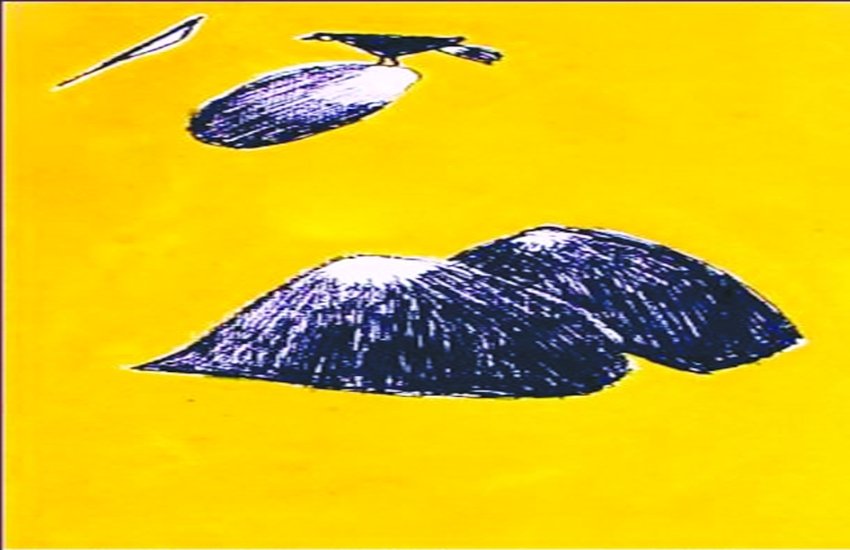सुरेश पंत
संस्कृत की धातु दृश् से हिंदी में दो शब्द परिवार बने हैं- देखना और दर्शन। संभवत: आम जन की लोक धारा में ‘देखना’ शब्द प्रचलित हुआ, पर कुछ विशेष औपचारिक स्थितियों में दर्शन शब्द ही चलता रहा। लगभग समानार्थी होते हुए भी अब दोनों शब्दों ने अपने-अपने अलग क्षेत्र चुन लिए हैं। देखना तो मूलत: आंखों से प्रकाश की सहायता से संपन्न होने वाला कार्य है। हम वह सब देखते हैं, जो हमारे सामने होता है। अंधेरे में कोई कुछ नहीं देखता। यह इसका सीधा प्रयोग है। पर इसके लाक्षणिक प्रयोग रोचक हैं और अनेक अर्थ छवियां दूर-दूर ले जाती हैं। जैसे-
’डॉक्टर रोगी की नब्ज देख रहा है (जांचना)
’रोगी को नर्स देख रही है (देखभाल)
’शिक्षक तुम्हारे उत्तर देख रहा है (जांचना)
’देखना, दूध उबल कर बिखर न जाए (सावधान रहना)
’तुम आवेदन पत्र दे आओ, बाकी मैं देखूंगा (ध्यान देना)
’इस चौकी को कौन देखता है आजकल? (चौकसी, पहरेदारी)
’भगवान सबको देखता है (ध्यान में रखना, विवेचन करना)
’लड़की देखने जाना है (पसंद करना)
’एक समिति मंदिर की व्यवस्था देख रही है (संचालन करना)
’पढ़ चुके हो, अब कुछ काम-वाम देखो (ढूंढ़ना)
’विज्ञान शिक्षक ने दिखाया, बर्फ कैसे जमती है (प्रयोग से समझाना)
’अच्छे आम देख-देख कर लाया हूं (चुनना)
’मैं सिनेमा नहीं, नाटक देखता हूं (मनोरंजन)
’सब देख लिया, पर पर्स नहीं मिला (खोजना)
’साहब कल तुम्हारा काम देखेंगे (निरीक्षण करना)
’आने दो, मैं उसे देख लूंगा (निपटना, धमकी का भाव)
’आप थोड़ी देर मेरा सामान देखिए, मैं अभी आया (निगरानी रखना)
’अभी चुप लगा जाओ, मौका लगने पर हम भी देखेंगे (बदला लेना)
देखने के अंदाज भी अपने-अपने, अलग-अलग हैं। कोई किसी को तिरछी नजर से देखता है, तो कोई उड़ती नजर से। किसी की कनखियों से देखने पर युवा मन ही नहीं, कवि कलाकार भी भटक जाते हैं। घूर कर देखने वाले के जवाब में जिसे देखा जा रहा है वह आंखें तरेर कर देख सकता है और आंखें फाड़ कर भी। और यह तो हम सभी जानते हैं कि देखते-देखते कुछ का कुछ हो जाता है। महाकवि ‘निराला’ के इस प्रयोग का तो कोई जवाब ही नहीं-
‘देखते देखा मुझे तो एक बार,
उस भवन की ओर देखा
छिन्नतार…’
देखना से बनी भाव वाचक संज्ञाएं भी देखते चलें। लोग दिखावा करते हैं और कुछ लोग उनकी देखा-देखी करते हैं। कुछ को इसमें अपव्यय होता दिखाई पड़ता है। अब यह ‘दिखाई’ भी अजीब है। राह दिखाई पर गाइड को कुछ दें न दें, मुक्ति के मार्ग की दिखाई का दावा करने वाले गुरुओं को गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ती है। मुंह दिखाई पर कुछ न कुछ देना तो रिवाज ही है। कुछ लोग रास्ता चाहे गलत दिखा दें, दिन में तारे दिखाने का दावा जरूर करते हैं। वैसे आजकल आप किसी पर भरोसा भी कैसे करेंगे, जब पता चलेगा, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं। इधर कोई विज्ञापन दावा करता है- ‘देखते रह जाओगे!’
दर्शन- अब ‘देखना के संभ्रांत और कुलीन किस्म के भाई ‘दर्शन’ और उसके परिवार के दर्शन भी करते चलें। यह ‘दर्शन’ औपचारिक भाषा का शब्द है, और है बड़ा आदरणीय शब्द। यह कभी एकवचन में प्रयुक्त नहीं होता। चाहे दर्शन करने वाला एक हो या दर्शन देने वाला भी अकेला हो, पर दर्शन सदा बहुवचन में होंगे।
’आपके दर्शन कब होंगे साहब? – देवता के दर्शन सहज नहीं हैं। – आभारी हूं, आपने दर्शन दिए। – इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं।
नित्य बहुवचन में होने के अलावा ‘दर्शन’ महाशय की एक और विशेषता है। ये वाक्य में प्राय: कभी अकेले उपस्थित नहीं होते, किसी क्रिया को अपनी सहायता के लिए अवश्य साथ रखते हैं। उनमें प्रमुख हैं, करना/ कराना, होना, पाना/ होना, देना। इनमें से कोई न कोई इनके साथ उपस्थित रहती है- देवदर्शन कर लिए/ करा दिए।- कब आपके दर्शन पाऊंगा / मिलेंगे? आदि।
यह ‘दर्शन’ जब ज्ञानमार्गी हो जाता है, तो वह किसी वाद, मत, विचारधारा का विमर्श या आत्मा/ परमात्मा, प्रकृति/ पुरुष, सत्य/ असत्य के तत्त्व ज्ञान का निरूपण करता है और तब भी इसे ‘दर्शन’ ही कहा जाता है। स्वयं भी तत्वज्ञान हो जाने के कारण यह दर्शन शब्द अपना स्वभाव बदल लेता है, इसमें अहंकार नहीं रहता और ‘नित्य बहुवचन’ वाली विशेषता छूट जाती है। जैसे:
’तुम्हारा जीवन दर्शन क्या है?
’भारतीय दर्शन छह प्रकार के हैें।
’बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है।
इस दर्शन परिवार के कुछ अन्य सदस्य हैं: दृश्य, दृष्टि, दृष्टा, दर्शक, दर्शनीय, दार्शनिक, प्रदर्शन, प्रतिदर्श आदि।
उछलकूद की बातें
सामान्यतया एक धरातल से वेगपूर्वक उठना ही उछलना है। संस्कृत में उद्+शल् (दौड़ना) से ल्युट् प्रत्यय जोड़ कर उच्छलन बनता है। हमारे राष्ट्रगीत के ‘उच्छल-जलधि-तरंग’ में यही ‘उच्छल’ है। इसका सामान्य अर्थों में प्रयोग है: गेंद उछलती है, बच्चे भी उछलते हैं, पर लाक्षणिक प्रयोग अधिक रोचक और विविध हैं। जैसे- अरहर के दाम उछलते हैं। – सोने में उछाल आता है।’आजकल शेयरों में उछाल दिखाई पड़ता है।
’मेरे सामने उछलो मत, मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। (घमंड करना)
’शुरुआती दौर का रुझान देखकर नेताजी उछल पड़े। (इतराना)
’सफलता का समाचार सुन कर विद्यार्थी उछल पड़ते हैं।
’भ्रष्टाचार की बात उछाली जाती है।
’किसी की प्रसिद्धि में भी उछाल आता है।
’लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं।
’समुद्री तूफान से लहरों में उछाल आता है।
अर्थ में उछलना के निकटस्थ मित्रों में हैं- कूदना, फांदना, छलांगना और लांघना। कूदना तो संस्कृत का कूर्दन ही है। कूदना में किसी सतह से उछल कर उसी धरातल पर वापस आने की क्रिया है। यह क्रिया के साथ जोड़ीदार बन कर भी आता है और स्वतंत्र भी।
’वह तालाब से कूदा।
’बंदर पेड़ से कूद पड़ा।
’उछलना-कूदना बच्चों का स्वभाव है।
’लोग किसी की बातों के बीच कूद पड़ते हैं। (दखल देना)
’अनेक लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। (अचानक शामिल होना)
’अब कूदना-फांदना व्यर्थ है।
’कूदने की प्रतियोगिताएं कल होंगी।
’रस्सी कूदना अच्छा व्यायाम है?
फांदना/ फलांगना
फांदना भी एक प्रकार से लांघना ही है। इसमें उछलना पहली क्रिया है और फांदना दूसरी। फांदने के लिए हम पहले हवा में उछलते हैं, फिर किसी दूरी या रोक को लांघते/ फांदते हुए कूद कर नीचे आते हैं। लांघना में दूरी कम होती है, बिना उछले ही कदम को लंबा करके भी पार की जा सकती है :
’बकरी भेड़ को लांघकर आगे निकल गई।
’सड़क में गड्ढा है, फांद कर आ जाइए।
’चोर दीवार फांद कर आया।
कभी-कभी यह फांदना एक उछाल में नहीं भी संपन्न होता, जैसे: पवर्तारोही अनेक पवर्तों को फांद कर अंतिम शिखर पर पहुंचे।
छलांगना में अंतर यह है कि छलांग उछल कर दूर तक कूदने की क्रिया है। इसका गंतव्य होता है, कूदना में नहीं होता। जैसे मेंढक छलांग लगाते हैं।
‘फुदकना’ में गति तो छलांग वाली है, पर गंतव्य आगे बदलता बढ़ता रहता है, जैसे- तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर फुदकती हैं।
’मेंढक फुदक-फुदक कर चला गया।
’टिड्डियां उड़ती हैं और फुदकती भी हैं।
’गौरैया आंगन में आई और फुदक-फुदक कर दाना चुगने लगी। ०