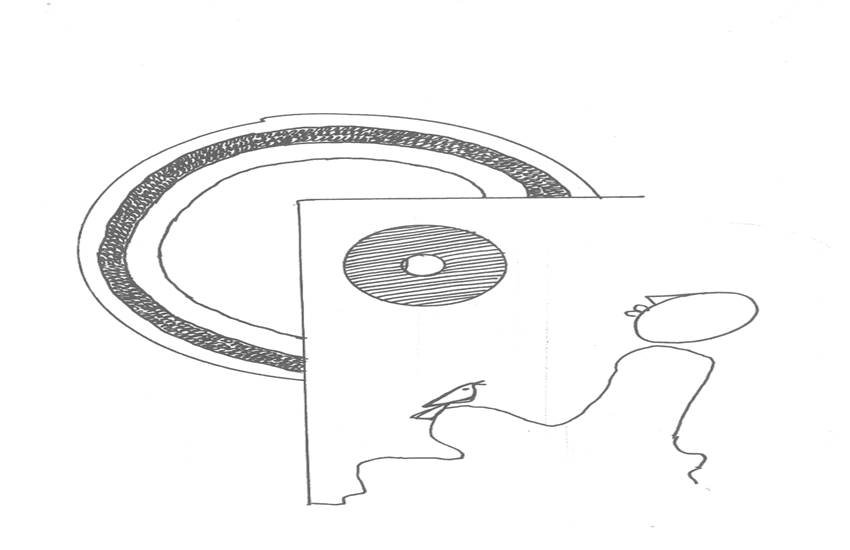देवशंकर नवीन
उपभोक्ता-वृत्ति और विज्ञापन के वर्चस्व के चलते भारत की सदियों पुरानी भाषिक विरासत आज कहीं नेपथ्य में बैठी है; क्योंकि उसके प्रयोक्ता खुद को विज्ञापनों की भाषा में सुर्खरू समझते हैं। सवाल है कि विज्ञापन किसलिए होता है—उपभोक्ता को ठगने के लिए या उत्पादक को संपन्न करने के लिए! ‘भाषा’ दरअसल, मनुष्य के सभ्य और स्वायत्त होने की पहचान के साथ-साथ अपने उत्पादकों और प्रयोक्ताओं की नीयत भी बताती है। बशर्ते आप उस नीयत को पहचान सकें! भाषा सभ्य, व्यवस्थित और उत्तरोत्तर उन्नत होने की दिशा में मनुष्य की सबसे बड़ी सहायिका रही है। भावाभिव्यक्ति के साधन के अलावा यह सामुदायिक संस्कृति और सोच-विचार का आधार भी है। भाषा के बिना कुछ भी सोचना असंभव है। अपने वैयक्तिक, पारंपरिक और राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान कोई मनुष्य इसी के जरिए करता है; और जिन मूल्यों और नैतिकताओं के कारण वह मनुष्य होता है, उनके संतुलन की चिंता करना भी सीखता है। पर विज्ञापनी वर्चस्व के आधुनिक दौर में हम भाषा को ऐसे नहीं देख सकते। उस दिशा में भारतीय समाज का भाषिक परिदृश्य विचित्र दशा में है। आज के प्रयोक्ताओं के पास शब्दों, संबोधनों, क्रियापदों, प्रयुक्ति की भंगिमा की बेहद गरीबी छाई हुई है। स्वायत्त और प्रभुत्वसंपन्न भारतीय समाज का भाषिक-बोध इतना सिमट गया है कि वह मुहावरों में भी अभिधेयार्थ ढूंढ़ता है। अपने उतावलेपन से आधुनिक हुए ऐसे भारतीय न्यूनतम क्रियापदों से सारा काम चलाना चाहते हैं। जबकि क्रियापद और सर्वनाम के जरिए भारतीय भाषाओं के संस्कार परिलक्षित होते हैं।
‘कामचलाऊ संप्रेषण’ और ‘बेशुमार धनार्जन’ के नशे में लिप्त, आधुनिकता के इन सिपाहियों को नहीं मालूम कि भाषा अंतत: मनुष्य की निजता और राष्ट्रीयता की पहचान होती है। इन्हें चूंकि अपनी भाषिक गरिमा का बोध नहीं है; इसलिए किश्तों में अपनी भाषिक क्षमता खोकर आज पूरी तरह भाषाविहीन हो गए हैं। इस दिशा में भारत के भाषाविदों, अध्यापकों, समाजसेवियों, शोधार्थियों और सत्ता के नियंताओं को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि लंबे समय तक औपनिवेशिक मनोदशा के अधीन रह कर भी जिन भारतीयों ने अपनी भाषा-संस्कृति की गरिमा कायम रखी; आजादी के कुछेक बरस तक भी वह अनुराग कायम न रह सका। अपने अनेक भाषा-व्यवहार में आज के भारतीय अपनी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय अस्मिता का संपूर्ण संकेत नहीं दे पाते। वे न केवल अपनी भाषिक प्रयुक्तियों की मर्यादाओं, विशिष्टताओं से नावाकिफ हैं; बल्कि भाषिक छवियां भी उनके लिए अजनबी हैं। चिंतनीय, पर सत्य है कि ऐसी स्थितियों में आकर भी वे खुद को अयोग्य नहीं समझते; ‘एडवान्स हो चुके’ समझते हैं।
भारत के भाषिक परिदृश्य में ऐसी नागरिक-निरपेक्षता का कारण सामुदायिक परिवेश में भोगवृत्ति का गहन प्रवेश है। चारों ओर उपभोक्ता संस्कृति छाई हुई है। लोगों की पूरी जीवन-व्यवस्था विज्ञापन और विज्ञापन की भाषा से संचालित हो रही है। छह दार्शनिक परंपराओं वाले देश के नागरिकों के लिए तर्क करना आज इतना निरर्थक लगता है कि मुर्गी के अंडे पर चिपकी पट्टी के कारण वे उसे उस कंपनी का अंडा मान लेते हैं। नारों के व्यापारिक लक्ष्य पर तनिक विचार नहीं करते। सम्मोहित अनुयायी की भांति चल पड़ते हैं। क्योंकि वे अपनी भाषा और भाषिक समझ खो चुके हैं।आम नागरिक ही नहीं, विज्ञापन की भाषा और पद्धति पर सोचने की जरूरत व्यवस्था-संचालन के नियंताओं को भी महसूस नहीं होती। सामाज में जागरूकता फैलाने वाले प्रसंगों के अलावा व्यक्तियों/ संस्थाओं की व्यावसायिक उन्नति को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को भी इन दिनों भारत में जनसंचार माध्यमों, सोशल मीडिया और मुनादी द्वारा प्रचारित करने की आजादी मिली हुई है। अधिकतर विज्ञापनों से सामाज में ठगी, असावधानी, अंधविश्वास, राष्ट्रीयता और नैतिकता के प्रति लापरवाही, तरह-तरह की विसंगतियां फैल रही हैं। पर्व-त्योहारों के आते ही मेल/ मोबाईल/ टीवी पर ‘आॅफर’ आने लगते हैं। इन उत्पादकों ने शायद तय कर रखा है कि आम नागरिक इधर-उधर न करे, जो भी कमा कर घर लौटे, लिए-दिए हमारे खाते में आकर डाल जाए।
विज्ञापन लिखने वालों, मॉडलिंग करने वालों को तो उत्पादकों से मोटी रकम उगाहनी होती है, उन्हें कोसने का कोई फायदा नहीं; पर इन विज्ञापनों के सम्मोहन में बेतहाशा दौड़ते आम नागरिक का आचरण हैरत में डालता है। गजब खेल है; उपभोक्ता समझता है कि वह फायदे में है; जबकि वह शिकार हुआ है। उत्पादक समझता है कि उसका निशाना सही लगा है, पर वह कहता है कि हम तो उपभोक्ता के सेवक हैं। निस्सहाय उपभोक्ता चूंकि लंबे समय से कथन का ‘आरोपित अर्थ’ समझता आया है; अपनी भाषिक भव्यता का निरंतर तिरस्कार करता आया है, इसलिए उसे यह तिलिस्म समझ नहीं आता, वास्तविक स्थिति का उसे बोध नहीं होता। इनकी तर्कशक्ति अवरुद्ध है; विज्ञापनकर्ताओं के लिए ये मुग्ध, सम्मोहित और उनके पीछे बेसुध दौड़ती हुई भीड़ हैं।
उत्पादकों को व्यावसायिक रणनीतियों के तहत सम्मोहन चित्तविजय का यह खेल खेलना पड़ता है! उन्हें मदारी खरीदना पड़ता है। ये बिके हुए मदारी तनिक भी नहीं सोचते कि जिस सामान्य नागरिक ने हमें राष्ट्र का आइकन बनाया; इन विज्ञापनों में हम उन्हें ही चूना लगा रहे हैं और पूंजीपतियों का खजाना भर रहे हैं! वे कभी देश के नियंताओं को नैतिक और राष्ट्रहितैषी पाठ पढ़ाने वाले विज्ञापनों की बात नहीं सोचते! वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में आगे रहने वाले भारत के शोध, अनुसंधान, शिक्षण, अध्यवसाय के उन्नयन की दिशा में विज्ञापन करने की बात नहीं सोचते! विज्ञापनों की वैधानिकता और भाषा पर गंभीर बहस होनी चाहिए।
मनुष्य से उसकी ‘भाषा’ छीनने की तरकीब भारत में नई नहीं है।
आजादी के कुछेक बरस बाद से ही शुरू हो गई थी। भारतीय लोकतंत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि और चयनित अधिकारियों में ‘शासक’ बनने की भूख बलवती हो उठी थी; वे जानते थे कि जिस मनुष्य के पास भाषा होगी, उस पर शासन नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाषा होगी, तो वह बोलेगा; तर्क करेगा; बोलता रहा, तर्क करता रहा तो विरुद्ध बोलेगा। पहले एक बोलेगा, फिर दो, फिर दस, सौ, हजार, करोड़… आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इसलिए शासितों के मुंह में जबान रहने देना, तर्क-शक्ति रहने देना शासकों को अपने लिए हितकर नहीं लगा; वे जनता की भाषा छीनने की जुगत बिठाने लगे। यह शातिरपना उस दौर के विशिष्ट कवि धूमिल को स्पष्ट दिख रही थी। उन्हें ‘भाषा के चौथे पहर में जुआ तोड़ कर भागते हुए शब्द’ दिखने लगे थे; ‘परिचित चेहरा भी तत्सम शब्द-सा अपरिचित’ लगने लगा था; ‘शब्दों के जंगल में शब्द और स्वाद के बीच भूख को जिंदा रखना’ भारी लगने लगा था। आम नागरिक को कथन के ‘प्रायोजित अर्थ’ समझाने और मनवाने की परंपरा चल पड़ी थी। क्योंकि ‘प्रायोजित अर्थ’ समझने का अभ्यासी नागरिक धीरे-धीरे अर्थान्वेष की अपनी प्रक्रिया भूल जाता है; अंतत: गूंगा हो जाता है। धूमिल इस तथ्य से अवगत थे, इसलिए ‘भाषा ठीक करने से पहले आदमी को ठीक’ करना चाहते थे। वे भाषा में, आदमी होने की तमीज ढूंढ़ रहे थे। ‘भूख और भाषा में सही दूरी’ न देख पाने वालों के मनुष्य होने पर वे आपत्ति करते थे। भूख सबसे पहले ‘भाषा को खा’ जाती है। अभिप्राय यह कि ‘भूख’ मनुष्य को कई तरह से मजबूर करती है। मजबूरी में भाषा बदलने में देर नहीं लगती। धूमिल के समय की भूख निश्चय ‘भाषा को खा’ जाती होगी; लोग विरोध त्यागने को मजबूर हो जाते होंगे। पर आज के नागरिक की तो अपनी कोई भाषा ही नहीं है। ०