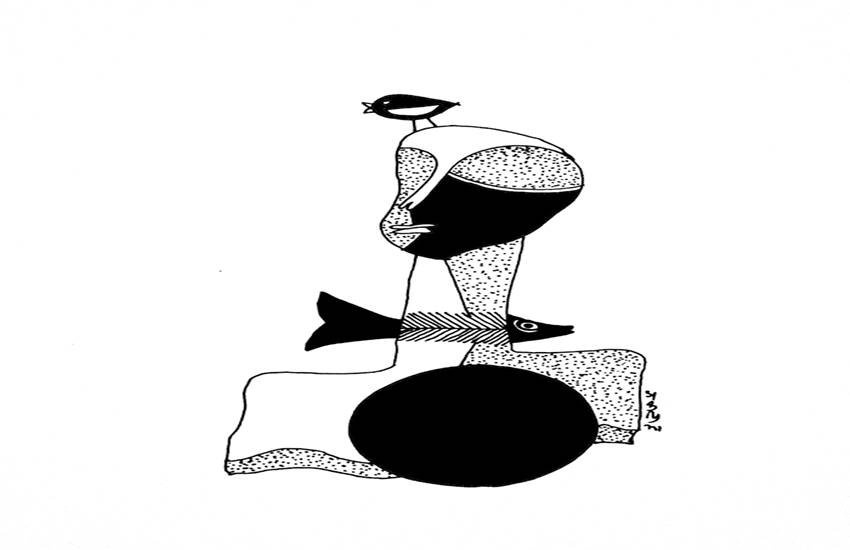राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया प्रारूप अब लोक-संवाद और तमाम शिक्षाविदों, बौद्धिकों और पेशेवर शिक्षकों के विचार-विमर्श के लिए जारी तो हो गया है, लेकिन उसके गुण-दोषों पर अच्छी चर्चा और प्रारूप में नीति के बजाय, राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा ही पहले भी हुआ था, जब तत्कालीन नीति को शिक्षा के तालिबानीकरण की संज्ञा दी गई थी।
अब प्रश्न है कि शिक्षा चाहे सरकारी स्कूल, कॉलेजों में दी जाए या मदरसों, शिशु मंदिरों में, क्या शिक्षा की कोई जाति या धर्म है? क्या शिक्षा कोई क्षेत्र-विशेष की राष्ट्र भाषा, राजभाषा या किसी विचारधारा का नाम है? शिक्षा के तो कई रूपक हैं। अंग्रेजी में एक पुस्तक भी है ‘मेटाफर्स आॅफ एजुकेशन’। हम इन रूपकों से शिक्षा का रूप निर्धारित करने के बजाय पार्टीवादी राजनीति क्यों करते हैं? सरकार किसी भी दल, किसी भी विचारधारा की हो, अच्छे को अच्छा कहने और खराब को खराब कहने का दल-निरपेक्ष बौद्धिक साहस हमारे अंदर क्यों नहीं? हमारी आंखों में जो दलवादी मोतियाबिंद है, उस जाले को साफ करना, शिक्षा की पहली जरूरत है। आमतौर पर शिक्षा के दो क्षेत्र माने गए हैं- एक है स्थानीय, जिसे लोकल या लोकेशन आधारित कहा गया है और दूसरा है ग्लोबल यानी लोकव्यापी, सर्वव्यापी या विश्वव्यापी। जैसे गांधी के लिए शिक्षा के मूल्य थे- सत्य और अहिंसा। दुनिया की कोई शिक्षा नीति सत्य और अहिंसा के मूल्य को निरस्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये ‘इटर्नल’ या सार्वकालिक मूल्य माने गए हैं। कुछ शिक्षाविद मानते हैं कि सार्वकालिक मूल्य कुछ नहीं होते। प्रत्येक मूल्य मनुष्य की चेतना, परिवेश, विचार और उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश जैसे मूल्य मनुष्य के विरुद्ध मनुष्य को क्रूर बनाने के बजाय, उसकी संवेदना को जाग्रत कर सकते हैं। आक्रोश हो तो अवश्य लेकिन अहिंसक हो, विरोध हो जरूर मगर सविनय अवज्ञा की तरह हो, असहमति हो मगर असहयोग आंदोलन की तरह हो।
शिक्षा के कितने भी विचार-संस्करण बना लिए जाएं, अगर मनुष्य की चेतना का संवेदन-तंत्र शिक्षा से स्पंदित नहीं होता, मनुष्य में बेहतर मनुष्य बनने, शिक्षक में बेहतर शिक्षक बनने और संस्थाओं को बेहतर, लोकतांत्रिक, उदार और बेहतर-संसाधनों से युक्त होकर तैयार नहीं करता, तो वह शिक्षा उन मूल्यों का निर्माण कैसे करेगी, जो सैकड़ों की संख्या में लिखे गए हैं और राष्ट्रीय संस्थाओं में मूल्य-शिक्षा विभाग ही रच दिए गए हैं? वास्तव में सच पूछा जाए, तो हमारी शिक्षा ने हमें ईमानदार न तो स्वयं के प्रति बनाया, न अपने विचारों के प्रति, न नीतियों के प्रति और न अपने काम के प्रति। जब लाख-दो लाख का प्रतिमाह वेतन पाने वाले प्राध्यापक कक्षाओं में नहीं जाते, न स्वयं पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, तो ऐसे प्राध्यापक शिक्षा के मूल्यों की चेतना कैसे जाग्रत करेंगे? अपनी बेईमानी से ईमानदार पीढ़ी का निर्माण कैसे करेंगे? ऐसे भी कुलपति देखे गए हैं, जो अपने विश्वविद्यालयों से गायब रह कर नैक, नेट, यूजीसी आदि के कामों से कमाऊ दौरे करते रहते हैं। क्या ऐसी आचरण-संहिता नहीं हो सकती कि कुलपति, प्राध्यापक अपने विश्वविद्यालय में रहें और अन्य कार्यों, निरीक्षण आदि के लिए पूर्णकालिक घुमंतू शिक्षाविद या विशेषज्ञ मूल्यांकन-कर्ता रखे जाएं? जब कुलपति, प्राध्यापक ही गैरहाजिर रहेंगे, तो छात्रों से हाजिर रहने की उम्मीद कैसे की जाएं?मूल्यों के कागजी पिटारे बनाने से क्या होगा? संस्कृति, सभ्यता के भग्नावशेषों में भटकाने से क्या होगा? विचारधाराओं के कंबल ओढ़ कर शिक्षा की ठंडक भगाने से भी क्या होगा! शिक्षा से तो पैदा होना चाहिए मनुष्य का आत्मविश्वास, अपनी शक्ति और हुनर से रोजगार पैदा कर लेने की बौद्धिक क्षमता और मनुष्य से मनुष्य के संवेदनशील संपर्क और संबंध। शिक्षा संस्थाओं में जितनी शिक्षा दी जाती है, उससे अधिक तो बाहरी वातावरण, घर, परिवार, परिवेश और अनुभव से सीखा जाता है। अगर हमारे पुरखे अपने गणित-ज्ञान से खगोल खंगाल कर पंचांग रच गए, तो उनके आगे का काम ही तो विज्ञान ने किया। शिक्षाशास्त्र ऐसा क्यों न हो कि वह जोे पहले था वह कितना सही, गलत, विश्वसनीय-अविश्वसनीय और शोधपरक था, उसका सही विश्लेषण हो सके और आगे के लिए ऐसे उपकरण तैयार हो सकें, जिनसे लगे कि शिक्षा का अर्थ केवल संस्कृति के कुंज में विहार करना नहीं, बल्कि विज्ञान के विवेक-विमान पर उड़ कर आसमान छूना भी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने का दायित्व जिन संस्थाओं को दिया जाता है, वे भी दुराग्रह से ग्रस्त होती हैं। अगर किसी संस्था प्रमुख को किसी विचारधारा विशेष के कोष्ठक में बंद करके काम करवाना होता है, तो उसी विचारधारा के तथाकथित शिक्षाविद, शिक्षक, विचारक, बौद्धिक नीति-निर्धारक और पाठ्यक्रम लेखक के रूप में बुलाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय संस्था के निदेशक ने अगर संस्था को इतना सक्रिय कर दिया कि मीडिया और अखबार में हर दिन वह संस्था हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बन गई, तो ऐसा निदेशक किसी प्रकार के पार्टीवादी खांचे में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वह कितना भी सक्रिय, ईमानदार और विचारधारा-निरपेक्ष रहा हो। जब उसका उत्तराधिकारी कोई तेजस्वी, विचारक और शिक्षाविद निदेशक बनता है, तो वह कितनी भी कल्पनाशील, बौद्धिक मेधा और क्षमता वाला हो, उसकी आस्था नीति के बजाय राजनीतिक विचारधारा से हो जाती है और उसके कार्यकाल में या तो पूर्व-निदेशक के समय के लोगों को निरस्त या बहिष्कृत कर दिया जाता है या फिर जातिगत समानता, परिचय, विचारधारागत समानता के आधार पर ही बुलाया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ऐसे लोग शिक्षाविद, बौद्धिक सक्रिय अध्यापक और कल्पनाशील, संवेदनशील, विशेषज्ञ नहीं होते, वे प्रखर होते हैं, जन-संवेदी होते हैं, मगर विचारधारा से मुक्त उदार, उदात्त और निरपेक्ष अपने को नहीं रख पाते।
ऐसा क्यों है? हम शिक्षा को लेकर राजनीति के बजाय नीति से संचालित क्यों नहीं होते, अपने-अपने विचार-विधान के बजाय संविधान से संचालित क्यों नहीं होते, धर्म के बजाय कर्म से संचालित क्यों नहीं होते, संस्कृति के नाम पर संप्रदायवाद की कट्टरता के बजाय लोकतंत्र के प्रति सच्ची आस्था से प्रेरित क्यों नहीं होते? सच पूछा जाए तो पश्चिमी विचारधाराओं और अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा का मॉडल हमारे अंदर इस कदर धंस गया है कि उसका हर विकल्प हमारे यहां विफल हो जाता है। राज्य स्तर पर स्थिति इतनी भयानक है कि वहां केवल विचारधारा भक्त ही शिक्षा नीति पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक का काम कर सकते हैं।
शिक्षा जिस दिन मुक्त विचारों का मानवीय संस्कार बनेगी उस दिन सरकार या राजनीति से नीति पैदा न होकर मनुष्यता की संस्कृति और संविधान की कृति से शिक्षा रची जाएगी और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, पाठ्यक्रम हो, पाठ्य-पुस्तक हो, उन्हें इजलास में मुल्जिम बन कर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि जन-विवेक के संवेदन की अदालत में राजनीतिक ओछेपन से मुक्त नीति शिक्षा का सच्चा कलेवर गांधी के स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वदेशी, सर्वत्रमय वर्जन और सत्य-अहिंसा की भारतीय भूमि पर खड़ी होगी। विज्ञान, तकनीकी, सूचनातंत्र, नए-नए उपकरण आदि के बावजूद शिक्षा को केवल यांत्रिक नहीं बनाया जा सकता। यह सही है कि नीति तो सरकार बनाती है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि सरकार अगर नीति को दलगत राजनीति से बनाती है, तो फिर ऐसी नीति में संविधान की सुगंध कैसे होगी? शिक्षा नीतियां, शिक्षा-आयोग पहले भी बने, कई बातें अच्छी भी थीं। यह भी सच है कि अंग्रेजों के मॉडल से पूरी तरह हटा नहीं जा सकता, मगर नीति में कम से कम मानवीय संवेदन और नैतिक दायित्व की झलक तो हो। नई नीति के प्रारूप पर अनेक शिक्षाविदों में मतभेद हैं, मगर क्या ये मतभेद नीति से हैं या नेताओं से यह विचार करना जरूरी है।