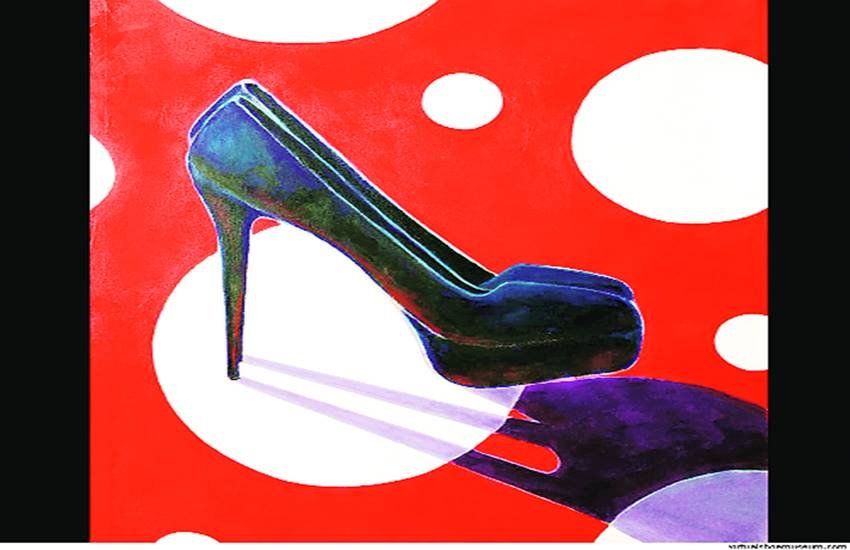कोरोना संक्रमण का संकट अभी बीता नहीं है पर इसको लेकर विमर्श के कई आधार जरूर तय हो गए हैं। इसमें सबसे अहम है महिलाओं के साथ सामाजिक व्यवहार और उन्हें लेकर समझ। दिलचस्प है कि इस महामारी के कारण तमाम बदलावों के बीच अगर कुछ पहले की तरह ही अपरिवर्तित है तो वह है लैंगिक दुराग्रह और अन्याय का अखिल संसार। अच्छी बात है कि इस अन्याय और दुराग्रह को तोड़ने का जिम्मा अब महिलाओं ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। मीटू आंदोलन की तर्ज पर पिछले साल जापान में ‘ड्रेसकोड’ में ऊंची हील वाली जूतियां पहनने के विरोध में आधी आबादी ने लैंगिक समानता का आंदोलन ‘कूटू’ छेड़ा था। दुनियाभर की आवाज बने इस अभियान का असर दिखने लगा है।
गौरतलब है कि जापान के दफ्तरों में महिलाओं के लिए ऊंची हील की जूतियां पहनना आवश्यक है। बीते साल जापान की अभिनेत्री और लेखिका यूमि इशिकावा ने ऊंची हील वाली जूतियां पहनने को बड़ी समस्या बताते हुए इसके खिलाफ ‘कूटू’ अभियान छेड़ने के साथ ही एक याचिका भी दायर की थी। इशिकावा ने 20 हजार लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका सरकार को सौंपते हुए कहा था कि ऊंची जूतियां पहनने को विवश करना एक लैंगिक भेदभाव है।
इस अभियान को एक बड़ी सफलता हाल ही में तब मिली जब जापान एअरलाइंस के लिए काम करने वाली महिला फ्लाइट सहायिका को हाई हील या स्कर्ट पहनने की बाध्यता से आजादी मिल गई। एअरलाइन ने इसे जापान में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे ‘कूटू’ आंदोलन के लिए एक बड़ी जीत बताया। ऐसा नहीं है कि जापान ही इकलौता देश है, जो अपनी महिला कर्मचारियों पर ‘ड्रेस कोड’ की बाध्यता लादता है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप की महिलाओं ने भी समय-समय पर कार्यस्थल पर ड्रेस कोड, मेकअप और ऊंची एड़ी की जूतियों की अनिवार्यता का विरोध किया है।
2016 में ब्रिटेन में ऊंची एड़ी वाली जूती को लेकर नौकरी से निकाले जाने के बाद निकोला थॉर्प नाम की महिला ने इसके खिलाफ अभियान चलाया था, उसकी याचिका को 50 हजार से भी ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर समर्थन दिया था। एक सर्वेक्षण के मुताबिक पहनावे से जुड़े बेतुके नियमों के चलते 12 फीसद लोग अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों के मामले में तो यह आंकड़ा 32 फीसद है।
आखिर आॅफिस ड्रेस कोड है क्या? विशेषकर जब बात महिलाओं के ड्रेस कोड की हो तो वे इसकी अमूर्त अवधारणा से यकीनन परेशान हैं। वे समझ ही नहीं पाती कि सही बिजनेस या आॅफिस ड्रेस क्या है। ऐसे में अचानक से किसी दिन उन्हें बताया जाता है कि आज आपका पहनावा कार्यालय के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। दरअसल, समस्या की जड़ महिलाओं के वस्त्रों को लेकर जुड़ी वह मानसिकता है, जो महिला का मानव से परे महज एक देह के रूप में देखने की इस कदर आदी हो चुकी है कि उसके आगे उसकी सुरक्षा, प्रतिभा और इच्छाएं सब बौनी हैं। यह विद्रूपता नहीं तो क्या है कि आस्ट्रेलिया की टेलीविजन एंकर कार्ल स्टीफेनोविक ने एक वर्ष तक एक जैसा नीला सूट पहना लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।
वहीं दूसरी तरफ उनकी सहयोगी महिला एंकरों के पहनावे पर लगातार टीका-टिप्पणियां होती रहीं। हैरानी वाली बात तो यह है कि महिलाओं के पहनावे और ड्रेस कोड को लेकर संकुचित सोच का दायरा कॉरपोरेट जगत से लेकर अशिक्षित समाज में यथावत व्याप्त है। नहीं तो यह कैसे संभव होता कि जापान जैसे विकसित देश में महिलाओं के ड्रेस कोड में चश्मा न पहनने का नियम है। नवंबर 2019 में यह बात सामने आई कि कई कंपनियां महिला रिसेप्शनिस्ट के चश्मा पहनकर आने पर काम से लौटा रही हंै जबकि पुुरुष कर्मचारियों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। निजी कंपनियों का तर्क है कि चश्मे से महिलाओं की सुंदरता प्रभावित होती है। यह नियम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से विश्व भर में कायम है।
बात सिर्फ कार्यस्थल तक ही सीमित नहीं है। स्कूल, घर, बाजार हर जगह यहां तक कि संसद भी महिलाओं के वस्त्रों से उनके चरित्र का आकलन करती दिखाई देती है। अमेरिका में सीनेट के हाउस चैंबर में दो वर्ष पूर्व एक महिला रिपोर्टर को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उसने स्लीवलेस कपड़े पहने थे। इस घटना के बाद वहां ड्रेस कोड पर विवाद छिड़ गया था। सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी की सांसद मार्थ मेंकसेली ने इसका तीस सांसदों के साथ विरोध किया।
विश्व में शायद ही कोई देश होगा, जहां महिलाओं के पहनावे को लेकर मापदंड तय न किए गए हों। दरअसल पूरी दुनिया महिलाओं के वस्त्रों को लेकर दो धड़ों में बंटी हुई है। एक ओर ऐसे परिधान की पैरवी, जहां स्त्री काया के प्रत्येक कोण को नापा जा सके और दूसरी ओर ऐसा परिधान जहां सिर्फ आंखें ही दिखाई दें। फ्रांस में मुसलिम औरतें शरीर को ढकने वाली तौराकी पोशाक पहनने के अधिकार से वंचित हैं तो वहीं ईरान में महिलाओं ने जबरदस्ती हिजाब पहनने के सरकारी नियमों के खिलाफ संघर्ष किया। 2018 में सऊदी अरब में महिलाओं ने बुर्के के खिलाफ सोशल मीडिया पर विरोध जाहिर किया। उन्होंने यह कहकर अपना विरोध जताया कि वे इसे उलटा पहनेंगी। बड़ी तादाद में महिलाओं ने ट्विटर पर ‘इनसाइट आऊट अबाया’ के तहत बुर्के की तस्वीर पोस्ट की, जिन्हें पहनने में वे दवाब महसूस करती रही हैं।
महिलाओं के वस्त्रों का इतिहास भी यह गवाही देता है कि सदियों से महिलाओं के कपड़े समाज निर्धारित करता रहा है। 1840 के आसपास का समय आधुनिक फैशन का माना जाता है। तब से लेकर आज तक फैशन डिजाइनर महिलाओं के लिए उनकी सुविधा के बजाय उनके शरीर के अंगों को उभारने वाले वस्त्र बना रहे हैं। समय के साथ फैशन की यह परंपरा इस कदर लाद दी गई कि आज इसके विरोध में आवाज उठने लगी है।
‘गिव अस पॉकेट’ अभियान ने बीते सालों में यूरोपीय देशों में दस्तक दी है। महिलाओं का अपनी पोशाक में जेब पाने का यह अभियान भले ही फैशन जगत को हास्यास्पद लग रहा है पर इस सोच के पीछे, बिना किसी बोझ के स्वतंत्रता और देह से परे महिलाओं के परिधान तैयार करने की दलील है। इन तमाम विरोधों के बाद भी महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक सोच में सहजता से बदलाव संभव नहीं है। इसका जीवंत उदाहरण ताजिकिस्तान है, जिसने सात साल से लेकर 70 साल की महिलाओं के लिए ड्रेस कोड तय किया है और इसके लिए किताब जारी की है।
सुखद है कि बदलाव के बयार के बीच महिला पहनावों को लेकर भी रूढ़ताएं तेजी से टूट रही हैं। पहनावे की परंपरागत अवधारणाओं को बदलने और लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के 120 निजी स्कूलों में ‘जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म पॉलिसी’ लागू की गई, जिसका उद्देश्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना व्यक्तित्व और यूनिफॉर्म चुनने का अधिकार देना है। इस लिहाज से भारत थोड़ी सुप्त स्थिति में है।
मुजफ्फरनगर के दुधाहांडी गांव में जींस की होली जलाने से लेकर 2016 में तिरुवनंतपुरुम के मेडिकल कॉलेज में लेगिन्स, स्कर्ट पर प्रतिबंध के बाद बीते वर्ष हैदराबाद में लड़कियों के लिए सेंट फ्रांसिस कॉलेज में प्रशासन द्वारा छात्राओं की आस्तीन की बांहों की लंबाई तथा कुर्तियों की घुटने से नीचे तक की लंबाई निर्धारित करने जैसे अनेक उदाहरण हैं जो महिला सशक्तीकरण की अवधारणा पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वस्त्र व्यक्ति की सौम्यता को प्रकट करते है परंतु इसके आधार पर उसके चरित्र और प्रस्थिति का आकलन अनुचित ही नहीं अपितु उसे उसके मानवीय अधिकारों से वंचित करना भी है। ल्ल