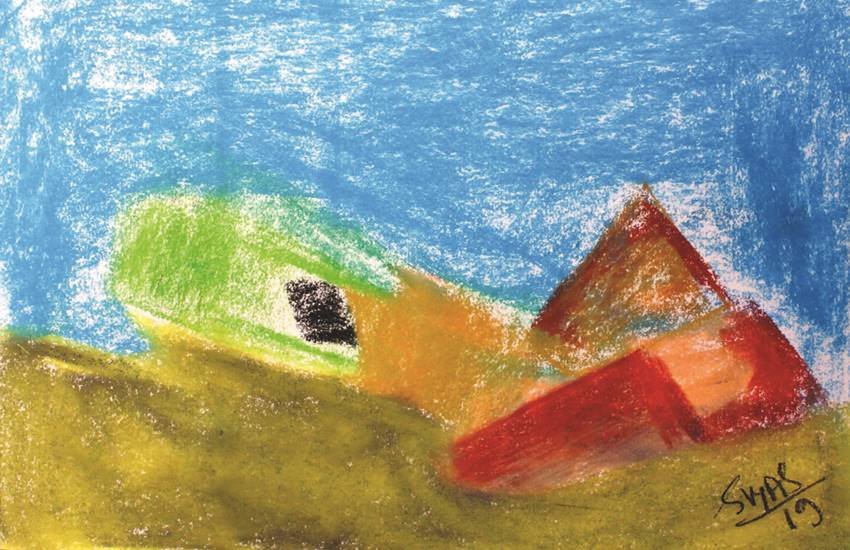पंकज पराशर
जिस भक्तिकाल में सत्ता और संत कवियों के बीच की दूरी को बताने के लिए प्राय: मध्यकालीन संत कवि कुंभनदास की बहुचर्चित काव्य-पंक्ति, ‘संतन को कहा सीकरी सों काम/ आवत जात पनहियां टूटी, बिसरि गयो हरि नाम’ को उद्धृत किया जाता है, वे संत कवि क्या वाकई सत्ता और व्यवस्था से इतने दूर रहते थे कि उनका हर पल हरि नाम के स्मरण में ही बीतता था? क्या वे भक्ति और ईश्वर की आराधना में इतने लीन रहा करते थे कि राजदरबार, सेना, युद्ध, खेल-कूद और सत्ता-व्यवस्था के पचड़ों की उन्हें कोई खबर ही नहीं रहती थी? जबकि सारे संत कवि इसी हिंदी समाज के निवासी थे, ईश्वर भजन के लिए हिमालय की कंदराओं-गुफाओं में रहने के लिए नहीं गए थे। तब यह भला कैसे संभव है कि सत्ता और समाज ने उनकी भाषा, सोच और दैनंदिन को प्रभावित न किया हो? भक्तिकाल के संत कवियों को लेकर विद्वानों ने कहा है कि उन्होंने लौकिक सत्ता की जगह ईश्वरीय सत्ता को माना और दरबारी कवि बन कर अपना इहलोक सुधारने की जगह त्यागी और वैरागी बन कर परलोक सुधारने की चिंता को ज्यादा श्रेयस्कर समझा।
भक्तिकाल के उदय से लेकर उसके सामाजिक आधारों तक पर विशुद्ध इतिहास से लेकर हिंदी आलोचना के विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है। पर इतिहास में पैठने के बाद जब इतिहास में भाषा और इतिहास की भाषा में छिपे हुए अनकहे इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं, तो बेहद रोचक चीजें निकल कर सामने आती हैं। कविता के स्रोतों का अध्ययन समाज के अध्ययन का ही अंग है। कला को कला के भीतर से नहीं, बल्कि उसके बाहर से (यानी समाज के भीतर से) देखना चाहिए। कला या साहित्य की आलोचना शुद्ध सर्जना या शुद्ध रसास्वादन से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें एक समाजशास्त्रीय तत्त्व निहित होता है। समाज की आलोचना और सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों पर चोट के संदर्भ में प्राय: कबीर की चर्चा की जाती है, बावजूद इसके कि कबीर पर भी संत कवि के दायरे में विचार किया जाता है, लेकिन तुलसीदास ने तो राम से बड़ा किसी और न मान कर और तत्कालीन मुगल दरबार से सर्वथा अलग रह कर भी दरबार, युद्ध और अन्य सामाजिक गतिविधियों को गहराई से देखा-समझा था। फारसी उस समय राजकाज की भाषा थी। जैसे आजकल राजकाज और प्रशासन से जुड़ी अंगरेजी के बहुत सारे शब्द हमारी समाज-भाषा में इस कदर घुल-मिल गए हैं कि निरक्षर लोग भी अनेक शब्दों का सहज की प्रयोग करते हैं। उसी तरह मध्यकालीन भारतीय समाज में दरबारी और प्रशासनिक शब्दों का जनता की भाषा में सहजता से घुल-मिल जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। दूसरी बात कि जनभाषा के आग्रही जिन तुलसी ने संस्कृत भाषा का अगाध पांडित्य के बावजूद लोकभाषा अवधी को अपनी कविताई के लिए चुना था, उन तुलसी की भाषा कृत्रिम और लोक की रंगो-बू से सर्वथा अलग कैसे हो सकती थी? तुलसी के काव्य में प्रयुक्त अरबी-फारसी-तुर्की के शब्द इसलिए आए हैं कि वे लोकभाषा में लिख रहे थे और तत्कालीन लोकभाषा में तत्कालीन शासन-प्रशासन से जुड़े विदेशज शब्द घुल-मिल कर खांटी देशज शब्द की तरह हो चुके थे। सत्ता की भाषा और उसकी शब्दावली के प्रयोग के माध्यम से उन्हें सत्ताधीशों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं थी।
आज भी फौज की तकनीकी शब्दावली से अपरिचित लोग प्राय: इस बात से परिचित नहीं होंगे कि फौज के सिपाही जहां रहते हैं, उस विशेष स्थान को क्या कहते हैं? मगर संत कवि तुलसी कहते हैं, ‘दीजै भगति बांह बैरक ज्यों सुबस बसै अब खेरो’ (विनयपत्रिका) यानी सिपाही ‘बैरक’ में रहते हैं। मुगलकालीन सत्ता संरचना में वजीर के साथ दीवान का ओहदा काफी अहम माना जाता था और अकबर के समय में ‘दीवान-ए-आला’, ‘दीवान-ए-सूबा’, ‘दीवान-ए-खालेसा’, ‘दीवान-ए- फौजदारी’ और ‘दीवान-ए-सरफे-खास’ जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण पद थे। इसी तरह तुलसी ने एक दिलचस्प प्रशासनिक शब्द ‘सरखत’ का प्रयोग किया है। सरखत दरअसल वह पत्र, था जो सरकारी कर्मचारी को पहले दिन लिखा जाता था और जितना भी द्रव्य उसे दिया जाता था उसी पर वसूल किया जाता था। इस शब्द के ‘आईन-ए-अकबरी’ में मिले संदर्भ के अनुसार सरखत जागीर प्रदान करने का एक फरमानचा था, जिसे ‘फरमाने-सब्त’ कहते थे। यह सरखत प्रधान बख्शी ‘तालिका’ के बदले में देता था और फिर यही सरखत बादशाह की सेवा में भेजा जाता था। इसी प्रकार तुलसी ने ‘मंसबदार’ शब्द का प्रयोग किया है। मुगलकाल में ‘मंसब’ दरअसल एक ओहदा या कहें रैंक होता था, जिस पद पर आसीन अधिकारी को ‘मंसबदार’ कहते थे। अबुल फजल के मुताबिक तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर के युग में सबसे बड़े मंसबदार शहजादा सलीम थे, जिन्हें दस हजार का मंसब मिला हुआ था। शहजादा मुराद को आठ हजार और शहजादा दानियाल को सात हजार का मंसब प्राप्त था। उस समय के चार सौ पंद्रह मंसबदारों में इक्यावन मंसबदार हिंदू थे।
‘तुपक’, ‘तोपची’ और ‘दारू’ यानी बारूद (काल तोपची तुपक महि दारू अनय कराल)। तुपक तथा तोपची शब्द फारसी भाषा से तुर्की में आए हुए हैं। तुपक तोप को कहते हैं और तोपची तोप चलाने वाले को कहा जाता है। कालांतर में आमजन के बीच तुपक से अधिक तोप शब्द प्रचलित हुआ और फारसी में इसका थोडा-सा अलग रूप तुपक की जगह ‘तुफंग’ प्रचलित हुआ। तुपक तथा तोप शब्द का प्रयोग भक्तिकाल के अनेक कवियों ने किया है और इस शब्द के प्रयोग के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। मसलन, पहले सिख गुरु, गुरु नानक कहते हैं, ‘कोटिन तुपक करोरन बाना सहसन अजगर चलै कमाना’ और ‘वीर चरित्र’ में केशवदास कहते हैं, ‘तुफ सर छुट्टहिं तरुबर टुट्टहिं फुट्ठहिं काय कवच्च घने’। ‘पलीता’ और ‘गोला’ (‘पाप पलीता कठिन गुरु गोला पुहुमी पाल’- तुलसी और ‘प्रेम पलीता सुरति नालि करि, गोला ज्ञान चलाया’-कबीर), ‘तरकस’ और ‘तीर’ (तन तरकस से जात है सांस सरीखे तीर’), ‘कमान’ (बान कमान निषंग कसें), ‘सीपर’ (लागति सांगि बिभीषन पर सीपर आपु भए हैं), ‘ताजी’ (पारावत मराल सब ताजी), ‘पील’ (पील-उद्धरन सील सिंधु ढील देखियत), ‘कोतल’ (कोतल सग जाहिं डोरिआए), ‘जीन’ (रुचि-रुचि जीन तुरंग तिन्ह साजे) और ‘जंजीर’ (झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जरे मद अंबु चुचाते)। तुलसी के काव्य में प्रयुक्त ये तमाम शब्द इस बात की तस्दीक करते हैं कि मध्यकालीन भारतीय समाज में फौज, युद्ध, सेना और हथियार से जुड़े हुए तमाम शब्द आम चलन में थे, क्योंकि इससे यह भी ध्वनित होता है कि युद्ध के बादल मध्ययुगीन समाज में बराबर छाए रहते थे।
एक शब्द है ‘शहर’ (बूझिए न ऐसी गति संकर सहर की) और जब आप शहर जाएंगे तो कुछ खरीदते हुए ‘दाम’ (करम जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधिन दाम को) तो चुकाएंगे ही। प्रशासन से जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द, जो तुलसी के काव्य में भी उसी तरह प्रयुक्त हुआ है, वह शब्द है ‘कोतवाल’ (कालनाथ कोतवाल दंड करि दंडपानि सभासद गनत से अनित अनूप), जिसके मूल उत्स के बारे में मध्यकालीन काव्य-भाषा के मर्मज्ञ विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि ‘कोट्टपाल’ संस्था का आविर्भाव हर्ष के समय में ही हो गया था। तुलसी के काव्य में बादशाह की सेना, युद्धास्त्र आदि के बारे में अनेक शब्द मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें तत्कालीन शासक के शस्त्रागार और लश्कर को देखने का अवसर अवश्य मिला होगा, वरना इस क्षेत्र से संबंधित उनकी शब्दावली इतनी समृद्ध न होती। उदाहरण के लिए देखें, ‘फौज’ (हहरानी फौजें महरानी जातुधान की) शब्द का प्रयोग तुलसी ने एकवचन फौज तथा बहुवचन फौजें दोनों ही रूपों में किया है। फौज दरअसल अरबी भाषा का शब्द है, जो सेना के लिए प्रयुक्त होता है। इसी शब्द में ‘दार’ जोड़ कर ‘फौजदार’ शब्द बनाता है, जिसका सुंदर प्रयोग केशवदास ने किया है, ‘फोजदार सिकदार सूर सरदार सहायक’। इन क्षेत्रों के अलावा तुलसी सहित भक्तिकाल के अनेक कवियों के काव्य में तत्कालीन वाद्य यंत्र, खेल-कूद, व्यवसाय, व्यवसायी तथा कला-कौशल से संबंधित क्षेत्रों की शब्दावली का इस्तेमाल भी भरपूर हुआ है।