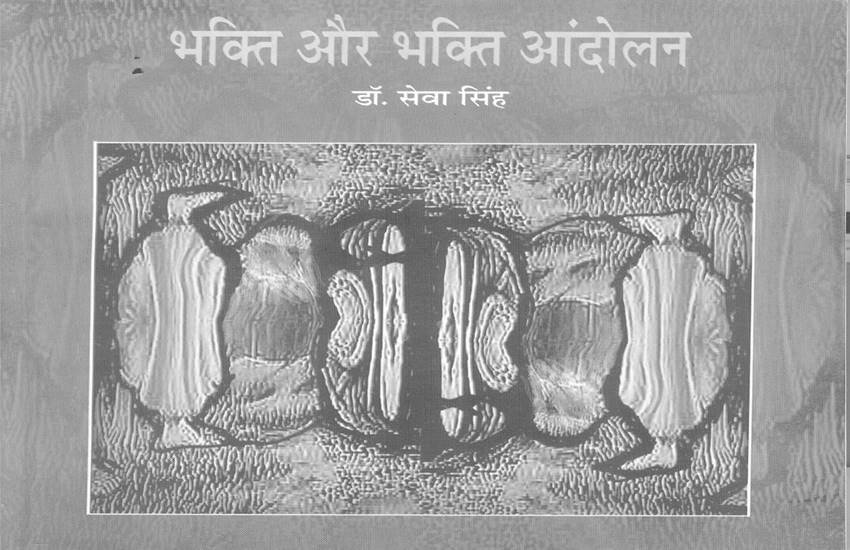मैं जब तक आई बाहर
मैं क्यों कहूंगी तुम से/ अब और नहीं/ सहा जाता/ मेरे ईश्वर’- गगन गिल की ये काव्य-पंक्तियां किसी निजी पीड़ा की ही अभिव्यक्ति हैं या हमारे समय के दर्द का अहसास भी? और जब यह पीड़ा अपने पाठक को संवेदित करने लगती है तो क्या वह अभिव्यक्ति प्रकारांतर से प्रतिरोध की ऐसी कविता नहीं हो जाती, जिसमें ‘दर्दे-तन्हा’ और ‘गमे-जमाना’ का कथित भेद मिट कर ‘दर्दे-इनसान’ हो जाता है? कविता इसी तरह इतिहास अर्थात समय का काव्यांतरण संभव करने की ओर उन्मुख होती है। गगन गिल की इन आत्मपरक-सी लगती कविताओं के वैशिष्ट्य को पहचानने के लिए मुक्तिबोध के इस कथन का स्मरण करना उपयोगी हो सकता है कि कविता के संदर्भ ‘काव्य से व्यक्त भाव या भावना के भीतर से भी दीपित और ज्योतित’ होते हैं, उनका स्थूल संकेत या भाव-प्रसंगों या वस्तु-तथ्यों का विवरण आवश्यक नहीं है। इन कविताओं का अनूठापन इस बात में है कि वे एक ऐसी भाषा की खोज करती हैं, जिसमें सतह पर दिखता हलका-सा स्पंदन अपने भीतर के सारे तनावों-दबावों को समेटे होता है- बांध पर एकत्रित जलराशि की तरह। यह भी कह सकते हैं कि ये कविताएं प्रार्थना के नए-से शिल्प में प्रतिरोध की कविताएं हैं- प्रतिरोध उस हर सत्ता-रूप के सम्मुख जो मानवत्व मात्र पर- स्त्रीत्व पर भी- आघात करता है। इन आघातों का दर्द अपने एकांत में सहने पर ही कवि-मन पहचान पाता है कि ‘मैं जब तक आई बाहर/ एकांत से अपने/ बदल चुका था मर्म भाषा का’। ये कविताएं काव्य-भाषा को उसकी मार्मिकता लौटाने की कोशिश कही जा सकती हैं।
मैं जब तक आई बाहर : गगन गिल, वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 199 रुपए।
भक्ति और भक्ति आंदोलन
भक्ति दरअसल एक ‘प्रतिक्रियावादी ज्ञानसत्तात्मक विचारधारा’ है, पर इसे इस रूप में देखने और व्याख्यायित करने से इसलिए परहेज किया जाता है, क्योंकि ऐसा करते ही हमारा भक्तिकाल की श्रेष्ठता के प्रति भावुक दृष्टिकोण अचानक अपनी जमीन खो देता है और वह जो एक भव्य उदात्त उत्तुंग प्रासाद की तरह दैवी आकाश में झांकता है और सामान्यजन के प्रति अपने गुरु प्रसाद के कोष खाली किया करता है, अचानक भरभरा कर गिरता दिखाई दे सकता है। तथापि ‘प्रच्छन्न’ होने की वजह से भक्ति में निहित बुद्धि-ज्ञान मूलक एवं भौतिक यथार्थ-मूलक विरोध-भाव एक अर्से तक अपने ‘प्रतिक्रियावादी चरित्र’ को प्रकट होने से रोके रखता है। ऐसा करने के लिए वह अपने इस विरोध-मूलक भाव को प्रवृत्ति पर प्रेम-समर्पण-करुणा-मृत्युभय-असुरक्षा-शरणागति, कातरता-दीनता-प्रार्थना-पुकार-जाप-कीर्तन जैसी भक्तिवादी व्यवहार-रीतियों का ‘आदर्शीकरण’ करता है। यह ज्ञान-विरोधी प्रतिक्रियावाद उसी शांकर अद्वैत में प्रच्छन्न रूप से मौजूद है, जो यथार्थ को मिथ्या और ब्रह्म को एकमात्र सत्य साबित करने के लिए बौद्धों के शून्यवाद की ‘विवर्तवादी व्याख्या’ करता है। पर इस अद्वैत अनुभववाद के पैर चूंकि यथार्थ की जमीन के मिथ्या होने से अधर में लटक जाते हैं, अत: इसे भक्तिवादी भाववाद की मदद से अनुभवगम्य बनाया जाता है।
तब हिंदी की भक्तिधारा के नव-मूल्यांकन के लिए हमारे पास आधार क्या बचता है? नाथ-सिद्ध परंपरा वाले और सूफीवादी आधार वाले काव्य को अगर हम अलहदा रख देते हैं, जो कायदे से होना चाहिए, तो हमारे पास बचता है प्रतिक्रियावादी भक्तिवाद, जिसे हिंदी के स्वर्णकाल की जमीन की तरह देखना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, तथापि दिक्कत वाली बात दूसरी है। हम कहने को तो उत्तर-औपनिवेशिक दौर में प्रविष्ट हो गए हैं, पर अपनी भक्तिवादी विरासत को लेकर हमारे भावुक दृष्टिकोण अभी कायम हैं। अपने इतिहास पर छाई धुंध से बाहर आए बिना यह संभव नहीं कि हम कदम आगे बढ़ा सकें। पूरी उम्मीद है कि इस संदर्भ में सेवा सिंह की ‘भक्ति और भक्ति आंदोलन’ जैसी पुस्तकें हमारी सभी दृष्टियों का हमसफर अवश्य हो सकेंगी।
भक्ति और भक्ति आंदोलन : सेवा सिंह; आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, एससीएफ 267, सेक्टर-16, पंचकूला; 250 रुपए।