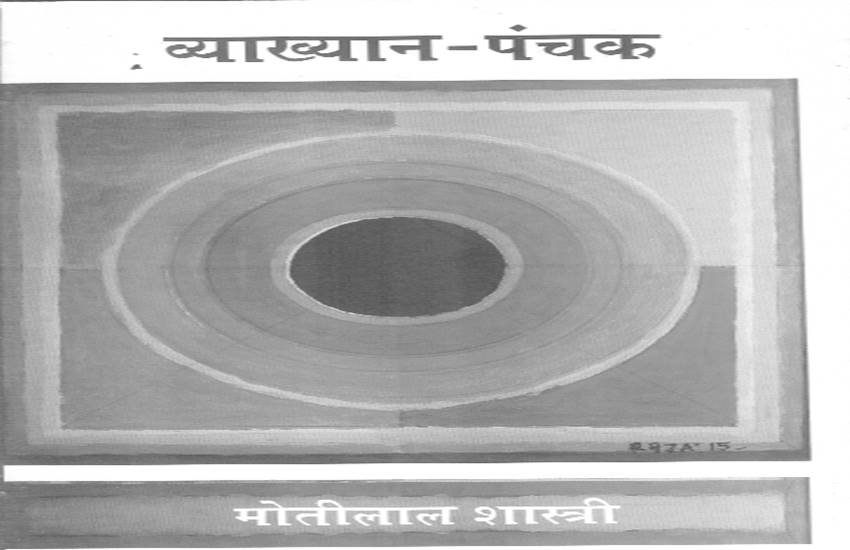आलोचना के परिसर
हिंदी आलोचना में प्राय: दो तरह की धाराएं दिखती हैं। एक, प्रगतिवादी और दूसरी प्रगतिवाद से मुठभेड़ करती। इन दोनों धाराओं के बीच बहुत कुछ वैचारिक गर्दो-गुबार भी है। प्रगतिवादी अलोचना ने निस्संदेह साहित्य को कुछ नए मूल्यों पर विचार करने का अवसर दिया, पर उसके प्रतिपक्ष में खड़ी हुई अलोचना ने भारतीय संदर्भों को नए सिरे से व्याख्यायित करने की दृष्टि विकसित की। दोनों धाराओं का संघर्ष चलता रहता है। पर गोपेश्वर सिंह इन दोनों के बीच से कुछ नए रास्ते निकालने का प्रयास करते रहे हैं। वे बार-बार दोनों दृष्टियों को आमने-सामने रख कर परीक्षा करते और उनके बिंदुओं को प्रश्नांकित करते हैं। इस क्रम में उनके लिए जो सबसे कारगर औजार नजर आते हैं वे हैं गांधी-विचार, जिनके जरिए वे साहित्य, समाज और राजनीति की विभिन्न प्रवृत्तियों को उलट-पलट कर परखने का प्रयास करते हैं। उनकी इस नई किताब में उन्हीं प्रयासों के तहत लिखे वैचारिक निबंध संकलित हैं।
यह किताब तीन खंडों में विभाजित है- कवि और कविता, हिंदी गद्य के विविध रंग तथा आलोचना और कविता। कविता वाले खंड में वे भक्ति काव्य से लेकर प्रगतिवादी-प्रयोगवादी कविता की परख तो करते ही हैं, कविता के राजनीतिक रुझान पर भी दृष्टि डालते हैं। वे कविता में तात्कालिकता की जगह तय करने का प्रयास करते हैं, तो जनांदोलनों में भी उसकी निशानदेही करते हैं। फिर सवाल खड़ा करते हैं कि गीत को देशनिकाला क्यों दे दिया गया, जबकि जीवन में गीत की भरपूर उपस्थिति है। इसी तरह गद्य वाले खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा आदि के अलोचनात्मक अवदान पर बात करते हैं, तो आलोचना की साख पर भी सवाल उठाते हैं। इसके साथ ही प्रेमचंद से लेकर रेणु, मनोहर श्याम जोशी आदि के कथा-साहित्य की परख करते हैं। फिर अलोचना और समाज वाले खंड में उनकी राजनीतिक रुझान वाली टिप्पणियां हैं, जिनमें वे स्वतंत्रता को समझने-समझाने का प्रयास करते हैं, तो गांधी-विचार पर विस्तार से चर्चा करते हैं। फिर लोहिया को भी केंद्र में लाते हैं। पर इन टिप्पणियों में भी उनकी दृष्टि बार-बार साहित्य की तरफ जाती है। इस तरह वे विशुद्ध दलगत राजनीति से ग्रस्त टिप्पणियां बनने से बच जाती हैं। अच्छी बात यह है कि गोपेश्वर सिंह अलोचना करते हुए भी आलोचना के बोझिल शब्दों, गझिन पारिभाषिक शब्दावली और उसके अबूझ-धुधंले-उलझाऊ सैद्धांतिक औजारों का उपयोग नहीं करते। सामान्य बतकही और अधिक से अधिक कक्षा के व्याख्यानों की शैली में अपनी बात कहते हैं। इस तरह उनकी अलोचना सुगम और ग्राह्य बनी रहती है।
आलोचना के परिसर : गोपेश्वर सिंह; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 395 रुपए।
उसके साथ चाय का आखिरी कप

सुधांशु गुप्त की कहानियां हमारे आसपास, रोजमर्रा जिंदगी में बिखरी, बेतरतीब चीजों में से कुछ चमकदार, मूल्यवान तलाश लेती हैं। उन्हें झाड़-पोंछ कर तरतीब दे देती हैं और उन्हें देख कर आश्चर्य होता है कि अरे, यह ऐसे भी हो सकता है। आधुनिक संवेदना की खलबलाहट है उनकी कहानियों में। इसीलिए वे तमाम असुंदरताओं में से कुछ सुंदर तलाश लाते हैं या यों कहें कि असुंदरताओं को बड़े कौशल से वे सुंदर बना देते हैं। प्रेम उनके यहां तमाम विषम परिस्थितियों में भी जादुई ढंग से उपस्थित हो जाता है और फिर अनेक संभावनाएं रंग-बिरंगी तितलियों की तरह तिरने लगती हैं। बड़े सहज ढंग से अपनी बात कहते हुए भी भाषा के साथ खेलने का उनमें गजब का हुनर है। उनकी कहानियों में यथार्थ के समांतर एक नए यथार्थ की रचना होते हुए प्रतीत होती है। उनकी कहानियों में दुनिया के भीतर एक नई दुनिया निर्मित होती दिखाई देगी। वह हर कहानी में अपनी बात कहने के लिए कोई-न-कोई नई डिवाइस भी विकसित करते हैं। वे प्रायोजित विमर्शों के डिजाइनर कहानीकार नहीं हैं। उनके लिए कहानी एक उत्पाद नहीं है और इसीलिए उनकी कहानियां बिलकुल अलग आस्वाद की कहानियां हैं। इन्हें सही रूप में समझने के लिए पाठक को घटनाओं, परिस्थितियों से अलग उनके व्यक्ति और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को समझना होगा।
उसके साथ चाय का आखिरी कप : सुधांशु गुप्त; भावना प्रकाशन, 109-ए, पटपड़गंज, दिल्ली; 395 रुपए।
उस दौर से इस दौर तक
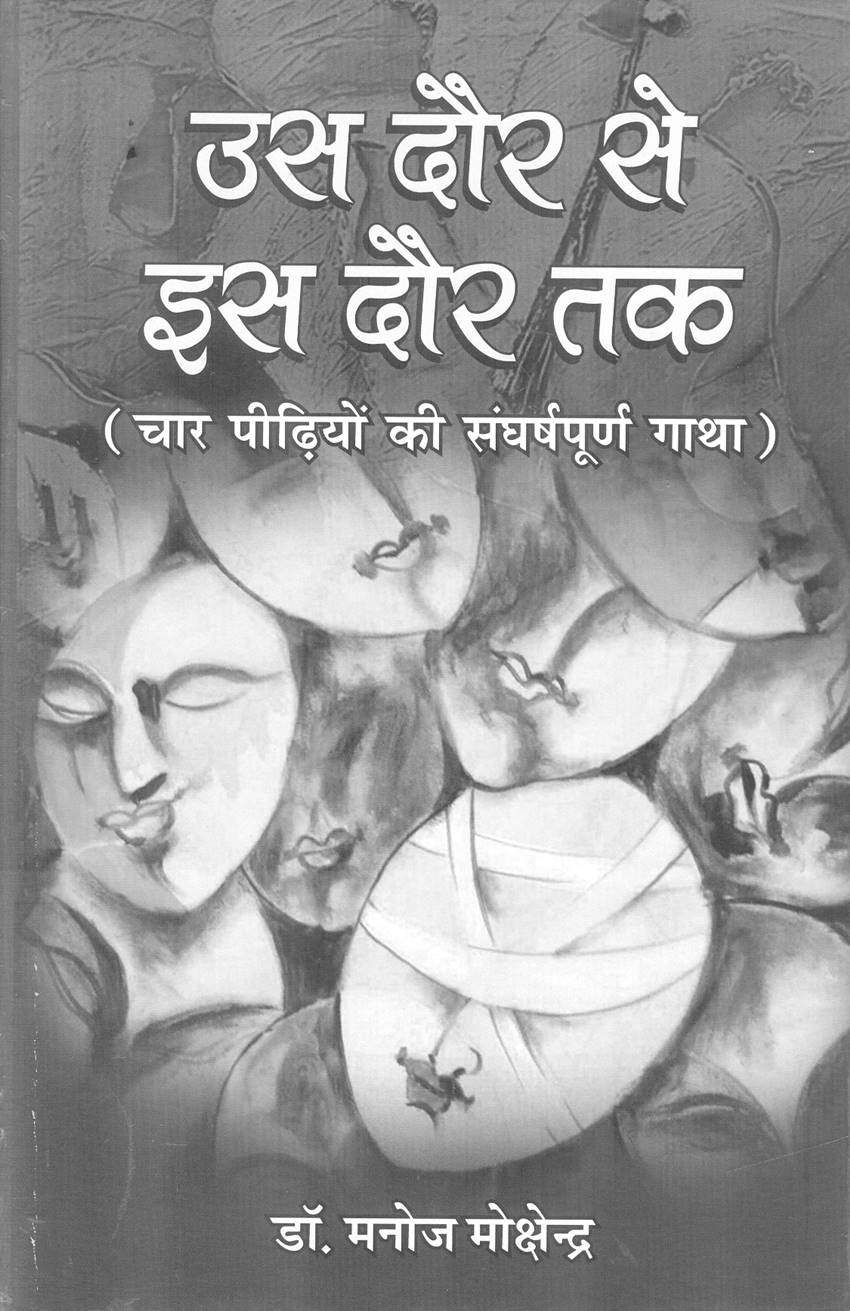
मनोज मोक्षेंद्र का यह उपन्यास जीवन को एक सामाजिक पर्व की तरह मनाता है। जेनरेशन कैप, पश्चिमी संस्कृति और व्यक्ति की नितांत आत्मकेंद्रितता के कारण उत्पन्न पारिवारिक जटिलताएं ही समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। हमारी आधुनिकताओं के चौरस्तों पर युवा हर कदम पर भटके हुए हैं और उनके इस भटकाव का खमियाजा उनकी पिछली पीढ़ी भुगत रही है। युवाओं द्वारा वृद्धों की उपेक्षा ने आयु से इन थके-मांदों का जीना मुहाल कर दिया है; पर मोक्षेंद्र वृद्धाश्रमों की पनाह में रह रहे ऐसे वृद्धों का मार्गदर्शन करते हैं। उपन्यास को आद्योपांत पढ़ते हुए एक विचार यह भी बनता है कि कहीं लेखक समाज की इस प्रयोगशाला में अत्याधुनिक समस्याओं को कठघरे में खड़ा करके किसी नई परंपरा का सूत्रपात तो करना नहीं चाहता है। क्योंकि वह उन फैशनों और चलनों से अत्यधिक डरा-सहमा हुआ है, जिनके नीचे असल आदमियत घुटती जा रही है। निस्संदेह, मानवता को तार-तार करने वाली नई-नई आदतों ने मनुष्य को कठपुतली बना डाला है। आज के मनुष्य की यह कैसी गुलामी है?
उस दौर से इस दौर तक : मनोज मोक्षेंद्र; राज पब्लिशिंग हाऊस, 9/5123, पुराना सीलमपुर (पूर्व), दिल्ली; 495 रुपए।
मंथन का सागर
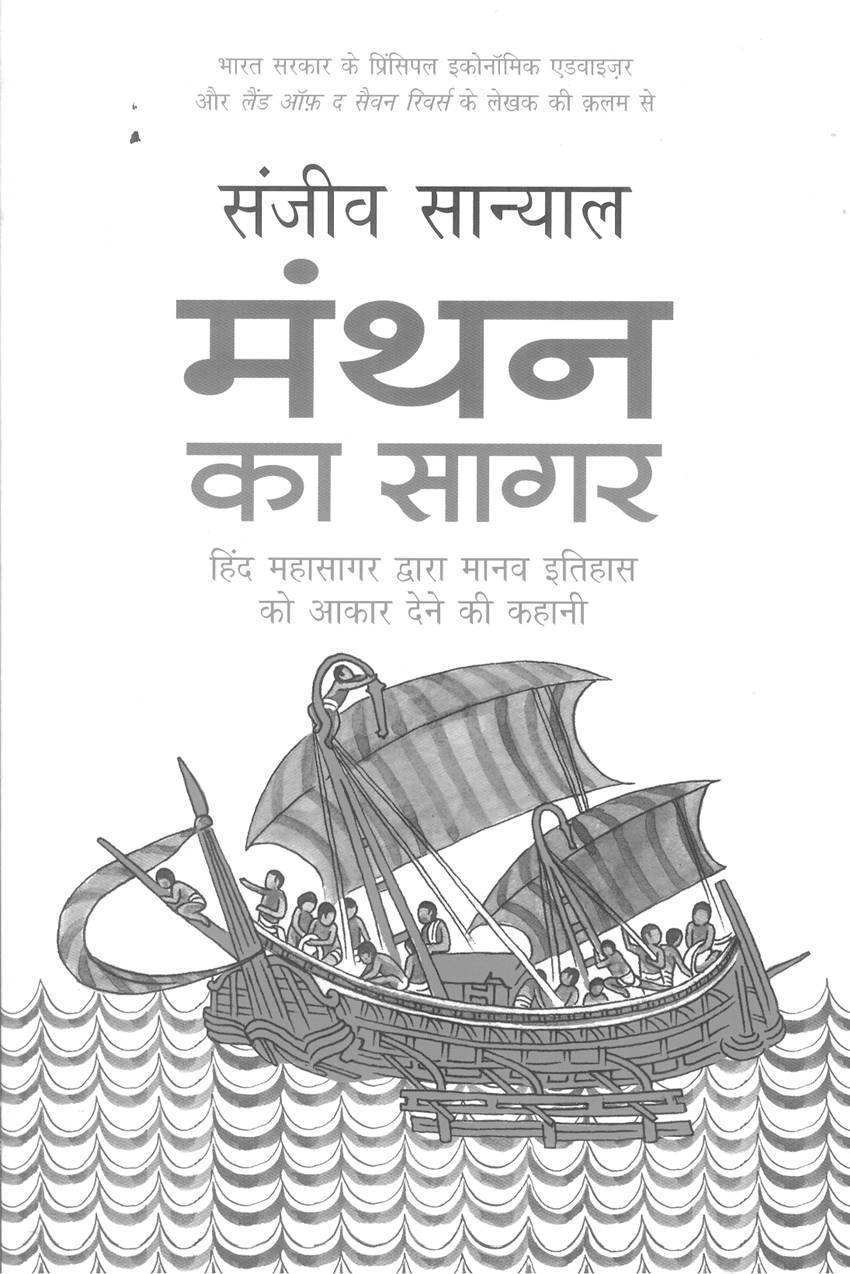
इस पुस्तक में संजीव सान्याल ने अंगकोरवाट और विजयनगर, मध्ययुगीन अरब साम्राज्यों और चीन के ‘खजाना बेड़े’ का समृद्ध, सजीव विवरण देते हुए पूर्वी अफ्रीका से लेकर आॅस्ट्रेलिया तक के युग-युगांतरकारी इतिहास को क्रमबद्ध किया है। आप नए साक्ष्यों के साथ दूर-दराज स्थित पुरातात्विक स्थलों, समुद्र-व्यापार नेटवर्कों और कुछ भूली-बिसरी मौखिक कहानियों को खंगालते हुए पूर्वस्थापित ऐतिहासिक कथानकों को चुनौती देते हैं। मध्ययुगीन भू-राजनीति और युगों पहले गुम हो गए शहरों पर नई रौशनी डालते हुए मूल अंग्रेजी से शुचिता मीतल द्वारा अनूदित ‘मंथन का सागर’ एक जीवंत सभ्यता के केंद्र में जाने का लुभावना सफर है। सान्याल स्रोतों का एक प्रभावशाली व्यूह रचते हैं और उन्हें बड़े जतन से विस्तार देते हैं। अद्यतन सामग्री और उसके निहितार्थों के प्रति पैनी दृष्टि रखते हुए इतिहास को पाठक तक पहुंचाने में इनकी दक्षता सराहनीय है। सान्याल की सबसे बड़ी उपलब्धि है इतिहास की अडिग चट्टान से छोटे-छोटे सांकेतिक रत्नों को तराशना। यह इस मायने में जीवंत पुस्तक है, जिसमें नाटकीयता का पूरा विस्तार समोया हुआ है। पुस्तक में सागर का एक बहुआयामी अध्ययन है, जो अत्यंत ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ निरंतर मनोरंजक भी है। हमारी समुद्री धरोहर का इस पुस्तक से बेहतर कोई समकालीन परिचय नहीं हो सकता।
मंथन का सागर : संजीव सान्याल; एका प्रकाशन, वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्रा.लि., 61, दूसरी मंजिल, सिल्वरलाइन बिल्डिंग, अलपक्कम मेन रोड, मदुरावोयल, चेन्नई; 350 रुपए।