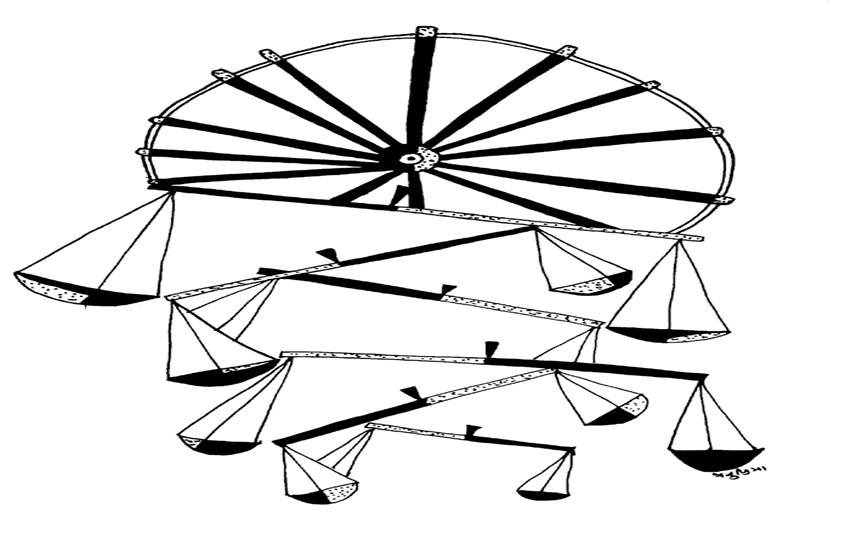लंबी प्रतीक्षा के बाद शिक्षा की नई नीति का प्रारूप देश के समक्ष रखा गया है। इस पर फिर से सुझाव मांगे गए हैं। प्रारूप का प्रारंभ ‘विजन’ से होता है : ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 भारत केंद्रित शिक्षा-व्यवस्था की परिकल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को निरंतर एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान-समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है।’ इसे पढ़ कर यह याद आना स्वाभाविक है कि लक्ष्य तो पिछली तीनों शिक्षा नीतियों- 1968, 1985 और 1992- का भी इससे अलग नहीं था, भले कहने की शब्दावली अलग रही हो। अगर भारत के भविष्य का निर्माण कोठारी आयोग के अनुसार 1964-66 में उसके स्कूलों की कक्षाओं में हो रहा था, तो आज भी ऐसा ही होना अपेक्षित है। यह सत्य सर्व-स्वीकार्य होना चाहिए।
समिति के अध्यक्ष के अनुसार प्रारूप बनाने के पहले ही यह संभावना उभरी थी कि ‘आउट आॅफ बॉक्स’ वैचारिकता सामने आने वाली है। ऐसा दिखाई भी देता है, मगर बहुत कुछ ऐसा भी लगातार सामने आया है, जिसे पहले भी कहा जा चुका है और कई बार दोहराया गया है। मुख्य प्रश्न फिर एक बार यही उभरता है कि अजादी के बाद देश को जिस प्रकार की शिक्षा और उसकी व्यवस्था करने वाला तंत्र चाहिए था, वह नीति-निर्धारकों को ज्ञात था, बार-बार नीति संबंधी दस्तावेजों का भाग भी बना, मगर क्रियान्वयन के स्तर पर अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिल सकी और महत्त्वपूर्ण सुझाव और संस्तुतियों को व्यवहारिक रूप में क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा सका? संखाएं बढीं, मगर गुणवत्ता, कर्मठता, मानवीय मूल्य, स्वीकार्यता और साख घटते चले गए! चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास परीक्षा में अंकों की दौड़ में पीछे छूटते गए। बहुत कुछ बिखरता चला गया। परिस्थितियां ही ऐसी बनीं, जिनमें यह तो होना ही था। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अठारह और माध्यमिक स्कूलों में पंद्रह फीसद शिक्षकों के पद 2016 में खाली थे। इसके अलावा अस्थायी, केवल थोड़े से मानदेय पर कार्य करने वाले अध्यापकों की संख्या भी दस-ग्यारह लाख थी! जो नियमित अध्यापक पदस्थ थे, उनसे पढ़ाने के अलावा क्या-क्या करवाया जाता रहा है, इसे सभी जानते हैं। परिणाम स्वरूप सरकारी स्कूलों की साख लगातार गिरती गई, निजी स्कूलों की ओर दौड़ बढ़ती गई। नीति प्रारूप में अपेक्षा है कि निजी स्कूल अपने को पब्लिक स्कूल नहीं कह सकेंगें! यह लोगों को अच्छा लगा है। मगर इससे चुनौतियां घटेंगी नहीं।
संविधान के मूल-स्वरूप में ‘चौदह साल तक के’ हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार को सौंपा गया था। सरकारों ने इसे उस गंभीरता से नहीं लिया, जिस साहसपूर्ण ढंग से संविधान निर्माताओं ने इसके महत्त्व को समझा और स्वीकार किया था। संविधान के छियासीवें संशोधन में अनुच्छेद 21-ए जोड़ा गया और शिक्षा के मूल अधिकार को छह से चौदह वर्ष में सीमित कर दिया गया। नीति प्रारूप में इसे सुधारने की संभावना उभरी है। स्कूल-पूर्व शिक्षा सरकारी विद्यालयों में नहीं थी, निजी स्कूलों में यह आकर्षण का मुख्या केंद्र थी। शिक्षा के मौलिक अधिकार और उसमें मातृभाषा द्वारा शिक्षा पाने की आवश्यकता और अनिवार्यता को सबसे पहले अत्यंत सशक्त ढंग से तो 8 दिसंबर, 1948 को संविधान सभा में डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। उनके शब्द आज भी बच्चों की प्रारम्भिक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्णता से व्यक्त करते हैं: ‘अगर प्राथमिक शिक्षा को लाभप्रद तथा प्रभावपूर्ण बनाना है तो उसे बच्चों को मातृभाषा में ही देना होगा। अन्यथा प्राथमिक शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा और वह निरर्थक हो जाएगी।’ शिक्षा में प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा माध्यम की व्यावहारिक स्वीकार्यता बहुत पीछे छूट गई है। अब तो इसका अनुपालन केवल वहीं हो रहा है, जहां पालकों को अंग्रेजी माध्यम के ‘पब्लिक स्कूल’ या तो उपलब्ध नहीं हैं या उनकी आर्थिक परिधि के दायरे के बाहर हैं। और यह आज का उठाया गया प्रश्न नहीं है। गांधीजी अपने व्यक्तिगत अनुभव और वैश्विक परिदृश्य के विश्लेषण के बाद इस पर कितने संवेदनशील थे, इसे नीति को अंतिम स्वरूप देने वालों को अवश्य सामने रखना चाहिए : ‘अगर मुझे एक निरंकुश शासक के अधिकार प्राप्त होते तो मैं अपने बालक-बालिकाओं की विदेशी माध्यम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पर रोक लगा देता और उन सभी अध्यापकों तथा प्राध्यापकों को निकाल बाहर करता, जो इस परिवर्तन को तुरंत स्थान दे पाने में असमर्थ होते। मैं पाठ्यपुस्तकों की तैयारी के लिए प्रतीक्षा न करता। परिवर्तन के पश्चात वे तैयार होती रहतीं। यह एक ऐसा दोष है, जिसका जड़-मूल से इलाज आवश्यक है।’
वैश्विक स्तर पर यह शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, मानविकी और समाजशास्त्र के विद्वान एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए, मगर भारत में जो दृष्टिकोण और परिस्थितियां बनी हैं, उनमें मातृभाषा की महत्ता की पुनर्स्थापन के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। साथ ही बाजार में और रोजगार के क्षेत्र में अंग्रेजी के एकाधिकार के बरक्स मातृभाषाओं को बराबरी पर खड़ा करना होगा। बच्चों का मूलभूत अधिकार तो यों भी कहा जा सकता है कि प्रारंभ में घर से स्कूल जाने पर उसे ‘घर जैसा वातावरण’ मिले। उसके सबसे बड़े कारक हैं : घर की भाषा, और संवेदनशील आत्मीयता बिखेरता अध्यापक! इनकी अनुपस्थिति उसकी मासूमियत पर कू्रर प्रहार के समान ही मानी जानी चाहिए। इसी कारण विश्व भर में प्रारंभिक कक्षाओं में महिला अध्यापिकाओं को प्रमुखता देने का चलन है।
स्कूल जाने के कुछ महीने के अंदर ही माता-पिता को यह ज्ञात हो जाता है कि बच्चे पर स्कूल और अध्यापक का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वह पहली बार उन्हें कहता है कि सर/ गुरुजी/ मिस ने जो कहा वही सही है, आपका कहा या बताया नहीं, तब जान लेना चाहिए कि बच्चा अपना आदर्श सबसे पहले स्कूल में ही अपने अध्यापकों में खोजता है। इसीलिए हर अध्यापक को अपने आचार्य होने का भान सदा सामने रखना चाहिए, और इसी कारण उनका आचरण केवल अनुकरणीय हो सकता है, अन्य कुछ भी नहीं! अध्यापकों से अपेक्षाओं, उनके प्रशिक्षण, सेवाकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, आगे बढ़ने के अवसरों का प्रावधान, नवाचार के लिए प्रोत्साहन जैसे पक्षों पर की गई संस्तुतियां विचारपूर्ण और तर्क-संगत लगती हैं। इसके क्रियान्वयन की संभावनाएं अनेक आशंकाओं को जन्म अवश्य देती हैं। अगर यह मनोयोग से क्रियान्वित हो सकीं, तो भारत की स्कूल शिक्षा का स्वरूप बदल जाएगा। शिक्षकों पर लिखे गए अध्याय में उद्देश्य को इन शब्दों में पिरोया गया है : ‘स्कूल शिक्षा के सभी स्तर के सभी विद्यार्थियों का शिक्षण उत्साहित, प्रेरित, उच्च योग्यता वाले, प्रशिक्षित और निपुण शिक्षकों द्वारा हो।’ उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ तो अध्यापक ही होंगे, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रारूप समिति ने अनेक सार्थक और सटीक सुझाव दिए हैं। शिक्षा और शिक्षकों की वर्तमान स्थिति तथा परिस्थिति से परिचित सभी लोग इसे एक पवित्र और निर्मल सदिच्छा ही कहेंगे।
योग्यतम व्यक्ति को ही शिक्षक बनाना चाहिए, इसे सभी मानेंगे।
यह भी निर्विवाद है कि अध्यापक वही बने, जिसकी गहन रुचि इस कार्य में हो; यानी जो पूर्णरूपेण ज्ञानार्जन के लिए समर्पित हो तथा नया ज्ञान सीखने, खोजने तथा बांटने में आनंद की अनुभूति प्राप्त करता हो। उसके सामने, उसके अपने कार्यक्षेत्र में उसे पूर्ण स्वायत्तता होनी ही चाहिए। सच्चा अध्यापक वही बन सकता है जो ‘यावद्जीवेत अधीयते विप्र:’ का अर्थ ही नहीं, उसमें निहित भाव तथा उत्तरदायित्व बोध को भी आत्मसात कर सके! इसके लिए आवश्यक है कि उसे पुस्तकें उपब्ध हों, समय मिले, नवाचार करने के लिए साधन संसाधन उपलब्ध हों! उसे एक अदना-सा सरकारी कर्मचारी ही मान कर हेय दृष्टि से न देखा जाय। शिक्षक छात्र अनुपात ऐसा हो कि अध्यापक अपने विद्यार्थी को पहचान सके यानी उसकी व्यक्तिगत रुचियों, प्रतिभा विकास की संभावनाओं तथा आवश्यकताओं से परिचित हो और एक-पर-एक संवाद बनाए रखे। अध्यापक को स्थानीय समुदाय से संपर्क बनाने तथा अपने विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति की समझ प्राप्त कने के लिए समय और प्रोत्साहन चाहिए। यह भी आवश्यक है कि गैर-शैक्षिक कार्यों का बोझ और उससे पड़ने वाला दबाव अध्यापक पर न हो। प्रारूप समिति ने इस सबसे सहमति व्यक्त की है, और यह माना है कि इस समय शिक्षकों की स्थिति ‘निम्न स्तर’ पर है, साथ ही यह भी कहा है कि ‘वर्तमान समय में निस्संदेह शिक्षकों के स्तर में गिरावट आई है।’ व्यवस्था को यह समझना आवश्यक है कि अगर अध्यापक के पास उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं है, उसके पास समय नहीं है, तो वह एक अबोध ‘व्यक्ति को व्यक्तित्व’ में कैसे बदल पाएगा, भले ही वह उन्हें परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए तैयार कर दे!