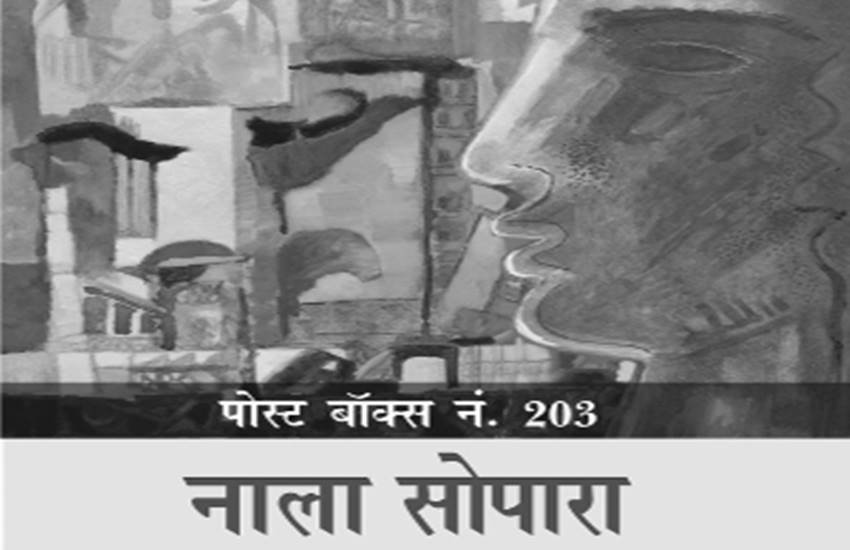चित्रा मुद्गल का नया उपन्यास पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि चिंतन, तथ्य और आंकड़ों से बोझिल किए बिना भी उपेक्षित तबकों की जिंदगी पर महत्त्वपूर्ण रचना लिखी जा सकती है। यह एक किन्नर की जिंदगी पर आधारित उपन्यास है। इसमें किन्नरों का जीवन-सत्य भी भरपूर है। पर, यह जीवन-सत्य तथ्यों और आंकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि कथा के भीतर ही कुछ इस तरह पिरोया गया है कि उपन्यास बेहद मार्मिक हो उठा है। जीवन-सत्यों के भीतर मार्मिक स्थलों की पहचान करना किसी भी रचनाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है। निस्संदेह इस लिहाज से यह उपन्यास उल्लेखनीय है, क्योंकि लेखिका से उन स्थलों की पहचान में कहीं चूक नहीं हुई है।
पूरा उपन्यास अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही किन्नरों की मंडली को सौंप दिए गए विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली द्वारा अपनी जीवन स्थितियों और घर की स्मृतियों का वर्णन करते हुए अपनी बा (मां) को लिखे गए क्रमवार पत्रों के रूप में संयोजित है। मां भी अपने किन्नर पुत्र को पत्र लिखती है, पर वे जवाबी पत्र पृष्ठभूमि में रहते हैं। बेटे द्वारा लिखे गए पत्रों से ही मालूम होता है कि मां ने अपने पत्र में क्या लिखा था! उपन्यास में ठहराव न होकर गति है। यह गति घटनाओं के क्रमिक विकास के कारण है और इसी कारण इसमें भरपूर कथा-तत्त्व भी है। पत्र-शैली चिंतन-प्रवाह या विचार-प्रवाह को अभिव्यक्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, पर लेखिका ने इसके माध्यम से कथा-प्रवाह को अभिव्यक्त करके एक अनूठा प्रयोग किया है और इसमें वे पूरी तरह सफल भी हुई हैं।
लिंगदोषी के रूप में पैदा हुए अपने मंझले बेटे विनोद से बहुत लगाव होते हुए भी सामाजिक दबाव, घर के भीतर बड़े बेटे-बहू की मानसिक परेशानी और सबसे बढ़ कर किन्नरों की मंडली के आतंक के डर से मां को लगभग चौदह वर्ष की अवस्था में अंतत: उसे किन्नरों को सौंपना ही पड़ता है। विनोद हर दृष्टि से स्कूल में पढ़ रहे अपने अन्य सहपाठियों जैसा ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि वह अन्यों की तरह स्कूल की चारदीवारी से सट कर पैंट के बटन खोल कर निवृत्त नहीं हो सकता। जहां तक पढ़ने का सवाल है, वह अपनी कक्षा में सदा प्रथम आता था। बावजूद इसके, विनोद को उस नरक में धकेल दिया गया। विनोद में कोई स्त्रैण प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वह साथी किन्नरों द्वारा लाख जबर्दस्ती करने और प्रताड़ित होने के बावजूद उनके अनुकूल नहीं हो पाता और श्रम करके जीने के लिए अनवरत संघर्ष करता है। वह अपनी बा को लिखता है: ‘सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया। सपनों ने मुझसे मुंह नहीं फेरा। आज भी वे मेरे पास बेरोक-टोक चले आते हैं।’
उसका सपना है- सामान्य मनुष्य की भांति गरिमापूर्ण जीवन। वह बार-बार प्रश्न उठाता है कि जननांग विकलांगता को इतना बड़ा दोष क्यों मान लिया गया है? सिर्फ इसी कारण उसे घर-परिवार, रिश्ते-नाते सबसे कट कर नरक की जिंदगी क्यों भोगनी पड़ रही है? वह कहता है- ‘जननांग विकलांगता बहुत बड़ा दोष है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम मान लो कि तुम धड़ का मात्र वही निचला हिस्सा हो। मस्तिष्क नहीं हो, दिल नहीं हो, धड़कन नहीं हो, आंख नहीं हो। तुम्हारे हाथ-पैर नहीं हैं। हैं, हैं, हैं, सब वैसे ही हैं, जैसे औरों के हैं। यौन-सुख लेने-देने से वंचित हो तुम, वात्सल्य सुख से नहीं। बच्चे तुम पैदा नहीं कर सकते, मगर पिता नहीं बन सकते, यह किसने नहीं समझने दिया तुम्हें?’
उपन्यास एक बड़ा प्रश्न उठाता है कि लिंग-पूजक समाज लिंगविहीनों को कैसे बर्दाश्त करेगा? उपन्यास इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचने को विवश करता है कि आखिर एक मनुष्य को सिर्फ इसलिए समाज बहिष्कृत क्यों होना पड़े कि वह लिंगदोषी है? सिर्फ इसी कारण उसकी उम्मीदों, सपनों, आकांक्षाओं, भावनाओं का गला क्यों घोंट दिया जाता है? दरअसल, इसके मूल में समाज का यौन-केंद्रित होना है। उपन्यास इस बात को प्रबलता से रेखांकित करता है कि हमारा समाज जब तक यौन केंद्रित बना रहेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। यौन केंद्रित समाज से मुक्ति ही इस उपन्यास का स्वप्न है और इसका केंद्रीय कथ्य भी।
समाज के यौन केंद्रीयता के शिकार लिंगदोषी तो हैं ही, स्त्रियां भी हैं। स्त्री विमर्श का लक्ष्य भी इस यौन केंद्रित समाज का खात्मा होना चाहिए। जो समाज लिंगदोषी मनुष्यों को बहिष्कृत करता है, वही स्त्रियों को एक यौन-वस्तु के रूप में देखता है। स्माज की यौन केंद्रित दृष्टि में परिवर्तन की जगह उपन्यास छोटे-छोटे सतही परिवर्तनों को नाकाफी मानते हुए खारिज करता है। मसलन, हिजड़ा शब्द की जगह किन्नर शब्द का प्रयोग या फॉर्म में अन्य जेंडर का एक अलग खाना। विनोद यह सवाल उठाता है कि लिंग की दृष्टि से किन्नरों का वर्गीकरण क्यों? उन्हें अपना लिंग चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, न कि अन्य में डाल दिया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग आदि सभी समाज के वंचित वर्ग हैं, पर वे बकायदा स्त्री-पुरुष भी हैं। ठीक इसी तरह लिंगदोषियों को वर्गीकरण में इन्हीं वंचितों के साथ रखा जाए।
उपन्यास इस सत्य को सामने लाता है कि मुख्यधारा की राजनीति की दिलचस्पी किन्नरों को मानवीय गरिमा दिलाने में नहीं, बल्कि आरक्षण का लालच देकर उन्हें वोट बैंक के रूप में सिर्फ उपयोग करने की है। पहले तो विनोद में संभावना देख कर सत्ताधारी पार्टी उसे प्रश्रय देती है, पर जैसे ही वह योजना मुताबिक उनके अनुकूल नहीं रह पाता और आरक्षण की भीख मांगने की जगह किन्नरों में स्वाभिमान जगाने लगता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उपन्यास का अंत मां द्वारा अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने किन्नर बेटे को सार्वजानिक रूप से स्वीकार कर अपनी संपत्ति को तीनों बेटों में बराबर-बराबर बांटने की घोषणा संबंधी विज्ञापन से होती है। स्पष्ट है, लेखिका किन्नर समस्या के राजनीतिक समाधान के प्रति घोर आशंकित हैं और सामाजिक समाधान को ही अनिवार्य विकल्प मानती हैं।
दिनेश कुमार
पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा: चित्रा मुद्गल; सामयिक प्रकाशन, 3320-21, जटवाड़ा, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 400 रुपए।