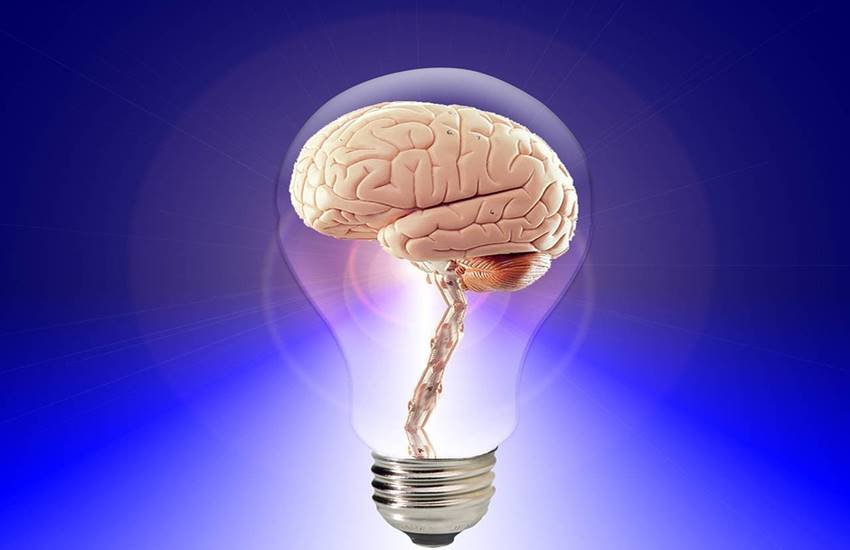समाज का विकास विज्ञान के विकास के समांतर हुआ है। इस बात को और विस्तार दें तो सुख, समृद्धि, शांति दुनिया भर में विज्ञान से ही आई है। दुनिया के सभी विकसित, उन्नत राष्ट्र इसीलिए विज्ञान का महत्त्व समझते हैं और इसीलिए अग्रणी बने हुए हैं। गौरतलब है कि पचास के दशक में रूस ने अंतरिक्ष विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में जैसे ही लंबी छलांग लगाई, अमेरिका में हलचल मच गई। वहां तुरंत विज्ञान पढ़ने-पढ़ाने और शोध को राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखा गया और दूसरे विश्वयुद्ध के बाद उस शीत युद्ध में धीरे-धीरे अमेरिका विज्ञान के बूते ही बाजी मारता चला गया। न केवल दूसरे विश्वयुद्ध के दौर से जर्मनी के वैज्ञानिक आइंस्टाइन आदि अमेरिका पहुंचते चले गए, बल्कि उसके बाद से आज तक अमेरिका दुनिया के वैज्ञानिकों की पहली प्राथमिकता बना हुआ है। भारत के हरगोविंद खुराना, चंद्रशेखर, वेंकटराम कृष्णा आदि अमेरिकी शिक्षा के बूते ही दुनिया में नाम कमा पाए हैं।
हम लगभग तीस वर्ष से लगातार यह देखते-सुनते आ रहे हैं कि चीन के विश्वविद्यालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेटेंट और नई खोजों के पैमानों से नापा जाए तो आज चीन की स्थिति अमेरिका से भी आगे है। विज्ञान और तकनीक के बूते ही छोटा-सा इजराइल कैसे अपनी धाक जमाए हुए है। जापान तो है ही पिछले लगभग सौ सालों से सबसे मजबूत। पड़ोसी चीन की ही बात करें, तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक को बदला है और इसीलिए दुनिया भर के शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों में पांच से ज्यादा चीन के होते हैं और हम पहले पांच सौ में भी मुश्किल से आ पाते हैं।
आजादी के बाद नारों और दीवारों पर तो वैज्ञानिक चेतना की बातें कही गर्इं, लेकिन न शिक्षा में कोई बुनियादी परिवर्तन आया और न इसी वजह से समाज में। माना हम बड़ा देश हैं, यहां कई जटिलताएं हैं, लेकिन अगर अंधेरा बढ़ता ही जाए, तो हमें पूरी नीति की समीक्षा की जरूरत है।
पिछली सरकार ज्ञान आयोग और उसकी अंग्रेजी पढ़ाने, लादने की जिद से इतनी व्यस्त थी कि सरकारी शिक्षा निजी स्कूलों की तरफ तो चली गई, उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं मिला। यानी अंग्रेजी ठीक करने के चक्कर में दुनिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में हम और पीछे होते गए। इसलिए पहले तो यह भ्रम हटाना होगा कि अंग्रेजी के बूते आप विश्वविद्यालयों को ठीक कर सकते हैं। कम से कम वर्तमान सरकार अंग्रेजी की वैसी दीवानी नहीं है और अगर विज्ञान को सही समझ पाए, तो मजबूत इच्छाशक्ति भी रखती है।
मौजूदा सरकार के पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। निश्चित रूप से समझने में समय लगता है, लेकिन बड़े परिवर्तन उस प्रक्रिया से ही संभव हैं जैसे दुनिया के राष्ट्रों ने संभव किए हैं। पांच सौ वर्ष पहले का यूरोप इसी विज्ञान के बूते भारत, चीन जैसी पुरानी सभ्यताओं को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया और आज भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सभ्यता तो चीन की भी पुरानी है, लेकिन उसे मौजूदा विज्ञान से कोई परहेज नहीं है। उसने मौजूदा विज्ञान के बूते अपनी स्थिति बहुत मजबूत की है। हमारा अतीत निश्चित रूप से गौरवशाली रहा है। शून्य की खोज, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सुश्रुत के कामों पर हमें गर्व है, लेकिन विज्ञान निरंतर बदलने वाली सोच है। दो हजार साल पहले दुनिया भर की सभ्यताएं बहुत अविकसित दौर में थीं। उसके बरक्स हम आगे थे और अगर हमें फिर से आगे होना है, तो कुछ अपनी पुरानी सभ्यताओं से उठाएं, उन्हें जांचें-परखें, दुनिया के सामने प्रमाणित करें और साथ ही दुनिया के अनुभवों को साथ लेकर आगे बढ़ें। हम महान थे, विज्ञान ऐसी किसी स्थापना को नहीं मानता। वह बार-बार उसका प्रमाण मांगता है। और इसके लिए हमारे स्कूली पाठ्यक्रमों में पूरा बदलाव चाहिए। विज्ञान श्रद्धा, भक्ति का नाम नहीं है। विज्ञान की शुरुआत ही शंका, संदेह से होती है। यह उसकी बुनियाद है। डाल्टन ने कहा- एटम सबसे छोटी इकाई है। दूसरे विज्ञानकों ने उसे तोड़ दिया कि नहीं, छोटी इकाई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं। दूसरे वैज्ञानिकों ने उसे और विखंडित कर दिया। विज्ञान की लाखों बातें ऐसे ही प्रश्नों, शंकाओं, बहसों से आगे बढ़ी हैं।
हर धर्म और उसकी बातें निर्जीवता की हद तक वहीं खड़ी रहती हैं, जबकि विज्ञान निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। इस पक्ष पर तुरंत काम करने की जरूरत है। स्कूली बच्चे तर्कशील बनेंगे, अपने आसपास की समस्याओं पर प्रश्न करना, उनसे जूझना सीखेंगे, उनके हल निकालेंगे और इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय दुनिया की खोजों से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर जरूरत हो तो पांच वर्ष तक सिर्फ विज्ञान की शिक्षा ही दी जाए, तो देश का कायापलट हो सकता है। यह केवल शिक्षा का मामला नहीं है, पूरे समाज को बदलने के लिए ऐसे ही कदमों की जरूरत है।
बुनियादी सामाजिक प्रश्न की तरफ लौटते हैं। जाति और धर्म के भेद-विवेद और उनसे उत्पन्न समस्याओं से पूरा देश जूझ रहा है। विज्ञान की समझ कहती है कि न केवल मनुष्य, बल्कि सभी जीवधारियों के सत्तानबे फीसद जीन समान होते हैं, यानी तीन फीसद की भिन्नता ही करोड़ों जीवों को अलग करती है। तो फिर मनुष्य की जाति, धर्म के भेद क्या नकली, बनावटी नहीं हैं? जब ऐसी तार्किक स्थापना हमारे बचपन में बैठा दी जाए, तो उसे कोई भी राजनीति, कोई भी धर्मगुरु अपने स्वार्थों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।
इन्हीं सब कारणों से संयुक्त राष्ट्र ने 2001 से दुनिया भर में विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष दस नवंबर को मनाने का फैसला किया, जिससे कि सभी देश विज्ञान के तार्किक रास्ते से सुख, समृद्धि और विकास की तरफ अग्रसर हो सकें। क्या तीन सौ वर्ष पहले हम इतने सुखी थे? चेचक से लाखों मर जाते थे। इंग्लैंड के डॉक्टर जीनर ने रास्ता खोजा और पूरी दुनिया आज चेचक से मुक्त हो गई है। क्या यह किसी माता, देवी या पीर-पैगंबर की पूजा से संभव हो सकता है? पोलियो का कीटाणु दुनिया भर में लाखों लोगों को पंगु बना देता था, आज हम उससे मुक्त हैं। पेंसिलीन, हैजा के टीके, बड़ी से बड़ी सर्जरी, कैंसर से पार पाना, यानी विज्ञान के बूते दुनिया आराम की जिंदगी जी रही है और इसीलिए मनुष्य की औसत आयु निरंतर बढ़ रही है।
भारत का ही उदाहरण लें, तो आजादी के वक्त औसत आयु सिर्फ बत्तीस वर्ष थी, आज सत्तर वर्ष के करीब है। यह सिर्फ विज्ञान ने संभव करके दिखाया है। इसलिए सभी सरकारों का दायित्व है कुछ दिनों के लिए दूसरी बहसों को एक तरफ रख कर सिर्फ विज्ञान में दुनिया के देशों की बराबरी करने की तरकीब निकालें। इससे हमारे समाज में तो बुनियादी परिवर्तन आएगा ही, हमें अरबों रुपए के हथियार भी आयात नहीं करने पड़ेंगे, और न जीवन रक्षक दवाएं आयात करनी होंगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही हैं।
विज्ञान शिक्षा की तार्किकता और दर्शन से हमारे सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान के शोध भी बदलेंगे और सही मायनों में हमारे विश्वविद्यालय भी। फिर हमारे बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड नहीं भागेंगे। हमारे अतीत में जो भी विज्ञान की कसौटी पर अच्छा है उसे भी सहर्ष अपनाएं और दुनिया के मौजूदा ज्ञान को भी।