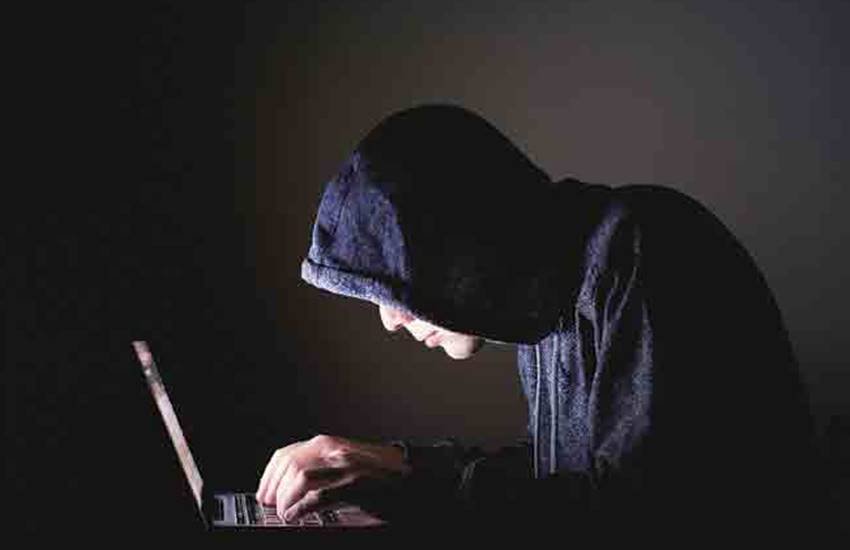सामाजिक प्रगति में इंटरनेट की सहभागिता ने एक नया आयाम दिया है। इसके कारण वैश्विक संप्रेषण और संचार के साथ विविध कार्यों में पारदर्शिता और गति बढ़ी है। इस पर आधारित सोशल मीडिया वैकल्पिक मीडिया की संकल्पना को पूरा करने की ओर बढ़ चुका है। हालांकि इसने आर्थिक और शैक्षिक आधार पर नीचे छूटे लोगों के दर्द को और बढ़ाया है। बहरहाल, देश में मोबाइल संख्या और इंटरनेट डाटा की खपत के आंकड़ों से इस तर्क को बल मिलता है कि बहुसंख्य परिवार सोशल मीडिया से कहीं न कहीं जुड़ा है। इस डिजिटलीकरण के दौर में जिन सक्षम हाथों में मोबाइल है, वे सभी पत्रकार हैं। सीसीटीवी से लेकर मोबाइल से लिए वीडियो विभिन्न दुर्घटनाओं को सामने लाने में अभूतपूर्व भूमिका में हैं और मुद्दों को सुलझाने में साक्ष्य के तौर पर भी काम आने लगे हैं। इन प्रकरणों के बाद जो सोशल मीडिया का स्वरूप बनता है, उससे लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार के सपनों को नए पंख लगे हैं। यह माध्यम इतना सशक्त है कि रातों-रात किसी को लोकप्रिय बना देता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के किसी प्रोफेसर को उसके नृत्य के लिए ख्याति मिल जाती है, तो शासन-प्रशासन के किसी प्रतिनिधि को जबाबदेही का भी बोध कराना संभव हो पाता है।
सोशल मीडिया के इन सभी सकारात्मक पहलुओं के बावजूद यहीं झूठ, ईर्ष्या और आत्म-प्रचार का एक ऐसा माहौल भी बना है, जिससे इसकी उपयोगिता पर नए सवाल उठ रहे हैं। अगर मुख्यधारा मीडिया में सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से इसकी तटस्थता प्रभावित होती रही है, तो सोशल मीडिया पर एक तरफ तो कुछ भोले-भाले लोग हैं, जो अपनी गतिविधियों को लेकर सक्रिय हैं, तो दूसरी तरफ एक शातिर तबका है, जिसका अपना सुनियोजित एजेंडा है। अगर कोई व्यक्ति, प्रतिष्ठान या समूह अपनी बात सार्वजनिक करने के लिए प्रेस-वार्ता के बजाय ट्वीट करके काम चला रहा है, तो प्रचार की इस सहजता का लाभ अफवाह फैलाने वालों के भी काम आ रहा है। देश में अनेक सांप्रदायिक दंगों का आधार ऐसी कुछ अफवाहें रही हैं। इसमें हालिया शिलांग में सद्भाव बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास भी रहा है। इस पूरे प्रकरण में दुर्भाग्य यह है कि तथ्य से परे जाकर संपादित तस्वीरें, ऑडियो या वीडियो जैसे संचार के प्रभावी माध्यमों को प्रसारित करने में पढ़े-लिखे लोगों का संरक्षण मिलता है, जिसका बड़ा कारण यह है कि यह झूठी सामग्री उनके एजेंडे या उद्देश्यों के अनुकूल होती है, जबकि समाज के जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में इनको झूठ के प्रसार को हर संभव रोकना चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी तेजी से विकसित हुआ है, जिसको न तो अपनी सार्वजनिक उपस्थिति की दशा में अपेक्षित मर्यादा की चिंता है और न समझदारी है। विदेश में फंसे अब तक सैकड़ों नागरिकों के डिजिटल अनुरोध पर उनकी समस्याओं से उबार चुकी देश की विदेश मंत्री भी इस चिंता में शामिल हैं कि सार्वजनिक उपस्थिति में भाषा शिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि वे खुद यहां की अशिष्टता का सामना कर चुकी हैं।
डिजिटल मीडिया जनसंचार का अद्यतन माध्यम है, जिसने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को अभूतपूर्व स्थान दिया है। इससे पहले के माध्यमों जैसे रेडियो, समाचार-पत्र, टीवी आदि में न तो स्व-अभिव्यक्ति के लिए इतना स्थान था और न ही इन माध्यमों की व्यापक सुलभता थी। आज डिजिटल मीडिया की उपस्थिति मोबाइल के रास्ते लोगों की हथेली पर है, जो दिन-रात लोगों की पहुंच में रहती है। इसलिए यहां जो कुछ हो रहा है वह हमारे समाज के एक बड़े वर्ग का प्रतिबिंब है और इसमें कुछ स्वार्थी और चालाक लोगों ने अपना उद्देश्य भी शामिल कर लिया है। डिजिटल मीडिया को दूषित करने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी है, जो अपनी दूषित मानसिकता को शातिराना तरीके से इस पर परोसते हैं और इससे बड़े दोषी वे हैं, जो ऐसे तत्त्वों को हतोत्साहित करने के बजाय अपने एजेंडे के अनुसार उसको प्रसारित करते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को हुआ है, जो अपनी रचनात्मकता, शिकायत और विचार सार्वजनिक करना शुरू ही किया था कि इस पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। जो मंच पूंजी और सत्ता के प्रभावों से परे सकारात्मक राजनीति में जनमत निर्माण का एक मंच हो सकता था और आज भी है, उस पर नकारात्मक तत्त्वों ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सजग लोग इनसे बचें और ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें, ताकि प्रथम चरण में ही विकृत और कुंठित अभिव्यक्तियों को रोका जा सके, जिससे समाज दूषित न हो। साथ ही डिजिटल अपराधों को रोकने के प्रभावी तंत्र विकसित हो।
समाज में झूठ और सच कोई नया नहीं है, बल्कि यह मानवीय सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है और यह आगे भी जुड़ा रहेगा। इससे बहुत फर्क पड़ता भी नहीं, लेकिन इनके प्रति समाज के सजग लोगों का रुख कैसा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। दुर्भाग्य है कि सोशल मीडिया में स्वाभाविक सच-झूठ से आगे तथ्यों को परोसा जा रहा है, वह भी ‘सच’ को झूठ के और ‘झूठ’ को सच की थाली में सजा कर। किसी लोकतंत्र की सफलता इसमें है कि समाज में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विचार भी लोगों के सामने आएं और इसके लिए सार्वजनिक बहस हो। फिलहाल इसके लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई मंच नहीं है, लेकिन ‘वायरल’, ‘ट्रोल’ और ‘फेक’ जैसे इतने रोग लग चुके हैं कि ‘प्रचार-तंत्र’ की बहसों के लिए इस नवीनतम मीडिया ने नई सामग्री उपलब्ध कराई है। आज देश-विदेश के सभी मुख्य राजनीतिक दल और प्रचार एजेंसियों ने अपने प्रचार अभियानों में इसको शामिल किया है। इससे भी आगे एक तबका है जो सिर्फ इसके साथ खेलता है और इस खेल का नुकसान अंतत: लोकतंत्र और इसके माध्यम को उठाना पड़ता है, क्योंकि एक माध्यम के रूप में सोशल मीडिया की गंभीरता और विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। सोशल मीडिया पर उपस्थित लोग न तो संपूर्ण समाज हैं और न ही इनकी प्राथमिकताएं संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन सार्वजनिक उपस्थिति में एक भ्रम इसके विपरीत बन रहा है और ‘नेटिजन’ सार्वजनिक कार्यक्रमों, नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए प्रमुख बनते जा रहे हैं। इसके साथ मुख्यधारा मीडिया ने रिपोर्टिंग छोड़ कर सोशल मीडिया की सामग्री को आधार बनाने लगा है। यह प्रवृत्ति समाज के अंतिम व्यक्ति के खिलाफ है और इस पूरे प्रकरण से उनमें हताशा और अवसाद ही विकसित होगा, जो एक नए तरह का वंचन है।