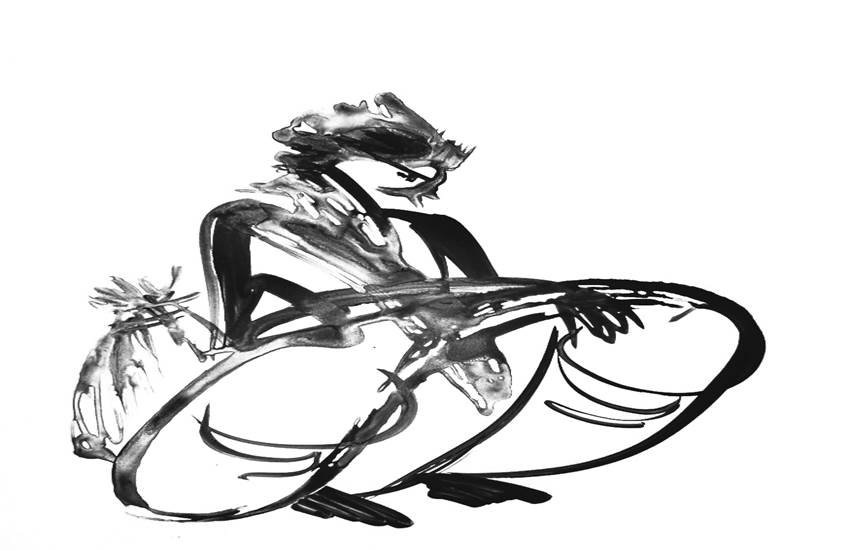कामकाजी औरतों की चर्चा होते ही प्राय: उन स्त्रियों की छवि आंखों के आगे तैर जाती है, जो किसी स्कूल, कार्यालय आदि में काम करती और बदले में निश्चित वेतन पाती हैं। इसी तरह आर्थिक जगत का नाम आते ही कुछ नामचीन महिलाओं का स्मरण स्वाभाविक है। लेकिन उन औरतों पर प्राय: ध्यान नहीं जाता, जो कामकाजी श्रेणी में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आतीं, पर परिवार, समाज और देश के लिए उनका आर्थिक योगदान बहुत मायने रखता है। उनका कौशल, उनकी व्यक्तिगत पहचान का दायरा भले सीमित हो, पर इनके कौशल का लोहा सभी मानते हैं। ये उस हाशिए की औरतें हैं, जहां उनकी मुख्य पहचान खांटी घरेलू औरत की होती है।
उद्यमिता की दृष्टि से ऐसी महिलाओं में से कुछ को कुटीर उद्योग, तो कुछ को लघुउद्योग से जुड़ा देखा जा सकता है। पर कुछ ऐसी भी हैं, जो किसी भी श्रेणी में दिखाई न देती हुई भी अर्थोपार्जन करती रहती हैं। देश में अनेक ऐसे लघु और कुटीर उद्योग हैं, जिनकी बुनियाद घरेलू औरतों के श्रम पर टिकी हुई है। ये औरतें कामकाजी श्रेणी के खांचे में नहीं आतीं। ये अपना परिवार संभालती हैं, बच्चे पालती हैं, सभी नाते-रिश्ते, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करती हैं। यहां तक कि घरेलू हिंसा का शिकार भी होती रहती हैं, फिर भी अपने परिवार के लिए चंद रुपए जुटाने के लिए अपने आराम के दो पल भी भेंट चढ़ा देती हैं। भले इनके श्रम को कोई महत्त्व नहीं मिलता, परिवार की ओर से भी इनके अर्थोपार्जन को महत्त्व नहीं दिया जाता, फिर भी ये काम करती और पैसे कमाती हैं और वह भी सम्मानजनक और वैधानिक ढंग से।
भारत में घरेलू उद्योगों का दायरा गांवों और शहरों दोनों में फैला हुआ है। इसमें विभिन्न उत्पादन, कृषि, गैर-कृषि आदि शामिल हैं। घरेलू उद्योग पुराना है, लेकिन नई आर्थिक नीतियों ने इसे प्रोत्साहित किया है। कृषि क्षेत्र में बढ़ रही अरुचि और गांवों में रोजगार के सीमित साधनों ने भी इस उद्योग को बढ़ावा दिया है। घरेलू कामगार अधिकतर महिलाएं और लड़कियां ही होती हैं। समाज में एक महिला की भूमिका उसके घरेलू कार्यों से ही आंकी जाती है। उस पर बच्चों की देखभाल और घर परिवार की सेवा का दायित्व होता है। इसलिए भी घरेलू उद्योग उसके अनुकूल रहता है। क्योंकि घर में रहते हुए आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने पर उसके घरेलू, सामाजिक दायित्व ज्यादा प्रभावित नहीं होते। जैसे एक बीड़ी लपेटने वाली महिला अपना काम करते हुए छोटे बच्चे को स्तनपान भी करा सकती है। सामाजिक प्रचलन भी महिला को घर बैठ कर काम करने को बढ़ावा देते हैं।
बीड़ी बनाने का काम दो स्तरों पर होता है। पहले स्तर पर बीड़ी बनाने के लिए तेंदूपत्ता जुटाना होता है, जिससे बीड़ी को आकार दिया जाता है। दूसरे स्तर पर बीड़ी लपेटने और उन पर ‘झिल्ली’ लगाने का काम होता है। इन दोनों कार्यों में पैंसठ से पचहत्तर प्रतिशत स्त्रियां कार्य करती हैं। ये जिन जीवन-दशाओं में रह कर कार्य करती हैं उन्हें निकट से देखने, जानने और अनुभव करने के बाद एक बात साक्ष्यांकित हो जाती है कि स्त्रियों में असीमित सहनशक्ति और परिवार के प्रति समर्पण की भावना होती है। देश में कई ऐसी निजी संस्थाएं हैं, जो तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे श्रमिकों के पक्ष में संघर्षरत हैं। विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर विभिन्न श्रम संगठन इन औरतों के अधिकार के लिए आवाज उठाते रहते हैं।
1991 की जनगणना के अनुसार अकेले मध्यप्रदेश की कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 26.3 प्रतिशत था। तेंदू पत्ता संग्रहण और बीड़ी बनाने के अलावा अगरबत्ती उद्योग में भी महिलाओं की बड़ी संख्या कार्यरत है। अगरबत्ती की मांग लगभग हर घर में होती है। घर बैठी महिलाओं के लिए यह स्वरोजगार के रूप में कमाई का महत्त्वपूर्ण साधन बन चुका है। अगरबत्ती के प्रति पैकेट उत्तमता के अनुसार एक रुपए से लेकर सौ-डेढ़ सौ रुपए तक मिलते हैं। इस काम के लिए किसी विशेष शिक्षा या दक्षता की आवश्यकता नहीं होती। काम करने की ललक ही सबसे बड़े कौशल के रूप में दक्षता दिलाता है। कम पढ़ी-लिखी या अशिक्षित महिलाएं भी अगरबत्ती बनाने के काम में निपुण साबित होती हैं।
अचार, पापड़ और चिप्स आदि बनाने के कार्य में पंचानबे प्रतिशत महिलाएं लगी होती हैं। ये अपने घरेलू दायित्वों के साथ बड़ी कुशलता से काम करती हैं। मसलन, पापड़ उद्योग में महिलाओं को पापड़ के लिए सामग्री दी जाती है। उन्हें घर जाकर सिर्फ बेलना पड़ता है। इस काम में हर महिला एक हजार से तीन हजार रुपए प्रतिमाह तक कमा लेती है। मसालों को साफ कर, पीस कर और पैक करने में जो महिलाएं अपना योगदान करती हैं, वे भी परोक्ष रूप से देश के कुटीर और लघु उद्योग को सुदृढ़ करती हैं।
केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वसहायता समितियों के गठन को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इनके अंतर्गत उन औरतों को एक समूह के रूप में संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो अकेली घर से निकलने, किसी पराए पुरुष से बात करने और घरेलू कार्यों से इतर काम करने से झिझकती हैं। ऐसी औरतें आपस में मिल कर एक-दूसरे का सहारा बनतीं और एक-दूसरे के लिए प्रेरक का काम करती हैं। ये वही औरतें हैं, जो घरेलू स्तर पर मसाला बनाने के व्यवसाय में कामगार की भूमिका निभाती हैं, ये वही औरतें हैं जो अचार और बड़ियां बनाती हैं। ये वही औरतें हैं जो लखनऊ के चिकन का कशीदा, वाराणसी के जरी, जयपुर की रजाइयों और बांधनी में अपना योगदान देती हैं। यों भी सलवार, कमीज, लहंगे-चुन्नी, रेडीमेड कपड़ों आदि सभी पर कढ़ाई का प्रचलन हमेशा रहा है।
मोमबत्ती और टेराकोटा की सजावटी वस्तुएं बनाने के काम में भी घरेलू औरतों का पुरुषों से अधिक प्रतिशत रहता है। बांस, नारियल के रेशे, जूट आदि से उपयोगी सामान बनाने का काम महिलाएं घर बैठे करती हैं और अपने परिवार को आर्थिक मदद करती हैं। बढ़ती महंगाई के जमाने में जितना भी धन कमाया जाए, वह परिवार के गुजारे के लिए अपर्याप्त है। अगर बच्चों को उचित शिक्षा दिलानी है या अपने परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना है तो महिलाओं को आगे आना ही पड़ता है। देश में सामाजिक, पारिवारिक ढांचा और शैक्षिक स्तर अब भी हर महिला को पूर्णरूप से कामकाजी बनने का वातावरण मुहैया नहीं कराता है।
ऐसी स्थिति में अपने पारिवारिक दायित्वों से समय बचा कर, घर में ही काम करते हुए चार पैसे कमाने का रास्ता इन औरतों का सहारा बनता है। इन महिलाओं को भले कामकाजी न कहा जाए या इनके आर्थिक योगदान को रेखांकित नहीं किया जाए फिर भी दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुएं इन्हीं के श्रम और कौशल से निर्मित होती हैं। दरअसल, चाहे सफाई के काम में आने वाली झाडू हो, ड्राइंगरूम को सजाने वाली वस्तु या फैशन की दुनिया में रैंप पर जगमगाते वस्त्रों का रंग और पैटर्न हो, ये सब आर्थिक जगत के हाशिए पर मौजूद इन औरतों का महत्त्वपूर्ण, पर मौन योगदान होता है।