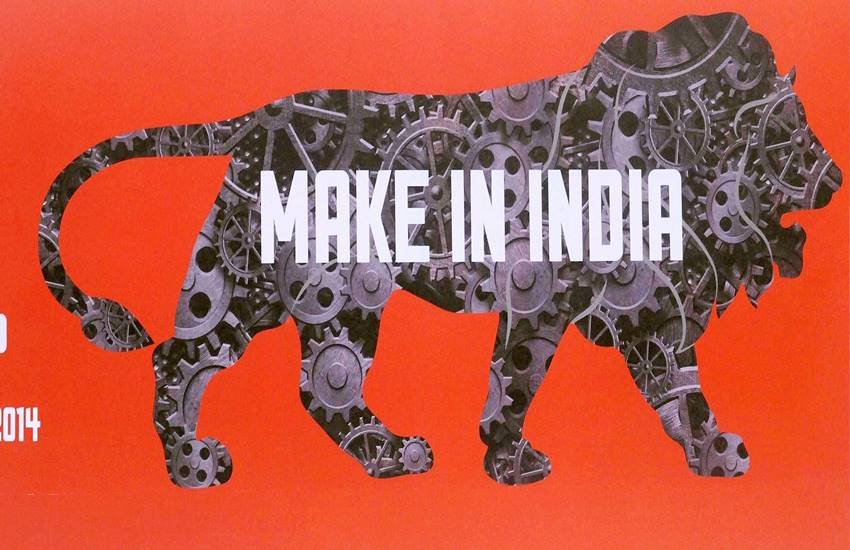कोई भी बड़ा देश उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के बिना समृद्ध नहीं हो सकता जिनकी मांग या खपत वहां के लोगों में होती है। अधिकतर खासकर बुनियादी सेवाएं, सामान्य तकनीक और कम कीमत वाली सेवाएं- हर हाल में देश के भीतर ही पैदा होनी चाहिए। किसी देश के लिए समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ने की खातिर यह जरूरी है कि वह अपने लोगों की जरूरत की चीजें और सेवाएं खुद पैदा करे, उनका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा निर्यात भी करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलकुल सही थे जब उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य मेक इन इंडिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है, और उन्होंने दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का आह्वान किया था कि वे यहां आएं और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भागीदार बनें।
मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा
भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा करीब 16.5 फीसद है। कृषिक्षेत्र का हिस्सा तेजी से कम हुआ है और सेवाक्षेत्र का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। लेकिन जीडीपी में इन दो क्षेत्रों की हिस्सेदारी में हुए बदलाव के बावजूद, मैन्युफैक्चरिंग ने प्रगति की है। सत्तर फीसद मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं और इनमें से एक तिहाई अर्ध-कॉरपोरेट और असंगठित इकाइयां हैं। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा तेजी से बढ़ा है, 1950 के दशक में जहां यह 9.8 फीसद था, वहीं 2010 के दशक में 16.2 फीसद के करीब पहुंच गया। मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ और ऊपर ले जाने का वादा किया था। कोई उत्पाद बनाना और बाजार में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी दखल करना आसान काम नहीं है। हो सकता है कोई या कई व्यक्ति पहले से वही उत्पाद बना रहे हों। हो सकता है उस चीज का आयात भी हो रहा हो। ऐसे में नए उद्यमी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह उस उत्पाद को बेहतर या सस्ता बनाए या उसे उपभोक्ता तक अपेक्षया जल्दी पहुंचाए, या कुछ ऐसी पेशकश करे जो उपभोक्ता की नजर में उसके उत्पाद को अधिक आकर्षक बनाती हो। यहीं पर कई तरह की दिक्कतों से सामना होता है। जमीन की उपलब्धता, श्रम, बिजली, तकनीक, परिवहन, पूंजी की लागत, ऋण की लागत, आदि। इनमें से सारी या कई बाधाएं जब तक दूर नहीं कर दी जातीं, कोई नया उद्यमी हाथ नहीं लगाएगा।
दुनिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्थाएं अपने इस मुकाम तक इसलिए पहुंच सकी हैं क्योंकि दूसरी जगहों के मुकाबले उन्होेंने अपने यहां बुनियादी कारकों को लाभप्रद बनाया, यानी उद्यमी कहीं और जाने के बजाय उनके यहां यूनिट बिठाए तो वह उसके लिए अधिक फायदेमंद साबित हो। यह ‘प्रतिस्पर्धात्मक लाभ’ मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने के इच्छुक देश को मुहैया कराना ही चाहिए। मसलन, कार को लें। पहले बड़े पैमाने पर इनका निर्माण अमेरिका में होता था। जब जर्मनी और जापान बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की पेशकश की, और फिर कार उद्योग ने जर्मनी और जापान का रुख किया। कुछ दशकों बाद, कार उद्योग ने दक्षिण कोरिया को अपना ठिकाना बनाया। दो दशक बाद, कार निर्माण उद्योग का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भारत पहुंच गया। उसका भारत आना आकस्मिक नहीं था। यह एक खूब सोची-विचारी रणनीति के चलते हुआ, जो स्पष्ट नीतियों में भी परिवर्तित हुई। वह कहानी जो 1991-92 में शुरू हुई थी, उसे बताने की गुंजाइश यहां नहीं है।जब मोदी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक वैश्विक केंद्र बनाने का वादा किया, तो मुझे लगा कि जिन बाधाओं को दूर किया जाना है उनके बारे में उन्हें बताया गया होगा- और उन्होंने खुद भी इस बारे में सोचा होगा। मैं यह मानने कातैयार नहीं हूं कि मेक इन इंडिया बस एक और नारा भर था, जिसका मकसद 2015 में स्वाधीनता दिवस पर जमा भारी भीड़ में जोश भरना रहा होगा।
तेज गिरावट
दो साल बाद, ‘मेक इन इंडिया’ की दशा क्या है?
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने स्थिर कीमतों (2011-12) पर मैन्युफैक्चरिंग के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की तिमाही वृद्धि दर के आंकड़े जारी किए हैं। मैंने उन्हें यहां कुल जीवीए के बरक्स रखा है:
2015-16 2016-17 2015-16 2016-17
(मैन्युफैक्चरिंग जीवीए) (कुल जीवीए)
पहली तिमाही 8.2 10.7 7.6 7.6
दूसरी तिमाही 9.3 7.7 8.2 6.8
तीसरी तिमाही 13.2 8.2 7.3 6.्7
चौथी तिमाही 12.7 5.3 8.7 5.6
मेक इन इंडिया की घोषणा 15 अगस्त 2015 को हुई, तब से मैन्युफैक्चरिंग के गति पकड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत, ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग ने अपना जोश-खरोश खो दिया है, और 2016-17 में काफी कमजोर हो गया है। 2016-17 की पहली तिमाही और चौथी तिमाही के बीच, मैन्युफैक्चरिंग जीवीए की वृद्धि दर घट कर आधी हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमजोरी कुल जीवीए की वृद्धि दर की भारी गिरावट में प्रतिबिंबित होती है।
निष्कर्ष यह है कि मेक इन इंडिया की घोषणा को नीतिगत या प्रशासनिक समर्थन बहुत कम मिला है। दूसरे आंकड़े भी इसी निष्कर्ष की तरफ इशारा करते हैं। 2015-16 की चौथी तिमाही से 2016-17 की चौथी तिमाही की पांच तिमाहियों के बीच जीडीपी के अनुपात में कुल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) गिरा है- 30.8, 31.0, 29.4 और 28.5। बारह महीनों में 2.3 फीसद की गिरावट एक संकट की तरह है। इस तथ्य के मद््देनजर कि कुछ ही साल पहले जीएफसीएफ 34-35 फीसद था, और सरकार ने न तो निजी निवेश बढ़ाने के लिए कुछ किया न ही सार्वजनिक निवेश बढ़ाया, यह संकट और बड़ा मालूम पड़ता है।
नाकामी के आंकड़े
आइआइपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) के आंकड़े भी इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं। मई 2014 में यह सूचकांक 183.5 था, अगस्त 2015 में 184.8 और मार्च 2016 में 208.1 था, जो कि फरवरी 2017 में गिर कर 190.1 पर आ गया। ऋणवृद्धि के आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। उद्योग क्षेत्र के लिए ऋणवृद्धि अक्तूबर 2016 से ऋणात्मक रही है। ऋणवृद्धि सूक्ष्म/लघु उद्योगों के लिए मार्च 2016 से और मझोले उद्योगों के लिए जून 2015 से ऋणात्मक रही है। रोजगार सृजन के आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। रोजगार-सृजन वाले आठ प्रमुख उद्योगों ने अप्रैल-सितंबर 2016 के दरम्यान केवल 109,000 रोजगार पैदा किए हैं। यह ठहराव का लक्षण है। बिजली की मांग के आंकड़े भी इसी निष्कर्ष की तरफ इशारा करते हैं। ताप विद्युत संयंत्रों का औसत प्लांट लोड फैक्टर करीब साठ फीसद होना बिजली की कम मांग का परिचायक है। मैंने ‘मेक इन इंडिया’ का स्वागत किया था। यह नवाचारी और महत्त्वाकांक्षी था। ऐसा लगता है कि पहले बहुत मामूली तैयारी की गई थी और बाद में नीतिगत समर्थन व्यावहारिक स्तर पर नहीं मिला। नतीजतन, ‘मेक इन इंडिया’ एक खोखला नारा होकर रह गया है। .