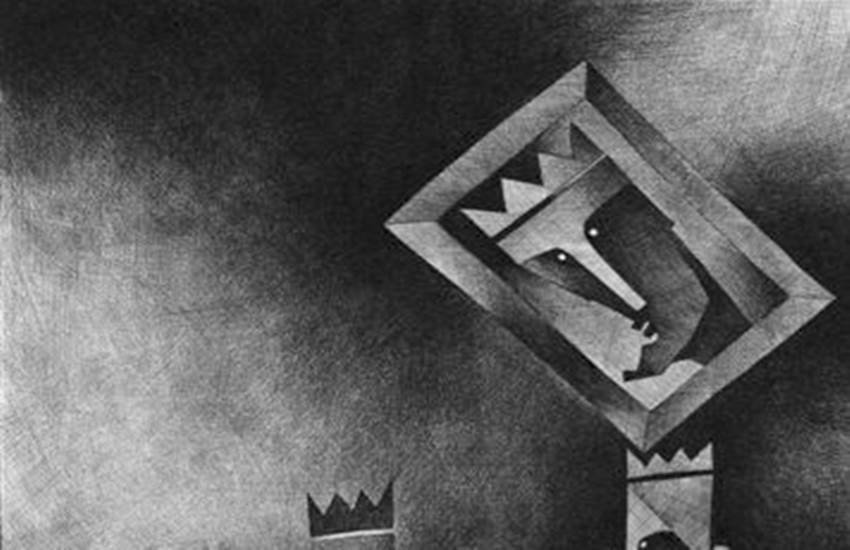साहित्य के संदर्भ में प्रासंगिकता का सवाल बार-बार उठाया जाता है और प्राय: इस तरह कि वही साहित्य श्रेष्ठ होगा, जो प्रासंगिक होगा। यानी, प्रासंगिकता वह कसौटी है, जिसके आधार पर किसी रचना या रचनाकार को कमतर या महत्त्वपूर्ण साबित किया जाता है। पूर्ववर्ती रचनाकारों के मूल्यांकन में तो इसका खूब उपयोग किया जाता है। यह साबित करने के लिए जी-जान लगा दिया जाता है कि अमुक रचनाकार आज भी उतना ही प्रासंगिक है और इसलिए वह महत्त्वपूर्ण है। जबकि अभिव्यक्ति के दूसरे रूपों- ललित कला, मूर्तिकला, नृत्य संगीत आदि में प्रासंगिकता कोई कसौटी नहीं है।
प्रश्न है कि प्रासंगिकता क्या कोई साहित्यिक कसौटी है या साहित्य का स्वभाव? जैसे प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य स्वभावत: प्रगतिशील होता है, क्या हम उसी तरह नहीं कह सकते कि साहित्य स्वभावत: प्रासंगिक होता है। यह बात बहुत हद तक ठीक है। जैसे प्रगतिशीलता साहित्य का अलग से कोई मानदंड नहीं हो सकती वैसे ही प्रासंगिकता भी। दरअसल, स्थायीत्व एक प्रमुख भेदक लक्षण है, जिसके द्वारा उसे विज्ञान या समाज विज्ञान से अलगाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में एक विषय पर नए तथ्यों के आलोक में दूसरी पुस्तक आ जाने पर पहली का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। पर, साहित्य में ऐसा नहीं होता।
वाल्मीकि, भावभूति, तुलसीदास, केशव, मैथिलीशरण गुप्त आदि द्वारा रामकथा को आधार बना कर लिखे गए सभी काव्यों का महत्त्व कायम है। इसी तरह, ‘राम की शक्ति पूजा’ का अपना महत्त्व है तो ‘संशय की एक रात’ का अपना। एक ही विषय पर बीसों रचनाएं लिखीं जा सकती हैं और सभी महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं। रचना के महत्त्वपूर्ण होने में विषय से अधिक योगदान रचनाकार का होता है। साहित्य की उत्कृष्टता विषय सापेक्ष नहीं, बल्कि विषय निरपेक्ष होती है और होनी भी चाहिए। अगर विषय ही साहित्यिक उत्कृष्टता का निर्णायक तत्त्व होता तो फिर सारी श्रेष्ठ रचनाएं एक ही विषय पर होनी चाहिए थीं। जाहिर है, ऐसा नहीं है।
साहित्यिक से लेकर अकादमिक गोष्ठियों तक में यह सुन कर बहुत कोफ्त होती है कि अमुक रचना इसलिए अच्छी है कि वह किसानों पर है, यह कहानी इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें एक स्त्री का संघर्ष है, इस उपन्यास की महत्ता इस बात में है कि यह ‘लिव इन’ पर लिखा गया है, आदि। ठीक ऐसे ही कहा जाता है कि प्रेमचंद इसलिए महान हैं कि उन्होंने गांवों, किसानों की समस्याओं आदि पर लिखा। अब इन विद्वानों को कौन समझाए कि रचना ऐसे विषयगत कारणों से कभी महत्त्वपूर्ण नहीं होती है।
एक गोष्ठी में एक पार्टीबद्ध कामरेड आलोचक ने बोलते हुए प्रेमचंद के समय के वे सारे आंकड़े गिनाए, जिनसे उस दौर में किसानों के दोहरे-तिहरे शोषण को प्रमाणित किया जा सके। इस तरह उन्होंने आंकड़े दे-दे कर प्रेमचंद का साहित्यिक मूल्यांकन किया। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए नामवर सिंह ने कहा कि ‘आंकड़े जुटाना पटवारियों का काम है और प्रेमचंद साहित्य के पटवारी नहीं थे। आलोचक को साहित्य के मर्म को पकड़ना चाहिए।’ उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण बात कही थी। इस बात की सर्वाधिक पुष्टि रामचंद्र शुक्ल के आलोचना कर्म से होती है।
विषय के आधार पर रचना को उत्कृष्ट या निकृष्ट बताने के मूल में प्रासंगिकता ही आलोचकीय मानदंड है। इस मानदंड को व्यापक स्वीकृति मिली, क्योंकि इसने आलोचना का काम एकदम आसान कर दिया। यह एक ऐसा अचूक फार्मूला बन गया, जिससे जटिल से जटिल रचना पर पलक झपकते मूल्य निर्णय दिया जाने लगा। समकालीन रचना हो या पूर्ववर्ती, आलोचक सिर्फ इतना देखता है कि उसमें जिन मुद्दों को उठाया गया है उनका हमारे समय की समस्याओं से रिश्ता है या नहीं। अगर है तो रचना उत्कृष्ट, नहीं है तो निकृष्ट। अब रचना के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। आलोचना की यह स्थिति राजनीतिक कार्यकर्तानुमा समीक्षकों और आलोचकों के लिए बहुत उर्वर साबित हुई।
प्रासंगिकता का सवाल साहित्य और समाज के संबंध का सवाल नहीं है। यह साहित्य की सामाजिक उपयोगिता का सवाल है। यह एक तरह से साहित्य को समाज और राजनीति के लिए उपयोगी उत्पाद में बदल देने की सुनियोजित परियोजना का हिस्सा है। साहित्य का इससे हीनतर उपयोग और कुछ नहीं हो सकता कि वह राजनीति के लिए उपयोग की वस्तु बन जाए। आजादी के बाद का हिंदी साहित्य का इतिहास इस बात का गवाह है कि न जाने कितनी महत्त्वपूर्ण कृतियों को सिर्फ राजनीतिक रूप से प्रासंगिक न होने के कारण खारिज कर दिया गया। क्या कोई कह सकता है कि ‘मैला आंचल’ में समाज नहीं है या वह समाज निरपेक्ष रचना है?
फिर, मार्क्सवादी आलोचना ने उसे खारिज क्यों किया? इसीलिए इस बात को जोर देकर रेखांकित करने की जरूरत है कि प्रासंगिकता का प्रश्न और कुछ नहीं, बल्कि पोलिटिकली करेक्टनेस का सवाल है। हाल के वर्षों में विमर्शों ने साहित्य में लगभग वही स्थान प्राप्त कर लिया है, जो पहले विचारधारा को प्राप्त था। पहले प्रासंगिकता का मतलब मार्क्सवादी विचारधारा के लिए प्रासंगिक होना था, अब इसका मतलब विमर्शों के लिए प्रासंगिक होना है। विचारधारा आधारित आलोचना और विमर्श आधारित आलोचना दोनों ने ही प्रासंगिकता को एक मानदंड के रूप में स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट है कि दोनों के लिए साहित्य उनकी परियोजना का उपकरण मात्र है।
प्रासंगिकता के संदर्भ में सबसे दिलचस्प स्थिति यह है कि जब किसी रचना या रचनाकार (खासकर पूर्ववर्ती) को प्रासंगिकता के आधार पर महान बताया जाता है, तो उस पूरी प्रक्रिया से रचना या रचनाकार का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं होता। सब कुछ सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। यानी, प्रासंगिकता का मानदंड रचना या रचनाकार सापेक्ष नहीं, बल्कि समाज सापेक्ष होता है। इसलिए प्रासंगिकता एक गैर-साहित्यिक मानदंड है, जिससे साहित्य का मूल्यांकन करना खतरे से खाली नहीं है। इससे विशुद्ध सामाजिक और राजनीतिक कारणों से साहित्य के मूल्यांकन का बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। नई सामाजिक शक्तियों- दलित, पिछड़े, आदिवासी, स्त्री आदि- के उत्थान के कारण पैदा हुए अस्मितामूलक विमर्शों के इस दौर में यही हो रहा है।
सबसे बड़ी बात यह कि प्रासंगिकता दुधारी तलवार है। किसी सामाजिक-राजनीतिक परिवेश विशेष में किसी रचना या रचनाकार को प्रासंगिकता के कारण महत्त्वपूर्ण मान लिया जाता है तो यह भी खूब संभव है कि वर्षों बाद सामाजिक-राजनीतिक परिवेश बदलने के बाद वह महत्त्वहीन हो जाए और जो रचनाकार प्रासंगिकता की कसौटी पर खारिज किए गए हों वे बदली परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण हो जाएं। एक समय में कोई रचनाकार प्रासंगिकता के कारण महत्त्वपूर्ण है तो समय बदलते ही वह महत्त्वहीन हो जाएगा। यही बात रचना पर भी लागू होती है। इसलिए, साहित्य के लिए सामाजिक-राजनीतिक प्रासंगिकता का सवाल गैरजरूरी है।
शेक्सपियर, तुलसीदास, प्रेमचंद आदि प्रासंगिकता के कारण महान नहीं हैं। जिन लोगों को गांव, किसान आदि से कोई मतलब नहीं होता वे भी प्रेमचंद को पढ़ते हैं। रवींद्रनाथ ने जो लिखा वह कितना प्रासंगिक है? क्या शरतचंद को इसलिए पढ़ा जाता है कि वे प्रासंगिक हैं?
साहित्य की प्रासंगिकता बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर निहित है। कोई भी श्रेष्ठ रचना हमारी संवेदना से जुड़ती है। जीवन के गहरे मर्म को पकड़ती है। अंदर के तारों को झंकृत करती है। भीतर ही भीतर ऐसा कुछ घटित होता है कि हमारा उससे एक गहरा आत्मीय रिश्ता बन जाता है। ऐसा साहित्य हमेशा प्रासंगिक रहेगा और महत्त्वपूर्ण भी। यह साहित्य की आंतरिक प्रासंगिकता है, जो प्रत्येक अच्छी रचना में होती ही है। अच्छी रचना इस लिहाज से स्वभावत: प्रासंगिक होती है।