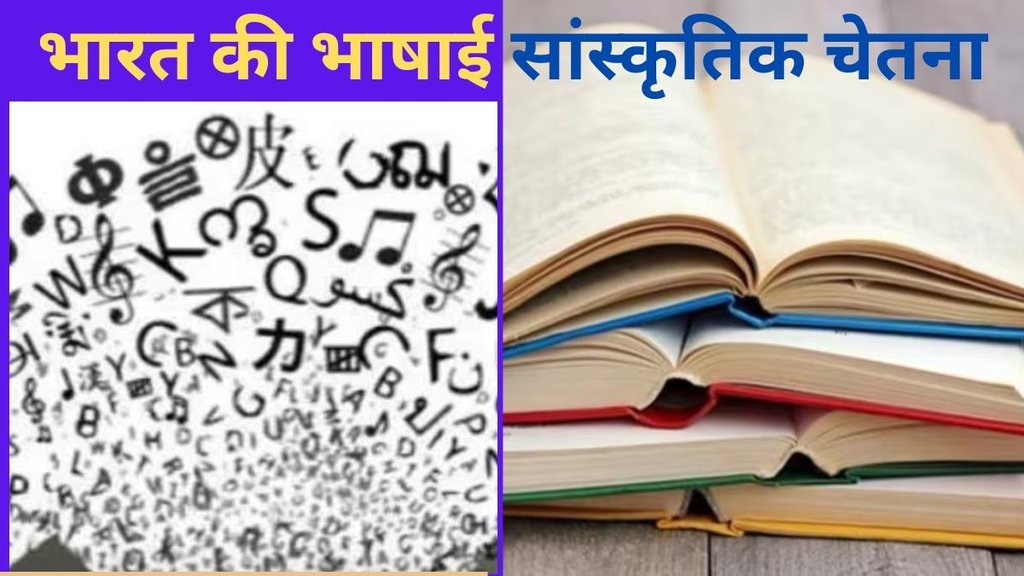उदय नारायण सिंह
भारतीय सभ्यता में कला, संगीत, नृत्य, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन में शास्त्रीयतावाद की एक महान परंपरा रही है, जिनमें से सभी ने एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में यहां भाषाओं पर अपनी पहचान छोड़ी है। शास्त्रीयतावाद समाज में सांस्कृतिक, बौद्धिक और कलात्मकता के बारे में एक स्पष्ट समझ बनाती है। केंद्र सरकार की ‘शास्त्रीय भाषाओं’ की घोषणा भी उसी कड़ी का हिस्सा है। भारत जैसे बहुजातीय, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में प्राय: हम संस्कृत की एकात्म परंपरा मानते रहे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि संस्कृत और प्राकृत के विभिन्न रूप एक-दूसरे के साथ-साथ चलते रहे और एक-दूसरे को समृद्ध भी करते रहे।
इस क्रम में एमबी एमेन्यू (1958) के शोध से ‘भारत एक भाषाई भू-क्षेत्र’ की धारणा मिलती है, जो दर्शाती है कि कई हजार वर्षों के साथ रहने से भारोपीय और द्रविड़ परंपराएं इतनी समृद्ध हुई हैं कि इसका प्रभाव भाषा-संरचना, शब्द-निर्माण, यहां तक कि ध्वनि-व्यवस्था पर देखा जा सकता है। संस्कृत और तमिल की तरह पालि और प्राकृत को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद कई गैरजरूरी आलोचनाएं हो रही हैं।
प्राकृत और संस्कृत की साझी विरासत
“प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि किस प्राकृत को मान्यता दी जा रही है। हम भूल रहे हैं कि प्राकृत और संस्कृत परंपराओं की पिछले चार हजार वर्षों की साझा विरासत रही है। संस्कृत नाटकों में आम आदमी की भाषा के रूप में प्राकृत का इस्तेमाल एक सामान्य प्रचलन था। इसके साथ ही, गाने अक्सर महाराष्ट्रीय प्राकृत में रचे जाते थे। अशोक के शिलालेखों में स्थानीय लोगों से संवाद करने के लिए अलग-अलग प्राकृत का इस्तेमाल किया गया है।”
प्राकृत-पालि और सांस्कृतिक संवाद
“ध्यान रहे कि वेदों, उपनिषदों और संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य ईश्वर को संबोधित करने का प्रयास करता दिखता था, लेकिन पालि और प्राकृत परंपराओं में व्यक्ति स्वयं से भी मुखातिब होता है और नायक स्वयं से भी तर्क करता है, जिनमें कई गूढ़ दार्शनिक मुद्दे सामने आते हैं। पालि का उपयोग बुद्ध के अनुयायियों द्वारा किया गया था, जहां ग्रीक वाली तार्किकता की तरह मुख्य ध्यान मनुष्य के स्वयं के साथ संवाद पर था। कमोबेश यह स्थिति पालि परंपरा में भी सामने आती है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के भाषण, कथन, प्रवचन और वार्तालाप मौखिक रूप से पीढ़ियों तक प्रसारित हुए और बाद में कुछ बौद्ध परिषदों द्वारा उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस करने के बाद ग्रंथों (सुत्त, धम्म और अभिधम्म) में लिखे गए। कुछ लोग इसे पूर्वी प्राकृत का एक रूप मागधी से जोड़ते हैं, वह इसलिए भी क्योंकि बुद्ध ने इसी क्षेत्र में अपना निर्वाण प्राप्त किया था।”
अशोक के समय में पालि का प्रचार और विस्तार
“पालि उस समय जंगल में आग की तरह फैली, जब सम्राट अशोक ने अपने बेटे महिंदा को ‘सद्धम्म’ सिखाने के लिए सीलोन (आधुनिक श्रीलंका) भेजा। पालि की तरह दर्शन, इतिहास, व्याकरण और विभिन्न गद्य और काव्य प्राकृत के बोले गए रूपों में भी सामने आए। प्राकृत के विभिन्न रूप थे, जिनमें महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अवंती शामिल हैं, जिनका प्रयोग नाटक और गीत काव्य में किया जाता था। कहने का तात्पर्य यह कि संस्कृत की तरह, प्राकृत की भी अपनी शास्त्रीय परंपरा थी, जिस पर अब व्यापक शोध हेतु नई ऊर्जा मिलेगी।”
शास्त्रीय भाषा का दर्जा और इसकी विशेषताएं
“शास्त्रीय भाषाओं की पहचान और घोषणा की शुरुआत 2004 में एक भाषाई विशेषज्ञ समिति की स्थापना के साथ हुई थी। बाद में समिति का विस्तार करके कई प्रतिष्ठित भाषाविदों और शिक्षाविदों को शामिल किया गया। वर्ष 2004 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शास्त्रीय विद्वानों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद हम जिस मापदंड पर पहुंचे थे, उसके चार मुख्य बिंदु थे: प्रारंभिक ग्रंथों/ लिखित इतिहास की प्राचीनता 1500 से 2000 वर्ष से अधिक हो, प्राचीन साहित्य/ ग्रंथों का एक समूह, जिसे एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो, संबंधित भाषा में साहित्यिक परंपरा मूल हो और दूसरों से उधार नहीं ली गई हो, और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक से अलग है, जहां शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक सातत्य-विच्छेद भी हो सकता है।”
खैर, वर्ष 2005 में भी, विशेषज्ञों की समिति ने पालि और प्राकृत की शास्त्रीय भाषा के दर्जे की सिफारिश की थी, क्योंकि पालि भगवान बुद्ध (563 ईसा पूर्व-483 ईसा पूर्व) के भाषणों, कथनों, प्रवचनों और बातचीत की भाषा थी, जिसे शुरू में मौखिक रूप से संरक्षित किया गया था, और बाद में सुत्त, विनय और अभिधम्म के रूप में लिखित रूप में दर्ज किया गया, जिससे तिपिटक का निर्माण हुआ, और प्राकृत (एक रूप) जिसका उपयोग तीर्थंकर महावीर (599-527 ईसा पूर्व) के कारण विकसित ग्रंथों के लिए किया गया था।
यह विशुद्ध औपनिवेशिक मानसिकता है, जो यह मानती है कि सिर्फ चीनी, संस्कृत, अरबी, ग्रीक और लैटिन ही ‘शास्त्रीय’ हैं। जबकि आज ऐसे मिथकों को तोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया से नए पुरातात्त्विक साक्ष्य सामने आने लगे हैं, जो अपने आयामों में अनेक प्राचीन सभ्यताओं को सत्यापित करते हैं। यह मामला सिर्फ काप्टिक, मिस्र, सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन, हिब्रू, फारसी, तमिल, पालि और सीरियाई को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का नहीं है, बल्कि यह भी विचार करने का है कि अनेक महत्त्वपूर्ण भाषाओं को इस परिधि में शामिल करने से छोड़ दिया गया है।
इन परंपराओं का अध्ययन करने के लिए समर्पित विद्वान चुपचाप काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजी वर्चस्व के विद्वानों की उपेक्षाओं के बीच न्यूनतम सरकारी संरक्षण के साथ शोधरत हैं। जहां तक इस सूची में बांग्ला, असमिया और मराठी का सवाल है, तो उन्हें यह दर्जा देने के लिए कई नए सबूत और तर्क सामने आए हैं, जिसकी वे हकदार हैं। कहने का आशय यह कि भाषाओं को शास्त्रीयता का यह दर्जा नए तरह के शोधों को बढ़ावा देगा।