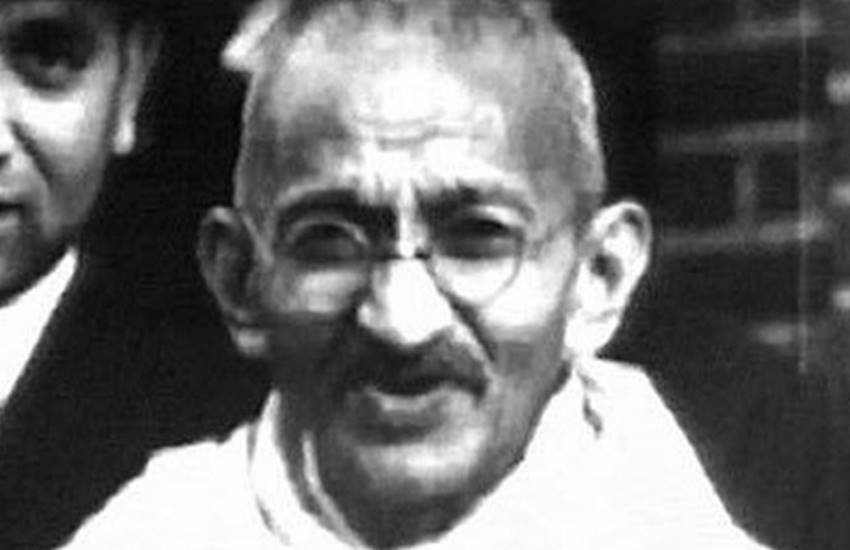व्यक्ति ही विशेष है। वही समाज को बनाता है। उसी से संवाद संभव है और संवाद एक निश्चिंत और विश्वासपूर्ण वातावरण में ही पनपता है। निश्चिंत वातावरण के लिए हर व्यक्ति के अधिकार और मौलिक जरूरतों को पूरी करना समाज का पहला और आखिरी कर्तव्य है।
जिंदगी में अगर सभी चीजें सलीके से सजी हों, अपने-अपने खांचे में फिट हों, तो कितना अच्छा लगता है। शायद यह फिट करने वाली प्रवृत्ति है, जो हमें बार-बार किसी भी सोच, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थिति या संबंध को उसकी मौलिक अवस्था में ग्रहण नहीं करने देती। हम उसके रूबरू होते ही अपने पहले से तैयार खांचे निकाल लेते हैं और उनमें इनको फिट करने में लग जाते हैं। खांचे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अगर फिट हो गए तो ठीक, वरना फिर समस्या हो जाती है। ज्यादातर खांचे हमें विरासत में मिले होते हैं। लंबे उपयोग की वजह से कुछ लचीले जरूर हो जाते हैं, पर रहते खांचे ही हैं। इनसे ही हम शुरुआत करते हैं और फिर परिवेश और सोहबत के हिसाब से अपने-अपने खांचे में घुस लेते हैं। हर चीज को इसी में फिट होना है। जिंदगी जीने का सलीका शायद इसी को कहते हैं। खांचे जरूरी हैं। समाज की संरचना इन्हीं के बल पर होती है। व्यक्ति भी इन्हीं में ढलता है। अच्छा व्यक्तित्व किसी परिचित खांचे में सफाई से ढला पुरुष है। उसी की वाह-वाह है; उससे मिल कर हम आश्वस्त होते हैं। खांचा भरोसा दिलाता है कि मानव प्रकृति को हम अपने अनुसार फिट कर सकते हैं, यानी पुरुष प्रकृति को विवश कर सकता है। उसको अपने अनुसार तोड़-मरोड़ सकता है। चौकोर छेद में चौकोर और गोल में गोल फिट करके आराम से सांस ले सकता है। सुव्यवस्थित मानव संरचना ही शायद हमारा पहला और आखिरी जीवन लक्ष्य है। उसी के लिए हम मरे जाते हैं।
खांचे बनाना हर समाज के लिए सरल है। उन पर अभिभूत होना भी लाजमी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब पेश आती है जब समाज और व्यक्ति खांचों में ही उलझ कर रह जाता है, उन्हीं में अपने को सीमित कर लेता है और नए सांचे ढालना भूल जाता है। न जाने कितने समाजों की दुर्दशा सिर्फ इस वजह से हुई है कि वे हर जन को कभी वर्ण, कभी वर्ग या धर्म और लिंग के खांचे में खोंसने में जुट गए थे।
सार्वजनिक जीवन भी इसी कारण दूषित हुआ है। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो हमारे खिलाफ हो की मानसिकता इन खांचों का नमूना है। ऐसी स्थिति में संवाद की जगह विवाद ले लेता है और फिर विवाद हिंसा में तब्दील हो जाता है। हिंसा किसी विवाद का अंत नहीं, बल्कि नए विवाद की शुरुआत है। राजनीति संवाद से होती है, अपने और दूसरों के बंधन काटने या फिर लांघने से होती है, न कि कट््टरता और असहिष्णुता से। पर राजनीति जब खांचों में फंस जाए तो वह दुर्भाग्य से ग्रस्त होगी ही। हर-जीत में हार निश्चित है। पर अगर हम मानव इतिहास उठा कर देखें, खासकर कलात्मक सृजन पर गौर करें, तो देखेंगे कि हमारा समाज तभी आगे बढ़ा है जब खांचों को अलग रख कर सांचों का नवनिर्माण हुआ है। बाल्मीकि रामायण इसका सबसे पुराना उदाहरण है। आदि कवि वाल्मीकि ने श्रीराम का सांचा गढ़ा, जो उस जमाने के खांचों से एकदम अलग था। दशरथ चाहे जैसे भी राजा या पिता थे, पर राम से एकदम अलग थे। राम आदर्श पुत्र, पति, वनवासी और शूरवीर राजा थे। मर्यादा का संदेश उनके व्यक्तित्व में निहित था। वे पुरुषोत्तम थे। वाल्मीकि ने सिर्फ राम का पूजनीय सांचा नहीं बनाया, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, जैसे कई जीवंत किरदार दिए, जिनके सांचे से खांचे बने और समाज को व्यवस्थित होने की दिशा मिली।
राम ने सभी से संवाद किया, चाहे वह केवट हो, हनुमान हो, बालि, सुग्रीव या फिर रावण का भाई विभीषण। इसी संवाद से आर्य संस्कृति को वे अरण्य के अंतिम छोर तक ले गए और वनवासी, वानर, रीछ, भालू से लेकर राक्षसों तक को अयोध्या की डोर से बांधा। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी और इसी कारण वे युगपुरुष माने गए हैं। राम के बाद श्रीकृष्ण का जन्म हुआ और उनका सांचा आदर्श पुरुषोत्तम राम से एकदम अलग था। राम अगर करीने से सजाया हुआ बाग थे, जिसमें सारे पेड़-पौधे सोच-समझ कर लगाए गए थे और जिसमें हर क्यारी विशिष्ट थी, तो कृष्ण प्राकृतिक रूप से उगा घना जंगल थे। यह जंगल अगर मोहक था, तो भयावह भी। कहीं अगर सूर्य का प्रकाश था, तो कहीं पताल का घुप्प अंधेरा भी। कृष्ण के जंगल में प्रकृति को समझ कर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। इस रास्ते की खोज ही कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। यशोदानंदन, माखनचोर, राधा के श्याम, नटवर नागर से होते हुए श्रीमदभगवतगीता के कर्म-ज्ञानयोगी द्वारकाधीश तक का उनका सफर इसी अव्यवस्थित जंगल के जरिए है। श्रीकृष्ण अपने देश और काल के नए सांचे की मिसाल हैं।
बुद्ध, महावीर, नानक और गांधी कुछ ऐसे सांचे हैं, जिन्होंने अपने समय के खांचों को नए रूप में ढाला। इन्हीं विशिष्ट युगपुरुषों की वजह से ही हम धर्म, संस्कृति, लोकनीति और जीवन दर्शन में आगे बढ़े, पनपे। इनके साथ असंख्य नाम ऐसे हैं, जिन्होंने समाज और शासन में प्रतिकूल माहौल होने के बावजूद अपने को पूर्वनिर्धारित खांचों में नहीं फिट किया और अपनी अलग पहचान की छाप छोड़ी है।
दरअसल, व्यक्ति ही विशेष है। वही समाज को बनाता है। उसी से संवाद संभव है और संवाद एक निश्चिंत और विश्वासपूर्ण वातावरण में ही पनपता है। निश्चिंत वातावरणके लिए हर व्यक्ति के अधिकार और मौलिक जरूरतों को पूरी करना समाज का पहला और आखिरी कर्तव्य है। उनका हनन सामाजिक अपराध ही नहीं, बल्कि सामाजिक पाप है।
दुर्भाग्यवश, समाज और उसके नायक अक्सर खुद को और बाकी सबको खांचों में फिट करके ही अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। राजकाज अमूमन खांचों पर ही चलता है और राजा इन खांचों को और सुशोभन बनाने में अपनी सफलता मानता है। ऐसे में व्यक्ति और समाज दोनों शीतल हो जाते हैं और धीरे-धीरे गलने लगते हैं। समाज कुछ वक्त के लिए शांत और स्थिर जरूर प्रतीत होता है, पर जल्दी ही घातक परिणाम सामने आने लगते हैं। राम और कृष्ण, बुद्ध और गांधी, राज-समाज के बावजूद पैदा होंगे और अपना प्रभाव छोड़ेंगे। इससे राजा अपनी जिम्मेदारी से नहीं छूट जाता; उसको ऐसा माहौल और व्यवस्था देनी ही होगी, जिससे खांचे कम से कम होते जाएं और नाना प्रकार के सांचे सामान्य जिंदगी का दस्तूर बन जाएं।