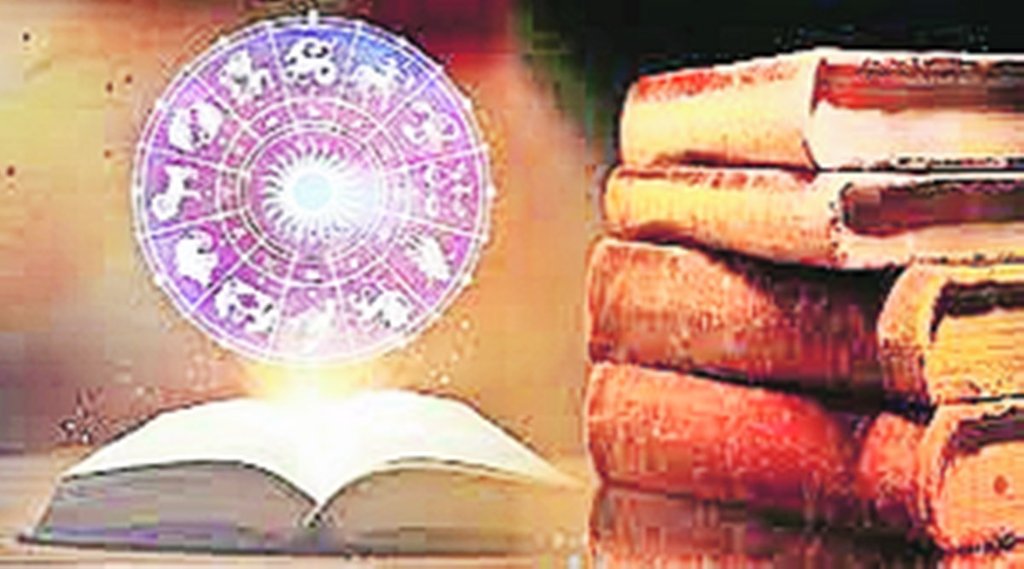शास्त्री कोसलेन्द्रदास
अस्पृश्यता यानी छुआछूत धर्म का हिस्सा है? क्या शास्त्रों की व्यवस्था ने किसी व्यक्ति को अछूत माना है? प्राय: यह प्रश्न उठाया जाता है। ध्यान देने की बात है कि सनातन वैदिक धर्म में पांचवें वेद के रूप में मान्यताप्राप्त महाभारत में महर्षि वेदव्यास का कथन है कि धरती पर मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। वह ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। इसका कारण है कि मनुष्य धर्म और अधर्म को जानकर अपने आचरण का निर्धारण करता है। मनुष्य के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए उसके सामने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, जो उसे सही और गलत का भेद बताते हैं। इन ग्रंथों में अस्पृश्यता कहीं नहीं है। कोई व्यक्ति अछूत नहीं है। यहां तक कि रामायण पढ़ने और सुनने का अधिकार हरेक वर्ण के व्यक्ति को है।
वैदिक धर्म है उदार और सहिष्णु
वैदिक धर्म प्रारंभ से ही अति उदार एवं सहिष्णु रहा है, इसमें शांतिपूर्ण एवं बेरोक-टोक धर्म-व्यवहार होता है। धर्म किसी संप्रदाय या मत का द्योतक नहीं है, प्रत्युत वह मनुष्य के संपूर्ण जीवन का ढंग या आचरण-संहिता है, जो समाज के किसी अंग एवं व्यक्ति के रूप में मनुष्य के कर्मों एवं कृत्यों को व्यवस्थापित करता है। मानव में क्रमश: विकास लाता हुआ उसे मानवीय अस्तित्व के लक्ष्य तक पहुंचने के योग्य बनाता है।
धर्म के भेद
धर्म को दो भागों में बांटा गया है – श्रौत एवं स्मार्त। श्रौत धर्म में उन कृत्यों एवं संस्कारों का समावेश होता है, जिनका प्रमुख संबंध वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मण-ग्रंथों से था, जैसे – तीन पवित्र अग्नियों की प्रतिष्ठा और पूर्णिमा एवं अमावस्या के यज्ञ आदि। स्मार्त धर्म में उन विषयों का समावेश था जो विशेषत: स्मृतियों में वर्णित हैं तथा वर्ण और आश्रम से संबंधित हैं।
कुछ ग्रन्थों में धर्म को श्रौत (वैदिक), स्मार्त (स्मृतियों पर आधारित) एवं शिष्टाचार (शिष्ट या भले लोगों के आचार-व्यवहार) नामक भागों में बांटा गया है। महाभारत का कथन है कि वेदों एवं स्मृतियों में कही गई बात और शिष्ट लोगों द्वारा आचरित व्यवहार धर्म है। याज्ञवल्क्य स्मृति में एक विभाजन के अनुसार धर्म के छह प्रकार हैं – वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, नैमित्तिक धर्म एवं साधारण धर्म। धर्म के विधान को जानने के लिए ऋषियों ने कई धर्मसूत्रों का प्रणयन किया है। विद्यमान धर्मसूत्रों में 28 अध्यायों में विभक्त गौतम-धर्मसूत्र सबसे पुराना है।
घृणा और विद्वेष
वैदिक शब्दों एवं नामों में कहीं भी ऐसे संकेत नहीं मिलते जो अस्पृश्य जातियों के द्योतक हों। अस्पृश्यता केवल जन्म से ही उत्पन्न नहीं होती, इसके उद्गम के दूसरे कई स्रोत हैं। भयंकर पापों अर्थात दुष्कर्म करने वाले लोग जाति निष्कासित एवं अस्पृश्य कर दिए जाते थे। अस्पृश्यता उत्पन्न होने का दूसरा स्रोत है, धर्मसंबंधी घृणा और परस्पर विद्वेष। तीसरा कारण है कुछ लोगों का कुछ विशेष व्यवसायों को पालन करना, जैसे शराब बेचने वाले को स्पर्श करने से लोग बचते थे। चौथा कारण है कुछ परिस्थितियों में पड़ जाना, यथा-शव का स्पर्श करने पर।
जात-पात पूछै नहिं कोई
अस्पृश्य शब्द का पहले-पहल प्रयोग विष्णुधर्मसूत्र एवं कात्यायन ने किया है। प्राचीन धर्मसूत्रों में केवल चांडाल को ही अस्पृश्य माना गया है। मनुस्मृति के मत से भी श्मशन में शवदाहक चांडाल ही अस्पृश्य है। कालांतर में सामाजिक विभेद बढ़ने पर संभवत: अस्पृश्यता बढ़ी होगी, जो भक्ति के धरातल पर वर्जित हो गई। यही कारण रहा है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में स्वामी रामानंद के शिष्यों में कोई जाति, वर्ग एवं लिंगभेद नहीं था। उनके भक्ति संप्रदाय में अनंतानंद, कबीर, रविदास, धन्ना, सैना, पीपा और पद्मावती तथा सुरसरि जैसे भक्तों के नाम हैं