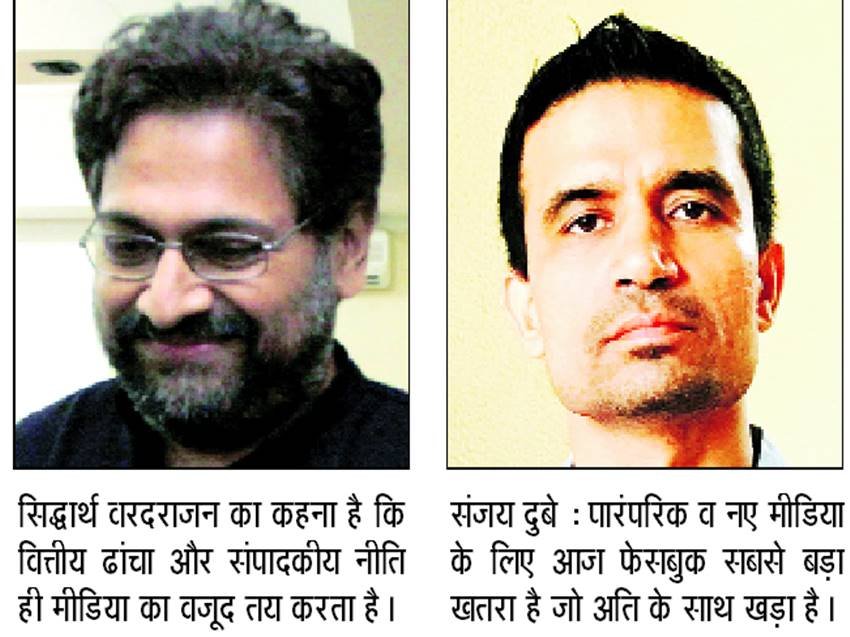आॅनलाइन मीडिया पर जब आप किसी खास वेबसाइट की खबर को पढ़ रहे होते हैं तो रिपोर्ट या लेख के अंत में पाठकों की प्रतिक्रिया मांगी जाती है और इसके साथ ही अपील होती है, ‘हम एक गैर लाभकारी संगठन हैं। हमारी पत्रकारिता को सरकार और कारपोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें’। बड़े मीडिया घरानों के बरक्स सहभागिता के आधार पर स्वतंत्र मीडिया समूह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यधारा की सत्ता सापेक्ष पत्रकारिता के सवाल पर ‘द वायर’ के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन कहते हैं, ‘मैं समझता हूं कि पहली दफा हम लोकतांत्रिक देश में देख रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पक्ष में अपना फर्ज निभा रहा है। खासकर टीवी चैनल सरकार की बातों का माउथपीस बन गए हैं। और शायद इसका कारण यही दिख रहा है कि मीडिया के मालिक सरकार के पक्ष में उसकी विचारधारा के प्रसार में अपना फायदा देख रहे हैं। उनके कारोबारी हित सत्ता की साझीदारी से ही पूरे हो सकते हैं इसलिए सभी बड़े मीडिया समूह सरकार के सुर में बोल रहे हैं। इस प्रवृत्ति के खिलाफ सोशल मीडिया एक उम्मीद जगाता है जहां आम नागरिक अपना नजरिया रखते हैं। इस मीडिया की भूमिका पर चर्चा हो, विश्लेषण हो जो हो भी रहा है। और मीडिया की प्रवृत्तियां जब कारोबार तय करता है तो फिर इसका इलाज उस कारोबार से अलगाव ही होगा। आज हमारे जैसे बहुत से स्वतंत्र समूह कंपनियों और इश्तहारों की मदद के बिना काम कर रहे हैं। वर्चस्ववादी मीडिया के बरक्स छोटे समूहों में लोग काम कर रहे हैं, आम लोगों के अनुदान पर चल रहे हैं और अपनी साख बना रहे हैं’।
जिन प्रवृत्तियों ने मुख्यधारा और पारंपरिक मीडिया को सत्ता और बाजार का भोंपू बना कर रख दिया वही प्रवृत्ति नए मीडिया के भी बड़े हिस्से में तेजी से उभर रही है। इस खतरे को लेकर सवाल के जवाब में वरदराजन कहते हैं कि हाल के कुछ ताजा उदाहरण सचमुच परेशान करने वाले हैं। नया मीडिया भी इश्तहारों के माध्यम से चलने की कोशिश कर रहा है। यहां भी ‘क्लिक’ आधारित प्रवृत्ति बढ़ रही है। नए मीडिया के भी खराब राह पर चलने की शुरुआत हो चुकी है। चाहे पारंपरिक मीडिया हो या नया मीडिया, उसका वित्तीय ढांचा और उसकी संपादकीय नीति ही उसका वजूद तय कर सकते हैं। आप तकनीक का कैसे और किनके लिए व किन संसाधनों के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है।
वहीं वेबसाइट ‘सत्याग्रह’ के संस्थापक संजय दुबे कहते हैं, ‘आज हर तरह के मीडिया की हालत खराब है। नए मीडिया ने अपनी प्रवृत्तियों से पारंपरिक मीडिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब पारंपरिक मीडिया में अलग से लोग नहीं हैं कि वेबसाइट पर कौन लिखेगा। अब तो पारंपरिक मीडिया भी फेसबुक के हिसाब से चलने लगा है। फेसबुक की लाइक और डिसलाइक पारंपरिक मीडिया का विषयवस्तु तय कर रहा है। जिस तरह वामपंथी और दक्षिणपंथी एक-दूसरे को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं उस तरह मैं मानता हूं कि मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा फेसबुक है क्योंकि वह अपने तरीके से चीजों को बढ़ा रहा है।
वह आपकी सोच को प्रभावित कर रहा है। नए मीडिया में फेसबुक ‘एक्सट्रीम’ के साथ खड़ा है। अगर आप एक पक्ष के खिलाफ भड़काऊ बात नहीं बोलेंगे, संतुलित होने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं है। कोई खबर आगे जाएगी या नहीं, यह फेसबुक तय करता है। और इन खबरों में होता क्या है? किसी चीज के चार कारण बता दिए जाते हैं। फेसबुक के ‘इंस्टेंट आर्टिकल’ जैसी चीजों के कारण लोग ‘क्लिक’ करते ही उसके पास से ही लौट जाते हैं और हमारी वेबसाइट तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका लक्ष्य पाठक को साधना नहीं है। और इसका बहुत नकारात्मक असर पारंपरिक मीडिया पर पड़ रहा है। पारंपरिक मीडिया के लेखकों को उदाहरण दिए जाते हैं कि फलां के लेख पर इतने क्लिक और लाइक हुए, तो आप उसकी तरह क्यों नहीं लिख रहे हैं। फिलहाल तो नए मीडिया में ज्यादातर समूह एकतरफा पक्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई एकदम ‘लेफ्ट’ है तो कोई एकदम ‘राइट’। इस लेफ्ट-राइट के दंगल में ‘राइट’ बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है’।
पारंपरिक और नया जब दोनों एक ही भाषा बोलने लगें, एक जैसी अपरिपक्वता दिखाएं, पाठकों को भेड़चाल का हिस्सा बनाएं तो फिर इसका समाधान क्या है? संजय दुबे कहते हैं कि हमें अच्छे काम को रोचक तरीके से करने की जरूरत है। थोड़ा ही सही पर टिक कर काम करने की जरूरत है। हमने जब ‘सत्याग्रह’ शुरू किया था तो हमारे पास एक पैसा नहीं था। नए मीडिया पर स्वतंत्र समूहों ने काम करना शुरू किया है लेकिन ऐसे लोग अभी बहुत कम हैं और अपनी जिद की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। नए मीडिया में जगह बनाना, आगे जाना बहुत आसान नहीं है। सर्कुलेशन का फंडा तो फिर भी बहुत आसान है ‘क्लिक’ के कारोबार को समझना और उससे जूझना बहुत मुश्किल है। दस हजार की सीमा पार करते ही बहुत पैसा खर्च होता है। तकनीक के बरक्स जहां मानव संसाधन की बात है तो पारंपरिक और नए मीडिया दोनों की समस्याएं एक हैं। अब लोग प्रशिक्षण में विश्वास नहीं करते हैं। हिंदी माध्यमों के पास संसाधन के नाम पर गूगल और अनुवाद हैं।