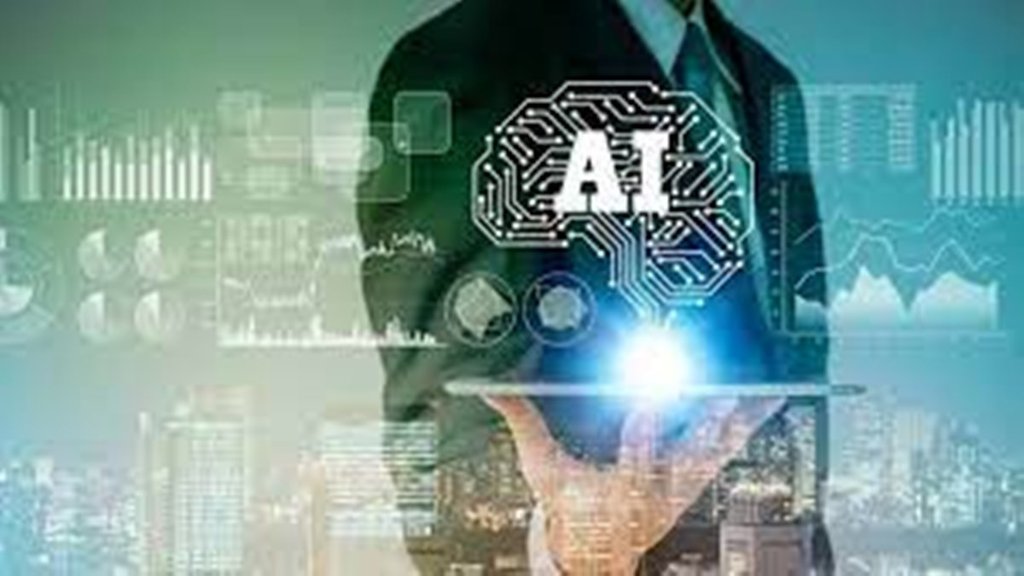अभिषेक कुमार सिंह
दुनिया भर में कई कंपनियां बढ़ती श्रम लागत के मद्देनजर उत्पादन का काफी कामकाज रोबोट और एआइ यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस मशीनों-कंप्यूटरों के हवाले कर रही हैं। भारत में भी सूचना तकनीक क्षेत्र की दस फीसदी नौकरियों पर ‘आटोमेशन’ यानी खुद काम करने वाली मशीनों के कारण खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है।
मानव सभ्यता के इतिहास में जिन कुछ चीजों की ईजाद ने इंसान के रहन-सहन का तरीका बदला, उनमें सबसे पहले हजारों साल पहले आग और पहिये के आविष्कार का नाम लिया जाता है। इसके बाद तस्वीर में बड़ा बदलाव औद्योगिक क्रांति यानी मशीनी युग में आया। आज से करीब पचास साल पहले पैदा हुए इंटरनेट को हाल तक इस रूप में देखा जाता था कि अब शायद इससे बड़ा कोई आविष्कार अगली सदियों तक न हो।
पर तकनीक की शायद यही सबसे बड़ी खूबी है कि वह हमारी जरूरतों के मुताबिक बदल जाती है। इंटरनेट के मौजूदा दौर में ये परिवर्तन कुछ ज्यादा ही तेजी से हो रहे हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल ‘चैटजीपीटी’ और उसके फौरन बाद अल्फाबेट (गूगल) द्वारा पेश ‘बार्ड’ नामक कृत्रिम बुद्धि वाले दो मंच हैं, जिन्होंने इधर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है।
इन्हें लेकर मची सनसनी का एक छोर जहां इस बात से जुड़ा है कि अब मौलिकता का भला क्या मोल रह जाएगा, क्योंकि इनकी बदौलत नकल होना आसान और उसके पकड़ना मुश्किल हो गया है। दूसरे छोर पर यह चिंता है कि कहीं तकनीक (कृत्रिम बुद्धि) इंसानों पर हावी न हो जाए या नकली बुद्धि से लैस मशीनें हमें अपना गुलाम ही न बना लें।
इन चिंताओं का तात्कालिक संदर्भ- सैनफ्रांसिस्को स्थित आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रिसर्च कंपनी ओपनएआई द्वारा विकसित चैटजीपीटी नामक एक चैटबाट (एक किस्म का कृत्रिम बुद्धि रोबोट) है, जिसे करीब तीन महीने पहले 30 नवंबर 2022 को आरंभिक स्वरूप (प्रोटोटाइप के रूप) में पेश किया गया। अंग्रेजी के शब्द चैटजीपीटी का पूरा नाम चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर है।
इसका मकसद ‘सर्च इंजन’ गूगल से आगे बढ़कर पूछे गए प्रश्नों के मौलिक हल प्रदान करना है। इसकी कई खूबियों में से एक यह भी है कि यह सवालों के जवाब हर बार नई शैली में और विस्तार से देता है, जिससे वे मौलिक और ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो उन्हें अलग-अलग लोगों ने दिया हो। असल में भारी मात्रा में इंटरनेट आदि से लिए गए डाटा से प्रशिक्षित किए गए चैटजीपीटी की खूबी सीखने की प्रवृत्ति और मानवीय शैली में विकास करना है। इसे ऐसे प्रशिक्षित किया गया है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है, तो जवाब में इंसान कैसी प्रतिक्रियाओं की उम्मीद करते हैं।
यही नहीं, चैटजीपीटी किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) क्षमता से लैस एक आम रोबोट से इस मायने में अलग है कि यह पूछे गए प्रश्नों में इंसान की मंशा को समझकर ऐसा उत्तर देता है जो वास्तविकता के करीब हो। ये जवाब लेख जैसी सामग्री के रूप में हो सकते हैं, वैसे नहीं जैसे गूगल पर जवाब में असंख्य वेबसाइटें सुझाव के रूप में आती हैं।
कुछ सवालों के उत्तर देने के बजाय चैटजीपीटी प्रतिप्रश्न पैदा कर सकता है और सवाल के उन हिस्सों को हटा भी सकता है, जो उसे समझ में नहीं आते हैं। कुछ मामलों में चैटजीपीटी गलत या आधे-अधूरे तथ्य प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि अभी इसमें मार्च 2022 तक की सूचनाओं के आधार पर डाटा भरा गया है। इसमें नया डाटा डालने की प्रक्रिया एक प्रकार से चैटबाट का प्रशिक्षण है।
हालांकि कृत्रिम बुद्धि के आधार पर खोजे जाने वाले मुख्य शब्दों (की-वर्ड्स), जिज्ञासाओं और सवालों को गूगल आदि सर्च इंजन अपनी-अपनी तरह से काफी समय से हल करते रहे हैं। लेकिन गूगल से मिली जानकारी की एक बड़ी सीमा यह थी कि वे प्रस्तुति के आधार पर मौलिक नहीं कही जा सकती हैं। वे एक जैसी होती हैं, इसलिए अगर चार लोग एक ही सवाल का जवाब गूगल से खोजकर देते हैं, तो वे समान होने के कारण पकड़े जा सकते हैं। साथ ही, अनुवाद के मामले में ‘गूगल ट्रांसलेट’ किसी भाषा के गूढ़ भावार्थ का अनुमान नहीं लगा पाता है। इन समस्याओं को चैटजीपीटी में दूर करने की भरसक कोशिश की गई है।
इसकी तारीफ करते हुए जीमेल के जनक पाल बूशीट कह चुके हैं कि ये गूगल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाल ने कहा था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित चैटजीपीटी सर्च इंजन के ‘रिजल्ट पेज’ को खत्म कर देगा। चैटजीपीटी से से लेखन, पत्रकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) समेत दर्जनों नौकरियों के खत्म हो जाने और स्कूल-कालेजों में निबंध, कविता, लेख, शोधपत्र, किताबें आदि में विद्यार्थियों की मौलिकता पर ग्रहण लगने का दावा किया जा रहा है।
यानी विज्ञान की एक उपलब्धि, जिसे असल में क्रांति मानना चाहिए, उसे लेकर दुनिया इस तरह भयभीत हो गई है कि उस पर प्रतिबंध लगाने के उपाय खोजे जाने लगे हैं। अमेरिका में कुछ विश्वविद्यालयों में चैटजीपीटी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। न्यूयार्क और सिएटल स्थित कुछ विश्वविद्यालयों-कालेजों में विद्यार्थी अपने स्मार्टफोन और लैपटाप और सर्वर से जुड़े कंप्यूटरों पर चैटजीपीटी नहीं खोल पा रहे हैं।
हालांकि इधर गूगल ने भी चैटजीपीटी की चुनौती को देखते हुए ‘बार्ड’ नामक चैटबाट की शुरुआत कर दी है। लेकिन आरंभिक दिनों में ही जेम्स वेब टेलीस्कोप संबंधी एक सवाल का गलत जवाब देने के कारण गूगल को तथ्यात्मक भूल के लिए माफी मांगनी पड़ी, जिससे उसके (कंपनी अल्फाबेट के) शेयरों की कीमतें एक ही दिन में आठ फीसदी तक गिर गए।
यों यह सच है कि खुद गूगल को इन चुनौतियों का अहसास काफी पहले से था। दो साल पहले एक साक्षात्कार में गूगल के प्रमुख सुंदर पिचाई ने दावा किया था कि अगले पच्चीस वर्षों में दो चीजें क्रांति करने वाली हैं। पहली है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दूसरी क्वांटम कंप्यूटिंग।
यहां एक गंभीर प्रश्न एआइ के असर से नौकरियों के खत्म होने और इंसान पर मशीनों के हावी होने का भी है। आज से बीस-पच्चीस साल पहले यह दावा किया जाता था कि कंप्यूटर, इंटरनेट के विस्तार और गूगल सर्च इंजन जैसे आविष्कार मौलिकता को समाप्त करते हुए कई तरह की नौकरियों के लिए काल बन जाएंगे।
लेकिन विज्ञान की इस तरक्की को अभिशाप ठहराने की कोशिश करने वालों ने देखा है कि इन वैज्ञानिक आविष्कारों और क्रांतियों के बल पर कामकाज आसान हुआ है और नए रोजगारों का सृजन हुआ है। इसलिए चैटजीपीटी के आविष्कार को लेकर बहुत आशंकित होना उचित नहीं लगता। आज दुनिया भर की मशीनें हमारे आसपास हैं, जो एआइ की बदौलत कई जटिल काम सीखकर उनमें इंसानों पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर रही हैं। पर किसी कंप्यूटरीकृत कामकाज में मशीन का आगे निकलना इतना खतरनाक नहीं समझा गया, जिससे कि इंसान मशीन के सामने बौना साबित हुआ हो। असली खतरा नौकरियों का ही है।
इसका एक सच यह है कि दुनिया भर में कई कंपनियां बढ़ती श्रम लागत के मद्देनजर उत्पादन का काफी कामकाज रोबोट और एआइ से लैस मशीनों-कंप्यूटरों के हवाले कर रही हैं। भारत में भी सूचना तकनीक क्षेत्र की दस फीसदी नौकरियों पर ‘आटोमेशन’ यानी खुद काम करने वाली मशीनों के कारण खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिक स्टीफन, मशहूर कारोबारी एलन मस्क और माइक्रोसाफ्ट के मालिक बिल गेट्स भी कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में कारखानों, घरों और दफ्तरों में कामकाजी इंसानों को मशीनों से चुनौती मिल सकती है।
यह अकारण नहीं है कि माइक्रोसाफ्ट जैसी कंपनी और एलन मस्क जैसे कारोबारी ‘ओपनएआइ’ की उन परियोजनाओं में खूब पैसा लगाते रहे हैं, जिनसे अक्लमंद मशीनें तैयार की जाएंगी। संकेत साफ है कि अगर इंसान ने खुद को समझदार मशीन से ज्यादा अक्लमंद साबित नहीं किया, तो उसके हाथ का काम छिनने वाला है।