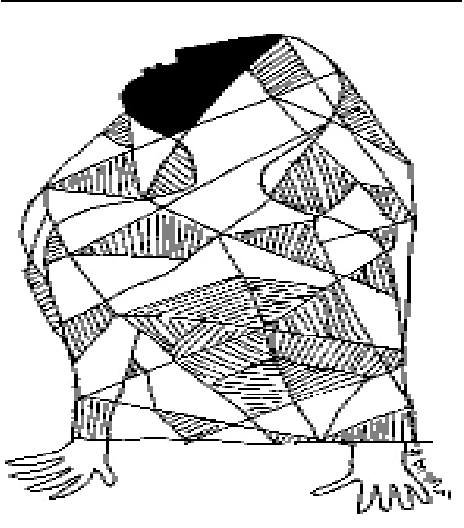य ह स्वागतयोग्य है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों से पांच सौ मीटर के दायरे में तंबाकू, गुटखा और शराब की दुकानों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। उसने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है। यह आदेश इस अर्थ में ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि स्कूली बच्चों में धूम्रपान की लत बढ़ रही है और उसे रोकने के लिए जरूरी है कि शिक्षण संस्थाओं के आसपास तंबाकू उत्पादों और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री न हो। पिछले साल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने खुलासा किया था कि कम उम्र में ही स्कूली बच्चे धूम्रपान की लत के शिकार हो रहे हैं और उनमें किस्म-किस्म की बीमारियां पनप रही हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था धूम्रपान के शिकार सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे ही नहीं बल्कि निजी शिक्षण-संस्थओं के बच्चे भी हैं, जहां बेहतर शिक्षा के साथ चरित्र-निर्माण का दावा किया जाता है। यह खुलासा रेखांकित करता है कि बच्चे आसपास के माहौल से प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही उन्हें नैतिक बनाने और धूम्रपान से दूर रखने में स्कूलों की भूमिका कमजोर पड़ रही है।
लेकिन गौर करें तो बच्चे सिर्फ शिक्षण-संस्थाओं के आसपास बेचे जा रहे नशीले पदार्थों की वजह से ही धूम्रपान के लती नहीं बन रहे हैं बल्कि घर का वातावरण और आसपास का माहौल भी उन्हें धूम्रपान के लिए उकसा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का फैलता जहर, फिल्मों के धूम्रपान वाले दृश्य, स्वयं माता-पिता का धूम्रपान का लती होना और बुरी संगत भी बच्चों के बालमन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ‘स्वीडिश नेशनल हेल्थ एंड वेल्फेयर बोर्ड और ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपिज’ के एक अध्ययन में बताया गया है कि बच्चों में धूम्रपान की लत के कई कारण हैं, जिनमें एक प्रमुख कारण सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे अपने आस-पास के लोगों को धूम्रपान करते देखते है जिससे आकर्षित होकर उनमें भी धूम्रपान करने की भावना पनपती है। यह तथ्य भी सामने आया है कि जिन बच्चों के माता-पिता धूम्रपान के लती होते हैं उनके बच्चे अतिशीध्र धूम्रपान के लती बन जाते हैं।
यह स्थिति बताती है कि घर और आसपास का दूषित वातावरण किस तरह बच्चों में धूम्रपान की प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। एक आंकड़े के मुताबिक सेकेंड हैंड स्मोकिंग से हर साल छह लाख से अधिक लोगों की मौत होती है जिनमें तकरीबन दो लाख से अधिक बच्चे ही होते हैं। ‘ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट’ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मोकिंग न करने वाले चालीस फीसद बच्चों और तीस फीसद से अधिक महिलाओं-पुरुषों पर सेकेंड हैंड स्मोकिंग का घातक प्रभाव पड़ता है। अगर यों कहें कि परोक्ष धूम्रपान बच्चों की सेहत खराब कर रहा है तो यह अनुचित नहीं है। देश और समाज को चिंतित होना चाहिए कि कम उम्र में धूम्रपान की वजह से बच्चे अस्थमा और फेफड़े के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार बन रहे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के ‘टुबैको-फ्री इनिशिएटिव’ के प्रोग्रामर डॉक्टर एनेट ने धूम्रपान को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा था कि अगर बच्चों को धूम्रपान की बुरी लत से दूर नहीं रखा गया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक नए अध्ययन से खुलासा हुआ है कि भारत में धूम्रपान करने की लत में पिछले सत्रह सालों में एक-तिहाई से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2015 में धूम्रपान करने वालों की तादाद बढ़कर 10.8 करोड़ हो गई है। अध्ययन में कहा गया है कि किसी भी तरह का धूम्रपान करने वाले 15 से 69 साल की उम्र के बीच के लोगों की संख्या 2.9 करोड़ यानी 36 फीसद बढ़ी है। इसी अध्ययन में कहा गया है कि 2010 में धूम्रपान की वजह से तकरीबन दस लाख लोगों की मौत हुई जो भारत में होने वाली कुल मौतों का दस फीसद है।
गौरतलब है कि बच्चों में धूम्रपान की कुप्रवृत्ति अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में सर्वाधिक है। इसका मूल कारण अशिक्षा, गरीबी और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। अब मौजूं सवाल यह है कि बच्चों को धूम्रपान की बुरी लत से कैसे बचाया जाए और किस तरह उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जाए? यह चिंता इसलिए भी जरूरी है कि देश के पचास फीसद बच्चे पहले से ही कुपोषण के शिकार हैं। अगर वे इस स्थिति में धूम्रपान जैसी बुरी लत के प्रभाव में आते हैं तो उनका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होगा। निसंदेह न्यायालय के आदेश के बाद अब शासन प्रशासन को शिक्षण-संस्थाओं के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना ही होगा। लेकिन क्या इस पहल मात्र से ही बच्चों में धूम्रपान की प्रवृत्ति पर रोक लग जाएगी? यह समझना होगा कि जब तक सरकार, समाज, स्कूल और स्वयंसेवी संस्थाएं इस बुराई को समाप्त करने के लिए मिलकर काम नहीं करेंगी तब तक परिवर्तन आने वाला नहीं है।
यह ठीक है कि सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। लेकिन सच यह भी है कि उस कानून का समुचित ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है। उचित होगा कि प्रशासन सुनिश्चित करे कि कानून का सही तरीके से अनुपालन हो। लेकिन यह भी समझना होगा कि सिर्फ कानून बनाकर ही धूम्रपान पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सामाजिक जागरूकता कहीं ज्यादा प्रभावी है। जब तक बच्चे धूम्रपान से उत्पन होने वाली खतरनाक बीमारियों से सुपरिचित नहीं होंगे और उनके मन में लोकलाज का भय नहीं होगा तब तक वे इस बुराई से दूर रहने वाले नहीं है। बेहतर होगा कि समाज और स्वयंसेवी संस्थाएं बच्चों को जागरूक करने के लिए आगे आएं। विचार करें तो इस दिशा में स्कूल बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए कि स्कूलों में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां और खेलकूद बच्चों के बालमन पर सकारात्मक असर डालती हैं।
इन गतिविधियों से उनमें नैतिक भावना और मर्यादित संस्कारों का विकास होता है। पहले स्कूली पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा अनिवार्य होती थी। अध्यापक बच्चों को आदर्श और प्रेरणादायक किस्से-कहानियों के जरिए उन्हें सामाजिक-राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते थे। धूम्रपान के खतरनाक प्रभाव को रेखांकित कर इससे दूर रहने की नैतिक शिक्षा देते थे। यही नहीं, धूम्रपान करने वाले बच्चों को दंडित भी करते थे। लेकिन यह त्रासदी है कि विगत कुछ समय से स्कूली शिक्षा पाठ्क्रम से नैतिक शिक्षा गायब है। शिक्षा का उद् देश्य सिर्फ वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने तक सिमटकर रह गया है। जबकि बच्चों को सभ्य, सुसंस्कृत और संवेदनशील बनाना स्कूलों की शीर्ष प्राथमिकता में शुमार होना चाहिए। इसलिए कि शिक्षा मंदिरों में ही बच्चों का चरित्र गढ़ा-बुना जाता है और उनके उदात्त भावनाओं को पंख लगाया जाता है। लेकिन विडंबना है कि शिक्षा मंदिर खुद चरित्र के संकट से जूझ रहे हैं।
पिछले साल महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि हर चौथा स्कूली बच्चा यौन षोशण का शिकार है। शोधों से यह भी उद्घाटित हुआ कि शिक्षकों में भी धूम्रपान की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह स्थिति चिंताजनक है। जब शिक्षक ही धूम्रपान करेंगे तो फिर बच्चों को धूम्रपान से कैसे रोकेंगे। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार न सिर्फ स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाए, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी धूम्रपान के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करे। बच्चे राष्ट्र की थाती हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिकरूप से सशक्त और सबल बनाना राष्ट्र का उत्तरदायित्व है। १