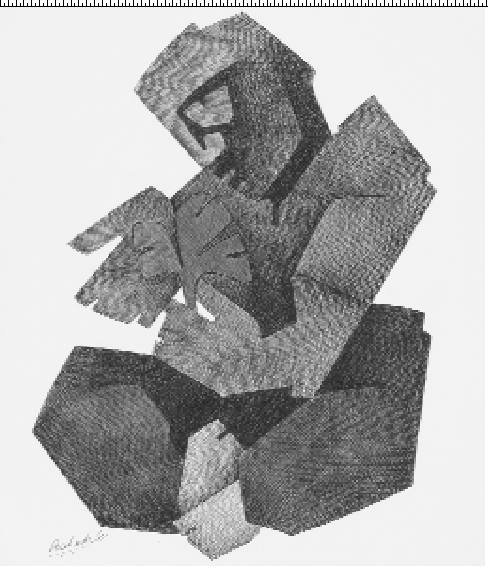बहुत संभव है कि कथा-तत्त्व से युक्त बहुत-सी कहानियां एकदम कमजोर हों, पर कथा-तत्त्व के बिना कहानी का श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण होना अपवाद ही है। कहानी में कथा-तत्त्व की उपेक्षा एक तरह से सामान्य जनता की उपेक्षा है। सामान्य जनता की उपेक्षा करके कोई भी हिंदी कहानी श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकती है।
नए यथार्थ के अनुरूप कहानी के स्वरूप में परिवर्तन स्वाभाविक है। हर दौर में कहानी के स्वरूप में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है। अपने समय की संवेदना और भाव-सत्य को मुकम्मल तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए कहानी ने अपने रूप को बार-बार बदला है। इस बदलाव के बिना हिंदी कहानी का विकास असंभव था। प्रयोग से हिंदी कहानी का न तो कोई विरोध रहा है और न परहेज। पर प्रयोग हमेशा कहानी के भीतर होना चाहिए। प्रयोग के नाम पर किसी भी गद्य रचना को कहानी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह कि नए जीवन सत्य के अनुरूप कहानी के रूप में परिवर्तन होना चाहिए, पर यह परिवर्तन ऐसा न हो कि कहानी कहानी न होकर कुछ और हो जाए। आज की कहानियों को पढ़ते हुए प्राय: महसूस होता है कि कहानी के नाम पर गद्य में कुछ भी प्रस्तुत कर देने का चलन बढ़ रहा है।
सवाल है कि कहानी का वह मूल तत्त्व क्या है, जिसके बिना कहानी का होना संभव नहीं है? वह तत्त्व है कहानीपन। कहानीपन के लिए कहानी में कथा-तत्त्व वांछनीय है और कथा-तत्त्व के कारण कथानक की मौजूदगी अपने आप हो जाती है। कहानीपन, कथा-तत्त्व और कथानक इन तीनों के बीच अनिवार्य संबंध तो नहीं, पर ये प्राय: एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। यह अकारण नहीं है कि इधर की कहानियों में कथा-तत्त्व के ह्रास, कथानक के लोप और कहानीपन के अभाव को एक साथ लक्षित किया जा सकता है।
दरअसल, गंभीर से गंभीर विचार, राजनीति, दर्शन, मनोविज्ञान, नीति, ज्ञान, परिस्थिति, घटना आदि को सहज सरल तरीके से अभिव्यक्त या प्रस्तुत करना ही कहानी की सार्थकता है। ज्ञान और तत्त्व की बातों को सुगम तरीके से समझाने के लिए कहानी विधा ही सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई और इसका प्रचलन प्राचीन काल से है। उपनिषद, जातक कथाएं, धर्म ग्रंथों की प्रतीक कथाएं, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी आदि इस बात के प्रमाण हैं। इन आख्यायिकाओं में कल्पना और यथार्थ का सुंदर मिश्रण है। हम जो कहना, बताना या समझाना चाहते हैं उसके लिए अपनी कल्पना शक्ति द्वारा किसी कथा को सृजत करना ही तो रचनात्मकता है। राजनीति, समाजशास्त्र आदि जैसे ज्ञान के दूसरे अनुशासनों और साहित्य का स्रोत तो एक ही होता है, पर वे अपनी अभिव्यक्ति में अनिवार्यतया भिन्न होते हैं। अभिव्यक्ति की यह भिन्नता ही कहानीपन है। अभिव्यक्ति की भिन्नता के कारण ही साहित्य का सीधा रिश्ता हमारी संवेदना से जुड़ता है। राजनीति, इतिहास और दर्शन को समझने के लिए ज्ञानी की जरूरत होती है, जबकि साहित्य को समझने के लिए सहृदय की।
एक बात और ध्यान रखने की है कि कहानी शुरू से जन-विधा रही है। प्राचीन काल से ही यह ज्ञानियों के लिए कम, व्यापक जनता को ध्यान में रख कर लिखी जाती रही है। सामान्य मनुष्य को संवेदनशील और शिक्षित बनाने में कहानियों की बड़ी भूमिका रही है। प्रेमचंद ने तो कहानी की तुलना में उपन्यास को भी विशिष्ट जनों की विधा माना है। उन्होंने लिखा है कि ‘उपन्यास वे लोग पढ़ते हैं, जिनके पास रुपया है, और समय भी उन्हीं के पास रहता है, जिनके पास धन होता है। आख्यायिका साधारण जनता के लिए लिखी जाती है, जिसके पास न धन है न समय। यहां तो सरलता में सरसता पैदा कीजिए, यही कमाल है।’ स्पष्ट है, कहानी का सरल-सुगम होना उसकी विधागत अनिवार्यता है।
यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि कहानी की सरलता का मतलब कहानी में अभिव्यक्त भाव-बोध की सरलता नहीं है, बल्कि इसका एक ही मतलब है- जटिल से जटिल भावों की सरल तरीके से अभिव्यक्ति। इस सरल अभिव्यक्ति के लिए कहानी में कथा-तत्त्व का होना आवश्यक है। कथा-तत्त्व के अभाव में राजनीति और समाजशास्त्र की तरह ही कहानी में भी यथार्थ अभिव्यक्त होने लगता है। अभिव्यक्ति की भिन्नता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण कहानी कहानी न होकर राजनीतिक या समाजशास्त्रीय निबंध बन जाती है। कथा-तत्त्व का सृजन कहानीकार की उच्च कलात्मक और कल्पनात्मक क्षमता का द्योतक है। उदाहरण के लिए, अगर कोई यह बताने के लिए कहानी लिखना चाहता है कि पूंजीवाद ने मनुष्य को महज एक उपभोक्ता में बदल दिया या कोई आधुनिक विकास के मनुष्य-विरोधी रूप को उजागर करने वाली कहानी लिखना चाहता है, तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह यथार्थ और कल्पना के योग से ऐसी कथा रच पाता है कि नहीं, जिसको पढ़ने से कथ्य महसूस होने लगता है।
कहानी का कथ्य अभिधा में नहीं व्यंजना में होता है। रचनाकार जितना समर्थ होगा, कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए उतना सशक्त कथा सृजत करेगा। जो रचनाकार समर्थ नहीं होता, वह कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए अभिधा में इधर-उधर से ज्ञान बटोर कर कहानी में परोस देता है। आजकल की कहानियों में कथा के माध्यम से नहीं, बल्कि विचारों के माध्यम से कथ्य को अभिव्यक्ति करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। यह निश्चय ही नए कहानीकारों के रचनात्मक न्यूनता का द्योतक है। कहानी का स्वधर्म उसका कथा-तत्त्व है और इसी वजह से वह ज्ञान की दूसरी अभिव्यक्तियों से भिन्न है। यथार्थ को कथा के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही कहानीकार का रचनात्मक संघर्ष है। कथा के जरिए ही तो वह यथार्थ की पुनर्रचना करता है। पुनर्रचित पात्रों और परिस्थितियों से हम वास्तविक पात्रों और परिस्थितियों की तुलना में अधिक लगाव महसूस करने लगते हैं। वास्तविक किसान की तुलना में कहानी के किसान से हमारा रिश्ता अधिक अत्मीय बन जाता है। यही कहानी की सफलता और सार्थकता है।
कहानी के संदर्भ में यथार्थ की रचनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब मुख्य रूप से उसे कथा के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। कहानी में कथा तत्त्व का होना या न होना सिर्फ कहानी-कला का प्रश्न नहीं, बल्कि यह एक रचनात्मक दृष्टि का भी प्रश्न है। कथा-तत्त्व से युक्त कहानी लिखने का मतलब है कि कहानीकार की नजर में आम पाठक महत्त्वपूर्ण है और वह अपनी कहानी आम जनता को ध्यान में रख कर लिख रहा है। दूसरी तरफ, कथा-तत्त्व के अभाव में कहानियां प्राय: जटिल, बौद्धिक और उलझावपूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कहानियों को कुछ ज्ञानी लोग ही समझ पाते हैं। सामान्य पाठक उससे दूर ही रहते हैं। जो कहानियां कथा-तत्त्व से युक्त होती हैं वे सामान्य पाठकों के साथ-साथ साहित्य के पंडितों को भी उतनी ही आकर्षित करती हैं। इसके सबसे सुंदर उदाहरण प्रेमचंद हैं। साहित्य-कला की बारीकियों के आधार पर प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने वाले नलिन विलोचन शर्मा ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि ‘प्रेमचंद की महत्ता इस बात में निहित है कि उन्होंने दिलचस्प और लोकप्रिय किस्सा-कहानी और साहित्यक तथा कलापूर्ण कल्प के बीच की झूठी खार्इं को मिटा दिया था…। हकीकत तो यही है कि बहुत से पाठक कहानियां कहानी पढ़ने के लिए ही पढ़ते हैं, उनकी दिलचस्पी कथावस्तु तक सीमित रहती है, ऐसे पाठकों को प्रेमचंद से पूरी तशफ्फी हासिल होती है। दूसरी ओर जो लोग कहानियों में साहित्यिक गहराई और मनोवैज्ञानिक बारीकियों की अपेक्षा रखते हैं, उन्हें भी प्रेमचंद से कोई शिकायत नहीं हो सकती।’
हिंदी में अब तक जितनी कहानियों को श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण माना गया है, प्राय: सबके बारे में यह बात कही जा सकती है। यह बहुत संभव है कि कथा-तत्त्व से युक्त बहुत-सी कहानियां एकदम कमजोर हों, पर कथा-तत्त्व के बिना कहानी का श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण होना अपवाद ही है। कहानी में कथा-तत्त्व की उपेक्षा एक तरह से सामान्य जनता की उपेक्षा है। सामान्य जनता की उपेक्षा करके कोई भी हिंदी कहानी श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकती है।