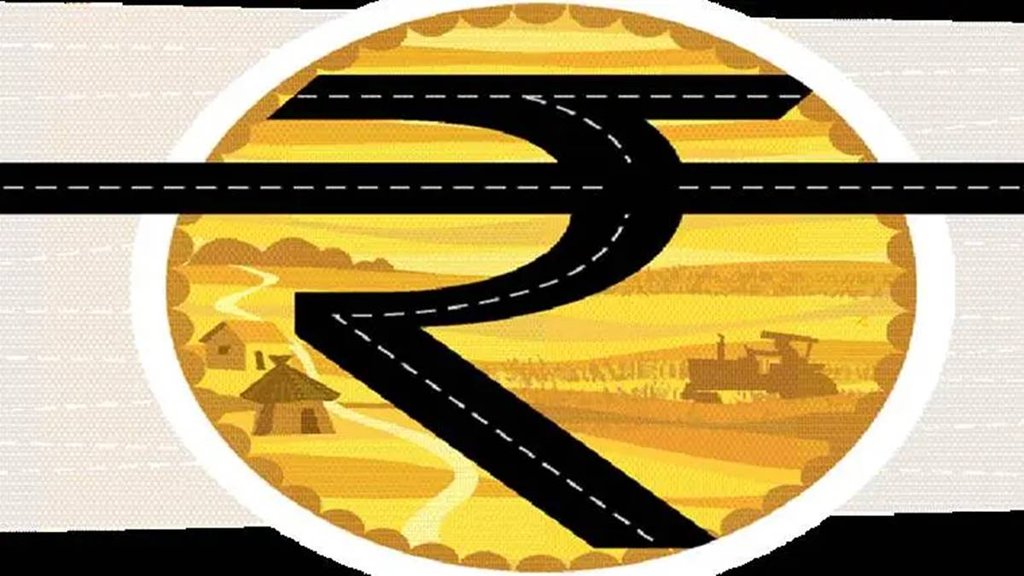अंतरिम बजट के बाद अब बड़ी शिद्दत से जुलाई माह में पेश होने वाले पूर्ण बजट का इंतजार हो रहा है। इसके साथ देश के आम आदमी की बहुत-सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सबसे पहले हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी की गारंटी चाहिए। नौकरशाही पर लगाम लगे, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो। महंगाई में रुकावट आए।
इन उम्मीदों के बारे में तो अगली सरकार के साथ देश के निवेशक, व्यापारी, प्रशासक और साधारण जन संघर्ष शुरू करेंगे। मगर फिलहाल वित्तवर्ष के समापन पर आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो लगता है कि 1991 में तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के समय में जिस उदारवाद की शुरुआत हुई थी, वह पिछले दशक में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। देश का जो आर्थिक माडल बदला है, उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी है। लेकिन उसमें निजी क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया जा रहा है, ताकि देश की विकास गति द्रुत हो सके। जब आजादी का शताब्दी वर्ष आए, तो यह देश न केवल विश्वगुरु हो, बल्कि दुनिया को पछाड़ते हुए अगर पहले नंबर की महाशक्ति बन जाए तो क्या ही बात।
इसी सिलसिले में अभी रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और इंडियन एक्सिस बैंक की एक रपट आई है। उसमें बताया गया है कि देश की शीर्ष पांच सौ निजी कंपनियों का कारोबार 2023 में 231 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इससे भी बड़ी बात यह कि देश पूरे वर्ष में जो सकल घरेलू उत्पादन करता है, उसका यह इकहत्तर फीसद है। पिछले वर्षों में देश की प्राथमिकताएं बदली हैं। अब पूंजीगत निवेश अधिक हो रहा है। मूलभूत आर्थिक ढांचे का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष कर का संग्रह बढ़ा है।
जीएसटी संग्रह न केवल अपने एक लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर गया, बल्कि पिछली कुछ गणनाओं में उसकी गिनती 1.60 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच गई है। इसी आधार पर सरकार कहती है कि भारत जो कभी दसवीं आर्थिक महाशक्ति था, वह छलांग लगाकर पांचवें स्तर तक पहुंच चुका है और जर्मनी तथा जापान को पीछे छोड़कर बहुत जल्द तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा।
एक अच्छी खबर यह भी है कि खुदरा महंगाई दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम घटने से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह इस समय 5.10 फीसद पर है। खुदरा महंगाई का लक्ष्य रिजर्व बैंक ने चार फीसद रखा हुआ है। इसे प्राप्त करने के बाद ही संभवत: मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो रिजर्व बैंक रेपो रेट में कोई परिवर्तन न करते हुए साख मंडियों में यथास्थिति बनाए हुए है। चाहे अर्थ विशारद यह कहते हैं कि मूल्य सूचकांक का बढ़ना-घटना अगर खाद्य उत्पादों पर ही निर्भर रहता है, तो यह संतोषजनक नहीं है। असल बात तो यह है कि हमारे औद्योगिक उत्पादन की दर क्या है?
गौरतलब है कि देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर सालाना आधार पर पिछले वर्ष 3.8 फीसद रह गई। इसका कारण था खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्र का खराब प्रदर्शन। दिसंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन 5.1 फीसद तक बढ़ा था। नवंबर 2023 में यह 2.4 फीसद हो गया। अब सालाना औसतन 3.8 फीसद है। इसी के साथ विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर भी बढ़नी चाहिए, जो अभी तक 3.9 फीसद है।
हम आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र पर भी निर्भर हैं। इससे पांच करोड़ तक रोजगार के मौके मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए तीन तरह के पर्यटन माने जाते हैं: रमणीक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन। भारत में आम जन की आस्था के कारण धार्मिक पर्यटन सबसे महत्त्वपूर्ण है।
अगले वर्षों में यह देखना होगा कि क्या इसके लिए यात्रियों की सुविधा, सड़कों का रखरखाव संतोषजनक है? सरकार का ध्यान इस ओर विकास के विषय में जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि यहां आने वाले पर्यटकों को दलालों या पंडों की ठगी को सहना नहीं पड़ेगा। उनके लिए उचित आवागमन के साधन प्रदान किए जाएं और उनके रहने-ठहरने की व्यवस्था भी सस्ती हो।
इधर इन स्थानों पर स्थानीय निवासियों ने ‘होम स्टे’ की परंपरा शुरू की है, जो कि होटलों के विकल्प के रूप में इन स्थलों पर उभर रही है। ध्यान रखा जाए कि इनकी लागत भी यात्रियों के लिए होटलों से कहीं कम हो, तभी लोग इनको स्वीकार करेंगे। वैसे, यह स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार का एक उचित साधन तो है ही। लेकिन इसके साथ ही देश की आर्थिक व्यवस्था में विषमता का जो वातावरण पैदा हो रहा है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है।
जीडीपी का इकहत्तर फीसद अगर शीर्ष पांच सौ निजी कंपनियों को जाएगा, तो देश में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास कैसे होगा, जो कि अधिक से अधिक रोजगार दे सकते हैं। कुटीर उद्योगों को भारत की ग्रामीण, ग्राम-बहुल अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छे ढंग से खपाया जा सकता है, लेकिन इसमें निवेशकों को शिकायत है कि उन्हें करों में रियायत का वह प्रोत्साहन नहीं मिलता, जो मिलना चाहिए। इसमें भी उन्हें बड़े निवेशकों के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है, जो किसी न किसी कंपनी के रूप में लाल डोरा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं।
देश के नौजवानों की तरक्की के लिए यह भी जरूरी है कि देश में स्टार्टअप उद्योगों की योजना को प्रोत्साहन मिले, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि यहां तो चार लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया, जो चिंताजनक है। सवाल यह भी है कि हमारे देश के अनुसंधान क्षेत्र में निजी क्षेत्र का योगदान कम क्यों है? विज्ञान की पढ़ाई में भारत की युवा पीढ़ी पिछड़ क्यों रही है? शोध में पैसे की कमी, प्रतिभा पलायन और सुविधाओं की कमी बड़ी समस्या बन रही है।
हकीकत यह है कि भारत में उच्च शिक्षा के चालीस हजार से ज्यादा संस्थान हैं, लेकिन यहां केवल एक फीसद में शोध होते हैं। दुनिया के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में भारत 149वें स्थान पर है। बेकारी की भीषण समस्या भविष्य के बंद रास्ते, महंगाई और भ्रष्टाचार के दबाव की वजह से भारत के काबिल युवा अपना कोई भविष्य देश में नहीं पाते। वे अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में अगर छात्र वीजा पर जाते हैं, तो वापस नहीं लौटते।
अमेरिका में विज्ञान पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में सबसे अधिक आबादी भारतीय छात्रों की है। दुनिया के शिखर वैज्ञानिकों में आठ भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये देश में काम नहीं कर रहे। यह स्थिति बदलनी चाहिए। भारत के आम आदमी, वंचित को अपना भविष्य भारत में ही मिले। कब तक यह विषमता बनी रहेगी कि देश का धनी वर्ग नब्बे फीसद संपदा पर काबिज रहेगा और देश की दस फीसद संपदा गरीबों के हिस्से में आएगी। नए आर्थिक ढांचे को गरीबी हटाओ, समता बढ़ाओ के धरातल पर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा?