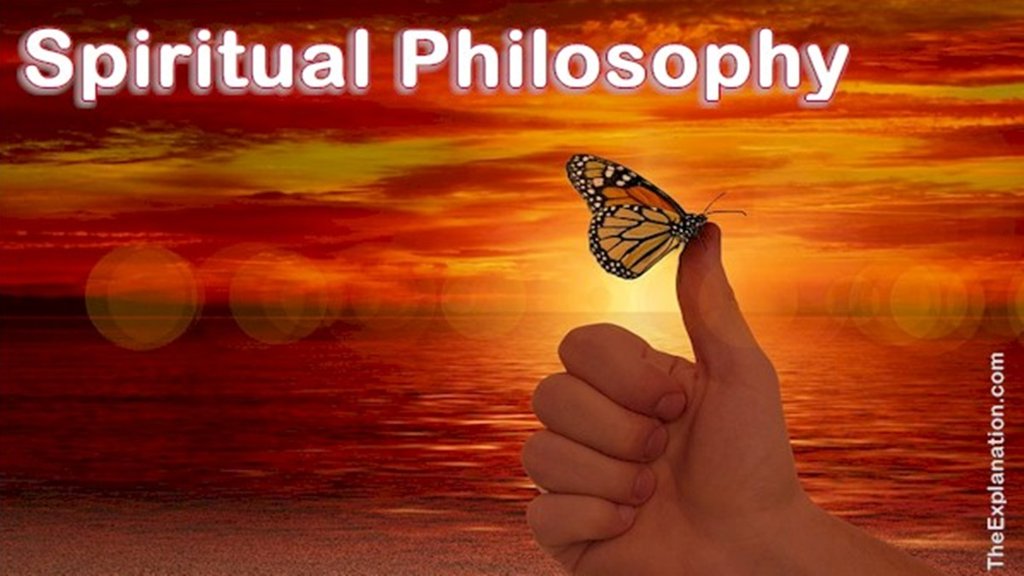राकेश सिन्हा
पहले की तुलना में पुस्तक पढ़ने की लालसा और क्षमता दोनों घटी है। इसके बावजूद 2010 में तेरह करोड़ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। अकेले भारत में 2022 में नब्बे हजार शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। नई पीढ़ी सोशल मीडिया पर अधिक समय गुजारती है। कम शब्दों में व्यक्त विचार पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आती हैं। इसी को विमर्श मान लिया जाता है। मन हल्के तरह से हल्की भाषा में बोलने और लिखने की आदत के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। यह वैश्विक प्रवृत्ति है।
इसके कारण और परिणामों पर चिंता की जगह चिंतन आज के दौर में उपलब्धि मानी जाएगी। विज्ञान अपनी तरह से उन्नति कर रहा है। उसकी प्रगति में मनुष्य को श्रमजीवी से तकनीकजीवी बनाना लक्ष्य है। शहरों-महानगरों में आर्थिक संपन्नता और तकनीकी उपलब्धता ने मनुष्य को शारीरिक श्रम से दूर किया है। इसका फलक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। डर है कि मनुष्य तकनीक की तरह और तकनीक मनुष्य की तरह न व्यवहार करना शुरू कर दे। यह प्रश्न उठता है कि क्या विज्ञान अपने आप में स्वायत्त एवं संप्रभु है। आज ऐसा ही लग रहा है।
दूसरे क्षेत्रों, आध्यात्मिक दर्शन, सामाजिक-सांस्कृतिक चिंतन आदि में प्रगति का सूचकांक कम होने से उनका प्रभाव घटा है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी को पुरानी संरचना और कर्मकांड में बांधकर रखने का काम उन्हें भौतिकवाद में मुक्ति दिखाता है। इसे भारतीय दर्शन में चार्वाक कहा गया। उदाहरणार्थ, अमेरिका में चर्च की सदस्यता 1937 में 73 फीसद थी, जो 2020 में घटकर 47 फीसद रह गई है।
यूरोप और अन्य इसाई भूभागों में भी इस प्रवृत्ति का बोलबाला है। नौजवानों को नई खोज, नए उपभोग की सामग्री उत्तेजित करती है। विज्ञान की सार्थकता समाज के उत्थान में है, पर विज्ञान भौतिकता को बढ़ा कर मनुष्य के मस्तिष्क को सामाजिक स्तर पर बंजर बना रहा है। इसलिए अध्यात्म, दर्शन, संस्कृति की भूमिका अहम हो जाती है।
जब अध्यात्म मानव जीवन मूल्यों को दर्शन के रास्ते परिभाषित करता है और उसे उस विचार को पढ़ने, सुनने, आत्मसात करने में व्यक्ति अपना सशक्तीकरण देखता है, तब आध्यात्मिक दर्शन की चौहद्दी फैलती जाती है। यही मस्तिष्क सृजनकर्ता बनता है। इसे मस्तिष्क की उत्पादकता भी कहते हैं। इसमें मानसिक श्रम और समय दोनों की आवश्यकता होती है। कर्मकांड से बंधी संस्थाएं सृजन का कार्य नहीं कर पाती हैं।
मस्तिष्क बंधक बना रहता है। भारत की स्थिति भिन्न रही है। भारतीय दर्शन को अध्यात्म से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए अध्यात्म कर्मकांड को आवश्यक मानता है, अनिवार्य नहीं। भारतीय परिवेश में जब व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना पैदा होती है, तब वह उसे अपने अधिनायकवाद में तब्दील कर अंतिम सत्य या पथ घोषित नहीं करता है। यही इसकी खूबी और खुशबू दोनों है। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य अपने ज्ञान को मिल रही चुनौती से न पीछे हटते थे, न ही उसे दार्शनिक हिंसा मानते थे।
बौद्धिकता और दर्शन की सृजनशीलता व्यक्तिगत होती है। इसका दायरा भी सीमित होता है। पर यह आम लोगों को सोचने, समझने, उलझने की पूरी स्वतंत्रता देता है। इसीलिए संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। शंकराचार्य ने चार धामों की स्थापना की। प्रत्येक धाम अपने आप में स्वायत्त है। ये धाम मूलत: दर्शन और मूल्यों के सृजन के पीठ के रूप में थे, जिसमें संस्कृति के प्रवाह को संदर्भित करने की क्षमता होती थी।
आठवीं शताब्दी में स्थापित ये धाम इक्कीसवीं शताब्दी में अपनी कितनी सृजनशीलता बनाए हुए हैं, यह अध्ययन का विषय है। महाराष्ट्र में तेरहवीं शताब्दी में समाज परिष्कार की मौलिक परंपरा कीर्तन (भजन मंडली) शुरू हुई थी। एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव के प्रवचनों को नृत्य, संगीत, कथा वाचन एवं अभिनय के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता था।
बौद्ध विद्वानों के बीच सामयिक प्रश्नों के साथ उसकी सार्थकता को लेकर तीन प्रसिद्ध विशाल परिषदें- राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में दो हजार वर्ष पूर्व हुई थीं। ये विचार विनिमय एकांगी नहीं होते थे। समाज, संस्कृति, प्रकृति, विज्ञान, मनुष्य सभी पक्षों को विचारणीय माना जाता था। ये यही मूल दर्शन अंतत: साहित्य, समाजशास्त्र, शासन कला और राजनीति को प्रभावित करता था।
यह इस बात का भी सूचक है कि संस्थानों का स्वस्थ, स्वायत्त होना और स्वतंत्र विचार-विमर्श का केंद्र होना कितना आवश्यक है। वे मानव की प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। प्रगति का तब तात्पर्य भौतिकता का ऐश्वर्य नहीं, समष्टि को प्रभावित और परिष्कृत करने वाले दर्शन का निर्बाध प्रवाह है। उपनिषद तभी तो चिरंजीवी हुआ है। प्रकारांतर से मस्तिष्क उत्पादक कम, उपभोक्ता अधिक बन गया है।
वह सतह से नीचे जाकर चीजों का जानने-परखने की क्षमता खो रहा है, मनोरंजन की आवश्यकता उसके मस्तिष्क की भूख शांत करने के लिए अनिवार्य पहलू बन जाती है। उस मनोरंजन में तात्कालिकता तो है, पर दीर्घकालिकता नहीं है। भौतिकता ने मस्तिष्क को विलासी उपभोक्ता बना दिया है। यह व्यक्ति की उदात्तता को न सिर्फ कम कर रहा है, उसे सीमित सामाजिकता में जीने के लिए बाध्य कर रहा है।
एक भिन्न प्रकार का व्यक्तिवादी चरित्र विकसित हो रहा है। विज्ञान और भौतिकता की सांठगांठ और भी प्रतिकूलता को जन्म दे रही है। विरासत की चादर ओढ़कर हम अपने कमजोर वर्तमान और बौद्धिक चरित्र को नहीं छिपा सकते है। प्राचीनता की उपयोगिता और उसके प्रभाव की अपनी सीमा है।