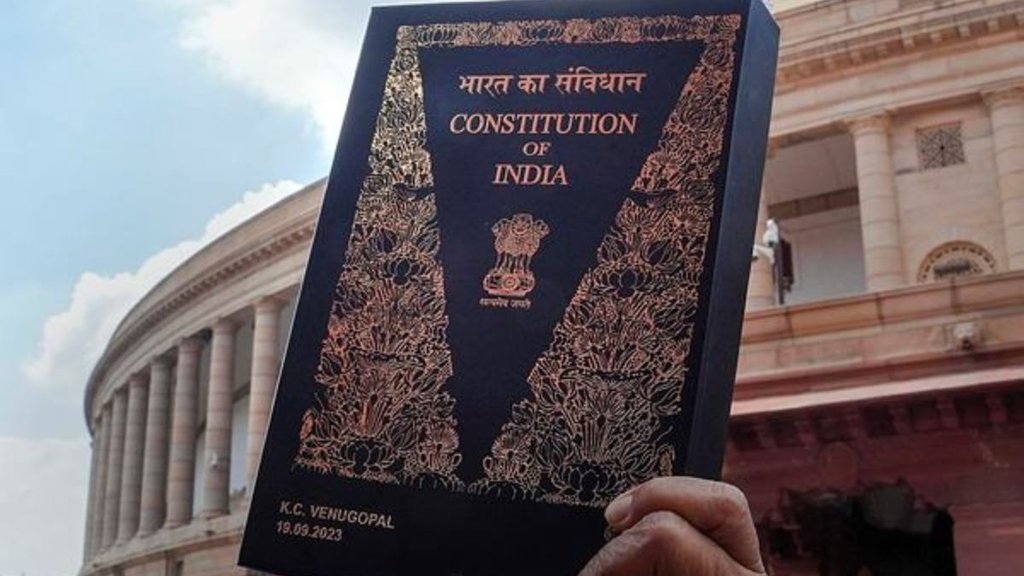शिवेंद्र राणा
छब्बीस जनवरी आधुनिक भारत के इतिहास का वह दिन है, जब भारतीय गणराज्य ने अपने संविधान को अंगीकृत और भारतीय जन-मन ने स्वयं को संविधान के साथ एकाकार किया। हालांकि यह तर्क भी महत्त्वपूर्ण है कि इतिहास केवल दिवस विशेष या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का शब्दकोश या संग्रहीकरण नहीं होता। इतिहास का यह भी दायित्व है कि वह अतीत के यथार्थ निरूपण का सत्य उद्भासित और वर्तमान के दिशा-निर्देशन में सहायक बने। यह सच है कि भारतीय संविधान फ्रांसीसी, अमेरिकी या सोवियत संघ के संविधान की तरह किसी राजनीतिक या सामाजिक क्रांति का परिणाम नहीं है। बल्कि यह लगभग दो शताब्दियों की औपनिवेशिक दासता के सांध्यकाल में भारतीय जनप्रतिनिधियों के समुच्चय द्वारा लंबे विचार-विमर्श, अनगिनत बहसों, शोधों की परिणति है।
भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संसदीय एवं संवैधानिक मूल्यों का प्रभाव
संविधान उन दस्तावेजों का प्रतीक भी है, जिन्हें साम्राज्यवादी सत्ता के विषाद काल में भारतीय जनता ने देखा-समझा था। अधिकृत भारत का शासन संचालन करने की नीयत से ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम, 1858 (21 तथा 22 विक्टोरिया, अध्याय-106) के रूप में पहला कानून बना। तब से भारत शासन अधिनियम, 1935 तक की इस कानूनी यात्रा ने संविधान के लिए एक आधार तैयार कर दिया था। भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संसदीय एवं संवैधानिक मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। संविधान सभा के सदस्य पीसी देशमुख ने संविधान मसौदे पर आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, ‘अंग्रेज जो शासन-व्यवस्था इस देश में छोड़ गए हैं, उसमें यह ठीक-ठीक बैठ जाए, इसी अभिप्राय से इसकी रचना हुई है।’
संविधान निर्माताओं ने ‘वेस्टमिंस्टर’ प्रारूप को अधिकाधिक ग्रहण किया
लगभग दो सौ वर्षों के ब्रिटिश मेधा से उपजे मूल संवैधानिक संस्थाओं के साहचर्य ने भारतीय जनता को उनका अभ्यस्त बना दिया था, ऐसा संविधान सभा का मत था। यह एक मुख्य वजह थी कि संविधान निर्माताओं ने ‘वेस्टमिंस्टर’ प्रारूप को अधिकाधिक आत्मसात किया। इतना ही नहीं, जितना संभव हो सका, जो भारतीय समाज के अनुकूल प्रतीत हुआ, जो राष्ट्रीय आधार बन सकें, ऐसे विभिन्न संवैधानिक मूल्यों को विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक संहिता से भी ग्रहण किया गया। मसलन, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति-निदेशक सिद्धांत, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आदि मूल्य ग्रहित हैं।
ओड़ीशा से संविधान सभा के सदस्य लक्ष्मी नारायण साहू ने तब कहा था कि ‘जिस आदर्श से हम यह संविधान बनाना चाहते थे, उस आदर्श से हम बहुत दूर भाग गए हैं। और अब जो आदर्श हमारे सामने रखा हुआ है, उसमें भारत की आत्मा का कुछ परिचय नहीं मिलता। यह एक खिचड़ी बन गया है।’ इसीलिए 26 नवंबर, 1949 को अर्धस्वीकृत और 26 जनवरी, 1950 को पूर्ण अंगीकृत भारतीय संविधान को उधार का संविधान, उधारी की टोकरी, ‘हाच-पाच कान्स्टिट्यूशन’ या पैबंदगिरी कहकर उसकी आलोचना होती रही है।
तो, सवाल है कि इसमें नया क्या है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने कहा कि ‘यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास में आज निर्माण किए जाने वाले संविधान में क्या कोई बात नई हो सकती है। जब पहला लिखित संविधान बनाया गया था, तब से सौ वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। उसके बाद अनेक देशों ने अपने संविधान को लेखबद्ध किया है। इन तथ्यों को जानकर सभी संविधानों के मुख्य उपबंध एक से दिखाई पड़ते हैं। अगर कोई नई चीज है, तो वह यह कि इतने वर्षों बाद बनाए गए इस संविधान में उन दोषों को दूर करने के लिए और अपने देश की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए गए हैं।’ फिर वे भारतीय संविधान को आसान शब्दों में परिभाषित करते हैं, ‘यह जीवन का माध्यम है और इसकी भावना सदैव युग की भावना है।’ युगीन भावनाएं अतीत में नहीं जीतीं। वे अतीत से प्रेरित हो सकती हैं, उन पर आधारित हो सकती हैं, लेकिन नवाचारों की प्रतिरोधी नहीं होतीं।
भारतीय संविधान की संरचना एक सतत गतिशील और जीवंत यात्रा का परिणाम है तथा उसका परिष्करण राष्ट्रीय उन्नयन की भांति उसी गतिशील प्रक्रिया की अनुगामी है। अगर ऐसा न होता तो देश को संविधान समीक्षा आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग तथा सौ से अधिक संशोधनों आदि की जरूरत न पड़ती। संवैधानिक परिमार्जन की प्रक्रिया अबाधित रूप से 26 जनवरी, 1950, यानी अपने लागू होने से वर्तमान तक निरंतर चलायमान रही है।
संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु वर्ष 2000 में गठित संविधान समीक्षा आयोग यानी वेंकटचलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सूचना का अधिकार कानून, ई-गवर्नेंस, जन-प्रतिनिधित्व कानूनों में सुधार, ग्रामीण रोजगार कानून, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर देश को विमर्श की दिशा मिली और अद्यतन संवैधानिक सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। यही नहीं, दो प्रशासनिक सुधार आयोगों के गठन हुए (प्रथम, जनवरी, 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में तथा द्वितीय, अगस्त, 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में) जिनकी रपटों के आधार पर यथायोग्य कानूनी सुधार भी हुए। तदंतर सुधार की यह प्रक्रिया गतिशील है।
जहां तक आरोपों की बात है, तो यह असंभव है कि कोई भी सरकार चाहे वह जितने भी प्रचंड बहुमत से सत्तासीन हुई, वह संविधान को खंडित करने की हिम्मत नहीं कर सकती है और न ही भारतीय जनतंत्र इसे सहन करेगा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आपातकाल में बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की मार्फत एक बार यह प्रयास कर और उसका दुष्परिणाम भी भुगत चुकी है। इसलिए कोई भी सामान्य राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले दल की सरकार ऐसा दुस्साहस शायद ही करे।
पिछले सात दशक से अधिक की अपनी अबाधित यात्रा में भारतीय लोकतंत्र की यात्रा वहां पहुंच चुकी है, जहां उसे अपने संविधान के कुछ आधारभूत सैद्धांतिक आधारों और कानूनों की विकल्पहीन समीक्षा तथा उन पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता है। मसलन, प्रस्तावना में सम्मिलित समाजवाद का विचार, जो वैश्विक राजनीति में अपना हकीकी अस्तित्व गवां चुका है, के आधुनिक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता की विवेचना क्यों नहीं होनी चाहिए?
गौरतलब है कि स्वतंत्र होते ही गांधीवादी सिद्धांतों को भी भुलाते हुए उन्हें संविधान सभा की दहलीज से ही लौटा दिया गया। अगर ऐसा न होता तो प्राथमिक संविधान में विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को सैद्धांतिक आधार मिलता। हाल ही में संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय न्याय संहिता द्वारा न्यायिक व्यवस्था, न्याय संहिता में सुधार के प्रयास किए गए हैं। क्या नए दौर में प्रासंगिक कानूनों की जरूरत नहीं है? इसी अनुकूल अगर अंग्रेजी काल के दो सौ से अधिक निरर्थक कानून समाप्त कर दिए जाएं, तो इसमें क्या बुराई है?
यह समझने की जरूरत है कि संविधान जीवंत भावना और प्रगतिवादी विचार है। उसकी समीक्षा से तात्पर्य उसके केंद्रीय सिद्धांत या मूल ढांचे के प्रति अस्वीकृति या असम्मान का भाव नहीं, बल्कि उसकी रूढ़िबद्धता या सैद्धांतिक ठहराव के प्रति असहमति है। वाद एवं विचारधाराएं, चाहे राजनीतिक-सामाजिक हों या धार्मिक, सार्वकालिक नहीं होतीं। वे तभी जीवित रहती और पल्लवित होती हैं, जब वे समाज के लिए उपयोगी हों। समय-काल के अनुकूल हों। मार्गदर्शन करने में सक्षम हों। वक्त के साथ परिवर्तन की अपेक्षा हर दौर में विचारधाराओं तथा वादों के लिए मौजूं हैं। जो इस परिवर्तन को निषिद्ध करने का प्रयास करते हैं, प्रतिगामी होते हैं। वे समाज के लिए अनुपयोगी और घातक होते हैं। सामाजिक विकास की धारा को भी अवरुद्ध करते हैं। भारतीय संविधानवाद की अवधारणा भी इस तर्क से परे नहीं है। इसलिए संविधान के परिष्कार और परिमार्जन की प्रक्रिया निरंतर गतिशील रहनी चाहिए।