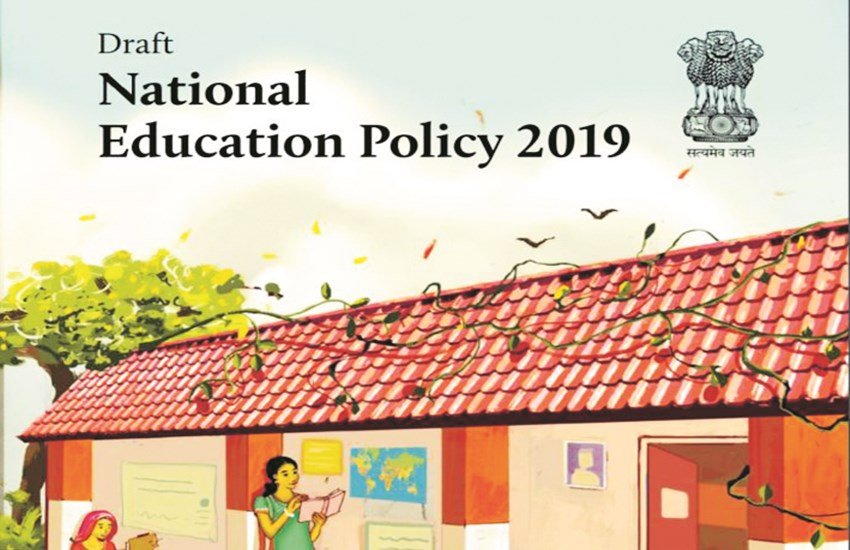स्कूल शिक्षाः
प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-भाल शिक्षा : नीति शुरुआती वर्षों की जरूतर पर जोर देती है और निवेश में पर्याप्त वृद्धि और नई पहलों के साथ 3-6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक-बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लक्षित है। 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की जरूरतों को आंगनबाड़ियों की वर्तमान व्यवस्था द्वारा पूरा किया जाएगा और 5 से 6 वर्ष की उम्र को आंगनबाड़ी / स्कूली प्रणाली के साथ खेल आधारित पाठ्यक्रम के माध्यम से, जिसे एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा, सहज व एकीकृत तरीके से शामिल किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याणतथा जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान : मूलभूत साक्षरता और मूल्य आधारित शिक्षा के साथ संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता पर एक राष्ट्रीय साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन स्थापित किया जाएगा। कक्षा 1-3 में प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एनईपी 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 3 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए।
पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र : मस्तिष्क विकास और अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए एक नई विकास-उपयुक्त पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5 + 3 + 3 + 4 डिजाइन पर विकसित की गई है। पाठ्यक्रम लचीलेपन पर आधारित होगा, ताकि विद्यार्थियों को अपने सीखने की गति और कार्यक्रमों को चुनने का अवसर हो, और इस तरह जीवन में अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार वे अपने रास्ते चुन सकेंगे। कला और विज्ञान, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच में कोई भेद नहीं होगा ताकि सभी प्रकार के ज्ञान की महत्ता को सुनिश्चित किया जा सके, और सीखने के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच की हानिकारक पदानुक्रमों और इनके बीच के परस्पर वर्गीकरण या खाई को समाप्त किया जा सके। इस तरह स्कूल में व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के एकीकरण के साथ सभी विषयों – विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, खेल, गणित इत्यादि पर समान जोर दिया जाएगा।
बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर जोर : कम से कम कक्षा तक, लेकिन कक्षा आठ और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होगी।
उच्चतर शिक्षाः
उच्चतर शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर कम से कम 50 फीसद तक पहुंचाना।
समग्र बहुविषयक शिक्षा : नीति में विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए एकीकृत व श्रमसाध्य ज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर एक व्यापक व बहु-अनुशासनिक समग्र कला शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इसमें कल्पनाशील और लचीली पाठय संरचना, अध्ययन का रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण के साथ कई प्रवेश/निकास हेतु अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।
अभिशासन: प्रत्यायन के आधार पर संस्थागत शासन की शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता परिकल्पित हैं जिसमें प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में एक स्वतंत्र शासक बोर्ड होगा।
विनिमियमन : उच्चतर शिक्षा की प्रोन्नति हेतु एक व्यापक सर्वसमावेशी (अम्ब्रेला) निकाय होगा जिसके अंतर्गत मानक स्थापन, वित्तपोषण, प्रत्यायन, और विनियम के लिए स्वतंत्र इकाइयों की स्थापना की जाएगी। हित के टकराव को खत्म करने व वित्तीय सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक-प्रकटन सुनिश्चित करने हेतु विनिमयन होगा जिसमें निरीक्षक शासन के बजाय पारदर्शी आत्म-प्रकटीकरण एक मानक होगा। विनियामक निकाय प्रौद्योगिकी के माध्यम से फैसले सविनियमन का कार्य करेगा और उसके पास मापदंड अथवा मानकों के विपरीत संचालित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त होंगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर नियमन, प्रत्यायन, फंडिंग व शैक्षणिक मानकों संबंधी मानदंड समान रूप से लागू किए जाएंगे।
मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, जिसके माध्यम से सकल नामांकन अनुपातको 50 फीसद तक बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ऑनलाइन कोर्स एवं डिजिटल रिपॉजिटरी, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण, बेहतर छात्र सेवाओं, मूक की क्रेडिट-आधारित मान्यता आदि उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा कि यह भी उच्चतम गुणवत्ता वाले नियमित कक्षा आधारित कार्यक्रमों के समान हो।
शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण, संस्थागत सहयोग व छात्र और संकाय गतिशीलता के माध्यम से किया जाएगा। शीर्ष विश्व रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों को परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी।
व्यावसायिक शिक्षा: सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। एकल तकनीकी, स्वास्थ्य विज्ञान, विधि और कृषि विश्वविद्यालय अथवा अन्य-विषयों के विश्वविद्यालय, बहु-विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। वोकेशनल शिक्षा समस्त प्रकार की शिक्षा का एक अभिन्न अंग होगी। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 50 फीसद छात्रों कोवोकेशनल शिक्षा प्रदान करना है।
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन : अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित और विस्तारित करने के लिए देश भर में एक नई इकाई स्थापित की जाएगी।
शिक्षा में प्रौद्योगिकी अधिगम, मूल्यांकन, योजना व प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग व विचारों के नि:शुल्क आदान-प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा। कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास का समर्थन, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन तथा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण किया जाएगा।