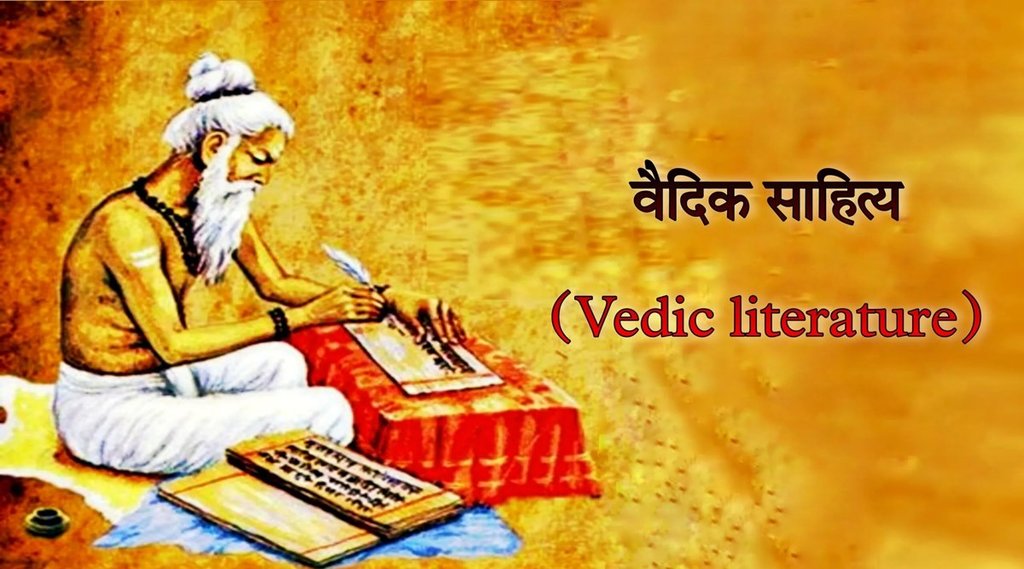पूनम नेगी
समूची सृष्टि पंचमहाभूत अर्थात अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से बनी है। यही पांच तत्व मिलकर समूचे विश्व ब्रह्मांड के जड़, चेतन और जीवों का निर्माण और पोषण करते हैं। वैदिक मनीषियों का प्रतिपादन है कि इन पंचमहाभूतों का संतुलन ही जीवनचक्र को नियंत्रित करता है और इसमें गतिरोध आते ही जीवन संकट में पड़ जाता है।
इसीलिए वैदिक ऋ षियों ने इन पंचतत्वों को शुद्ध एवं संरक्षित रखने हेतु अनेक नियम-उपनियम बनाए थे। ऋ ग्वेद में अग्नि के रूप-गुण और रूपांतर, यजुर्वेद में जल तथा वायुतत्व के गुणों, कार्य और विभिन्न रूपों एवं अथर्ववेद में पृथ्वीतत्व के गुणों की अद्भुत व्याख्या की गई है। वैदिककाल में इन प्राकृतिक शक्तियों को देवस्वरूप माना जाता था। इसीलिए उस युग में समस्त सृष्टि में सुख-शांति व समृद्धि का वातावरण था।
ऋ ग्वेद की ऋ चा कहती है-हे वायु! अपनी औषधि ले आओ और यहां से सब दोष दूर करो, क्योंकि तुम ही सभी औषधियों से भरपूर हो। ऋग्वेद का एक अन्य मंत्र जल की शुद्धता का वर्णन करते हुए कहता है, आओ सभी मिल कर प्रवाहित जल के प्रशंसा के गीत गाएं जो हजारों धाराओं से स्फटिक की तरह बहकर आंखों को आनंद देता है। उपनिषद्कारों ने भी ऊर्जा के अपरिमित स्रोत सूर्य को जगत की आत्मा कहकर उसकी अभ्यर्थना की है, सूर्य को प्राण की संज्ञा दी है।
यज्ञों के माध्यम से वायुमंडल को शुद्ध करना भी वेदों का विषय रहा है। वैदिककाल में पर्यावरण के परिष्कार के लिए यज्ञ-हवन संपन्न किए जाते थे। सामवेद में जीवन की मंगलकामना और प्रकृति की अविरल उपासना के भाव वर्णित हैं। इसमें वनस्पतियों और पशुजगत तथा औषधि विज्ञान के सुंदर मंत्रों के उद्धरण हैं। सामवेद कहता है झ्र हे इंद्र, सूर्य रश्मियों और वायु से हमारे लिए औषधि की उत्पत्ति करो। हे सोम, आपने ही औषधियों, जलों और पशुओं को उत्पन्न किया है।
अथर्ववेद में भी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संबंधी चिंतन का गौरवगान हुआ है। पृथ्वी सूक्त में अथर्वण ऋषि धरा की महानता, उदारता, सर्वव्यापकता आदि अनंत गुणों पर विस्मित हो कह उठते हैं, हे माता! आपके लिए ईश्वर ने शीत, वर्षा तथा वसंत ऋ तुएं बनाई हैं। दिन-रात के चक्र स्थापित किए हैं। इस कृपा के लिए हम ईश्वर के आभारी हैं।
वे खनन से पूर्व धरती माता से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, जीविकोपार्जन के लिए हम ऐसा करने को बाध्य हैं, किन्तु हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह तुम्हें पुन: हरा-भरा कर दे। हम भूमि के जिस स्थान पर खनन करें, वहां शीघ्र ही हरियाली छा जाए। आपसे प्रार्थना है कि ऐसी सद्धबुद्धि दें जिससे हम आपके हृदय स्थल को न तो आहत करें, और न ही आपको दु:ख पहुंचाएं। व्यक्ति स्वस्थ, सुखी दीर्घायु रहे, नीति पर चले और पशु वनस्पति एवं जगत् के साथ साहचर्य रखे, यही वैदिक साहित्य की विशेषता है।
वैदिक कर्मकांडों की अनेक विधाओं में भी पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा का दायित्व निभाया गया है। अरण्यों में रहकर पर्यावरण के प्रति विशेष जागरूक रहने वाले ऋषियों ने आरण्यक साहित्य का सृजन कर विश्व में पर्यावरण के महत्त्व को रेखांकित किया है।आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों के बीच की कड़ी हैं। ‘अरण्ये भवमेति आरण्यकम्’ कहकर आरण्यक का अर्थ स्पष्ट किया गया है। बृहदारण्यक भी ‘अरण्येनूत्यमानत्वात अरण्यकम के रूप में इसका समर्थन करता है। इसका विषय प्राणविद्या है।
अंतरिक्ष और वायु से प्राण का संबंध अन्योन्याश्रित है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों में भी वायु और अंतरिक्ष का विशेष योगदान रहता है। सृष्टि के सभी तत्वों में इन दोनों का समावेश है। इन्हीं गुणों के कारण सृष्टि के सभी तत्वों को प्राणशक्ति मिलती है जिससे विकास की गति अग्रसर होती है।
दु:ख का विषय है कि आधुनिकता की आंधी ने पर्यावरण संरक्षण की इस वैदिक परंपरा को भारी नुकसान पहुंचाया है। दोहन और शोषण, वैभव एवं विलास की रीति नीति ने पर्यावरण को घोर संकट में डाल दिया है। समस्या के सार्थक निदान के लिए जरूरी है कि हम अपनी विरासत को संभालें। पर्यावरण संरक्षण की टूट-बिखर रही कडियÞों को पुन: जोड़े। हममें से प्रत्येक मन-वाणी-कर्म से इस सत्य का वेदकालीन महर्षियों के स्वर-में-स्वर मिलाकर सस्वर उद्घोष करें-ॐ द्यौ शांति: अंतरिक्ष शांति: पृथ्वी शांति: आप: शांति:। जब हम अपने आचरण व्यवहार से माता प्रकृति के कोप को शांत करेंगे, तभी हमारा अपना जीवन भी शांत और सुखी होगा।
उपनिषदों में विशद् वर्णन
उपनिषदों में जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष का विशद् वर्णन हुआ है। इनके अनुसार पदार्थ की उत्पत्ति एवं जीव-जगत् की सृष्टि अग्नि, जल और पृथ्वी के विनियोग से हुई है। पृथ्वी का रस जल है और जल का रस औषध है। रामायण व महाभारतकालीन मनीषियों ने भी पर्यावरण की गौरव गरिमा को महिमा मंडित किया है।
विभिन्न साहित्यिक उद्धरण बताते हैं कि उन दिनों पर्यावरण अत्यंत समृद्ध था। रामायण कालीन ग्रंथों में प्रकृति को सजीव व निर्जीव दोनों ही तत्वों से चेतना संपन्न बताया गया है। उन दिनों वृक्षों की पूजा का प्रचुर प्रचलन था। वृक्षों को काटना महापाप समझा जाता था। वहीं महाभारत काल में भगवान् कृष्ण ने भगवद्गीता में प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण बताया गया है।
श्रीकृष्ण कहते हैं , प्रकृति के कण -कण में सृष्टि का रचयिता समाया हुआ है। प्रकृति के समस्त चमत्कारों को परमेश्वर का स्वरूप बताते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सभी भूत-प्राणियों को धारण करता हूँ। चंद्रमा बनकर औषधियों का पोषण करता हूं। महाभारतकाल में प्रत्येक तत्व को देवता सदृश स्वीकार कर उनकी अभ्यर्थना की जाती थी। महाभारत के आदिपर्व में वर्णन है कि गाँव में जो जगह पेड़ फूल और फलों से भरपूर हो, वह स्थान हर तरह से अर्चनीय है। पवित्र और शीतल जलाशय तथा जंगल पहाड़ व पर्वतों आदि को प्रकृति व पर्यावरण के अद्भुत प्रसंगों से महाभारत के सभी पर्व भरे पड़े हैं।