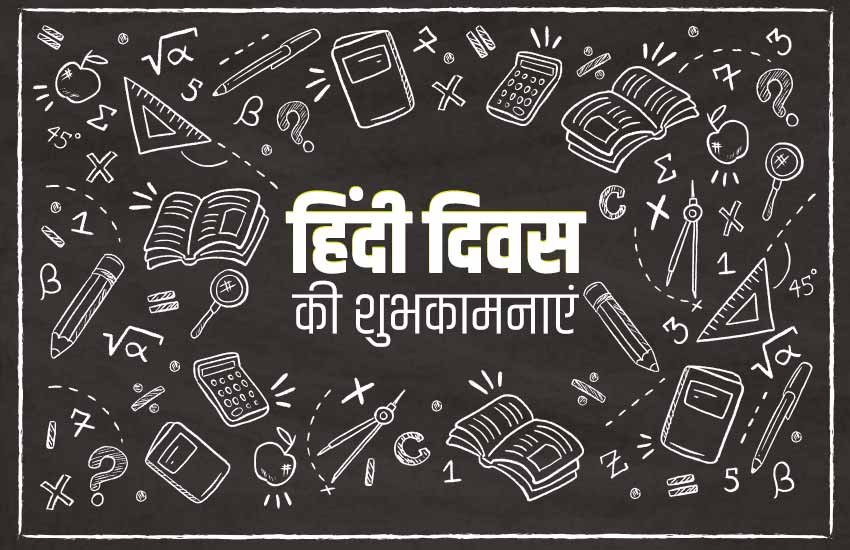इंसान जन्मदिवस मनाता है ताकि वह अपने अस्तित्व का उत्सव मना सके। किसी की पुण्यतिथि मनाता है ताकि उस व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा ले सके। लेकिन हम किसी भाषा के लिए कोई खास दिवस क्यों मनाते हैं? उस भाषा का प्रचार-प्रसार करने के लिए या उस सामूहिक भावना के लिए, जिसके ज़रिए किसी ख़ास क़िस्म के गर्व की चर्चा की जा सके। वैसे भी श्रेष्ठता दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान की प्राकृतिक चाहत होती है फिर वह चाहे किसी क्षेत्र में न क्यों न हो। अपनी भाषा को लेकर लोगों के लगाव को तो किसी भी पैमाने से नापना मुश्किल हो सकता है।
आज की हिंदी, कल की हिंदी, नई वाली हिंदी, पुरानी वाली हिंदी; ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आजकल हिंदी साहित्य की दुनिया में प्रचलित हैं। भाषा का यह वर्गीकरण कितना सही या ग़लत है, यह तो हिंदी को बेहतर तरीक़े से समझने वाले ही बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कम्प्यूटर युग के फोनेटिक और इंस्क्रिप्ट वाले दौर में भी हिंदी ने अपनी जगह स्मार्ट तरीक़े से बनाई है। किसी भाषा को इतना लचीला होना भी चाहिए कि वह बदलती पीढ़ी के आम लोगों से जुड़ी रहे। भाषाओं के हज़ारों साल पुराने इतिहास में हिंदी जैसी नई-नवेली भाषा के लिए यह और ज़रूरी हो जाता है कि इसमें प्रयोग जारी रहें।
प्रश्न यह उठता है कि क्या हिंदी में नए प्रयोग इसकी मौलिकता को नुक़सान पहुंचा रहे हैं। इस सवाल का जवाब कुछ लोग हां, तो कुछ ना में देंगे। लेकिन इससे भी ज़रूरी सवाल यह है कि हिंदी की मौलिकता है क्या। क्या भाषा सिर्फ़ शब्दावली से बनती है? और हिंदी की शब्दावली की क्या सीमा है? शब्दावली को कौन बढ़ाता-घटाता है? हम बचपन से पढ़ते आएँ हैं कि फ़लां शब्द फ़ारसी या लैटिन मूल का है। अंग्रेज़ी के तो ज़्यादातर शब्द दूसरी भाषा से आयातित ही मिलते हैं फिर भी आज वह दुनिया की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। तो क्या हिंदी के लिए ‘मौलिकता’ को मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या भाषा बस लिपि का वहम मात्र होती है? ऐसे न जाने कितने सवाल हो सकते हैं, जिन पर हिंदी या किसी भी भाषा के ‘दिवस’ पर चर्चा हो सकती है।
हिंदी के नज़रिए से यह अच्छी बात है कि इसने तमाम कठिन सवालों की फ़िक्र छोड़कर अपने जवाब बहुत सरल तरीक़े से तय किए हैं। हिंदी ने हर उस शख़्स को अपनाया है जिसने इसके प्रति ज़रा-सी भी इज़्ज़त बख़्शी है। अंग्रेज़ी के दबाव में हीन भावना से पार पाते हुए जिस किसी ने भी हिंदी को तवज्जो दी है उसे उसका रिटर्न मिला है। लेकिन समस्या यह है कि हिंदी को लेकर हिंदुस्तानियों, ख़ासकर उत्तर भारतीयों की अधिकारात्मकता बहुत सुविधाजनक तरीक़े से विकसित होती है। ज़रूरत बस इसी तरीक़े को बदलने की है। निस्संदेह, तमाम सरकारी नीतियां और बाज़ार की ज़रूरत भाषा की रफ़्तार को नियंत्रित करने की ताक़त रखती हैं लेकिन यह भी बिना हमारी ‘अनुमति’ के भी संभव नहीं। दक्षिण भारतीय भाषाओं के मामले में यह देखा जा सकता है।
हिंदी की ख़ूबसरती इसकी विविधता है जो लगातार और विस्तारित हो रही है। अपने अस्तित्व को ख़तरे में डालकर कई आँचलिक बोलियों ने हिंदी को पोषित किया है, इसे भाषा बनाया है। हम सभी हिंदीभाषियों की ज़िम्मेदारी है कि अपनी विरासत को सही तरीक़े से संभालते हुए इसके विकास में अपना योगदान देते हुए आगे बढ़ें। हिंदी को ‘मां’ मानने से आगे बढ़ते हुए हमें ख़ुद को हिंदी कुल का वह सदस्य बनना होगा, जिसे हमेशा अपने परिवार के अस्तित्व और सम्मान की फ़िक्र होती है।
ये हमारे लेखक, नूतन कुमार गुप्ता के निजी विचार हैं