भारत में राजनीति लंबे समय से जाति और धर्म से बंधी हुई है। उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास भी इससे अलग नहीं है। जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है, जाति ने राज्य के चुनावी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
शुरुआत से ही उत्तराखंड राज्य की मांग विकास और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर थी। उच्च जातियों के प्रभुत्व वाले इस पहाड़ी क्षेत्र में 1994 के आरक्षण विरोधी आंदोलन ने इस लंबे समय से चली आ रही मांग को गति दी, जिसके कारण अंततः 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ।
ब्राह्मणों और ठाकुरों का रहा वर्चस्व
उत्तराखंड की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर ऊंची जातियों की तरफ झुकाव साफ दिखाई देता है। यहां ब्राह्मण और ठाकुर दो सबसे बड़े मतदाता वर्ग हैं। राज्य की आबादी में ठाकुरों की संख्या लगभग 35% है, वहीं ब्राह्मणों की संख्या लगभग 25% है। इन जातियों का प्रभुत्व राज्य में नेतृत्व पर भी साफ़ दिखाई देता है। 2000 के बाद से, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए किसी ठाकुर या ब्राह्मण नेता को नॉमिनेट किया है।
उत्तराखंड की राजनीति में ठाकुरों और ब्राह्मणों का बोलबाला
उत्तराखंड में ब्राह्मण और ठाकुर समुदायों के बीच सदियों से विभाजन देखा गया है। ऐतिहासिक रूप से, इन दो उच्च जाति समूहों में सत्ता और प्रभाव के लिए होड़ रही है। दोनों ही जातियों का राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। ब्राह्मण जो परंपरागत रूप से पंडित- पुरोहित के काम में लगे हुए हैं, ज़्यादातर कुमाऊं की पहाड़ियों में प्रभावी हैं। वहीं, ठाकुर जो अपनी मार्शल विरासत के लिए जाने जाते हैं, गढ़वाल के मैदानी इलाकों में काफी प्रभाव रखते हैं।
इस विभाजन ने न केवल उत्तराखंड के सामाजिक ताने-बाने को आकार दिया है बल्कि इसकी गूंज यहां के राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी है। राज्य में ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं की अच्छी-खासी हिस्सेदारी रही है।
उत्तराखंड के प्रमुख ब्राह्मण नेता
सबसे बड़े ब्राह्मण नेताओं में भाजपा के दो बार के सीएम बीसी खंडूरी हैं। उन्हें अक्सर “गढ़वाल के मुख्यमंत्री” के रूप में जाना जाता था क्योंकि वह इसी क्षेत्र से आते थे। राज्य के अन्य प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में कांग्रेस के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हैं। ठाकुर नेताओं में बीजेपी के मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़े चेहरों में से एक हैं। अन्य वरिष्ठ ठाकुर नेताओं में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और भगत सिंह कोश्यारी और कांग्रेस के हरीश रावत और भाजपा के राज्य मंत्री सतपाल महाराज शामिल हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इन नेताओं का अपने-अपने समुदायों के मतदाताओं पर काफी प्रभाव होने के बावजूद, भाजपा और कांग्रेस दोनों व्यापक चुनावी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं जिससे चुनावों में राज्य के अन्य मतदाता भी जुड़ाव महसूस कर सकें।
उत्तराखंड की राजनीति में दलितों और मुस्लिमों की भूमिका
राज्य में दलित समुदाय भी चुनावी नतीजों पर असर डालने की क्षमता रखता है। हालांकि, उनका प्रभाव मुख्य रूप से हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। राज्य की आबादी का लगभग 19% हिस्सा दलितों का है जो मुख्य रूप से कारीगर, शिल्पकार और सीमांत किसान हैं। दलित यहां तीन मुख्य उप-जातियों में विभाजित हैं – कोलता, डोम, और बाजगी या लोहार। आरक्षण के लाभ का हकदार होने के बावजूद यह समुदाय सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार से जूझ रहा है और राजनीतिक रूप से हाशिए पर है।
उत्तराखंड के गठन के शुरुआती वर्षों में, दलित और ओबीसी समुदाय बड़े पैमाने पर बसपा और उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) जैसे अन्य क्षेत्रीय दलों के पीछे एकजुट हुए। हालांकि, पिछले कुछ सालों में भाजपा दलित वोटों (मुख्य रूप से जाटवों) को अपने पक्ष में एकजुट करने में सफल रही है।

उत्तराखंड के मुस्लिम किसके साथ?
वहीं, दूसरी ओर मुस्लिम जो राज्य की आबादी का लगभग 13% हैं, पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ रहे हैं। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल (हल्द्वानी) और उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में मुस्लिम समुदाय का प्रभाव है। उत्तराखंड में मुसलमानों का एक वर्ग रोजगार की तलाश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से पलायन कर गया है।
राज्य में एक फॉल्टलाइन कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रों के बीच विभाजन पर भी केंद्रित है। संस्कृति, बोली और सामाजिक-आर्थिक पैटर्न के मामले में ऐतिहासिक रूप से अलग, कुमाऊं और गढ़वाल का अंदाज अक्सर पूरे उत्तराखंड से अलग रहा है। जहां कुमाऊं की विशेषता उसकी घाटियां, विशिष्ट लोककथाएं और कृषि पद्धतियां हैं। वहीं गढ़वाल ऊबड़-खाबड़ इलाके, धार्मिक परंपराओं और मार्शल वीरता से भरा हुआ है।
पढ़ें गढ़वाल से ग्राउंड रिपोर्ट
BJP Garhwal Lok Sabha candidate Anil Baluni: मंदिर से शुरुआत, गंगा आरती से समाप्ति…हर परिवार को रोजगार और पर्यटन को रफ्तार की उम्मीदों के साथ ऐसे चल रहा अनिल बलूनी का प्रचार

राज्य में मैदानों पर पहाड़ों पर अलग हैं लोगों के मुद्दे
उत्तराखंड के 13 जिलों में से 6 जिले और 70 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं जबकि गढ़वाल में सात जिले और 41 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि, लोकसभा चुनावों के संदर्भ में यह क्षेत्रीय रेखाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं और यह विभाजन कम महत्व रखता है।
एक और विभाजन कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में पहाड़ियों और मैदानों के बीच है, जिसे पार्टियों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जहां कठिन इलाकों में रहने वाली आबादी को बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसरों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं, दूसरी ओर मैदानी इलाके संसाधनों, आर्थिक अवसरों और शहरी सुविधाओं तक अपेक्षाकृत बेहतर पहुंच रखते हैं।
यह विभाजन अक्सर पहाड़ी समुदायों को उपेक्षित और हाशिए पर रखा हुआ महसूस करता है जो विकास की प्रक्रिया में खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। पहाड़ियों और मैदानों के बीच समान विकास और संसाधन आवंटन का मुद्दा राज्य के राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता से उठता है क्योंकि उम्मीदवार दोनों पक्षों की शिकायतों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं।
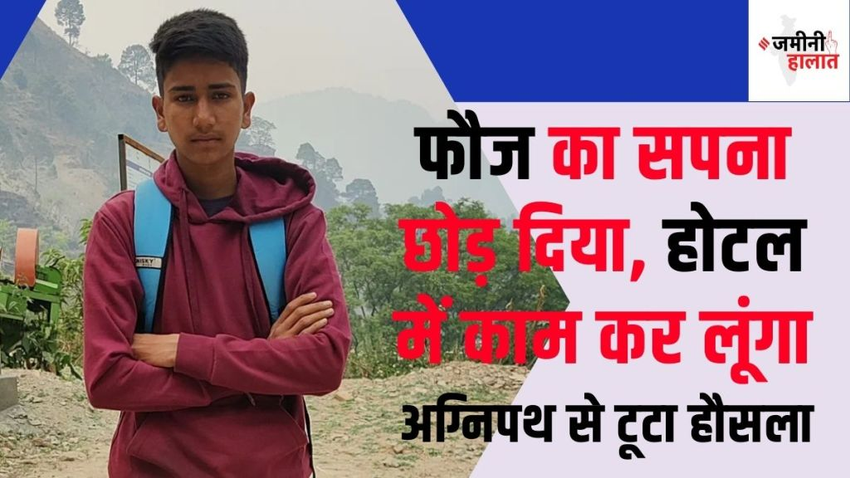
उत्तराखंड में पिछले चुनाव के परिणाम
उत्तराखंड में पिछले दोनों चुनाव में भाजपा ने सरकार बनाई थी। 2019 के आम चुनावों में सभी 5 सीटें भाजपा ने जीतीं थीं। पार्टी को इस चुनाव में 61.01% वोट हासिल हुए थे। वहीं, 2014 के चुनावों की बात की जाए तो उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। पार्टी ने सभी 5 सीटें जीतते हुए 55.30% वोट हासिल किया था।


