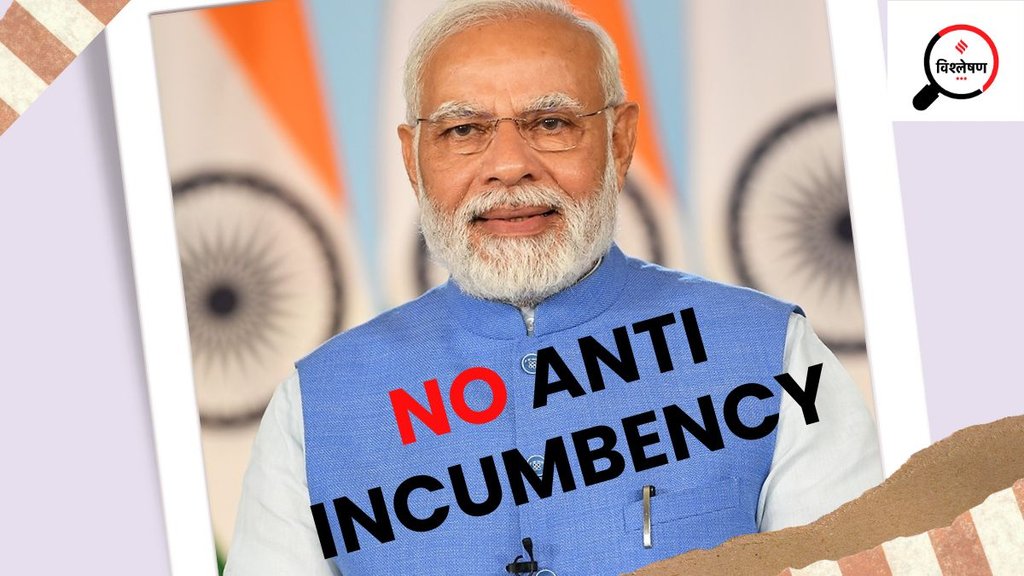क्या लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता विरोधी लहर (एंटी-इंकम्बेंसी Anti-Incumbency) कोई फैक्टर है? चुनाव विश्लेषक प्रणय रॉय और दोराब आर. सुपारीवाला की राय में नहीं। रॉय ने इस मुद्दे पर सुपारीवाला के साथ चर्चा का एक वीडियो अपने प्लैटफॉर्म ‘डिकोडर’ पर पोस्ट किया है और एंटी इंकम्बेंसी से जुड़े कई पहलुओं पर आंकड़ों के साथ बात की है।
विश्लेषण के मुताबिक पिछले 2002 से 2024 के बीच हुए चुनावों (बड़े राज्यों में हुए 83 चुनावों सहित) में 51% में सरकार को दोबारा मौका नहीं मिला, वहीं 49% सरकारों को दोबारा चुना गया। मतलब सरकार रिपीट होने का चांस 50-50 रहा।
दोआब ने बताया कि 1977 से 2002 के दौरान सबसे ज्यादा एंटी-इंकम्बेंसी देखी गयी। इन 25 सालों (1977-2002) के दौरान लगभग 71% सरकारों (बड़े राज्यों के 93 चुनाव सहित) को जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया। वहीं, छोटे और मंझोले राज्यों में लगभग 94% मौजूदा सरकारों (32 राज्यों के चुनाव) को जनता ने पलट दिया।
भारतीय चुनाव के इतिहास के शुरुआती 25 सालों के दौरान सत्ता समर्थक लहर
विश्लेषक दोआब ने इसके पीछे का कारण भी बताया। उनके मुताबिक, आपातकाल के बाद जनता को लगा कि उसके पास सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत है। इससे पहले जनता को लगा ही नहीं था कि वह ऐसा कर सकती है। सपा, बसपा, आरजेडी, बीजेपी जैसी तमाम पार्टियां 1977 से 2002 के दौरान ही खड़ी हुईं। साथ ही क्षेत्रीय दल भी इस दौरान मजबूत हुए।
वहीं, भारतीय चुनाव के इतिहास के शुरुआती 25 सालों के दौरान एक सत्ता समर्थक लहर थी। 1952-1977 के बीच लगभग 82% सरकारों को दोबारा सत्ता हासिल हुई, 5 में से सिर्फ 1 सरकार को ही वापसी का मौका नहीं मिला था।
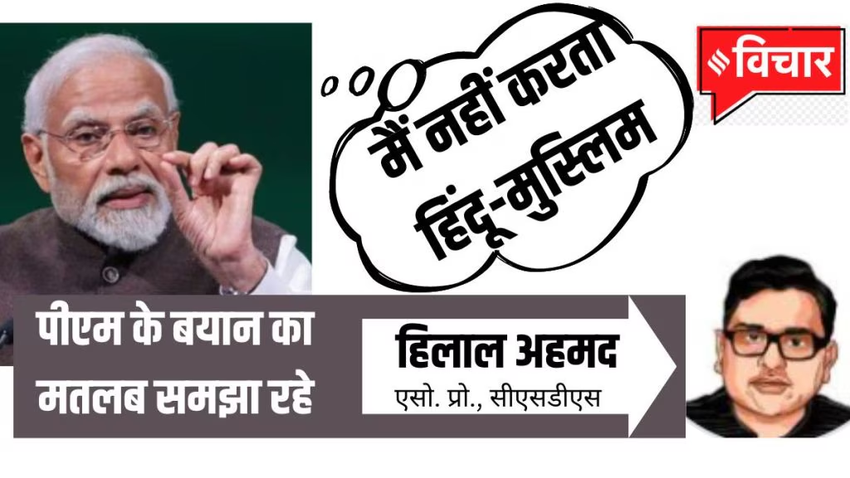
इस विश्लेषण के आधार पर प्रणय रॉय ने एंटी इंकम्बेंसी के लिहाज से भारतीय लोकतंत्र को तीन चरणों में बांटा। पहला- सत्ता समर्थक दौर (1952-1977) जहां 82% सरकारों को दोबारा सत्ता हासिल हुई। दूसरा- सत्ता विरोधी दौर (1977-2002) जहां 71% सरकारों को जनता ने वापस वोट नहीं किया और तीसरा और वर्तमान दौर (2002-2024) जहां वापस सत्ता में आने और दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली दोनों सरकारों की संख्या 50-50% रही।

सांसदों पर एंटी इंकम्बेंसी का कितना असर
सत्ता-विरोधी लहर को दो तरीकों से मापा जा सकता है- पार्टी या सरकार-स्तर पर, यानी सरकार की लगातार कार्यकाल जीतने की क्षमता और व्यक्तिगत स्तर की सत्ता, यानी सांसदों की दोबारा निर्वाचित होने की क्षमता।
सांसदों की बात करें तो नीच के टेबल से समझा सकता है कि 1991 से 2014 के बीच कितने सांसदों को लगातार संसद पहुंचने का मौका मिला।
| चुनावी वर्ष | सांसद जो लगातार चुनाव लड़े (%) | सांसद जो लगातार चुनाव जीते (%) |
| 1991 | 68.9 | 43.5 |
| 1996 | 67 | 34.4 |
| 1998 | 83.1 | 44.8 |
| 1999 | 83.4 | 50.3 |
| 2004 | 76.6 | 41.6 |
| 2009 | 66.3 | 32.6 |
| 2014 | 72 | 30.8 |
ऐसे बदलता गया पहली बार बने सांसदों का ट्रेंड
1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद, 1971 में इंदिरा गांधी ने कई नए उम्मीदवारों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। 1977 में जनता गठबंधन की जीत ने भी संसद में कई नए सांसद लाए। 1990 के दशक के दौरान पहली बार सांसद बनने वाले नेताओं का का अनुपात अपेक्षाकृत कम हो गया। 1999 में अधिकांश पार्टियों ने पुराने सांसदों को ही दोबारा चुनाव में खड़ा किया। 2014 में, नए सिरे से चुनाव लड़ने वाले अधिकांश भाजपा सांसद फिर से निर्वाचित हुए (88.8%), जबकि उनमें से आधे पांच साल पहले चुने गए थे।
पहली बार लोकसभा पहुंचने वाले सांसद
| चुनावी वर्ष | पहली बार लोकसभा पहुंचने वाले सांसद (प्रतिशत) |
| 1971 | 72.8 |
| 1977 | 77.5 |
| 1980 | 63.3 |
| 1984 | 60.3 |
| 1989 | 58.6 |
| 1991 | 43.0 |
| 1996 | 55.6 |
| 1998 | 42.9 |
| 1999 | 32.8 |
| 2004 | 40.7 |
| 2009 | 53.4 |
| 2014 | 58.4 |
कांग्रेस और बीजेपी की तुलना
भाजपा और कांग्रेस औसतन 46% अपने सत्ताधारी सांसदों को फिर से मैदान में उतारते रहे थे। 2004 के बाद, संख्या में गिरावट आई क्योंकि पार्टी ने अपने अधिकाधिक मौजूदा सांसदों को खारिज कर दिया। 2014 में, वापस चुनाव में खड़े होने वाले सांसदों की संख्या फिर से थोड़ी बढ़कर 40.6% हो गई। उनमें से अधिकांश (88.8%) पुनः निर्वाचित हुए। वहीं, कांग्रेस अपने आधे से भी कम सांसदों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका देती है।
प्रदर्शन के मामले में, दोबारा चुनाव लड़ने वाले बीजेपी सांसद कांग्रेस के सांसदों से अधिक सफल होते हैं।