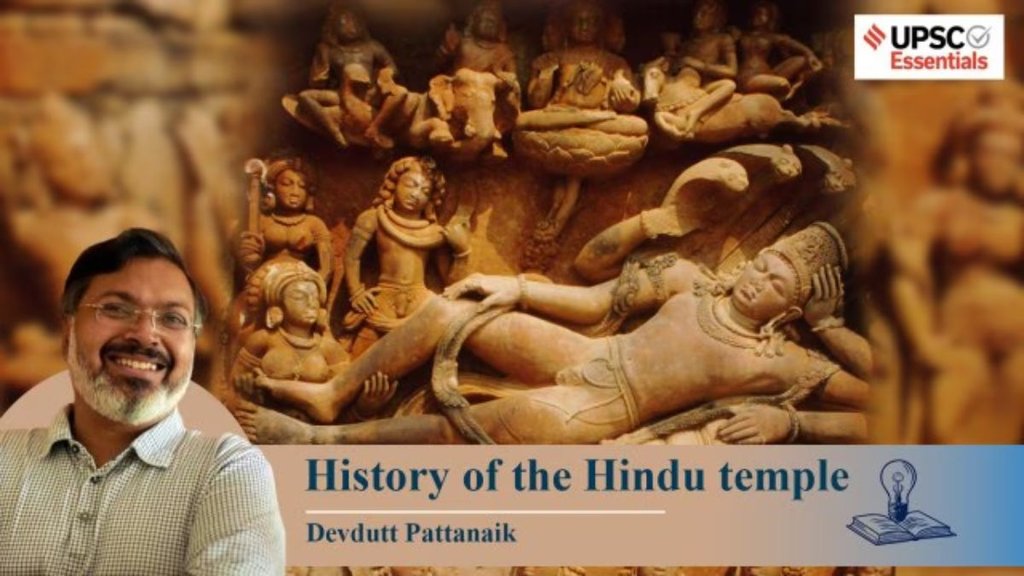(द इंडियन एक्सप्रेस ने UPSC उम्मीदवारों के लिए इतिहास, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कला, संस्कृति और विरासत, पर्यावरण, भूगोल, विज्ञान और टेक्नोलॉजी आदि जैसे मुद्दों और कॉन्सेप्ट्स पर अनुभवी लेखकों और स्कॉलर्स द्वारा लिखे गए लेखों की एक नई सीरीज शुरू की है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ें और विचार करें और बहुप्रतीक्षित UPSC CSE को पास करने के अपने चांस को बढ़ाएं। पौराणिक कथाओं और संस्कृति में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपने इस लेख में हिंदू मंदिरों के बारे में बात की है।)
जैसा कि हम आज जानते हैं, हिंदू मंदिर 5000 साल पुराना नहीं है। प्राचीन काल में लोग अपने देवताओं की पूजा बंद गर्भगृहों या मूर्तियों में नहीं करते थे। बल्कि, प्रकृति में ही ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव होता था। पेड़, जानवर, नदियां, पहाड़ और चट्टानें, सभी पवित्र रूप थे। लगभग 2,000 साल पहले ही हमें मथुरा में हिंदू देवताओं की पहली मूर्तियां दिखाई देने लगीं। दिलचस्प बात यह है कि उसी काल के कुषाण सिक्कों पर शिव, विष्णु और देवी की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं, हालांकि, विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये वास्तव में हिंदू देवता हैं या पारसी और यूनानी प्रभावों से प्रभावित प्रतीक हैं।
प्रकृति पूजा से मूर्ति पूजा तक
लगभग 1800 साल पहले लगभग 200 ईस्वी तक, मथुरा की बलुआ पत्थर की मूर्तियों में हिंदू देवताओं को पहचानने योग्य रूपों में साफ तौर पर दर्शाया गया है। यहां हम शिवलिंग देखते हैं, जिन पर कभी-कभी मुख खुदे होते हैं। साथ ही विष्णु, कृष्ण और बलराम की मूर्तियां भी होती हैं। ये अभी तक मंदिरों के अंदर नहीं रखे गए थे जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। इसके बजाय, उन्हें पवित्र उपवनों में अक्सर नदियों के किनारे स्थापित किया जाता था और खुली जगहों में उनकी पूजा की जाती थी, बिल्कुल पहले के प्राकृतिक मंदिरों की तरह। यह चरण हमें प्रकृति पूजा से मूर्ति पूजा की ओर क्रमिक परिवर्तन दर्शाता है।
अगला चरण इन मूर्तियों को संरचनाओं के भीतर स्थापित करना था। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में, लगभग 500 ईस्वी पूर्व का, हमें एक ईंटों का मंदिर मिलता है जहां मूर्तियों को एक गर्भगृह के अंदर स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के नचना में एक शिव मंदिर का निर्माण किया गया था जिसने हिमालय के इकोसिस्टम को दोहराने का प्रयास किया था। इसकी छत एक पर्वत के आकार की थी और द्वार पर नदी देवियों गंगा और यमुना की नक्काशी की गई थी।
झांसी के पास देवगढ़ में, हमें पूरी तरह से पत्थर से बने सबसे पुराने विष्णु मंदिरों में से एक मिलता है। इस मंदिर में अनंत नाग पर लेटे हुए विष्णु और चार भुजाओं वाले गरुड़ पर सवार विष्णु की प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, जो राम और कृष्ण के जीवन से संबंधित हैं। ये शास्त्रीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत हैं।
रॉक-कट और स्वतंत्र मंदिर
इस चरण के बाद 600 ईस्वी के बाद स्मारकीय चट्टान-कट मंदिरों का युग आया। यहां, कला सचमुच विशाल हो गई। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं, कर्नाटक के पट्टाडकल के मंदिर और चेन्नई के पास मामल्लपुरम के तट मंदिर की चट्टानों पर उकेरी गई नक्काशी, सभी शिव और विष्णु के भव्य चित्रण प्रस्तुत करती हैं। ये केवल पूजा स्थल ही नहीं थे, बल्कि शाही शक्ति के प्रतीक भी थे, जिन्हें सीधे पहाड़ों और चट्टानों पर उकेरा गया था, मानो यह दर्शाने के लिए कि राजा धरती को भी आकार दे सकते हैं।
आठवीं शताब्दी तक हमें और भी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। एलोरा में, कैलाशनाथ मंदिर को एक ही चट्टान को तराशकर शिव के लिए एक पहाड़ी महल जैसा बनाया गया था। इस काल में स्वतंत्र मंदिरों का भी उदय हुआ, जो चट्टानों को तराशने के बजाय पत्थर दर पत्थर बनाए गए थे। ये कर्नाटक के हम्पी और पट्टाडकल के साथ-साथ प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर के केंद्र कांचीपुरम में भी दिखाई देते हैं।
स्वतंत्र मंदिर प्रयोगात्मक रूपों से स्थायी स्थापत्य शैलियों की ओर बदलाव का प्रतीक है। दसवीं शताब्दी तक मंदिर वास्तुकला की जटिलता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसमें उत्तर की वक्ररेखीय ‘नागर’ शैली और दक्षिण की पिरामिडनुमा ‘विमान’ शैली शामिल। मंदिर तांत्रिक मंडलों पर बनाए जाते थे, जो न केवल देवताओं के घरों के रूप में, बल्कि अनुष्ठान शक्ति के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। इनके अंदर, पुजारी धन, सुरक्षा और सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करते थे।
ये प्रारंभिक मंदिर उन भक्ति मंदिरों से बहुत अलग थे जिनसे हममें से ज्यादातर लोग आज परिचित हैं। ये अनुष्ठान प्रयोगशालाओं के ज्यादा पास थे, जहां कला और मंत्र मिलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के क्षेत्र बनाते थे।
मंदिरों ने परिवर्तनों और आक्रमणों का सामना कैसे किया
बाद में भक्ति आंदोलन के उदय के साथ मंदिरों में एक बार फिर बदलाव आया। गुप्त तांत्रिक अनुष्ठानों से हटकर जनभागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। लोगों को गायन, नृत्य और सक्रिय रूप से पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यही वह समय था जब पुरी में जगन्नाथ और तमिलनाडु में श्रीरंगम जैसे महान वैष्णव मंदिर लोकप्रिय हुए। यहां मंदिर लोगों के लिए भगवान का घर बन गया।
आम धारणा के विपरीत 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर हमले के तुरंत बाद की शताब्दियों में भारत में कई मंदिरों का निर्माण हुआ। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर परिसर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाद में व्यापार मार्ग बदलने पर इसे छोड़ दिया गया। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर परिसर भी लगभग इसी समय बनाया गया था। अकबर के राजपूत सेनापति मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में वृंदावन में गोविंदराज मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया।
ये भी पढ़ें: तुर्क और अफगानी आक्रांताओं ने कैसे बदला भारत में युद्ध करने का तरीका?
जब मुस्लिम सरदारों ने मंदिरों पर हमला किया, तो लोग अक्सर निजी घरों में रखी जाने वाली देवताओं की छोटी-छोटी पोर्टेबल मूर्तियों की ओर चले गए या राजस्थान में सुरक्षित हवेली-शैली के घरों में चले गए। 17वीं शताब्दी के दौरान, बंगाल में कृष्ण को समर्पित नए टेराकोटा मंदिर दिखाई दिए, जो स्थानीय कलात्मक परंपराओं और भक्ति आवश्यकताओं, दोनों को दर्शाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों के उदय के साथ मंदिर निर्माण की एक नई लहर आई। भोंसले और होल्कर जैसे नेताओं ने हिंदू मंदिरों का निर्माण किया, विशेष रूप से नासिक, ग्वालियर और काशी जैसे स्थानों में, विशेष रूप से राम को समर्पित। इस प्रकार, हिंदू मंदिर सहस्राब्दियों से स्थिर नहीं रहे हैं। ये निरंतर विकसित होते रहे हैं और दर्शन में सभी प्रकार की चुनौतियों और बदलावों का सामना करते रहे हैं।
लेख से जुड़े प्रश्न
प्राचीन काल में बंद मंदिरों और मूर्तियों के उद्भव से पहले ईश्वर का अनुभव कैसे किया जाता था?
प्रकृति पूजा से मूर्ति पूजा में परिवर्तन ने प्रारंभिक हिंदू धार्मिक प्रथाओं को कैसे आकार दिया?
भक्ति आंदोलन के उदय के साथ मंदिरों में क्या बदलाव आया?
यद्यपि स्वतंत्र मंदिर ने प्रयोगात्मक रूपों से स्थायी स्थापत्य शैलियों में बदलाव को चिह्नित किया, बाद की शताब्दियों में कौन सी अन्य प्रमुख स्थापत्य शैलियां उभरीं?
हिंदू मंदिर सहस्राब्दियों से स्थिर नहीं रहे हैं और निरंतर विकसित होते रहे हैं और दर्शन में सभी प्रकार की चुनौतियों और बदलावों का सामना करते रहे हैं। विस्तार से बताएं।
(देवदत्त पटनायक एक प्रसिद्ध पौराणिक कथाकार हैं जो कला, संस्कृति और विरासत पर लिखते हैं।)