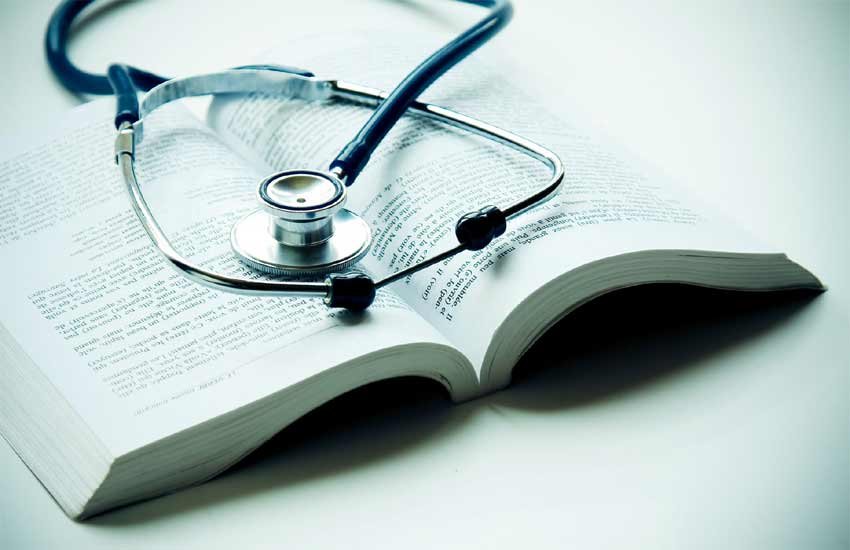दुख हर इंसान की शिराओं में बहता है, रग-रेशे में सुलगता रहता है। पर इसकी आंखों में झांकने से भी डर लगता है। जितना मुमकिन हो सके, इससे दूर भागने में ही कल्याण है। लेकिन दुख को समझना है, तो उसे सहेज कर रखना पड़ेगा। दुष्यंत कुमार ने इसे बखूबी व्यक्त किया है- ‘दुख को बहुत सहेज के रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया-सा उड़ गया।’
आखिर क्या है इस दुख में ऐसा कि दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। दुख बस व्यक्तिगत नहीं। पेशावर से पेरिस तक, कश्मीर से कैलिफोर्निया तक, परिंदों और पेड़ों का दुख- कई तरह के, कई स्तर, रंग-रूप और महक वाले दुख को हमने देखा है। कोई संबंध है हमारे खुद के दिल में रिसते दुख और दुनिया में धधक रहे दुख के बीच? दर्द तो दैहिक है और इसकी दवा है, पर दुख का निवारण शायद किसी गहरी प्रज्ञा की मांग करता है। ग्रीक पौराणिक पात्र प्रोटियस की तरह यह इधर डूबता है तो उधर उबरता है। लगातार जीवन के दरवाजे पर इसकी दस्तक सुनी जा सकती है। आमतौर पर मन इससे भाग लेने में ही अपनी भलाई समझता है। इसके विराट ढांचे के भीतर प्रवेश करने का साहस विरलों में ही होता है। दरअसल, ‘दुख को जानना’ और ‘दुख के बारे में जानना’ एक ही बात नहीं।
जो सोचते हैं कि दुख के बारे में चर्चा एक निराशावादी, सिनिकल और रुग्ण मनोदशा की ओर इशारा है, उन्हें एक बार रोज की खबरें देखने-पढ़ने की जरूरत है। इस देश में हर बीस मिनट में एक स्त्री के साथ बलात्कार होता है, दुनिया में करोड़ों की संख्या में लोग भूख से मरते हैं और न जाने कितने लोग बेघर-बेरोजगार हैं। जिस धर्म का आविष्कार हमने अपने सुख और शांति के लिए किया, वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है। इसीलिए बुद्ध ने तो किसी रहस्यवादी, आत्मविषयक प्रश्नों का उत्तर देने से ही इनकार कर दिया और बार-बार यह स्पष्ट किया कि उनका सरोकार सिर्फ मानव के दुख और उसके निरोध से ही है।
हमारा व्यक्तिगत जीवन हो सकता है बड़ा सुरक्षित हो, लेकिन सिर्फ भयंकर रूप से आत्मकेंद्रित और स्वार्थी व्यक्ति ही अपने सीमित सुख के छोटे से द्वीप पर चैन से रह सकता है। आप जितने अधिक संवेदनशील होंगे, दुख की कील आपके कलेजे में उतनी अधिक चुभेगी। यहां बात सिर्फ उस दुख की है, जिसका एक प्रबल मनोवैज्ञानिक अवयव होता है, देह की पीड़ा की नहीं। दुख प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है उन रिश्तों के साथ, जिन्हें हम बनाते-तोड़ते हैं। कई तरह के संबंधों के संजाल के बीच सबसे महत्त्वपूर्ण होता है अपना संबंध, खुद के साथ। जो खुद के साथ खुश नहीं, खुद से ही उकता गया है, वह चाहे किसी के साथ भी रह ले, देर-सवेर उसे भी दुखी कर डालेगा। सुख की छाछ को पहले से ही फूंक-फूंक कर पिया जाए तो दुख का उबलता दूध कलेजे को थोड़ा कम ही जलाएगा।
दुख के बारे में एक लोकप्रिय मिथक यह है कि समय बड़े से बड़े दुख का इलाज है। जबकि होता यह है कि दुख देने वाली घटना और उसकी स्मृति पर कई नए विचारों और स्मृतियों की परतें चढ़ जाती हैं, पर उसके भीतर दुख ठीक अपनी जगह पर ही बैठा रहता है। समय बीतने के साथ वह हमारे अवचेतन का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद वहां से कई अप्रत्याशित, विचित्र और कभी-कभी विकृत अभिव्यक्तियों के रूप में बाहर आता है। दूसरा झूठ यह है कि दुख बांटने से कम होता है। ऐसा होता नहीं। दो-चार या दस-बीस दुखी लोग मिल कर किसी एक को सुखी नहीं बना सकते। दुख सिर्फ छितरा जाता है। दुख बांटने की आदत जारी रही तो आगे चल कर आत्मदया का भाव भी इससे ही उपजता है। दुख सिर्फ इसके कारण की समझ और उसके अंत से ही समाप्त हो सकता है।
दुख का हर अनुभव या तो हमें कोमल और समझदार बनाता है या फिर नए पूर्वग्रहों, नई कड़वाहट के लिए जगह बना देता है। पहली बात बहुत दुर्लभ है और बहुत अधिक समझ और धैर्य की मांग करती है; दूसरी बात बड़ी सामान्य है। दुख के अनुभव के बाद कठोर, सीमित हो जाना, सिकुड़ कर अपनी खोल में बंद हो जाना, ये सामान्य बातें हैं। कोई कवि या शायर दुख को लेकर रूमानी हो जाए, उसका महिमामंडन करने लगे या फिर उसे नियति भी मान ले, ऐसा कुछ कहे कि ‘मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों’, तो उसे संदेह के साथ ही देखना ठीक है। दुख में ऐसा कुछ भी नहीं जो खूबसूरत हो। मस्तिष्क की कोशिकाओं को यह भौतिक रूप से नष्ट कर डालता है। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि दुख की भर्त्सना दुख से मुक्त नहीं करती; ठीक वैसे ही, जैसे इसका महिमामंडन मुक्त नहीं करता। अब सवाल है कि कुछ गिने-चुने लोग अगर इस दुख के दरिया को पार कर भी लें, तो क्या मानव जाति की पीर का पर्वत थोड़ा भी पिघलता है?