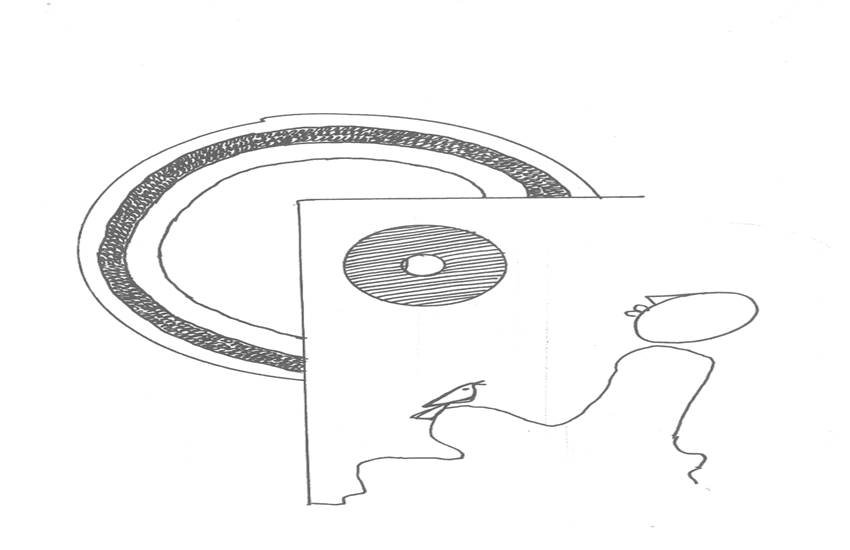कालू राम शर्मा
विवाह के लिए छपे सुंदर से निमंत्रण पत्र के सबसे नीचे विशेष ‘बाल मनुहार’ में एक पंक्ति छपी थी- ‘मेले मामा ती छादी मे जलुल-जलुल आना।’ इस पंक्ति का उस विवाह की पत्रिका में खासा महत्त्व है। उस घर-परिवार के कुछ बच्चों की ओर से तुतलाती जबान में मासूम अनुरोध किए जाने का हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। दरअसल, अक्सर बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो कुछ शब्दों को बोलने के दौरान अक्षरों के उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं। हालांकि जो व्यक्ति बच्चे की बात सुन रहा होता है, वह सही तौर पर समझ पाता है कि बच्चा क्या कहना चाहता है। इसके मायने ये हैं कि बच्चे जो कुछ भी बोलते हैं, वह अर्थपूर्ण होता है। लेकिन अक्सर कोई भी बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उच्चारण उतना सटीक नहीं होता। वैसे इस ‘सटीकता’ को भी हम वयस्क ही परिभाषित करते हैं। दरअसल, जब बच्चा भाषा सीखता है तो वह एक बड़ा काम करता है। इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। बोलना शुरू करने के पहले बच्चा बहुत कुछ सुनता है। क्या कभी आपने किसी नवजात शिशु और उस घर में बालक की मां, दादी-दादा, नानी-नाना और बच्चों के बीच के वार्तालाप को सुना है? मेरा अवलोकन है कि वे यह जानते-समझते हैं कि शिशु कोई प्रकट प्रतिक्रिया नहीं करेगा। फिर भी वे ऐसा करते पाए जाते हैं। इसे अर्थहीन नहीं कहा जा सकता। हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो उसे एक इंसान के रूप में ही देखते हैं। इतना ही नहीं, हम वयस्क, शिशु से तुतलाती जुबान में बात करते हैं। मसलन, ‘तुम का (क्या) कल (कर) लहे (रहे) हो… तुमने दुदा (दूध) पिया… तुम बली प्याली (बड़ी प्यारी) हो… तुम एछा कुं कलती (ऐसा क्यों करती) हो..!’
यह दिलचस्प है कि शिशु अपने जन्म के कुछ समय बाद ही हमारे बोलने की ओर ध्यान लगाना सीखता है और कुछ न कुछ सांकेतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देता है।अध्ययनों से पता चलता है कि एक महीने के शिशु के सामने मां न भी हो तो उसकी आवाज सांत्वना देने वाली होती है। एक बच्चा जब छह-आठ माह का होता है तो वह कुछ ध्वनियां और कुछ शब्दों के जरिए खुद को अभिव्यक्त करता है। यह उसके लिए भाषा सीखने का एक अहम चरण होता है। इस दौरान वह उच्चारण क्षमता को सुधारता जाता है, माता-पिता के साथ नई-नई ध्वनियां सीखता है। बच्चे के लिए यह एक प्रकार का खेल ही होता है। मनोवैज्ञानिक वैलेंटिन के मुताबिक बच्चे का ध्वनि के साथ खेलने को निरर्थक होने से बचाने के लिए जरूरी है कि उसे खुद ही खेलने दिया जाए। हमारे हस्तक्षेप से ध्वनि पकड़ने का खेल निरर्थक हो जाता है। वे कहते हैं कि अपने बेटे को वे ‘कॉफी’ कहवाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चा बार-बार कॉफी को ‘फोफी’ बोलता। अगली बार फिर से कॉफी बोलने को मजबूर करने पर वह अचानक जोर से बोली ‘टी’। यानी बच्चों के सही उच्चारण पर जोर देना बालमन के खिलाफ है। खुद मेरा बेटा जब छोटा था तब वह ‘वेलकम’ को ‘गिलबम’ बोलता था। उसकी इस मासूम अदा पर हम खुश होते थे। कभी उसे टोका नहीं गया। हालांकि वह बाद में अपने आप ही ‘वेलकम’ बोलना सीख गया।
हम अपने आसपास ऐसे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी देखते हैं कि वे बोलते हुए कुछ शब्दों का उच्चारण सही तौर पर नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों को मैं देखता हूं कि वे ‘श, ष, स’ में फर्क नहीं कर पाते हैं। खासकर क्लिष्ट शब्दों में बच्चों का उच्चारण कुछ अलग होता है, जैसे कि ‘क्या’ को वे ‘किया’ और ‘स्कूल’ को ‘इस्कूल’ कहते हैं। हालांकि उच्चारण के मामले में कई वयस्कों में भी ऐसा ही चलन देखा जा सकता है। प्रारंभिक स्तर पर स्कूलों में बच्चों को अक्षरों के उच्चारण पर जोर दिया जाता है। उच्चारण आने पर क्या समझ में आता है, यह हमें समझने की सख्त जरूरत है। असल में हमारा दिमाग अर्थपूर्ण चीजों को ही ग्रहण कर पाता है। मात्र उच्चारण पर जोर देने पर बच्चे प्रकट रूप से झल्लाते हुए भले ही न दिखें, मगर उनके दिलो-दिमाग पर काफी प्रतिकूल असर पड़ता है।बोलना दरअसल बोलने से आता है। इसलिए बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बोलने यानी बातचीत करने के भरपूर अवसर दिए जाने की जरूरत है, जिसका हमारी स्कूली शिक्षा में भारी अकाल देखने को मिलता है। अगर एक बच्चा घर में तोतली जबान में बोलता है तो उसे प्यार भरी नजरों से देखा जाता है। मगर जब स्कूल में वह तुतलाता है तो शिक्षक उसे उचित तरीके से नहीं बरत पाते। जबरन सिखाने के दौरान भाषा शिक्षण के आवश्यक तत्त्व नजरअंदाज होते जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि बच्चे को उन शब्दों को बार-बार सहज रूप से बोेलने के अवसर दिए जाएं, बिना यह बताए कि वह गलत उच्चारण कर रहा है। असल में उसके बोलने में अर्थ खोजने की जरूरत को पहचानना जरूरी है।