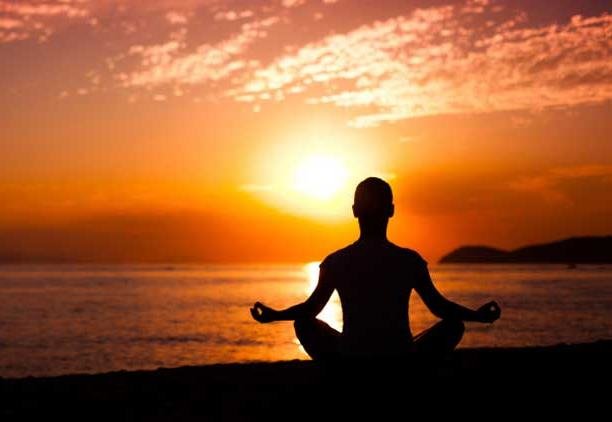सुधांशु कौशिक
सोचते-सोचते चाय का कप कब खाली हुआ, यह पता ही नहीं चला। मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। करीब आधा घंटा हो गया था मुझे इस चाय की गुमटी पर बैठे। इन्हीं खयालों से दो-चार होता हुआ मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में देखता हूं कि सीमेंट की कितनी ही डिब्बेनुमा इमारतें फ्लेक्सबोर्ड और निआॅन होर्डिंगों से अटी पड़ी हैं, जिन पर अधिकतर उन कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन थे, जो मानो कहती हों कि आप हमें रोजगार दीजिए, हम आपको रोजगार का मार्ग दिखाएंगे। सभी विज्ञापनों में छात्रों को आकर्षित करने के अलग-अलग तरीके हैं लेकिन इन सबमें एक रोचक समानता है कि इनमें कुछ लोग स्वयं को एक ‘विषय विशेषज्ञ’ होने के साथ-साथ एक मोटीवेशनल गुरु (प्रेरक गुरु) और कुछ एक सक्सेस गुरु (सफलता गुरु) की तरह पेश कर रहे हैं। इन दृश्यों को देखकर मैं अचरज में पड़ गया कि ये जो स्वघोषित गुरु हैं, वे किस चीज के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। व्यक्ति को स्वयं की प्राप्ति के लिए या इनकी सेवा या उत्पाद को खरीदने के लिए। अगर ये महात्मा गांधी, विवेकानंद जैसे महापुरुषों की भांति युवा पीढ़ी और हताश लोगों को जाग्रत करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि सच्चे दिग्दर्शकों ने कभी स्वयं को लोगों पर नहीं थोपा। इनको जो भी उपाधियां दी गर्इं, वे दूसरों ने उन्हें उनके सम्मान में दीं। गांधीजी ने खुद को कभी महात्मा नहीं कहा।
आज के दौर के ये तथाकथित गुरु चीख-चीख कर कह रहे हैं कि वे आपको पंद्रह मिनट में इतना प्रेरित कर देंगे कि आप कुछ दिनों में ही करोड़पति बन जाएंगे। इन्हीं में से कुछ वे लोग भी होते हैं जो किसी विचारधारा विशेष से प्रभावित होते हैं और उसी दायरे में अपनी बात लोगों पर थोपते हैं। कहीं-कहीं तीन-तीन घंटों के सेमीनारों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य वक्ता को हिंदी सिनेमा के किसी हीरो की तरह पेश किया जाता है। इनमें आए हुए ज्यादातर लोग इस क्षणिक प्रेरण का आनंद लेने के बाद हॉल से निकलते हुए मिले ‘ज्ञान’ को कपड़ों पर चिपकी धूल की तरह झाड़ कर चलते बनते हैं और अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। इन सबके बीच होने वाली बातचीत सुनो तो पता चल जाता है कि लोगों को इस तरह के प्रेरक गुरुओं की आवश्यकता क्यों होती है!
इन्हीं विचारों के आरोह-अवरोह के साथ मैं अपने किराए के मकान पर आया तो मुझे इसका एक नमूना देखने को मिला। मेरे दो मित्र मेरे साथ ही रहते हैं, वे चुपचाप थे। दोनों एक-दूसरे की मौजूदगी से अनजान इंटरनेट की आभासी दुनिया के रसास्वादन में लगे थे, एकदम शांत। इस अंतर्जाल का सबसे बुरा प्रभाव यही होता है कि व्यक्ति इसे ही अपनी वास्तविक दुनिया मान लेता है और अपनी असल जिंदगी से कट जाता है और छोटी-छोटी समस्याओं से इतना घबरा जाता है कि वह खुद को हारा हुआ महसूस करने लगता है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए बाद में वह इन प्रेरक गुरुओं की ओर रुख करता है।
आजकल यही संवाद का अभाव परिवारों में देखने को मिल जाता है। जहां एकल परिवार के कारण सदस्यों की संख्या वैसे ही सीमित है और उनमें से भी कई लोग अपने मोबाइल, टैब-लैपटॉप या कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए अपने आसपास से कटे हुए रहते हैं। नए अध्ययन बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग अवसाद के शिकार हो रहे हैं। न तो इनके पास अपने लिए समय होता है और न ही अपने परिवार और समाज के लिए। परिवारों में बढ़ती संवादहीनता लोगों की हताशा का मुख्य कारण है। परिवार व्यक्ति की जड़ों की भांति होता है, जहां से उसे आत्मबल और आत्मतोष रूपी पोषण मिलता है। जब यह पोषण मिलना बंद होता है तो मानवरूपी वृक्ष सूखने लगता है। हमें चाहिए कि परिवारों में बढ़ती इस खाई को भरा जाए। आजकल यह भी देखा जा रहा है कि लोगबाग अच्छे साहित्य से भी किनाराकशी करते जा रहे हैं। परिवार में अच्छी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने का संस्कार खत्म होता जा रहा है। जो कुछ है बस इंटरनेट है। सारा ज्ञान इसी से मिल रहा है। इस अंतर को पाटने के लिए साहित्य का सहयोग लिया जा सकता है। क्या पता किसी किताब के किसी पन्ने पर आपको कोई प्रेरित करने वाली पंक्ति मिल जाए जो आपके जीवन की कठिनाइयों को सुलझाने में मददगार साबित हो।
इन सबके बीच कुछ लोगों को अकेलेपन से भी घबराहट होती है। पता नहीं क्यों वे इस अपने एकांत को असहनीय बना लेते हैं। अकेलापन कोई रोग नहीं है बल्कि इसे बेहतर मौका ही मानना चाहिए, जहां चुपचाप अपनी आत्मा का संगीत सुनने का समय मिलता है। एकांत का एक सकारात्मक और उजला पक्ष भी है। कभी अकेले बैठना भी सुकून देता है, एकदम खाली। इसके लिए हर वह स्थान उचित है जहां आप खुद से दो बातें कर सकें। भीड़ भरे माहौल में भी अपने अतंर्मन में उठती लहरों की आवाज सुन सकें। कोई बगीचा या बस स्टॉप, आपका कमरा या कोई चाय की गुमटी। क्या पता, इसी बातचीत में आप कुछ पा लें।