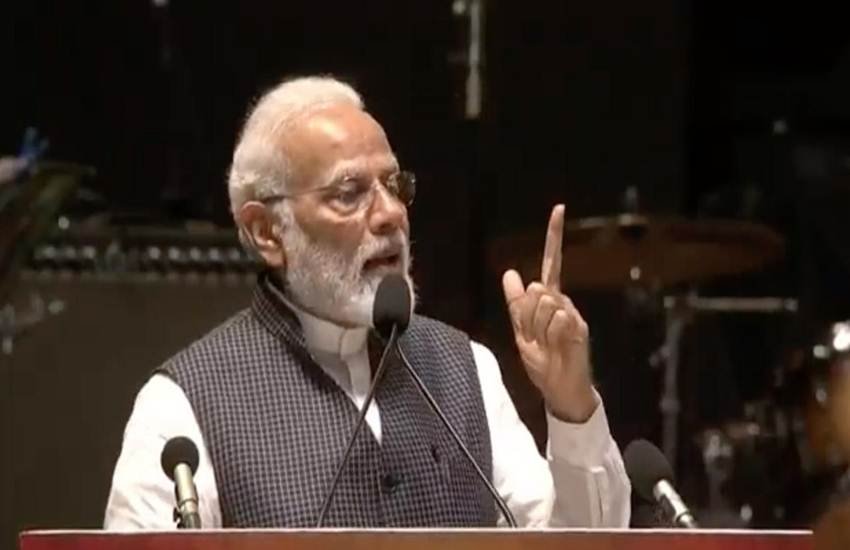वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में बैंकों का स्वरूप लगातार बदल रहा है। जहां पहले बैंकों में लंबी कतारें लगी रहती थीं वहां अब सूचना तकनीक ने इस कार्य को सरल-सुगम बना दिया है। इसमें मुद्रा बैंक, एनबीएफसी, पेमेंट बैंक, जन धन, डीबीटी, बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट की नियुक्ति जैसी अच्छी पहल के जरिए सरकारें लगातार वित्तीय समावेशन पर जोर दे रही हैं। लेकिन नकदी रहित (कैशलेस) अर्थव्यवस्था में धोखाधड़ी,आज भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की पहुंच न होना, एनपीए की समस्या आदि चिंता के विषय हैं। उम्मीद है कि व्याप्त कमियों को दूर कर बैंकिंग व्यवस्था यह नया स्वरूप जनता के सामाजिक-आर्थिक और गुणात्मक विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
’कपिल एम वड़ियार, पाली, राजस्थान
विनाश को न्योता
हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ आवास की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। जहां कुछ वर्ष पहले खेती होती थी, वहां अब घर बनते जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि अगर खेती योग्य पर्याप्त जमीन ही नहीं होगी तो लोगों का पेट कैसे भरेगा? यही हाल नदियों का है जिनका अस्तित्व धीरे-धीरे मिट रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती हमारी संस्कृति रही हैं लेकिन सरस्वती तो अब कहानियों में सिमट कर रह गई और यमुना इतिहास बनने की राह पर है। गंगा से भी राजनीतिक फायदा उठाने पर जोर है। उसकी गंदगी तक दूर करने में सरकार सफल नहीं हो रही है। छोटी-छोटी नदियों के संदर्भ में सबसे विकट स्थिति यह दिख रही है अतिक्रमण कर उनके तट पाट दिए गए हैं। नदी-नालों को मिट्टी से भर कर रहने के लिए जमीन तलाशी जा रही है। जिस तरह जल बहाव के रास्ते पर अतिक्रमण कर घर बनाए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि जल स्रोत और जल निकासी को अवरुद्ध कर हम खुद अपने विनाश को न्योता दे रहे हैं।
’दिनेश चौधरी, सुरजापुर, सुपौल, बिहार</p>
बदहाल स्कूल
हमारे देश में शिक्षाअधिकार कानून के बावजूद एक बड़ा तबका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित है। यह कटु सच्चाई है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकित अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े, गरीब और वंचित समाज के होते हैं। संपन्न और उच्च व मध्य वर्ग के बच्चे तो निजी स्कूलों में अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। नेताओं और नौकरशाहों की बात दूर, अधिकतर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकोंके बच्चे भी सुविधा संपन्न निजी स्कूलों में ही पढ़ाई करते हैं। अफसोसनाक है कि सरकार द्वारा विद्यालयों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी धरातल पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाए और पढ़ाई से लेकर बुनियादी सुविधाओं को जांचा जाए तो निश्चय ही हालात बदलते नजर आएंगे।
’मंजर आलम, रामपुर डेहरु, मधेपुरा, बिहार
जंगल की जगह
हम और हमारी धरती एक खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। इसी डर ने हमें पेड़ लगाने और पानी बचाने की तरफ मोड़ दिया है। बच्चों की ड्राइंग से गायब होते प्राकृतिक दृश्यों को फिर से बनाने की कोशिश में पौधारोपण जैसे कार्यक्रम एक अच्छी पहल हैं। इसी क्रम में सजावटी पौधों को मुफ्त या उपहार देने का चलन भी इन दिनों जोर पकड़ रहा है। शायद पौधे बड़े होकर उजड़ते जंगलों की जगह लेंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक खुशखबरी बन सकती है। मगर यहीं से हमारी कोशिशों पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सचमुच नए जंगल बसाने के प्रयासों में हम ईमानदार हैं? तुलसी या सजावटी पाम जैसे पौधे लगा कर हम कितने घने जंगल बनाने में कामयाब होंगे? तरक्की की देन कंक्रीट के जंगलों ने फलदार और छायादार पौधों के लिए जगह नहीं छोड़ी है। हमें वह जगह तलाशनी होगी जहां हरे वृक्षों के घने जंगल की वसीयत आने वाली पीढ़ी के नाम कर सकें।
एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड</p>