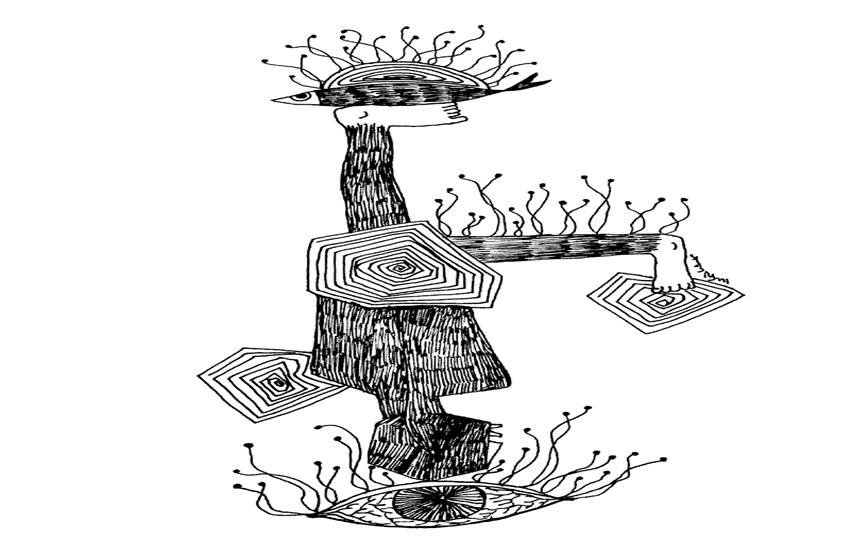राजेश मल्ल
साहित्य में स्थानीयता की जगह
साहित्यकार का एक दायित्व अपनी भाषा को समृद्ध करना भी है। यह काम वह क्षेत्रीय बोलियों से शब्द, मुहावरे, भाषाई छवियां लेकर पूरा करता है। मगर पिछले कुछ सालों में हिंदी में स्थानीयता का घोर अभाव महसूस किया जा रहा है। भाषा में एकरसता-सी नजर आने लगी है। वह एक घिस चुकी भाषा है। उसमें चमक नहीं है। नई अर्थ-छवियां नहीं हैं। वहां अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों का चलन तो खूब बढ़ा है, पर क्षेत्रीय बोलियों से प्राय: दूरी बना ली गई है। कथा सहित्य में भाषाई विविधता की गुंजाइश काफी होती है, पर वहां भी एक-सी भाषा नजर आती है। इसकी क्या वजहें हैं, इस बार की चर्चा इसी पर। – संपादक
अपने समय के ढेर सारे कवियों, कथाकारों और आलोचकों को पढ़ते समय आपको लगेगा कि अगर नाम-छाप न हो तो पहचानना मुश्किल होगा कि यह रचना किसकी है। एक ही तरह की शब्दावली, चित्र-योजना, वाक्य-विन्यास और रूप-विधान मिलेगा। सघनता-संश्लिष्टता हो या सहजता-सरलता। एक तरह से लुगदी हो गई भाषा और अनंत दुहराव से चमक खो चुके शब्द। निष्प्राण और निष्प्रभावी। कोई नयापन नहीं। जैसे सोता ही सूख गया हो। व्यक्ति का अनूठापन जैसे तिरोहित हो गया हो। सन उन्नीस सौ नब्बे के बाद ऐसी रचनाओं की बाढ़-सी आ गई है। सोशल मीडिया के साथ तो भयावह और अराजक माहौल-सा बन गया है। नए कवियों-कहानीकारों की सूची जारी करने वाले आचार्य और इस सत्कर्म में लगे हजारों साहित्यसेवी, हो सकता है इस बात पर कुछ आपत्ति करें, लेकिन हकीकत यह है कि यह संकट हिंदी के आम पाठक का भी है और जन-सरोकारों से जुड़े प्रत्येक साहित्य प्रेमी का भी।
साहित्य अपने अंतिम निष्कर्षों में शब्द साधना है। ध्यान रहे, इस शब्द साधना के पीछे स्पष्ट दृष्टि और वैचारिकी होती है। चूसे हुए शब्दों का मलबा और राजनीतिक जार्गन साहित्य को जन-सरोकारों से विलग करता है। हर नया कवि अपने पूर्ववर्ती साहित्य संस्कारों की जड़ता को तोड़ कर नया रास्ता बनाता है। यह भाव-संवेदना के स्तर पर भी होता है और ‘शब्द’ साधना के स्तर पर भी। भाव नए होंगे तो वे नए शब्दों की मांग करेंगे। मुक्तिबोध ने एक लंबी कविता लिखी, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं : ‘सत्ता के परम ब्रह्म/ ईश्वर के आसपास/ सांस्कृतिक लहंगों में/ लफंगों का लास-रास/ खुश होकर तालियां/ देते हैं गोल-मटोल/ बिके हुए मूर्खों के होठों के हीन हास।’
पूरी कविता ‘शब्दों’ के अर्थ से विलग होने और अपनी गरिमा खोने की महागाथा है। शायद यही वह प्रस्थान बिंदु है, जहां से मुक्तिबोध नए अर्थ से संपन्न शब्दों की खोज करते या साधना करते हैं। नए शब्दों की आवक का न होना भावों की गहराई और उसकी सघनता के अभाव का सूचक भी है और जीवन तथा भाव-चेतना के बीच फासले का द्योतक भी। पिछले दिनों हिंदी कविता के भाषा संस्कार पर अचानक चर्चा तेज हुई। विषय बना एक युवा कवि की शब्दावली का। उनकी कविता में प्रयुक्त शब्द बोलचाल से उठाए गए हैं। लेकिन वह बोलचाल बहुत ही सीमित दुनिया के लोगों की है। व्यापक जन-समुदाय के बीच ‘ब्रेकअप’ की कोई अवधारणा ही नहीं है। अब भी वहां प्रेम का अर्थ मध्यकालीन दैहिक मात्र है या अत्यंत पवित्र। सो, उनकी शब्दावली अपनी नवीनता के बावजूद इस विराट जनमानस का हिस्सा नहीं बन पाई। यही कारण है कि गांव-गंवई के रचे-बसे शब्द आज लुप्त होते जा रहे हैं और जहां दिखते हैं, वहां हमें आकर्षित करते हैं। नया अर्थ देते हैं।
अपने विकास यात्रा के समकालीन पड़ाव पर आकर साहित्य सृजन की आंतरिक गति ही कहीं टूट गई है। जीवन के व्यापक और गहरे भाव-संवेदना तक आवेग की जगह सतही पाठ- ‘सरफेस रिडिंग’- तक सीमित होते जाने की स्थिति अपनी जड़ों से कटने और बहुविध फंसे हुए भारतीय जीवन के विलाप से उपजी है। सूचनाएं, आंकड़े, घटनाएं और मीडिया द्वारा बनाया जीवन साहित्य सृजन के लिए नाकाफी होता है। जीवन की गहरी संवेदनात्मक अनुभूतियां तो गहरे उतरने पर ही प्राप्त होती हैं। मूलत: नए शब्दों का अभाव व्यापक जीवन के बहुविध रूपचित्रों या बिंबों का अभाव ही है। इसलिए आज भी पुराने-नए साहित्य सृजन में व्यापक जन-जीवन की अर्थ-छवियां हमें आकर्षित करती हैं, बांधती हैं। वरना अखबार, बाजार और विज्ञापन की भाषा से साहित्य सृजन संभव नहीं है। इस संदर्भ में हमारे समय के बड़े कवि केदारनाथ सिंह का खयाल अनायास ही आता है। आप कहीं से कोई कविता चुनें, पढ़ें तो आपको कोई न कोई, नई अर्थ-छवि वाले शब्द या शब्द-चित्र मिल जाएंगे। निश्चय ही वे शब्द नए होंगे और गांव-जवार के होंगे। मसलन, उनके ‘सृष्टि पर पहरा’ संकलन को लें, तो ‘पहरा’, झरनाद, फुनगी, सिराना आदि शब्द सहज मिल जाते हैं।
इसी प्रकार नए लोगों में अनुज लुगुन, महेश पुनेठा, केशव तिवारी, सुधांशु फिरदौस, शैलजा पाठक, संध्या निवेदिता जैसे कुछ कवि हैं, जो लोक चेतना में रचे-बसे शब्दों को लाते हैं और नया अर्थ संभव करते हैं। पुराना वाक्य है नई जमीन तोड़ना। कोई भी कवि-रचनाकार अपनी प्रतिभा और जीवन की व्यापक अनुभूतियों, जो निश्चय ही नई होती हैं, से नया शब्द विन्यास सृजित करता है। वह तत्सम या अनूदित शब्दों से नहीं, बल्कि उन्हें जीवन के गहरे संदर्भों और आशाओं से प्राप्त करता है। उल्लेखनीय है कि अगर स्वयं रचनाकार का जीवन बहुमंजिले फ्लैट से शुरू होकर स्कूल-कॉलेज-घर के बीच कैरिअर निर्माण में लगा होगा, तो निश्चय ही वहां नए शब्दों की आवक कम होगी। साहित्य कोई पार्ट टाईम जॉब नहीं है। सृजन आपके सर्वश्रेष्ठ की मांग करता है। सपने की मांग करता है। यह मात्र शब्द साधना के स्तर पर नहीं या मात्र जीवन के प्रेक्षक होने से नहीं बनता है। बल्कि व्यापक जीवन की पाठशाला से, जीवन की आंच में तपने से होता है। घाम-ताप-बारिश का, प्रकृति के हर रंग का, जीवन की बहुरूपी कल्पना का गहरा अहसास आपको नए शब्द-चित्र के लिए अवसर प्रदान करता है।
पर, आज शहर की तरफ आकर्षण बढ़ने या फिर मजबूरी में शहरों की तरफ पलायन बढ़ने की वजह से लोक-संवेदना का स्रोत सूखता गया है। मगर विचित्र है कि जो रचनाकार गंवई संवेदना लेकर शहरों में आते हैं, वे भी उसे अपनी रचनाओं में कहीं पिरो नहीं पाते। एक खास तरह की बनी-बनाई भाषा को स्वीकार कर लेते हैं और जिस तरह बाजार में ‘ट्रेंड’ बिकता है, उसी तरह वे भाषा के बने-बनाए खांचे में अपनी रचना को ढालना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनके अनुभव की ईमानदारी भी प्रश्नांकित होती है। लोक से जुड़ी समस्याएं उन्हें दिखती तो हैं, पर वे उन्हें आंदोलित क्यों नहीं कर पातीं, यह भी हैरानी का विषय है। वही शहराती विषय या फिर चर्चित विदेशी विषय वे उठाना शुरू कर देते हैं और स्वाभाविक रूप से उनकी रचनाओं में बासीपन, ऊबाऊपन और नीरस छवियां भर जाती हैं। भाषा में चमक, नए शब्दों की पैठ तभी संभव हो पाती है, जब संवेदना तीक्ष्ण होती है, पैनी है। वह संवेदना रोजी-रोटी या जोड़-जुगाड़, तिकड़मों में कुंद होती है, तो हैरानी नहीं।
आज साहित्य के घटते पाठक आधार का भी संदर्भ कहीं न कहीं इस समस्या की परिधि में आता है। सृजनकर्ता का अनूठापन और भाव संवेदना जहां नए जीवन संदर्भ को नवीन भाषिक शब्द रचना के साथ सृजित करती है, वहीं उस भाव के सार्वजनीन होने की स्थिति में पाठक की चेतना को भी उन्नत धरातल पर ले जाती है। दुहराव की स्थिति में पाठक-ग्रहीता उससे ऊबता है। उसके लिए सहज बोरियत पैदा करने वाला यह पीड़ादायक प्रक्रिया बनती है। इसलिए आवश्यक है कि शब्द और भाव-दृष्टि-विकार की नवीनता बरकरार रहे। आज के साहित्य के घटता पाठकीय आधार का यह भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।