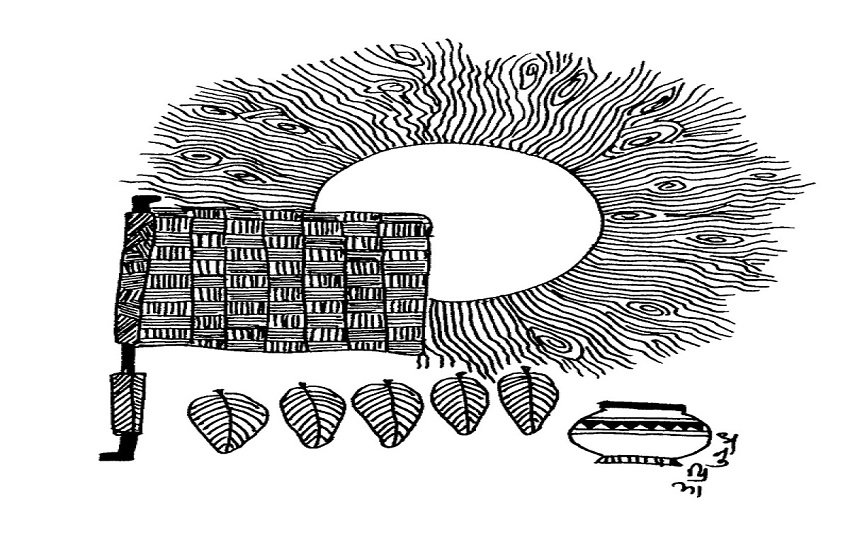भारत अनेक भाषाओं वाला देश है। यह भाषाई विविधता हमारी समृद्धि का प्रमाण है। मगर इस समृद्धि को समझने और इससे लाभान्वित होने के बजाय हम भाषाई आधार पर झगड़ते रहते हैं। अगर हम इतनी बात समझ लें कि भाषाई विविधता का संबंध हमारी भौगोलिक विशेषता से है, तो बहुत-सी मुश्किलें आसान हो जाएं। भाषा वैज्ञानिक जो कहें, पर हमारा लोकमन जाने कबसे कहता रहा है कि कोस कोस पर पानी बदले नौ कोस पर बानी। भाषा का यह बदलाव स्वाभाविक और प्राकृतिक है। इसीलिए भाषाई बहुलता और विविधता भारत का वैभव है।
अंग्रेजों ने हमें यह समझा दिया कि विभिन्न भाषाओं का होना अभिशाप है। वे हमको यह भी समझाने में सफल रहे कि हमारी मातृभाषाएं देशी भाषाएं हैं और इन्हें बोलना, बरतना, पढ़ना, पढ़ाना गंवार होने का प्रमाण-पत्र है। अंग्रेजों ने यह प्रमाण-पत्र जिस उत्साह से जारी किया उसके दुगुने उत्साह से हमने इसे ग्रहण किया। हमने इस बात पर भरोसा कर लिया कि देशज भाषाओं को बरतना दूसरे दर्जे का नागरिक होना है। हमने पहले दर्जे की नागरिकता हासिल करने की जी-तोड़ कोशिश की। इस कोशिश में हम पहले दर्जे के नागरिक हो पाए या नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषाओं की नागरिकता खो बैठे।
मातृभाषाओं की नागरिकता खोने का अर्थ है मातृभाषाओं के स्मृतिकोष में संचित ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, अनुभव-संवेदन, शिल्प, साहित्य और संगीत सब कुछ को खो बैठना। इस तरह हम सब कुछ खोते चले गए। हिंदी हमने इसलिए नहीं सीखी कि वह हमारी राष्ट्रभाषा है, उसे क्या सीखना। हमें यह भी बोध हुआ कि मातृभाषाओं में ही नहीं, राष्ट्रभाषा में भी नौकरी और रोजगार नहीं है। अब हर व्यक्ति को रोजी-रोजगार और सम्मान तो चाहिए ही। और ये दोनों अंग्रेजी में ही मौजूद हैं। इसलिए अंग्रेजी का दबदबा कायम है। नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे हम भाषाई विकलांगता के शिकार हो गए। इस वजह से हमारा सांस्कृतिक जीवन पंगु-सा हो गया।
जिस तरह हमारी सामाजिक दृष्टि मातृभाषाओं के विरुद्ध बनी और उन्हें हीन समझने लगी, उसी तरह हमारी अकादमिक दृष्टि निर्मित हुई। केवल यही नहीं हुआ कि हमने अपनी शिक्षा के लिए एक पराई भाषा को चुना, बल्कि साथ ही साथ लगातार अपने को समझाते और विश्वास दिलाते रहे कि हमारी मातृभाषाएं नाकाबिल हैं और वे शिक्षा के काम नहीं आ सकतीं और अगर कहीं उनसे शिक्षा का काम लिया गया, तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे।
एक तरफ मातृभाषाओं की नाकाबिलियत का सतत अहसास और दूसरी ओर शिक्षा के माध्यम के रूप में पराई भाषा के व्यवहार ने हमें एक अजब तरीके से दुविधाग्रस्त बना दिया। यह दुविधाग्रस्तता हमारी शिक्षा-व्यवस्था को खोखला करती जा रही है।
कभी शिक्षाविद कृष्ण कुमार ने कहा था- ‘उपनिवेश रह चुके देशों के लिए शिक्षा की एक बड़ी समस्या अपनी भाषाओं को ज्ञान की संभाल और रचना के लिए बरतने की है। अगर देशज भाषाओं को ज्ञान की चर्चा, संवार और रचना के कामों में नहीं लाया जाता और ये भूमिकाएं अंग्रेजी जैसी औपनिवेशिक भाषा में सिमटी रहती हैं, तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था और समाज के संबंधों में तनाव और असंतुलन बना रहना और बढ़ना स्वाभाविक है।’
यह असंतुलन और तनाव लगातार बढ़ता गया है और हमारी शिक्षा, जिसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सब शामिल हैं और समाज के बीच बेगानापन बढता गया है। देशज भाषाओं में मौजूद परंपरित ज्ञान की अवहेलना और मौलिक ज्ञान के सृजन में विफलता के नाते शिक्षा प्रणाली लगातार प्रश्नांकित हुई है।
ऐसा नहीं कि हमारे नीति निर्माताओं का ध्यान शिक्षा प्रणाली की विफलता पर नहीं गया और उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की वाला मामला साबित हुआ। क्योंकि हमने इस बेगानेपन को दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया। देशज भाषाओं की ज्ञान परंपरा को लेकर हम कुंठित बने रहे। प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं की बात जरूर की गई है, पर उसमें सुचिंतित विचार और कार्य योजना का अभाव दिखता है।
हमारी चिंतन परंपरा में जनपद, जनपदीयता और जनपदीय भाषाओं के महत्त्व के स्वीकार का भाव रहा है। अथर्ववेद का पृथ्वीसूक्त पृथ्वी की महिमा का गान ही नहीं करता, बल्कि वह हमें पृथ्वी से जोड़ता है- माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:। यानी भूमि हमारी मां है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी के जिस हिस्से पर हम निवास करते हैं, उसके साथ हमारा आवयविक संबंध होता है।
भाषा भी भूमि से जुड़ी हुई है। हमारे लोकमन में भी यह बात बसी हुई है। अनेक भाषाओं का अस्तित्व भी नैसर्गिक है। पृथ्वी सूक्त की व्याख्या करते हुए वासुदेवशरण अग्रवाल कहते हैं- ‘आपस में भिन्नता होना, अनेक भाषाओं और धर्मों का अस्तित्व कोई त्रुटि नहीं है। अभिशाप के रूप में उसकी कल्पना उचित नहीं है।
ऋषि की दृष्टि में विविधता का कारण भौतिक परिस्थिति है। नाना धर्म, भिन्न भाषाएं, बहुधा जन- ये सब यथौकस अर्थात अपने निवास स्थानों के नाते पृथक हैं। इस स्वाभाविक कारण से जूझना मनुष्य की मूर्खता है।’ यानी विविध भाषाओं और उनके बोलने वालों का होना प्राकृतिक है। इसलिए भाषाएं श्रेष्ठ, हीन या छोटी या बड़ी नहीं होतीं। भाषाई विविधता प्राकृतिक निधियां हैं। इन निधियों को बचाना और बरतना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
भाषाई विविधता केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में है और इस विविधता की रक्षा करना समकालीन दुनिया की बहुत बड़ी चुनौती है। भारत की तरह अफ्रीकी देश भी लंबे समय तक औपनिवेशिक गुलामी झेलते रहे हैं। औपनिवेशिक शक्तियों ने जैसे भारतीय भाषाओं की तबाही की पटकथा लिखी, वैसे ही अफ्रीकी भाषाओं की तबाही की भी।
इस मामले में अफ्रीका सौभाग्यशाली है कि वहां न्गूगी वा थ्यांगों जैसे विचारक भी हुए हैं, जिन्होंने भाषाई तबाही को औपनिवेशिक साजिश के रूप में पहचाना और इसके विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अफ्रीकी लोगों को चेताया कि आंख मूंद कर पराई भाषा का इस्तेमाल और उस पर निर्भरता एक तरह से भाषाई आत्महत्या है।
इससे हमारे लोगों की संस्कृति और समाज की स्मृतियां लुप्त हो जाएंगी। न्गूगी इस बात से इतने क्षुब्ध हुए कि उन्होंने कह दिया कि अफ्रीका में अंग्रेजी विभागों को बंद कर देना चाहिए और अफ्रीकी भाषा विभाग खोलने चाहिए। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी से उनकी कोई जाती दुश्मनी थी। उनका विरोध अफ्रीकी भाषाओं का दमन करने वाली अंग्रेजी से था।
उन्होंने कहा कि मातृभाषा में लिखने का आग्रह कोई अंग्रेजी की प्रतिक्रिया में नहीं है, बल्कि यह शताब्दियों से जारी औपनिवेशिक लूट, जिसने अफ्रीका को आत्मिक और आर्थिक रूप से खोखला और राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाल दिया है, के विरुद्ध सकारात्मक हस्तक्षेप है। हमारे सामने भी यह बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि हम अंग्रेजी या किसी और भाषा के विरोधी नहीं हैं। हमारा विरोध भाषाई वर्चस्व की उस राजनीति से है, जो लोक भाषाओं को लीलने पर आमादा होती है।
हमें यह जानना होगा कि औपनिवेशिक प्रभुओं द्वारा निर्मित भाषा दृष्टि से भारत में भी मातृभाषाओं की आत्महत्या हो रही है। इसे रोकने के लिए आगे आना होगा और इस दिशा में पहला कदम यह होगा कि हम मातृभाषाओं की नागरिकता वापस हासिल करें। निज भाषा में हमारी मौलिकता न केवल सुरक्षित रहती है, बल्कि उसका स्वाभाविक विकास होता है, हमारी समझ विकसित होती है।
सब उन्नति का रास्ता मौलिकता और समझ से होकर निकलता है। इस बात को समझ लें, तो गुलामी के दौर में बनी भाषाई समझ या पूर्वाग्रह से मुक्ति मिलेगी और हम वापस मातृभाषा के नागरिक हो सकेंगे और तभी अपना सत्व ग्रहण कर सकते हैं। इस सत्व ग्रहण में ही ‘सत्व निज भारत गहै’ का रहस्य भी छिपा हुआ है।
विविध भाषाओं और उनके बोलने वालों का होना प्राकृतिक है। इसलिए भाषाएं श्रेष्ठ, हीन या छोटी या बड़ी नहीं होतीं। भाषाई विविधता प्राकृतिक निधियां हैं। इन निधियों को बचाना और बरतना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।