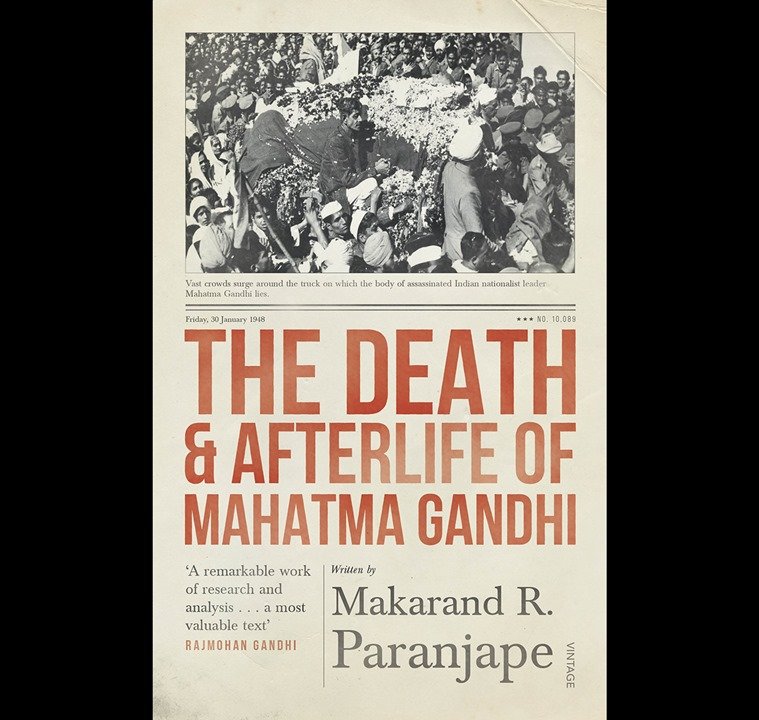पिछले कुछ सालों में पढ़ने की प्रक्रिया में आए बदलाव प्रकट हैं। पारंपरिक साहित्य की जगह हमारे जीवन में बदली है। मसलन, अब एक उपन्यास को मांग कर पढ़ने वाले कम मिलते हैं। ‘क्लासिक’ की जगह ‘बेस्टसेलर’ ने ले ली है। किताबों से एकात्म्य की प्रक्रिया रुक-सी गई है। ऐसा नहीं कि दुनिया या भारत के शिक्षित वर्ग में पढ़ना कम हो गया है। पढ़ने की जगह अब भी बची है, लेकिन उसमें बड़ा बदलाव आया है। पढ़ने के पारंपरिक ढंग को धकिया कर वर्चुअल रीडिंग ने ले ली है। समाचार, लेख, ब्लॉग-पोस्ट, फेसबुक अनेक तरह के पढ़ने के आयाम हैं।
पढ़ना मानवीय क्रियाकलाप का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। सामूहिक और व्यक्तिगत चेतना को गढ़ने में ‘पढ़ने की संस्कृति’ की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यूरोप से लेकर एशिया तक आधुनिकता के विस्तार में ‘पढ़ने की संस्कृति’ निर्णायक रही है। आधुनिक काल का इतिहास इस बात का गवाह है कि तमाम सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनों को गढ़ने में ‘पढ़ने की संस्कृति’ प्रमुख कारक रही है। बंगाल नवजागरण की परिकल्पना पढ़े-लिखे मध्यवर्ग के बिना नहीं की जा सकती। भारत में छापेखाने की स्थापना के बाद लोकवृत्त में धर्म और विवेक की चर्चा को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। धर्म, विवेक और परंपरा की यही चर्चा आगे चल कर उपनिवेश-विरोधी चेतना में परिवर्तित हो जाती है।
स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भाषा, उपनिवेश का औचित्य, धन की निकासी से लेकर आजादी तक की बहसें पढ़ने की प्रक्रिया का परिणाम थीं। हिंदी नवजागरण का विकास जिस रूप में हुआ, उसमें पढ़े-लिखे वर्ग की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। पढ़ने की संस्कृति का प्रभाव शिक्षित मध्यवर्ग तक सीमित नहीं किया जा सकता। उसका विस्तार अन्य लोगों में होना स्वाभाविक है। इसे उपनिवेश-विरोधी चेतना के स्वाधीनता आंदोलन में तब्दील होने से समझा जा सकता है। पढ़ने का प्रभाव कितना दूरगामी होता है, इसे ब्रिटिश उपनिवेश के दौर में शिक्षित वर्ग के विकास से समझा जा सकता है। जिस शहरी मध्यवर्ग को ब्रिटिश राज ने ब्रिटिश साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया, उसी ने उपनिवेश-विरोधी चेतना के विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाई। ये परिवर्तन छापेखाने के विकास के बिना संभव नहीं थे।
क्रिस बायल ने भारत में छापेखाने के विकास की चर्चा करते हुए लिखा कि ‘जब प्रिंटिंग प्रेस की तकनीक यूरोप में आम हो चली थी तब भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ, लेकिन उल्लेखनीय यह है कि 1920-40 के बीच भारत के आधुनिक होते अभिजन ने इसका अभूतपूर्व और तेजी से विस्तार किया।’
पठन संस्कृति का प्रभाव कितना दूरगामी होता है, इसे बेनेडिक्ट एंडरसन की ‘इमेजिंड कम्युनिटीज’ में देखा जा सकता है। एंडरसन ने यूरोप में विकसित हो रही उप-राष्ट्रीयताओं को सोलहवी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस के आगमन का परिणाम माना। वे लैटिन से उपजी यूरोपीय वर्नाकुलर रीडिंग-कल्चर को यूरोप में राष्ट्रीयताओं का कारक मानते हैं। उनकी धारणा इस बात की ताकीद करती है कि कल्पना आधारित निर्मिति किस तरह वास्तविकता में बदल जाती है। एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म के संदर्भ में इमेजिंड जियोग्राफीज का उपयोग अनिवासी के लिए किया। हैबरमास ने लोकवृत्त निर्मित करने में प्रिंट-मीडिया को महत्त्वपूर्ण माना।
यह समझना मुश्किल नहीं है कि पढ़ने की संस्कृति के प्रभाव दूरगामी होते हैं। इसकी प्रमुख वजह आम जन में प्रिंट के अनुकरण की प्रवृत्ति है, लेकिन विभिन्न युगों में इस अनुकरण की अभिव्यक्ति एक जैसी नहीं, बल्कि संश्लिष्ट रही है।
उदारीकरण के साथ पढ़ने के नए आयाम उभर रहे हैं। बाजार और नए किस्म की उभरती शिक्षा प्रणाली के बीच हिंदीभाषी समुदाय का अंगरेजी से संपर्क बढ़ रहा है, वहीं इंटरनेट और मोबाइल तकनीक नए किस्म के पाठकीय अनुभव रच रहे हैं। इंटरनेट ने एक नई पाठकीय दुनिया का निर्माण किया है, जो देशिक सीमाओं के आरपार मौजूद है। यह ऐसा पाठक है, जो स्वाधीनता आंदोलन यानी बीसवीं सदी के पाठक से इस मामले में अलग है कि इसके संवेदन जगत में राष्ट्रीय मुक्ति के सवालों से अधिक महत्त्वपूर्ण मानवता और पर्यावरणिक प्रश्न हैं। साहित्य के पारंपरिक पाठक जिस तरह किसी पाठ से अर्थ का निर्माण करते थे, उससे भिन्न तरीके से यह पाठक अर्थ का निर्माण करता है।
बीसवीं सदी के पाठक की चिंताओं में राजनीति को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, लेकिन इस नए पाठक की चिंताओं का निर्माण सांस्कृतिक अस्मिता कर रही है और ये अस्मिताएं नए तरह के मीडिया से निर्मित हो रही हैं। मीडिया के नए रूपों ने भाषा, लिंग, नस्ल, स्वाद आदि अस्मिता निर्माण के नए घटकों को जन्म दिया है। मीडिया के इसी बदलाव की प्रभविष्णुता के आकलन के लिए यूनेस्को ने मैकब्राइट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने माना कि मीडिया के लिए संदेश या माध्यम के बजाय संदर्भ अधिक महत्त्वपूर्ण कारक होता है। यानी संदेश का ग्रहीता उसे अपने लिंगीय, भाषिक, जातीय, नस्ली संदर्भ में ग्रहण करता है। प्रसारित हो रहे संदेश में अपने संदर्भ से अर्थ भरने की इसी प्रक्रिया में पाठक व्यापक सांस्कृतिक विमर्श का अंग बन कर नई अस्मिताओं का सृजन करता है। मीडिया में प्रसारण पर एकाधिकार और ग्रहण में विविधता को नए युग में टकराव का सबसे प्रमुख बिंदु माना जाता है, जिसके तहत ये ‘पाठकीय अस्मिताएं’ मूलत: प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ती हैं। मीडिया जगत में सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व मूलत: सबलीकरण का ही एक रूप है।
हिंदी प्रकाशकों के खोए आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो ऊपरी तौर पर पुस्तकों की बिक्री में इजाफा हुआ है। पर इससे कोई निष्कर्ष निकालने से पहले अंगरेजी साहित्य पढ़ने वालों की संख्या में आए बदलाव पर गौर करने की जरूरत है। हिंदी पाठकों की संख्या का विस्तार एक बात है, लेकिन एक हिंदी पाठक के स्पेस में आया मात्रात्मक और गुणात्मक बदलाव दूसरी बात। नेशनल रीडरशिप के सर्वे लगातार हिंदी पत्रिकाओं और पत्रों के पाठकों की संख्या में इजाफे की बात करते हैं, लेकिन गौर करने की बात है कि क्या सरस्वती, हंस, प्रताप, मतवाला और आज की पत्र-पत्रिकाओं के पाठकों को एक नजरिए से देखना चाहिए। इसी के विस्तार में देखे तो क्या प्रेमचंद के गबन, गोदान और ‘फाइव पॉइंट सम वन’ को एक तरह से समझा जा सकता है। भारतीय साहित्य चिंतन में ‘सहृदय’ और ‘साधारणीकरण’ और ‘रस’ की अवधारणा रही है। इसलिए समझ और संवेदना की पठन संस्कृति के बाद सूचना की पठन संस्कृति एक महत्त्वपूर्ण स्थानांतरण है, जिसे व्यापक संदर्भों में समझने की जरूरत है। हिंदी का यह नया पाठक लिखित शब्द से अलग तरह की अपेक्षाएं रखता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसकी सामाजिक अवस्थिति में अंतर आया है। अब उसके जीवन में निजी और सार्वजनिक का भेद अधिकाधिक खत्म हो रहा है और वह निरंतर प्रतीकों की दुनिया में अलगाव को दूर करने के लिए दखल के नए तरीके खोज रहा है।
पढ़ने की संस्कृति का विस्तार जहां छापेखाने के अविष्कार और विभिन्न समाजों के बीच उसके आगमन से तेजी से शुरू होता है, वहीं नई तकनीकी विकास मुद्रित सामग्री के पढ़ने की संस्कृति को समेटता दिखाई देता है। इसका संबंध राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर व्यवस्थापरक ढांचे के निर्माण से भी जुड़ा है। जब हम बाजारवाद कहते है, तो वहां तकनीक के साथ दूसरे कारक भी पढ़ने की संस्कृति को प्रभावित करते दिखाई पड़ते हैं। पिछले दो दशक में आर्थिक उदारीकरण और इंटरनेट की तकनीक ने सांस्कृतिक बर्ताव और परिदृश्य को निर्णायक ढंग से बदल दिया है। शौक से पढ़ने की परंपरा में बुनियादी बदलाव आए हैं। संवेदना को विकसित करने वाले साहित्य की जगह उपयोगिता प्रधान सामग्री पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इंटरनेट पर अंगरेजी वर्चस्व के चलते हिंदीभाषी पाठक अंगरेजी सामग्री पढ़ने को मजबूर हुए हैं।