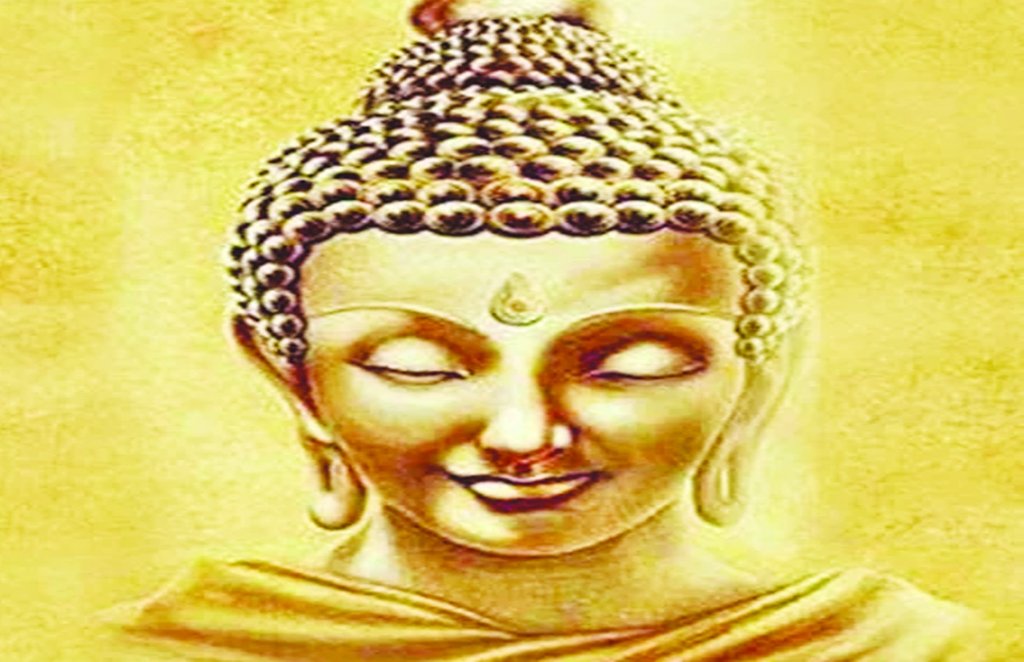नरपतदान चारण
जब हम दर्शनशास्त्र पढ़ते है,तो उसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं विशेष आकर्षित करती हैं क्योंकि उनका सीधा संबंध जीवन के नैतिक शिष्टाचार, व्यवहार, चरित्र और अनुभव से है। और उसमें बताए ‘आर्य आष्टांगिक मार्ग’ तो जीवन मार्ग की अनैतिक क्रियाओं के कारण – निराकरण का प्रतिपादन करते हुए बहुत सीख दे जाते हैं। यह आर्य आष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जिसमे दु:खों से मुक्ति पाने एवं आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। बौद्ध धर्म मानता है कि यदि आप अभ्यास और जागृति के प्रति समर्पित नहीं हैं तो कहीं भी पहुंच नहीं सकते हैं। यह अष्ट मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि यह हर दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है।
बुद्ध ने इस दु:ख निरोध प्रतिपद आष्टांगिक मार्ग को ‘मध्यमा प्रतिपद’ या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी है। अर्थात जीवन में संतुलन ही मध्यम मार्ग पर चलना है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि तृष्णा ही सभी दु:खों का मूल कारण है। अत: तृष्णा का सर्वथा प्रहाण करने का जो मार्ग है, वही मुक्ति का मार्ग है। इसे दु:ख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। और इस मार्ग के आठ अंग है, जिसे आर्य आष्टांगिक मार्ग कहा है। इसमें निहित आठ धारणाएं ऐसे दृष्टिकोण और व्यवहार हैं, जिन्हें जीवन यापन करने के साधन के रूप में अनुकरण करने के प्रयास में उपयोग करना होता हैं। ये आठ धारणाएं तीन मुख्य श्रेणियों- प्रज्ञा (बुद्धि), शील (आचरण), और समाधि (एकाग्रता) में विभक्त हैं। शील शुद्ध होने पर ही आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रवेश पा सकता है। ये हैं आष्टांगिक मार्ग…
1. सम्यक दृष्टि : चार आर्य सत्यों (दुख, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग) को जानना। सम्यक् दृष्टि का संकल्प हमारे सत्य की अवधारणा से होता है जो कि उचित और अनुचित, हानिकर और हितकर के मध्य सम्यक भेद कर सके। जो है, वही देखना। जैसा है, वैसा ही देखना। अन्यथा न करना। सुख-दुख में सम्यक दृष्टि रखना।
2. सम्यक संकल्प : चित्त से राग-द्वेष नहीं करना, ये जानना की राग-द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। करुणा, मैत्री, मुदिता, समता रखना, दुराचरण ना करने का संकल्प लेना, सदाचरण करने का संकल्प लेना, धम्म पर चलने का संकल्प लेना।
3. सम्यक वाक : इसमें वाक यानी वाणी के संयम की सीख दी गई है। सम्यक वाणी के अन्तर्गत आता है, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलने का अभ्यास करना, मधुर बोलने का अभ्यास करना, धम्म चर्चा का अभ्यास करना,चुगली नहीं करना और कठोर वचन नहीं बोलने की शिक्षा दी गई।
4. सम्यक कर्मांत : सम्यक कर्मांत के अन्तर्गत आता है, कर्म के साथ कर्म फल जुड़ा हुआ है इसलिए कर्म से किसी का अहित ना हो, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमें नुकसान हो, समस्या हो या तनाव हो, अहंकार और अहं को भूलें पर दोष दर्शन से मुक्त अपने काम से काम रखें, अपना दृ्रष्टिकोण सही रखें।
5. सम्यक आजीव : मेहनत से आजीविका अर्जन करना, पांच प्रकार के व्यापार नहीं करना, जिनमें आते हैं, शस्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, विष का व्यापार। यानी जिसके व्यापार से आप दूसरों की हानि का कारण बनते हैं,वह निषिद्ध है।
6. सम्यक व्यायाम :आष्टांगिक मार्ग का पालन करने का अभ्यास करना, शुभ विचार पैदा करने वाली चीजों/बातों को मन मे रखना, पापमय विचारों के दुष्परिणाम को सोचना, उन वितर्कों को मन में जगह ना देना, उन विर्तकोंं को संस्कार स्वरूप मानना, गलत वितर्क मन में आए तो निग्रह करना, दबाना, संताप करना।
7. सम्यक स्मृति : कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, ये सब मिलकर विपस्सना साधना कहलाता है, जिसका अर्थ है, स्वयं को ठीक प्रकार से देखना। यह जानना की राग-द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। किसी भी मनुष्य को, जिसे स्वयं को जानने की इच्छा हो, को विपस्सना (पश्चाताप) जरूर करनी चाहिए, इसी से दुख-निवारण के पथ की शुरुआत होगी।
8. सम्यक समाधि : अनुत्पन्न पाप धर्मो को ना उत्पन्न होने देना, उत्पन्न पाप धर्मो के विनाश में रुचि लेना, अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पत्ति मे रुचि, उत्पन्न कुशल धर्मों के वृद्धि में रुचि। इन सबको शब्दश: पालन करने से जीवन सुखमय होगा, निर्वाण, शाश्वत खुशी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति की प्राप्ति होगी।