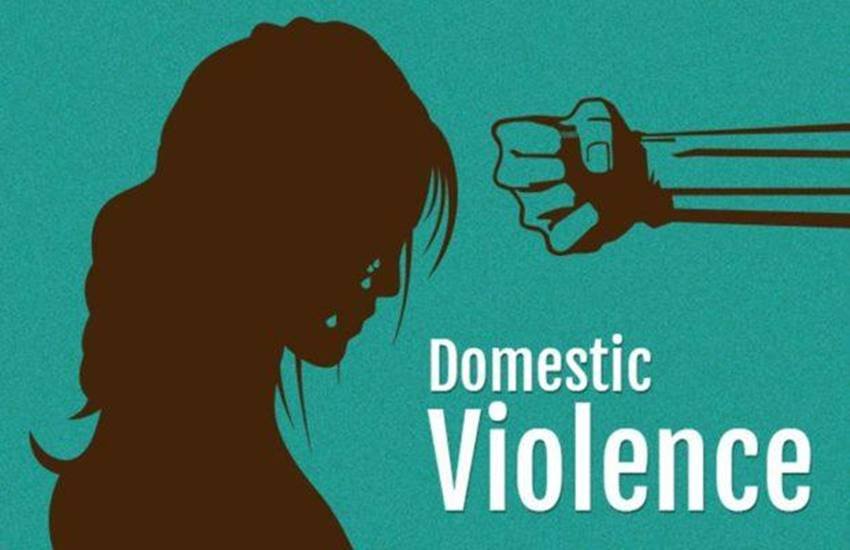हमारे समाज की पारिवार नामक संस्था की सुदृढ़ता को पूरी दुनिया में महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सहयोग भरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी घर की महिलाएं ही हैं। इसके बावजूद जिस आत्मसम्मान और सुरक्षा का परिवेश उनके हिस्से आना चाहिए था, वह आज भी नहीं आया है। हाल ही में एक गैर-सरकारी संगठन ‘सहज’ और इक्वल मीजर्स 2030 के एक सर्वेक्षण के नतीजे घरेलू स्तर पर महिलाओं के इन्हीं दर्दनाक हालात को बयान करने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक भारत में करीब एक-तिहाई शादीशुदा महिलाएं पतियों से पिटाई खाती हैं। इस दुर्व्यवहार से जुड़ा सबसे दुखद पहलू यह है कि अधिकतर महिलाओं को इस पीड़ादायी बर्ताव से कोई खास शिकायत भी नहीं है। यानी शिक्षा के बढ़ते आंकड़ों और सामाजिक बदलाव के दावों के बीच आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा के दंश को अपनी नियति मान कर स्वीकार कर रही हैं। यह अध्ययन बताता है कि पंद्रह से उनचास साल के आयु वर्ग की महिलाओं में से करीब सत्ताईस प्रतिशत महिलाएं तो पंद्रह साल की उम्र से ही देहरी के भीतर की जा रही यह हिंसा बर्दाश्त करती आ रही हैं। आज एक ओर हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं, तो दूसरी ओर ऐसे आंकड़े सोचने को विवश करते हैं कि बाहर ही नहीं, घर में भी औरतों को लेकर हमारी मानसिकता में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। सार्वजनिक जीवन के साथ-साथ व्यक्तिगत मोर्चे पर भी स्त्रियां पीड़ादायी परिस्थितियों में जी रही हैं।
दुनिया में हर एक इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक है। ऐसे में यह अफसोसनाक तो है कि हमारे समाज में घर के बाहर तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान एक बड़ा सवाल है ही, दहलीज के भीतर भी हालात अच्छे नहीं हैं। इस सर्वेक्षण के आंकड़े भले ही हमें हैरान और परेशान करें, पर देश की आधी आबादी के हालात की कड़वी सच्चाई को सामने लाने वाले हैं। इससे निकलने वाले संकेत हमारे समाज और परिवार का वह स्याह चेहरा दिखाते हैं जहां स्त्रियां अपने ही आंगन में, अपने ही लोगों की हिंसा झेलने को विवश हैं। मौजूदा दौर में घर के कामकाज के साथ-साथ औरतों को बाहर की जिम्मेदारी तो मिल गई, पर उनके आत्मसम्मान और अस्तित्व का मोल आज भी कुछ नहीं आंका जाता।
दरअसल, ज्यादातर पुरुष पत्नी पर हाथ उठाना या उसे ताना देना अपना हक समझते हैं। कई बार तो इस हद तक मारपीट की जाती है कि महिला की जान तक चली जाती है। बाहर आपराधिक हालात का सामना करने वाली कितनी ही महिलाओं की गरिमा को उनके घर के भीतर ठेस पहुंचाई जाती है। आए दिन होने वाले ऐसे दुर्व्यवहार से कई बीमारियां जड़ें जमा लेती हैं। महिलाएं भावनात्मक टूटन का शिकार बनती हैं। लेकिन आज भी सामाजिक-पारिवारिक दबाव इतना है कि आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार को जीते हुए भी अधिकतर महिलाएं चुप्पी को ही चुनती हैं।
एक गैर-सरकारी संस्था के मुताबिक भारत में केवल 0.1 प्रतिशत महिलाएं ही ऐसी हिंसा के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए आगे आती हैं। विडंबना ही है कि हमारे परिवारों में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को व्यवस्थागत समर्थन भी मिलता है। साथ ही पितृसत्तात्मक सोच इसे और पोषित भी करती है। कभी दहेज के नाम पर तो कभी बेटी को जन्म देने के उलाहने रूप में। मारपीट कर उनकी मान-मर्यादा पर आघात करना हमारी पारिवारिक व्यवस्था में आम बात है।
भारत को भले ही एक प्रगतिशील देश माना जाता है, पर समाज में मौजूद परंपरागत सोच और रूढ़िवादी मानसिकता की जकड़न ने बहुत कुछ बदल कर भी कुछ न बदलने जैसे हालात बना रखे हैं। यही वजह है कि घरेलू हिंसा का दंश आज भी समाज के हर वर्ग में देखने को मिलता है। अपने ही घर में महिलाओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार करने वाले शिक्षित और अशिक्षित हर तबके के लोग हैं। यहां तक कि संभ्रांत परिवारों के उच्च शिक्षित और ऊंचे ओहदों पर कार्यरत पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ भाषाई हिंसा और हाथापाई करते हैं। समस्या यह भी कि स्त्री जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाले इस दुर्व्यवहार को आज भी व्यक्तिगत मुद्दा माना जाता है। परिवार के लोग भी उस महिला की मदद करने आगे नहीं आते जो अपने पति की ज्यादतियों का शिकार होती है। अफसोस यह भी है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों को लेकर सजग महिलाएं भी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। आमतौर पर हम लोग पढ़ी-लिखी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को हर तरह से सशक्त और सफल मान लेते हैं। लेकिन महिलाओं के सशक्तीकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही नहीं है।
गौरतलब पहलू यह है कि कामकाजी हों या गृहिणियां, महिलाएं हर घर की रीढ़ हैं। शिक्षित और कामकाजी हैं तो देश की तरक्की में भागीदार हैं। दूरदराज के गांव में बसी हैं तो अन्नदाता हैं और परिवार को पाल रही हैं। इसके अलावा, किसी न किसी रूप में महिलाएं अनगिनत ऐसे काम संभाल रही हैं जिनका मोल ही नहीं आंका जा सकता। अपने ही स्वास्थ्य की संभाल में सबसे पीछे और दायित्वों के निर्वहन में सबसे आगे। ऐसे में हर जिम्मेदारी निभाने के बावजूद सराहना तो दूर, अपने ही परिवार में उनके साथ हिंसक व्यवहार किया जाए तो स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण ही कही जाएंगी।
दरअसल, बुनियादी सोच में बदलाव आए बिना घर के भीतर सम्मानजनक और सुरक्षित व्यवहार स्त्रियों के हिस्से नहीं आ सकता है। यह मनुष्यता के मान का मामला है। स्त्री-पुरुष के भेद से परे हर इंसान के आत्मसम्मान का मोल समझने का विषय है। कहना गलत नहीं होगा कि कठोर कानून, योजनाएं और लोगों को जागरूक करने वाले विज्ञापन समाज में महिलाओं की स्थिति न तो बदल पाए हैं और न बदल पाएंगे। सामाजिक-पारिवारिक और उससे भी ज्यादा जरूरी वैचारिक बदलाव आए बिना जमीनी स्थितियों में सुधार संभव नहीं। सरकार महिलाओं को कानूनन हक तो दे सकती हैं, पर जब तक उनके अपनों की और सामाजिक सोच में परिवर्तन नहीं आता, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने वाला ऐसा पीड़ादायी व्यवहार अपनी जड़ें जमाए रखेगा। स्त्रियों को घर के दायरे में रहने के पीछे उनकी सुरक्षा को एक बड़ा कारण बताया जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि दहलीज के भीतर महिलाओं के साथ होने वाली मारपीट मानवाधिकार का एक संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि घर के हर सदस्य को भावनात्मक सहारा देने वाली महिलाएं क्यों अपने ही घर के भीतर हिंसात्मक व्यवहार झेलने को विवश हैं? क्यों अपने जीवनसाथी से मिलने वाले कटुतापूर्ण और हिंसक व्यवहार को घर वालों का भी समर्थन मिलता रहता है?
जबकि बंद दरवाजों के पीछे होने वाली इस शारीरिक और मानसिक हिंसा को झेलने वाली महिलाएं चाहे कामकाजी हो या गृहिणी, इस देश की नागरिक हैं। घर हो या दफ्तर, देश का संविधान उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देता है। इसके बावजूद अपनी ही चौखट के भीतर महिलाओं के हिस्से यह वेदना क्यों आ रही है यहां तक कि वे इस पीड़ा के बारे में कोई जिक्र या कोई संवाद तक नहीं कर पातीं, मानो हर दर्द झेलना उनकी नियति ही बना दी गई है। हिंसा की इस मानसिकता से बाहर आने के लिए जरूरी है कि स्त्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक या देवी न मान कर मनुष्य होने का मान दिया जाए।