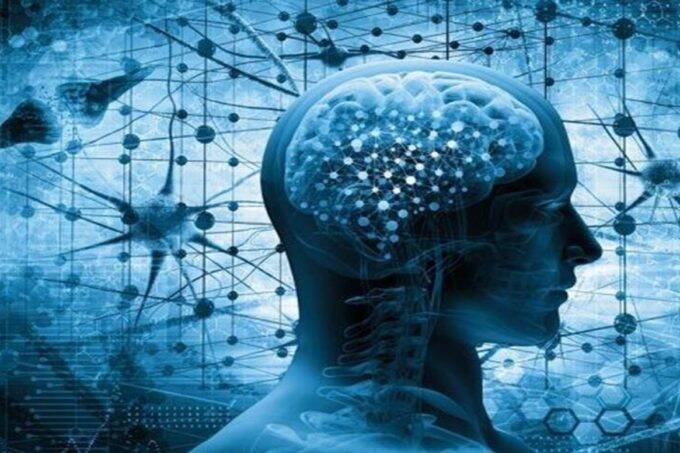कोरोना के टीकाकरण का विरोध अनेक देशों में हुआ। उसमें पूर्व से पश्चिम तक अनेक प्रकार के पूर्वाग्रहों की उपस्थिति देखी गई। किसी भी समाज में पूर्वाग्रहों की उपस्थिति को सामान्य प्रचलन ही माना जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर हिंसा, अविश्वास और अशांति की जड़ में सबसे प्रबल पोषक तत्त्व पंथों को लेकर बने पूर्वाग्रहों में निहित है। भारत विभाजन और दोनों देशों के मध्य लगातार बनी रहने वाली तनावपूर्ण स्थिति में भी मुख्य तत्त्व यही है। पूर्वाग्रहों का पोषण अज्ञान, अशिक्षा और अविश्वास से होता है। यह मनुष्य की तार्किक विश्लेषण क्षमता को कुंद कर देते हैं। जीवन कौशलों की सौम्यता और सुंदरता को मलिन कर देते हैं। शिक्षा के समावेशी प्रसार और सभ्यता के विकास से अपेक्षा तो यही की जाती है कि शिक्षित व्यक्ति पूर्वाग्रह का तार्किक विवेचन कर सकेगा और स्वयं अपना निर्णय लेगा।
व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रारंभ से ही अति महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है। उसके महत्त्व और आवश्यकता को हर सभ्यता और समाज सदा से स्वीकार करता आया है। पद्धतियां अलग-अलग रही हैं, मगर उद्देश्य मूल रूप से एक ही रहे हैं। आज की व्यवस्था में बच्चा जब स्कूल आता है तो वह पूर्व ज्ञान और अनेक मान्यताएं साथ लाता है, जिनका बृहत परिवेश में परिष्करण आवश्यक होता है। संभव है कि इनमें से कुछ केवल अज्ञान और अशिक्षा की उपज हों। शिक्षा इस खाई को पाट सकती है। इसीलिए पिछले सात-आठ दशकों से शिक्षा के वैश्विक विस्तार की आवश्यकता को न केवल स्वीकार गया है, उसे साकार स्वरूप देने के सघन प्रयास लगभग हर देश ने किए हैं। शैक्षिक रूप से अगली पंक्ति में माने जाने वाले देशों ने अपनी व्यवस्था को समयानुकूल बनाने के प्रयास में उसे गतिशीलता प्रदान करने की ओर लगातार ध्यान दिया है।
अपेक्षा तो यही थी कि सारे विश्व में शिक्षित समाज विध्वंसकारी, विभेदक और अपमानजनक पूर्वाग्रहों से मुक्ति दिलाने में पूर्ण रूप से सफल होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसे में यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि आधुनिक शिक्षा मानव समाज को भाईचारे, शांति, सदभाव, पारस्परिक विश्वास और सहयोग की तरफ ले जाने में सफल क्यों नहीं हुई? मनुष्य अपने पूर्वाग्रहों और विभेदक प्रवृत्तियों से उबर क्यों नहीं पा रहा है?
शिक्षा के सर्वजनीय प्रसार और उपलब्धता में अन्य की अपेक्षा बहुत पहले से अग्रणी देशों में अमेरिका और ब्रिटेन निश्चित ही आगे रहे हैं। लेकिन वहां का समाज भी पूर्वाग्रहों पर विजय अभी भी प्राप्त नहीं कर सका है। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव सामाजिक पूर्वाग्रहों से सीधे जुड़ता है। आज भी वहां अश्वेत समुदाय के प्रति घोर नस्लीय भेदभाव हर तरफ और हर स्तर पर देखा जा सकता है। समय-समय पर ऐसी घटनाएं या कष्टकर दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं जो स्पष्ट कर देती हैं कि वहां की शिक्षा की श्रेष्ठता की कितनी ही प्रशंसा क्यों न की जाए, उसकी असफलताओं और कमियों को नकारा नहीं जा सकता है। आज का अमेरिका यूरोप से गए प्रवासियों के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चल कर ही बनाया गया है और वे उस पर अपना पहला अधिकार मानते हैं।
पिछले साल 25 मई को बीस डालर की नकली पर्ची उपयोग करने के कारण जार्ज फ्लॉयड को एक गोरे पुलिसकर्मी डेरेक चाउविन ने बीच सड़क पर गर्दन दबा कर मार डाला। इस घटना का वीडियो सारी दुनिया ने देखा था। उसे देख कर सारा अमेरिका ही नहीं, अन्य देश के लोग भी दहल गए थे। इसी दबाव में अपराधी को साढ़े बाईस साल की जेल की सजा हुई है, और इसे अपवाद माना जा रहा है! कहते हैं कि वहां पहली बार पुलिसकर्मी द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या करने के लिए सजा हुई है! यह इस कारण भी संभव हुआ है कि आज जब लगभग हर घटना का वीडियो उपलब्ध हो सकता है और अमानवीय पूर्वाग्रहों की उपस्थिति से उत्पन्न घटनाएं सारे विश्व के समक्ष आ जाती हैं।
अमेरिका के गोरे लोगों के पूर्वज यूरोप से आये थे और उनमें अग्रणी था ब्रिटेन। इस साल 12 जुलाई को लंदन के वेम्बले स्टेडियम में आयोजित यूरो कप फाइनल के बाद वहां दर्शकों ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया कि पढ़े-लिखे, शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न होने से पूर्वाग्रहों से मुक्ति नहीं मिल जाती है। जो शिक्षा से ऐसी अपेक्षा करते रहे हैं, वे एक अलभ्य लक्ष्य को पाने की संकल्पना कर रहे थे। ब्रिटेन और इटली के बीच खेले जा रहे इस फाइनल मैच में पेनाल्टी शूट-आउट में जो तीन ब्रिटिश खिलाड़ी गोल करने में सफल नहीं हुए, वे तीनों ही गोरे नहीं थे, मगर ब्रिटेन के सम्मानित नागरिक हैं। उन्हें जिस रंगभेद जनित नस्ली आलोचना का शिकार होना पड़ा, वह इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में किसी भी सभ्य कहे जाने वाले देश में स्वीकृत नहीं हो सकती है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अत्यंत आहत मन से अपने ऐसे देशवासियों के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। हार की पीड़ा को सहन न कर पाने वालों के उत्पात का यह कोई पहला प्रकरण नहीं है, दर्शकों के ऐसे व्यवहार की आलोचना अनेक बार पहले भी हो चुकी है। लेकिन न लोग बदले, न ही पीढ़िया बदलने का कोई प्रभाव पड़ा। नस्ली भेदभाव या भेदभाव के अन्य कारकों को लेकर पूर्वाग्रहों की दुखदायी और अपमानजनक उपस्थिति से भारत अपरिचित नहीं है। इन्हें रोकने के सघन और सकारात्मक प्रयास अनेक मनीषियों ने किए। वे बड़े पैमाने पर सफल भी हुए, परंतु अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद, भीमराव आंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुष यही प्रयास करते कि रहे कि छुआछूत, लिंगभेद और जातिगत भेद समाप्त होने चाहिए। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए, नियम और उपनियम बनाए गए, समाज सुधारकों ने अपना योगदान किया और शिक्षा व्यवस्था ने अपना उत्तरदायित्व निभाने का निरंतर प्रयास किया।
पंथिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के प्रयास अनेक ढंग से किए गए। पंथ-निरपेक्षता को आधारभूत सिद्धांत के रूप में संविधान के प्रावधानों में शामिल किया गया। हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लिए अपने धर्म/पंथ को सर्वश्रेष्ठ माने, मगर साथ ही अन्य सभी के धर्मों के उनके लिए सबसे श्रेष्ठ माने, और उसी भाव से अन्य सभी धर्मों का आदर करे। भारत के पास तो विविधता के हर पक्ष के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता की संस्कृति को व्यवहार में लाने और उसकी सफलता का उदाहरण सभी के सामने प्रस्तुत करने का हजारों वर्षों का अनुभव है। अंग्रेजों ने अत्यंत गहराई से सोची-समझी कूटनीति के अंतर्गत भारत के दो बड़े समुदायों के मध्य अविश्वास पैदा करने के प्रायोजित प्रयास लगातार किए और वे इसमें सफल रहे।
स्वतंत्र भारत में जैसे-जैसे राजनीति केवल चुनावों में जीत तक सीमित होती गई, सामजिक सद्भावना और पंथिक समरसता की ओर ध्यान देना कम होता गया। देश ने अनेक बार ऐसे दंगे देखे हैं जिनके पीछे राजनीति ही एकमात्र कारण रही। देश ने जाति-आधारित राजनीति को पनपते और उसके द्वारा सामाजिक विभेद बढ़ते देखा है। जब भी बड़े स्तर पर प्रजातंत्र की मूल भावना के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से राजनीतिक दल खिलवाड़ करते हैं तो वे देश-हित भूल जाते हैं। यदि जाति प्रथा की समाप्ति के प्रयासों को रोका न गया होता, तो शायद आज यह इतिहास बन गई होती। अब इसके समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार पंथिक सदभाव अनेक पूर्वाग्रहों के कारण आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसी स्थितियां ही हिंसा को जन्म देती हैं। इक्कीसवीं सदी में शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य ‘साथ-साथ मिलकर रहना सीखना’ निर्धारित किया गया है। जो देश इसे समझ लेगा, भविष्य उसी का होगा।