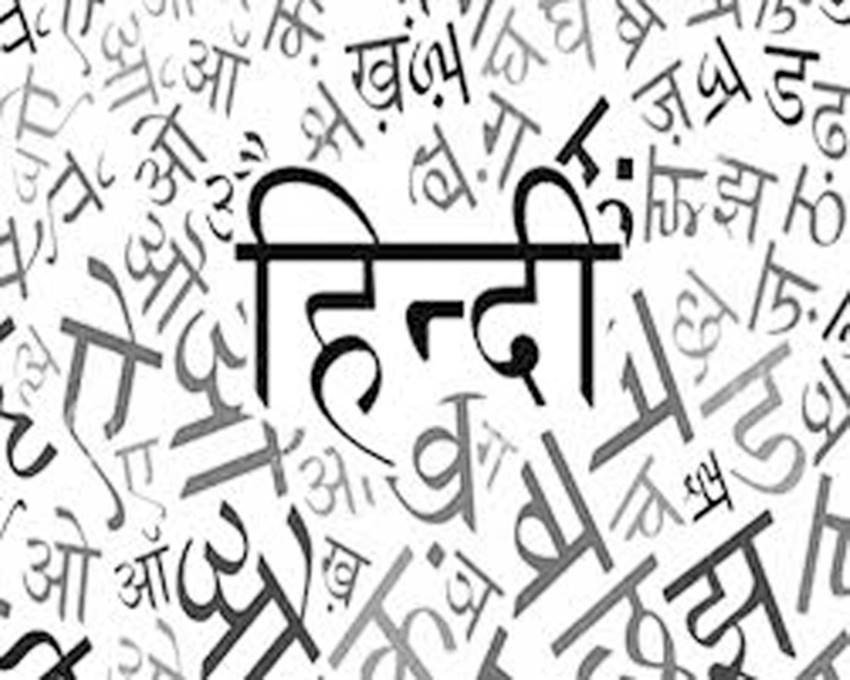धर्मेंद्र प्रताप सिंह
वर्तमान समय में भाषा का स्वरूप सामाजिक और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में अधिक जांचा-परखा जा रहा है। वर्तमान हिंदी भाषा जिसे सामान्यत: खड़ी हिंदी के रूप में जाना जाता है, की विकास-यात्रा के विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए आज विश्व बाजार की भाषा बन चुकी है। विभिन्न सोपानों से गुजरती हुई खड़ी बोली ने तीन शताब्दियों की यात्रा तय कर ली है। वैसे हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास बहुत पुराना है। यह एक सच्चाई है कि आज कंप्यूटर और इंटरनेट पर अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी की सामग्री भले कम हो, लेकिन पिछले दशक का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो विकीपीडिया और अन्य वेबसाइटों पर हिंदी अंग्रेजी के सम्मुख खड़ी दिखाई दे रही है और इसकी संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति के बाद काफी तेजी से बदलाव आए हैं। आज हिंदी के लिए महत्त्वपूर्ण यह है कि उसे समावेशी बना कर अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकारने की ओर प्रयास करना चाहिए।
संकीर्णता के साथ उसका बचाव करने की अपेक्षा इसमें अधिक से अधिक शब्दों को आत्मसात करने की ओर बल देने का प्रयास होना चाहिए।
पिछली शताब्दी के अंतिम दशक का अवलोकन करते समय हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गलियारों में एक शब्द की गूंज सुनाई देती है जिसे ‘भूमंडलीकरण’ कहा जाता है। इसके मूल में विश्व की महाशक्तियां अमेरिका, रूस, चीन आदि की अपनी आर्थिक योजनाएं हैं। वे संपूर्ण विश्व में सहभाग और साहचर्य को बढ़ाने के पक्षपाती दिखाई पड़ रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए तीसरी दुनिया के देशों को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं। हालांकि भूमंडलीकरण के प्रभाव में समाज, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर भी अघोषित संकट दिखाई पड़ा रहा है। इसके साथ-साथ परंपराओं, मूल्यों और स्थापनाओं आदि के पुनर्मूल्यांकन की भी बात हुई है। ऐसे में हिंदी भाषा भी भूमंडलीकरण रूपी रथ पर सवार होकर क्षेत्रीयता की परिधि से बाहर निकल कर वैश्विक परिपे्रक्ष्य में अपना वर्चस्व बनाने में सफल हुई है, जो हिंदी भाषा के महासागरीय रूप में दिखाई पड़ रहा है। भूमंडलीकरण ने अस्मिता की लड़ाई को तीव्र से तीव्रतर कर दिया है। इसने अलग-अलग तरह की अस्मिताओं को जन्म दिया, जिनमें भाषायी अस्मिता प्रमुख है। भूमंडलीकरण ने लोगों को अपनी संस्कृति, मिट्टी और बोली की ओर लौटने के लिए बाध्य किया है। यही कारण है कि लोग आज के समय में लोक साहित्य और संस्कृति की ओर मुखर हो रहे हैं।
तकनीक के विकास ने हिंदी को जहां लोकप्रिय बनाया है, वहीं उसके समक्ष अनेक चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। इन चुनौतियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली का व्यावहारिक न होना, प्रशासनिक और न्यायालयी शब्दावली, अनुवाद की समस्या आदि प्रमुख हैं। जनसामान्य में प्रचलित शब्दों को अपना कर इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो पारिभाषिक शब्द गढ़े जा रहे हैं, उन्हें निरंतर शोध और पर्यवेक्षण के आधार पर स्वीकार किया जाए। इसके लिए ऐसी कार्य योजनाएं तैयार की जानी चाहिए जिनसे पर्यवेक्षक जनसाधारण के बीच जाकर उन शब्दों का चयन करें। इसके साथ ही पारिभाषिक शब्दों के प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता है, जिससे आमजन को उनकी जानकारी मिल सके।
भाषाएं किसी भी समाज, सभ्यता व संस्कृति की वाहक होती हैं। भारतीय समाज में हिंदी की विभिन्न बोलियों के भी कई रूप देखने-सुनने को मिलते हैं। हिंदी प्रदेश की प्रमुख बोलियों जैसे भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, अंगिका, अवधी, ब्रज आदि में तो इस विविधता को खासकर महसूस किया जा सकता है। भोजपुरी की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों में इसके ही कई रूप देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह मैथिली-वज्जिका-अंगिका, राजस्थानी-हरियाणवी-गुजराती-मराठी, दक्षिण भारत की विभिन्न बोलियां आदि भी ऐसे ही साम्य-वैषम्य को लेकर चलती हैं।
व्यक्ति अपने परिवेश की उपज होता है और भाषा उसके परिवेश के निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। वह जब संस्कृतियों का वहन करती है तो साथ-साथ मनुष्य के भावों का भी वहन कर रही होती है। व्यक्ति चाहे किसी भी भाषायी परिवेश में चला जाए, उसकी अपनी भाषा या बोली कहीं न कहीं उसके अवचेतन में बनी रहती है। वह स्वयं को या किसी भी अन्य वस्तु को अपने ही भाषायी संदर्भों से जोड़ कर देख पाता है। यह सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, बल्कि किसी अन्य भाषा-भाषी के लिए भी उतना ही सच है। चूंकि हिंदी और हिंदी की बोलियों में इतनी विविधता है, उसके इतने अधिक और अलग-अलग अर्थ-संदर्भ हैं कि हिंदी के मामले में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाती है। हिंदी की इस विविधता को समझने के लिए वास्तव में उसकी बोलियों को बहुत बारीकी से समझना होगा।
भाषायी विविधता वाले हिंदुस्तान में किसी भी भाषा या बोली को किसी खास दायरे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। यह भाषा के लोकतंत्र का तो हनन है ही, साथ ही एक नए तरह की भाषायी तानाशाही को बढ़ावा देना भी है। हमें यह मान कर चलना होगा कि भाषा सीखने और उसके प्रयोग का अधिकार भी कहीं न कहीं शिक्षा और जीवन के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, क्योंकि सदियों से भाषा ही मानव जाति और विभिन्न सभ्यताओं की पहचान बनी है। यही कारण है कि हमेशा सबसे पहले भाषा ही अस्मिताओं और संस्कृतियों के टकरावों का शिकार हुई है। हिंदी ने भी ऐसे कई प्रहार झेले हैं। उसे कभी राजनीतिक अवसरवादियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा, तो कभी कुछ अन्य असामाजिक और शरारती तत्त्वों ने उसका दुरुपयोग किया। भूमंडलीकरण की कोख से पनपा बाजार भी इन्हीं शरारती तत्त्वों में से है। बाजार ने अंग्रेजी को माध्यम बना कर हिंदी और हिंदुस्तानियों की जातीय स्मृतियों को, उनकी भाषायी संस्कृतियों को खरोंच-खरोंच कर मिटाने का प्रयास किया है। बाजार ने धर्म-राजनीति, मीडिया, विज्ञापन जैसे अपने औजारों की मदद से हिंदी की अस्मिता को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, पर वह बार-बार अपनी पूरी शक्ति से उठ खड़ी हुई है।
किसी सभ्यता का अंत करने के लिए सदैव वर्चस्ववादी शक्तियों ने वहां की भाषा को अपना लक्ष्य बनाया है। हिंदी ने भी उपनिवेशवादी शक्तियों का सामना किया है, लेकिन वह बिखरी नहीं है। आज वह साम्राज्यवादी राष्ट्रों की भाषा की बराबरी में खड़ी है और कई मायनों में ज्यादा विस्तार और लोकप्रियता पा रही है। हिंदी का विस्तार उसकी बोलियों का विस्तार है, क्योंकि हिंदी अकेली ‘हिंदी’ नहीं है, बल्कि वह अपनी सभी बोलियों के साथ मिल कर ‘हिंदी’ है।
आज हिंदी ने अपना अंतरराष्ट्रीयकरण किया है। यह अंतरराष्ट्रीयकरण सिर्फ प्रचार-प्रसार के संदर्भ में नहीं है, बल्कि हिंदी की कुछ स्वभावगत विशेषताओं के कारण भी है। ये विशेषताए हैं- हिंदी की आत्मसात करने और अनुकूलन की प्रवृत्ति। हिंदी ने बदलते वक्त के साथ खुद को इतना लचीला बनाया कि सिर्फ भारतीय बोलियों के शब्दों को ही नहीं, बल्कि विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी अपने भीतर समेटा है। फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश, जापानी, अरबी, अंग्रेजी और न जाने कितनी ऐसी विदेशी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग एक हिंदीभाषी अपने रोजमर्रा के जीवन में बड़े ही सहज व स्वाभाविक रूप में कर लेता है। बाजार के इस भयाक्रांत कर देने वाले दौर में भी हिंदी अनुकूलन की इस क्षमता के कारण ही अपनी पहचान बनाए रखने में सफल हुई है। आज हिंदी ने यह साबित कर दिया है कि तथाकथित तीसरी दुनिया की भाषा होते हुए भी वह बेचारी या हीन भावना से ग्रस्त नहीं है। ज्ञान-विज्ञान-तकनीक के क्षेत्र में अब वह एक नए तेवर और अपने नए अंदाज के साथ स्वयं को प्रस्तुत कर सकती है।