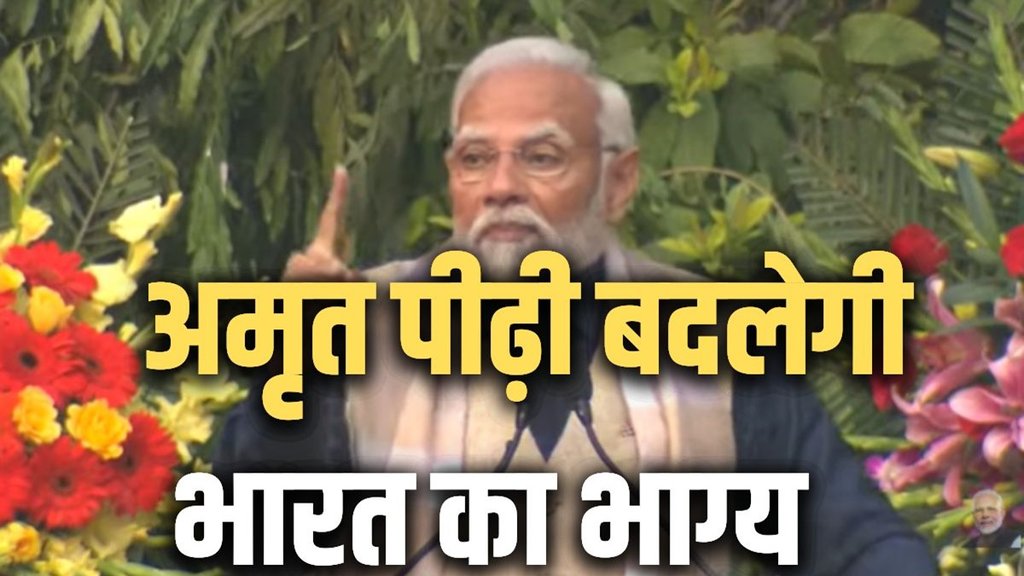भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। स्वाधीनता के अमृत काल में देश के विकास में योगदान देने वाली युवा शक्ति को ‘अमृत पीढ़ी’ का नाम दिया गया है। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से वे सभी भारतीय युवा सम्मिलित हैं जो पैंतीस वर्ष से कम आयु के हैं। इनकी संख्या कुल आबादी की लगभग पैंसठ फीसद है और ये देश के विकास में योगदान दे रहे हैं और भविष्य को आकार दे रहे हैं।
इस समय भारत की युवा आबादी ‘अमृत पीढ़ी’ का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि अमृत पीढ़ी के सभी सपनों को पूरा करना उनके लिए अनगिनत अवसर पैदा करना और उनके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना सरकार का संकल्प है। इस पीढ़ी के लिए सरकार ने अपने बजट और अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। मगर घोषित उद्देश्यों और जमीनी स्तर पर खड़ी चुनौतियों के आईने में ही प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन हो पाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी को प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया।
बजट में शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यावहारिक और उद्योग-उन्मुख बनाने के लिए उसके पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। जिसे ‘अमृत काल’ के रूप में जाना जा रहा है, उसके लिए भारत के दृष्टिकोण में एक मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ के माध्यम से जनभागीदारी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। इस दृष्टिकोण को साकार करने का आर्थिक एजंडा मुख्य रूप से तीन बातों पर केंद्रित है। नागरिकों, विशेषकर युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना।
पिछले एक दशक में देश में विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में प्रगति की है। आइआइटी, आइआइएम और एम्स जैसे संस्थानों में सुधार और विस्तार के साथ सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और भविष्य के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में 13.8 फीसद की वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2014-15 में 51,534 से बढ़ कर मई 2025 तक 70,683 हो गई है। इसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी और अनुसंधान एवं विकास संस्थान शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक, विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 2014-15 में 760 थी, जो बढ़ कर मई 2025 तक 1,334 हो गई। उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए कालेजों की संख्या वर्ष 2014-15 में 38,498 से बढ़ कर मई 2025 तक 51,959 हो गई। वर्ष 2014 में सोलह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान थे। इनकी संख्या मई 2025 तक बढ़ कर तेईस बताई जा रही है।
इसी तरह, वर्ष 2014 में तेरह भारतीय प्रबंधन संस्थान थे, जिनकी संख्या मई 2025 तक बढ़ कर इक्कीस हो गई। वर्ष 2014 तक एम्स की संख्या सात थी जो बढ़ कर अब तेईस हो गई है। सरकार का मानना है कि ये सभी युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने की दृष्टि से अहम कार्य कर रहे हैं। बजट 2023-24 के अंतर्गत अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की गई। नौकरी के लिए प्रशिक्षण, उद्योग की साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के निर्माण पर जोर दिया गया। इस योजना के तहत नए दौर के तमाम कौशल को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।
इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों में से एक है। मगर इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल में प्रशिक्षित किया जाए। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में अब तक 1.63 करोड़ युवाओं को विविध कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया किया जा चुका है। यह कौशल योजना देश के युवाओं को लघु अवधि प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण के माध्यम से कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। वर्ष 2020-21 में 7.37 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
अमृत पीढ़ी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत निरंतर बढ़ने के कारण इस पीढ़ी के सामने आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं। पारंपरिक रोजगार की जगह असुरक्षित और कम पगार वाली नौकरियां बढ़ रही हैं जिससे वित्तीय स्थिरता में कमी आ रही है। ऋण की कम उपलब्धता, स्थिर वेतन की कमी और बेरोजगारी के कारण ऐसे युवाओं को परिवार चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत से युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता।
नतीजतन, उनको कम स्तर की नौकरियों में काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे चिंता, तनाव और अवसाद एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही हैं। इससे उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है। कई युवाओं को भ्रमित करने वाले माहौल का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और इस कारण वे नशाखोरी और अपराध जैसे गलत रास्तों पर चले जाते हैं। इंटरनेट पर कुछ सामग्री भी युवाओं को भटकाव की ओर ले जाती है, जिससे उनके पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ता है और वे अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं।
देश की युवा पीढ़ी के सामने खड़ी इन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। युवाओं के लिए स्थिर और गुणवत्तापूर्ण रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक समृद्ध एवं किफायती बनाने की जरूरत है। इसके लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए, ताकि उद्योग व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप युवा अपने कौशल का विकास कर सकें और आधुनिक अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। युवाओं को अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए सहायता और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
आज की युवा पीढ़ी में नशे की समस्या विकराल हो रही है। इससे करोड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में है। सवाल है कि नशे के फैलते दायरे में उलझ रही अमृत पीढ़ी को उसके हाल पर छोड़ कर उनके सहारे कैसा भविष्य बनाने की उम्मीद की जा रही है। यह जरूरी है कि मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए और नशे के दुष्परिणामों के बारे में युवाओं को जागरूक किया जाए।
इसके अलावा, युवाओं में नैतिक मूल्य भरने के साथ जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना सिखाना चाहिए। इस कार्य में प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों और रोजगार-स्वरोजगार में मार्गदर्शन देने वाले लोगों और संस्थाओं की अहम भूमिका हो सकती है। माता-पिता को अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहिए और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए। युवाओं की समस्याओं को हल करने के लिए व्यापक नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन करना चाहिए।