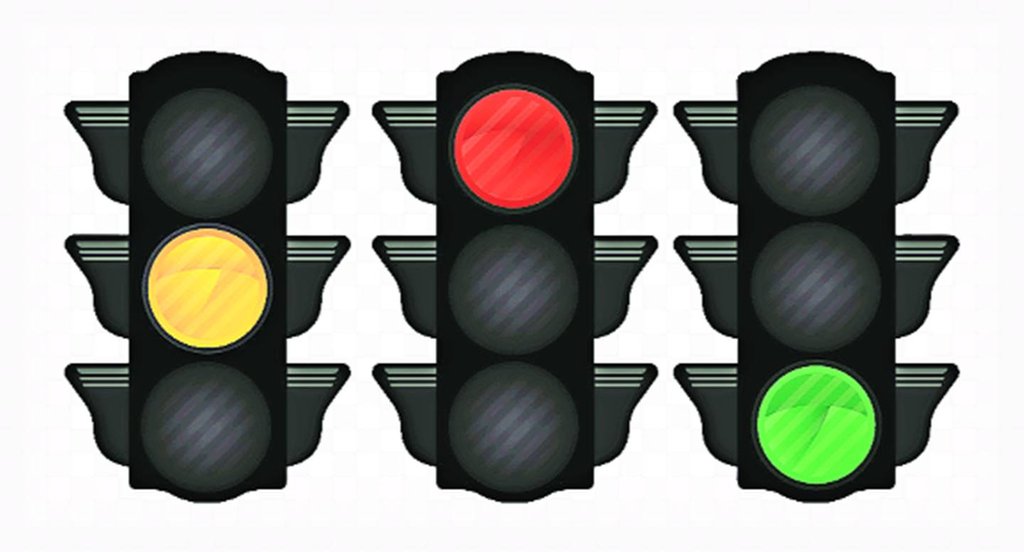इसकी वजह से सैकड़ों सालों से महिलाओं ने इसके खिलाफ बोलने के बजाए इसे अपने अस्तित्व पर बोझ की तरह झेलने का विकल्प चुना। यहां तक कि सबसे प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग से आने वाली महिलाओं के पास भी ऐसा माहौल और भरोसा नहीं था कि वे अपनी देह और दिमाग के दर्द को उघाड़ सकें।
यह सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे वैश्विक संदर्भ में है कि महिलाएं उस मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए खुद से मुठभेड़ करती हैं कि इसमें मेरी क्या गलती थी, ये मेरे साथ क्यों हुआ, दर्द मुझे हुआ तो मेरे लिए कोई दवा क्यों नहीं। खुद को ही दोषी करार दिए जाने के कलंक के भय से वो इसे छिपाए भी रहती थीं। जब महिलाओं ने इस मानसिक पीड़ा से मुक्त होना चाहा तो उन पर पितृसत्ता की मानहानि का हमला शुरू हो गया।
महिलाएं इस फिक्र से आजाद हुईं कि समाज इस सच को सुनने को तैयार है या नहीं। उन्हें लगा कि उन्हें बोले बिना ये सब ऐसे ही चलता जाएगा। मी-टू मुहिम महिलाओं की दैहिक और मानसिक उत्पीड़न से मुक्ति का मार्ग बन कर सामने आई। दुनिया के हर कोने से उठने वाली महिलाओं की आवाज जब सुर से सुर मिलाते हुए इंकलाबी तरन्नुम की शक्ल में गूंजने लगी तो उसे खारिज करना मुश्किल हो गया।
अपने व्यक्तिगत को सामूहिकता की शक्ल देकर महिलाएं आज वैश्विक एकजुटता दिखा रही हैं। प्रिया रमानी के मामले को ही लें तो इसका संदर्भ इकहरा नहीं है। एक महिला अपने अंदर सालों से जिन जटिलताओं को झेल रही थी, यह उससे निकलने का प्रयास है। इसलिए मानहानि मामले में प्रिया को फंसाने की कोशिश जब आखिरकार नाकाम रही तो कि यह उन हजारों महिलाओं के लिए जीत की खुशी बन गई, जो पितृसत्ता के खिलाफ इस दौरान गोलबंद हुई हैं। यह फैसला कई लिहाज से महिला आंदोलन को निर्णायक दिशा देने वाला साबित होगा।