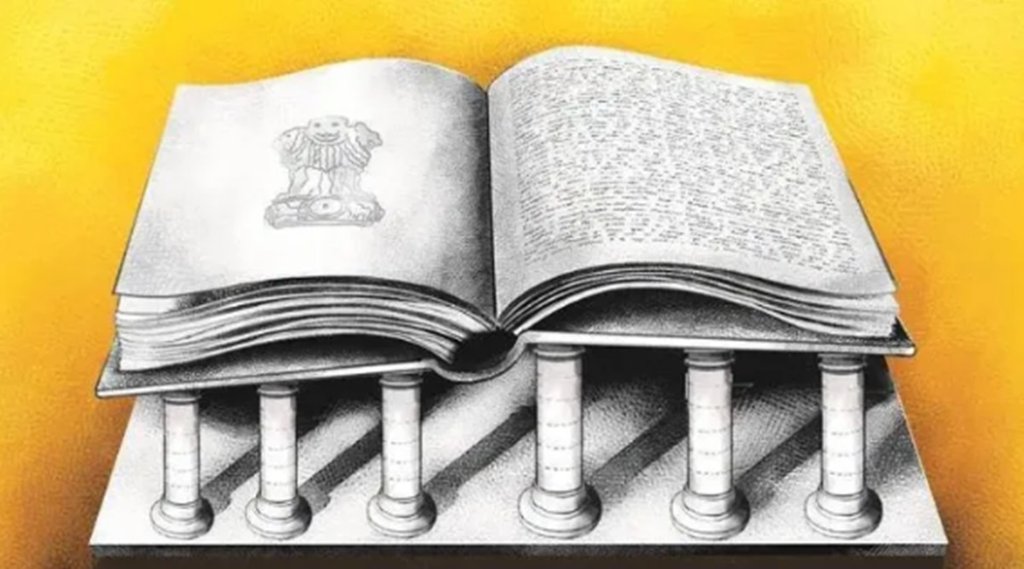अनिमेष झा
भारत का संविधान एक जीवित संविधान है। यह भारत की 135 करोड़ जनता के लिए आस्था, निष्ठा एवं गर्व का केंद्र भी है। हमारे संवैधानिक मूल्य समस्त प्रतिकूलताओं के सामने भी देश को एक सूत्र में पिरोये हुए हैं। भारतीय संविधान देश एवं विदेश के अनेकों विद्वानों के लिए निरंतर जिज्ञासा एवं कौतुहल का विषय बना रहता है। अनेक बुद्धिजीवियों ने समय- समय पर संविधान पर कुछ प्रश्न एवं संदेहों को भी प्रकट किया है। इन प्रश्नों में एक मूल प्रश्न इस आशय का भी है कि क्या भारत का संविधान एक आयातित संविधान है, जिसे अन्य देशों के संविधानों के प्रावधानों को जोड़-तोड़ कर बनाया गया है या ये संविधान अपनी मूल अवधारणा में भारतीय है। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास को समझना पड़ेगा।
स्वतंत्रता के बाद से ही पूरे विश्व ने भारत की संवैधानिक यात्रा को टकटकी लगाकर देखा है। यह आशंका सभी के मन में थी कि क्या भारत एक समावेशी, दूरगामी एवं प्रभावी संविधान का निर्माण कर पाएगा? भारत ने सदियों दासता का दंश झेला, जिसके परिणामस्वरूप शोषण और अन्याय भारतीय जन-मानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए। ऐसे में एक राष्ट्र का आत्मबोध नष्ट हो जाना स्वाभाविक बात थी। इसी आशा के साथ अंग्रेजों ने भी आशंका प्रकट की कि भारत एक समाज के रूप में इतना परिपक्व नहीं है कि अपनी हितचिंता स्वयं कर सके। ब्रिटिश राजनेता चर्चिल ने घोषणा की थी भारतीय नेतृत्व अक्षम लोगों से भरा हुआ है जो संभवतः देश को कुछ वर्षों तक भी नहीं चला पाएंगे।
वर्तमान में एक भारतवंशी को इंग्लैंड का नेतृत्व करता देख निश्चित रूप से चर्चिल की आत्मा अपने दम्भ पर पुनर्विचार कर रही होगी। इस नकारात्मकता के अतिरिक्त एक बड़ी बाधा इसकी भी थी कि भारत एक विषमरूप एवं भिन्नताओं से भरा हुआ राष्ट्र है जिसमें भाषा, मत, संप्रदाय, जाति जैसे जिसे कई विभेद थे। इन भेड़ों की तुलना विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्र से नहीं की जा सकती थी। यूरोप का इतिहास हमारे सामने हैं जहां केवल भाषा के आधार पर न केवल राष्ट्र बंटे बल्कि रक्तपात भी हुआ। ऐसे समय में यह दायित्व हमारे संविधान निर्माताओं के सामने आया कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो भारत की संप्रभुता, आकांक्षा एवं भविष्य की रक्षा कर सके।
भारत के संविधान निर्माताओं ने अथक परिश्रम से 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जो संविधान लिखा उसने विश्व के विशालतम संविधान होने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। संविधान सभा ने लम्बे वाद विवाद के बाद एक ऐसे ग्रन्थ का निर्माण किया जो अपने मूल्यों में दृढ, विचारों में प्रगतिशील एवं क्रियान्वन में लचीला था। संविधान निर्माण के बाद देश विदेश में कई लोगों ने आक्षेप लगाया की संविधान मौलिक नहीं वरन एक नक़ल किया हुआ दस्तावेज है जहाँ अलग-अलग प्रावधान विश्व के विभिन्न संविधान और विधि व्यवस्था से लिए गए हैं। दुर्भाग्य है कि आज भी कई लोग इस दुष्प्रचार को सत्य मानते हैं और ऐसा मानने वालों में कई तथाकथित बुद्धिजीवी भी हैं। इस दुष्प्रचार का खंडन इसलिए भी आवश्यक है कि ऐसी बातें उस निष्ठा एवं समर्पण को प्रभावित करती हैं जो हर भारतीय नागरिक अपने संविधान के प्रति रखता है।
भारत के संविधान का शरीर एवं आत्मा पूर्णरूपेण भारतीय है। भारत की सनातन संस्कृति की झलक भारतीय संविधान के प्रत्येक शब्द में देखी जा सकती है। यह सत्य है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों की प्रेरणा विश्व के अन्य व्यवस्थाओं से ली गई है लेकिन उनका स्वरूप, उनके पीछे का दर्शन, उनके पीछे की चिंता भारतीय जनमानस की ही थी। उदाहरण के रूप में हमने अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा तो ली, लेकिन वहां के घातक अस्त्रों को रखने के प्रावधान को स्थान नहीं दिया। हमने संपत्ति का अधिकार तो बनाया लेकिन उसका स्वरूप स्थाई नहीं बनाया एवं संविधान बनने के कुछ समय बाद यह अधिकार हमने हटा भी दिया।
भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया की तुलना हमारे पौराणिक समुद्र मंथन से भी की जा सकती है जिसमे पूरे समुद्र का मंथन करके अमृत निकाला गया था, उसी प्रकार विश्व के समस्त संविधानों का मंथन करके भारतीय संविधान की रचना की गयी है। इसके अतिरिक्त सभी वाह्य विचारों को अस्वीकार कर देने की पाश्चात्य संकीर्णता भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है।
भारत सदा से इस विचार का पोषक रहा है कि सत्य एक नहीं, वरन अनंत और सापेक्ष है। ‘आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः’ (पूरे विश्व से कल्याणकारी विचार हमें प्राप्त हों) की वैदिक परंपरा के हम एक राष्ट्र के रूप में रक्षक हैं भारतीय संविधान भी इसी सनातन परंपरा को आत्मसात करता है। भारत के संविधान में भारत की कालजई सनातन संस्कृति के अनेक प्रमाण है। संविधान की प्रस्तावना का भ्रातृत्व इसी विचार का द्योतक है कि हम सभी भारतीय अपने समस्त भिन्नताओं के होते हुए भी एक वंश, एक रक्त एवं एक राष्ट्र है।
संविधान में अनेकों ऐसे प्रावधान है जो भारत की प्राचीन संस्कृति को परिलक्षित करते हैं। इसका एक दृष्टान्त संविधान के अनुच्छेद 14 की समानता के अधिकार से समझा जा सकता है। इस अनुच्छेद में वर्णित समानता एक आभासी समनता नहीं है, बल्कि ऐसी समानता है जिसमें एक राष्ट्र के रूप में समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की रक्षा का दायित्व भी शासन पे आता हैं। यह विचार रामराज्य की उस परिकल्पना के निकट है जिसमें राजा तभी सुखी एवं संतुष्ट होता है जब पूरी प्रजा संतुष्ट एवं प्रसन्न रहे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित सभी व्यक्तियों के लिए न्यायालय जाने का अधिकार संभवतः विक्रमादित्य के उस दरबार के सदृश है जिसमे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय न्याय को अधिकारस्वरूप मांग सकता है। संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व तो ऐसे अनेकों प्रावधानों से भरा है जो भारतीयता से ओतप्रोत हैं। गांधी जी के विचारों के अनुरूप सत्ता का विकेन्द्रीकरण (अनुच्छेद 40) भी इसका एक उदाहरण है। ग्रामों को स्वायत्ता देना एक गांधीवादी लक्ष्य है जिसकी जड़ें प्राचीन भारत की महाजनपदीय व्यवस्था में हैं। इसके अतिरिक्त गौ रक्षा (अनुच्छेद 48), मद्य निषेध (अनुच्छेद 47), पर्यावरण की रक्षा एवं प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव (अनुच्छेद 48अ) भारत की सनातन संस्कृति का ही परिचायक है। संविधान में अनेकों प्रावधान लोकहित को समर्पित हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि समष्टि की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग स्वीकार्य है। इस त्याग की भावना का मूल भारतीय सनातन संस्कृति ही है। पाश्चात्य देश जो भोग प्रधान है, उनमें व्यक्तिवाद ही संवैधानिक मूल्य है। इसके विपरीत भारत में राष्ट्रवाद ही मूल संवैधानिक मूल्य है।
संविधान की मूल प्रति में इतिहास एवं पुराणों के चित्र हो या राष्ट्रगान में शंख ध्वनि कर भारत का नेतृत्व करने वाले चिरसारथि की परिकल्पना, भारत के संविधान को भारत की संस्कृति से पृथक करके देखा ही नहीं जा सकता। भारत का संविधान पंथनिरपेक्ष होते हुए भी धर्म सापेक्ष है। हम एक धार्मिक समाज एवं धार्मिक राष्ट्र हैं जो भले ही पूजा पद्धति में निरपेक्ष हों लेकिन सत्य के प्रति सदैव सापेक्ष और प्रतिबद्ध हैं। हमारी नैतिकता हमारे संविधान में रची बसी है, जिसे देखने के लिए केवल एक भारतीय दृष्टि और एक भारतीय ह्रदय आवश्यक है। संविधान की इस 73वीं वर्षगांठ पर हमें अपनी युवा पीढ़ी को अपने संविधान को देखने का सही दृष्टिकोण देना होगा। यही एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में हमारे लिए श्रेयस्कर है।
(अनिमेष झा, जबलपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य हैं)